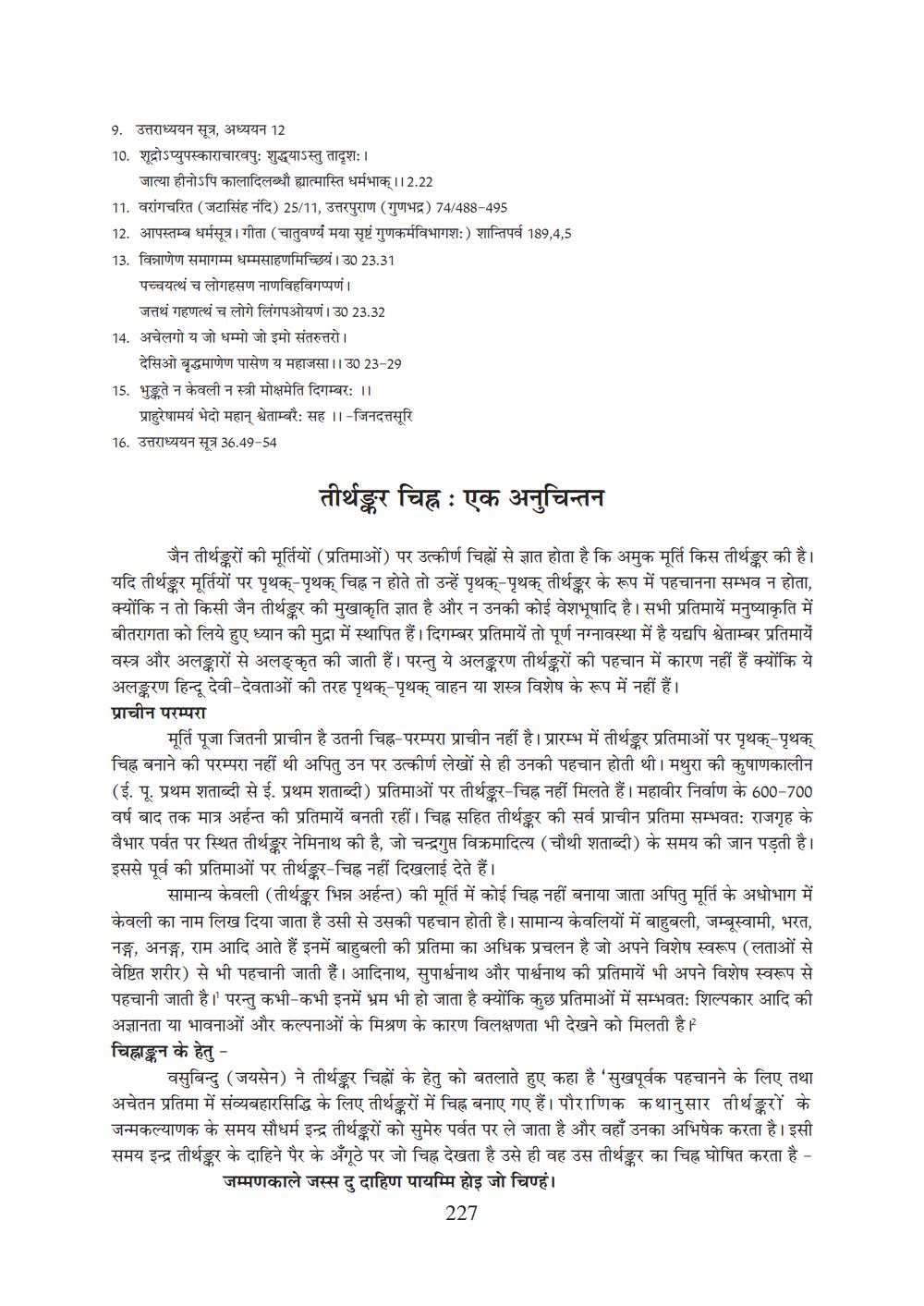________________ 9. उत्तराध्ययन सूत्र, अध्ययन 12 10. शूद्रोऽप्युपस्काराचारवपुः शुद्ध्याऽस्तु तादृशः। जात्या हीनोऽपि कालादिलब्धौ ह्यात्मास्ति धर्मभाक् / / 2.22 11. वरांगचरित (जटासिंह नंदि) 25/11, उत्तरपुराण (गुणभद्र) 74/488-495 12. आपस्तम्ब धर्मसूत्र / गीता (चातुवयं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः) शान्तिपर्व 189,4,5 13. विनाणेण समागम्म धम्मसाहणमिच्छियं / उ0 23.31 पच्चयत्थं च लोगहसण नाणविहविगप्पणं / जत्तथं गहणत्थं च लोगे लिंगपओयणं / 30 23.32 14. अचेलगो य जो धम्मो जो इमो संतरुत्तरो। देसिओ बृद्धमाणेण पासेण य महाजसा।। 30 23-29 15. भुङ्कते न केवली न स्त्री मोक्षमेति दिगम्बरः / / प्राहुरेषामयं भेदो महान् श्वेताम्बरैः सह / / -जिनदत्तसूरि 16. उत्तराध्ययन सूत्र 36.49-54 तीर्थङ्कर चिह्न : एक अनुचिन्तन जैन तीर्थङ्करों की मूर्तियों (प्रतिमाओं) पर उत्कीर्ण चिह्नों से ज्ञात होता है कि अमुक मूर्ति किस तीर्थङ्कर की है। यदि तीर्थङ्कर मूर्तियों पर पृथक्-पृथक् चिह्न न होते तो उन्हें पृथक्-पृथक् तीर्थङ्कर के रूप में पहचानना सम्भव न होता, क्योंकि न तो किसी जैन तीर्थङ्कर की मुखाकृति ज्ञात है और न उनकी कोई वेशभूषादि है। सभी प्रतिमायें मनुष्याकृति में बीतरागता को लिये हुए ध्यान की मुद्रा में स्थापित हैं। दिगम्बर प्रतिमायें तो पूर्ण नग्नावस्था में है यद्यपि श्वेताम्बर प्रतिमायें वस्त्र और अलङ्कारों से अलङ्कृत की जाती हैं। परन्तु ये अलङ्करण तीर्थङ्करों की पहचान में कारण नहीं हैं क्योंकि ये अलङ्करण हिन्दू देवी-देवताओं की तरह पृथक्-पृथक् वाहन या शस्त्र विशेष के रूप में नहीं हैं। प्राचीन परम्परा मूर्ति पूजा जितनी प्राचीन है उतनी चिह्न-परम्परा प्राचीन नहीं है। प्रारम्भ में तीर्थङ्कर प्रतिमाओं पर पृथक्-पृथक् चिह्न बनाने की परम्परा नहीं थी अपितु उन पर उत्कीर्ण लेखों से ही उनकी पहचान होती थी। मथुरा की कुषाणकालीन (ई. पू. प्रथम शताब्दी से ई. प्रथम शताब्दी) प्रतिमाओं पर तीर्थङ्कर-चिह्न नहीं मिलते हैं। महावीर निर्वाण के 600-700 वर्ष बाद तक मात्र अर्हन्त की प्रतिमायें बनती रहीं। चिह्न सहित तीर्थङ्कर की सर्व प्राचीन प्रतिमा सम्भवतः राजगृह के वैभार पर्वत पर स्थित तीर्थङ्कर नेमिनाथ की है, जो चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (चौथी शताब्दी) के समय की जान पड़ती है। इससे पूर्व की प्रतिमाओं पर तीर्थङ्कर-चिह्न नहीं दिखलाई देते हैं। सामान्य केवली (तीर्थङ्कर भिन्न अर्हन्त) की मूर्ति में कोई चिह्न नहीं बनाया जाता अपितु मूर्ति के अधोभाग में केवली का नाम लिख दिया जाता है उसी से उसकी पहचान होती है। सामान्य केवलियों में बाहुबली, जम्बूस्वामी, भरत, नङ्ग, अनङ्ग, राम आदि आते हैं इनमें बाहुबली की प्रतिमा का अधिक प्रचलन है जो अपने विशेष स्वरूप (लताओं से वेष्टित शरीर) से भी पहचानी जाती हैं। आदिनाथ, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ की प्रतिमायें भी अपने विशेष स्वरूप से पहचानी जाती है। परन्तु कभी-कभी इनमें भ्रम भी हो जाता है क्योंकि कुछ प्रतिमाओं में सम्भवतः शिल्पकार आदि की अज्ञानता या भावनाओं और कल्पनाओं के मिश्रण के कारण विलक्षणता भी देखने को मिलती है। चिह्नाङ्कन के हेतु - वसुबिन्दु (जयसेन) ने तीर्थङ्कर चिह्नों के हेतु को बतलाते हुए कहा है 'सुखपूर्वक पहचानने के लिए तथा अचेतन प्रतिमा में संव्यबहारसिद्धि के लिए तीर्थङ्करों में चिह्न बनाए गए हैं। पौराणिक कथानुसार तीर्थङ्करों के जन्मकल्याणक के समय सौधर्म इन्द्र तीर्थङ्करों को सुमेरु पर्वत पर ले जाता है और वहाँ उनका अभिषेक करता है। इसी समय इन्द्र तीर्थङ्कर के दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिह्न देखता है उसे ही वह उस तीर्थङ्कर का चिह्न घोषित करता है - जम्मणकाले जस्स दु दाहिण पायम्मि होइ जो चिण्हं। 227