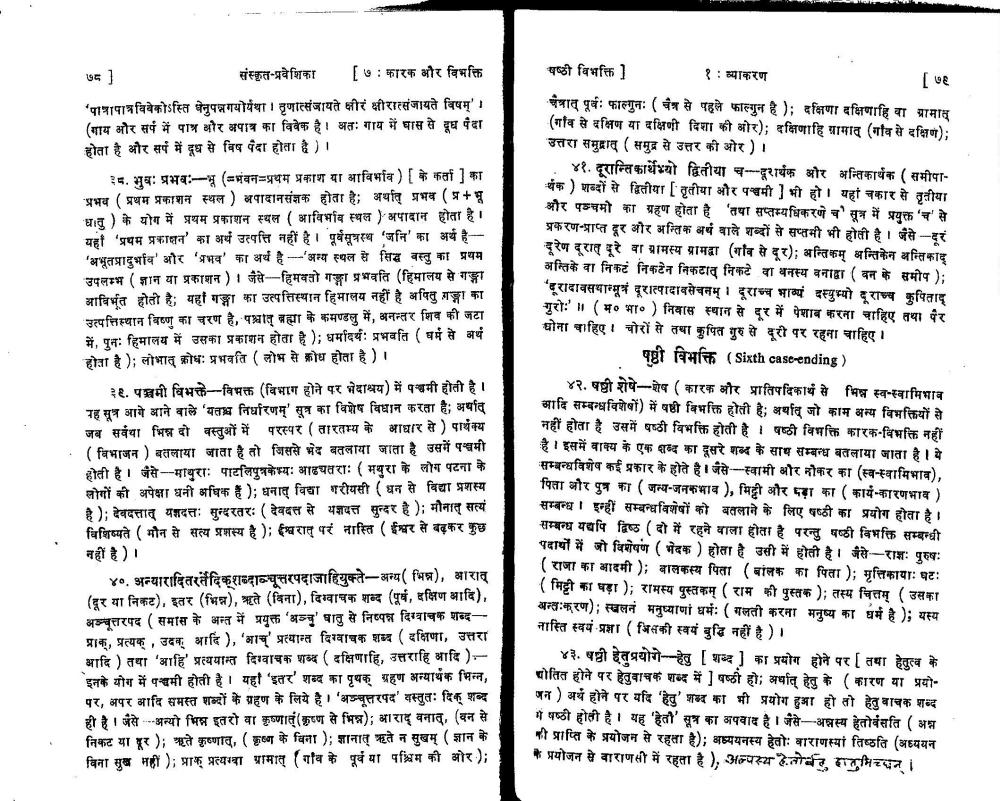________________ 78] संस्कृत-प्रवेशिका [7 : कारक और विभक्ति 'पात्रापात्रविवेकोऽस्ति घेनुपन्न गयोर्यथा / तृणात्संजायते क्षीरं क्षीरात्संजायते विषम्'। (गाय और सर्प में पात्र और अपात्र का विवेक है। अत: गाय में घास से दूध पैदा होता है और सर्प में दूध से विष पैदा होता है)। 15. भुवः प्रभवः-भू (भवन-प्रथम प्रकाश या आविर्भाव) [ के कर्ता ] का प्रभव (प्रथम प्रकाशन स्थल ) अपादानसंज्ञक होता है; अर्थात् प्रभव (प्रभू धातु ) के योग में प्रथम प्रकाशन स्थल ( आविर्भाव स्थल ) अपादान होता है। यहाँ 'प्रथम प्रकाशन' का अर्थ उत्पत्ति नहीं है। पूर्वसूत्रस्थ 'जनि' का अर्थ है'अभूतप्रादुर्भाव' और 'प्रभव' का अर्थ है-'अन्य स्थल से सिद्ध वस्तु का प्रथम उपलम्भ (ज्ञान या प्रकाशन)। जैसे-हिमवतो गङ्गा प्रभवति (हिमालय से गङ्गा आविर्भूत होती है। यहाँ गङ्गा का उत्पत्तिस्थान हिमालय नहीं है अपितु गजा का उत्पत्तिस्थान विष्णु का चरण है, पश्चात् ब्रह्मा के कमण्डलु में, अनन्तर शिव की जटा में, पुनः हिमालय में उसका प्रकाशन होता है); धर्मादर्थः प्रभवति (धर्म से अर्थ होता है); लोभात् क्रोधः प्रभवति ( लोभ से क्रोध होता है)। 36. पन्चमी विभक्ते-विभक्त (विभाग होने पर भेदाश्रय) में पञ्चमी होती है / यह सूत्र आगे आने वाले 'यतश्च निर्धारणम्' सूत्र का विशेष विधान करता है; अर्थात जब सर्वथा भित्र दो वस्तुओं में परस्पर (तारतम्य के आधार से ) पार्थक्य (विभाजन) बतलाया जाता है तो जिससे भेद बतलाया जाता है उसमें पञ्चमी होती है। जैसे-माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढयतराः (मथुरा के लोग पटना के लोगों की अपेक्षा धनी अधिक हैं); धनात् विद्या गरीयसी (धन से विद्या प्रशस्य है); देवदत्तात् यज्ञदत्तः सुन्दरतरः ( देवदत्त से यज्ञदत्त सुन्दर है); मौनात् सत्यं विशिष्यते (मौन से सत्य प्रशस्य है); वरात् परं नास्ति (ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है)। 40. अन्यारादितरतेदिकशब्दाब्यूत्तरपदाजाहियुक्ते-अन्य( भिन्न), भारात् (दूर या निकट), इतर (भिन्न), ऋते (विना), दिग्वापक शब्द (पूर्व, दक्षिण आदि), अचूत्तरपद (समास के अन्त में प्रयुक्त 'अञ्च' पातु से निष्पन्न दिग्याचक शब्दप्राक्, प्रत्यक् , उदक आदि), 'आच्' प्रत्यान्त दिग्वाचक शब्द ( दक्षिणा, उत्तरा आदि) तथा 'आहि' प्रत्ययान्त दिग्वाचक शब्द (दक्षिणाहि, उत्तराहि आदि)इनके योग में पन्चमी होती है। यहाँ 'इतर' शब्द का पृथक् ग्रहण अन्यार्थक भिन्न, पर, अपर आदि समस्त शब्दों के ग्रहण के लिये है। 'अञ्चूतरपद' वस्तुतः दिक् शब्द ही है। जैसे - अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात (कृष्ण से भिन्न); आराद बनात, (वन से निकट या तूर); ऋते कृष्णाव, (कृष्ण के विना); ज्ञानात् ऋते न सुखम् (ज्ञान के / विना सुख मही): प्राक् प्रत्यग्दा प्रामात् (गांव के पूर्व या पश्चिम की ओर); षष्ठी विभक्ति ] 1: व्याकरण [76 त्रात् पूर्वः फाल्गुनः (चैत्र से पहले फाल्गुन है); दक्षिणा दक्षिणाहि वा प्रामा (गाँव से दक्षिण या दक्षिणी दिशा की ओर); दक्षिणाहि ग्रामात् (गांव से दक्षिण); उत्तरा समुद्रात ( समुद्र से उत्तर की ओर)। ... 41. दूरान्ति कार्थेभ्यो द्वितीया च-दूरार्थक और अन्तिकार्षक ( समीपार्थक) शब्दों से द्वितीया [तृतीया और पञ्चमी ] भी हो। यहां चकार से तृतीया और पञ्चमो का ग्रहण होता है तथा सप्तम्यधिकरणे च' सूत्र में प्रयुक्त 'च' से प्रकरण-प्राप्त दूर और अस्तिक अर्थ वाले शब्दों से सप्तमी भी होती है। जैसे-दरं दूरेण दुरात् दूरे वा ग्रामस्य ग्रामद्वा (गाँव से दूर); अन्तिकम् अन्तिकेन अन्तिकाद अन्तिके वा निकटं निकटेन निकटात् निकटे वा वनस्य बनाद्वा ( बन के समीप); 'दूरादावसथान्मूत्र दूरात्पादावसेचनम् / दूराच्च भाव्यं दस्युभ्यो दूराच्च कुपिताद् गुरोः' / (म० भा०) निवास स्थान से दूर में पेशाब करना चाहिए तथा पैर घोना चाहिए। चोरों से तथा कुपित गुरु से दूरी पर रहना चाहिए। षष्ठी विभक्ति (Sixth case-ending) 42. षष्ठी शेषे-शेष ( कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्व-स्वामिभाव आदि सम्बन्धविशेषों) में षष्ठी विभक्ति होती है; अर्थात् जो काम अन्य विभक्तियों से नहीं होता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है / षष्ठी विभक्ति कारक-विभक्ति नहीं है। इसमें वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ सम्बन्ध बतलाया जाता है। ये सम्बन्धविशेष कई प्रकार के होते है / जैसे-स्वामी और नौकर का (स्व-स्वामिभाव), पिता और पुत्र का (जन्य-जनकभाव), मिट्टी और पड़ा का (कार्य-कारणभाव) सम्बन्ध / इन्हीं सम्बन्धविशेषों को बतलाने के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है। सम्बन्ध यद्यपि द्विष्ठ (दो में रहने वाला होता है परन्तु षष्ठी विभक्ति सम्बन्धी पदार्थों में जो विशेषण (भेदक) होता है उसी में होती है। जैसे-राज्ञः पुरुषः ( राजा का आदमी); बालकस्य पिता (बालक का पिता); मृत्तिकायाः घटः (मिट्टी का घड़ा); रामस्य पुस्तकम् ( राम की पुस्तक); तस्य चित्तम् ( उसका अन्तःकरण); स्खलनं मनुष्याणां धर्मः (गलती करना मनुष्य का धर्म है); यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा (जिसकी स्वयं बुद्धि नहीं है)। 43. षष्ठी हेतुप्रयोगे हेतु [शब्द ] का प्रयोग होने पर [ तथा हेतुत्व के चोतित होने पर हेतुवाचक शब्द में ] षष्ठी हो; अर्थात् हेतु के (कारण या प्रयोजन) अर्थ होने पर यदि हेतु' शब्द का भी प्रयोग हा हो तो हेतु वाचक शब्द में षष्ठी होती है। यह 'हेतो' सूत्र का अपवाद है / जैसे--अन्नस्य हेतोर्वसति ( अन्न की प्राप्ति के प्रयोजन से रहता है); अध्ययनस्य हेतोः वाराणस्यां तिष्ठति (अध्ययन के प्रयोजन से वाराणसी में रहता है), अम्पस्य है.तो दातुमिच्चन /