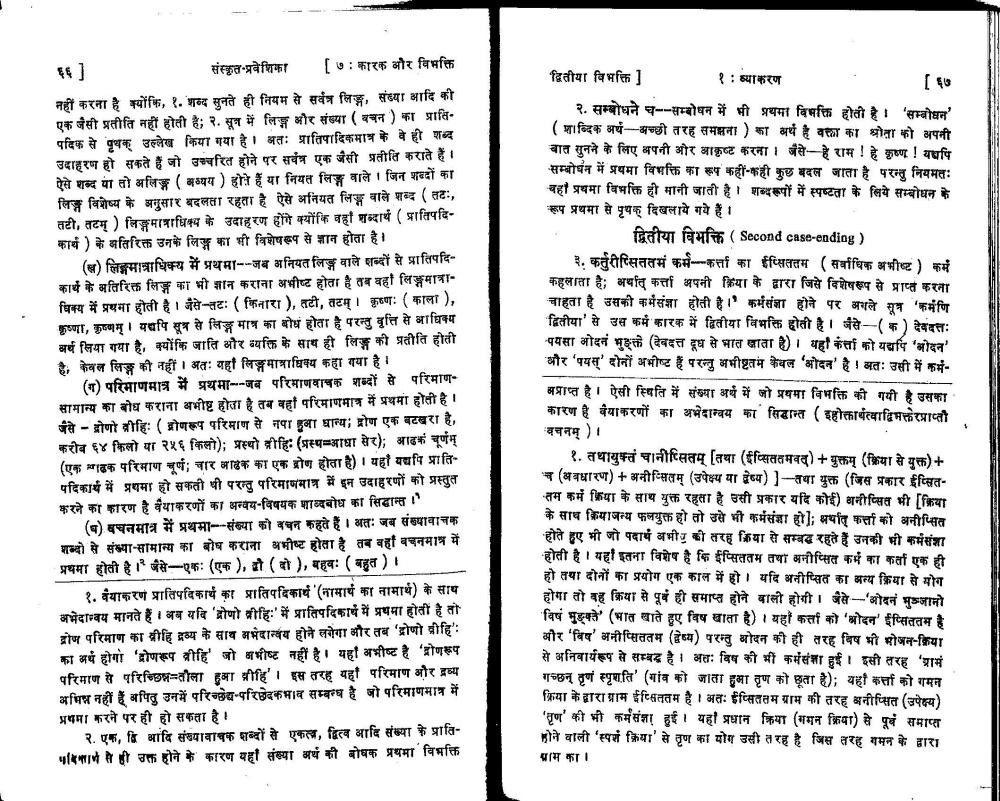________________ संस्कृत प्रवेशिका [७:कारक और विभक्ति नहीं करना है क्योंकि, 1. शब्द सुनते ही नियम से सर्वत्र लिङ्ग, संख्या आदि की एक जैसी प्रतीति नहीं होती है; 2. सूत्र में लिङ्ग और संख्या ( वचन ) का प्रातिपदिक से पृथक् उल्लेख किया गया है। अतः प्रातिपादिकमात्र के वे ही शब्द उदाहरण हो सकते हैं जो उच्चरित होने पर सर्वत्र एक जैसी प्रतीति कराते हैं। ऐसे शब्द या तो अलिङ्ग (अव्यय) होते हैं या नियत लिङ्ग वाले / जिन शब्दों का लिङ्ग विशेष्य के अनुसार बदलता रहता है ऐसे अनियत लिङ्ग वाले शब्द (तटः, तटी, तटम् ) लिङ्गमात्राधिक्य के उदाहरण होंगे क्योंकि वहाँ शब्दार्थ (प्रातिपदिकार्य) के अतिरिक्त उनके लिङ्ग का भी विशेषरूप से ज्ञान होता है। (ख) लिङ्गमात्राधिक्य में प्रथमा--जब अनियत लिङ्ग वाले शब्दों से प्रातिपदिकार्य के अतिरिक्त लिङ्ग का भी ज्ञान कराना अभीष्ट होता है तब वहाँ लिङ्गमात्राधिक्य में प्रथमा होती है। जैसे-तटः (किनारा), तटी, तटम् / कृष्णः (काला), कृष्णा, कृष्णम् / यद्यपि सूत्र से लिङ्ग मात्र का बोध होता है परन्तु वृत्ति से आधिक्य अर्थ लिया गया है, क्योंकि जाति और व्यक्ति के साथ ही लिङ्ग की प्रतीति होती है, केवल लिङ्ग की नहीं / अतः यहाँ लिङ्गमात्राधिक्य कहा गया है। (ग) परिमाणमात्र में प्रथमा--जब परिमाणवाचक शब्दों से परिमाणसामान्य का बोध कराना अभीष्ट होता है तब वहाँ परिमाणमात्र में प्रथमा होती है। जैसे-द्रोणो व्रीहिः (द्रोणरूप परिमाण से नपा हुआ धान्य द्रोण एक बटखरा है, करीब 64 किलो या 256 किलो); प्रस्थो व्रीहिः (प्रस्प आधा सेर); आढर्क चूर्णम् (एक ढक परिमाण चूर्ण; चार आठक का एक द्रोण होता है। यहाँ यद्यपि प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो सकती थी परन्तु परिमाणमात्र में इन उदाहरणों को प्रस्तुत करने का कारण है वैयाकरणों का अन्वय-विषयक शाध्यबोध का सिद्धान्त / ' (प) बचनमात्र में प्रथमा--संख्या को वचन कहते हैं / अतः जब संख्यावाचक शब्दों से संख्या सामान्य का बोध कराना अभीष्ट होता है तब वहाँ बचनमात्र में प्रथमा होती है। जैसे-एक: (एक),दो (दो), बहवः (बहुत)। 1. वैयाकरण प्रातिपदिकार्थ का प्रातिपदिकार्थ (नामार्थ का नामार्थ) के साथ अभेदान्वय मानते हैं / अब यदि 'द्रोणो व्रीहिः' में प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है तो द्रोण परिमाण का व्रीहि द्रव्य के साथ अभेदान्वय होने लगेगा और तब 'द्रोणो व्रीहि': का अर्थ होगा 'द्रोणरूप बीहि' जो अभीष्ट नहीं है। यहाँ अभीष्ट है 'द्रोणरूप परिमाण से परिच्छिन्नतीला हुआ बीहि'। इस तरह यहाँ परिमाण और द्रव्य अमित नहीं हैं अपितु उनमें परिच्छेद्य-परिछेदकभाव सम्बन्ध है जो परिमाणमात्र में प्रथमा करने पर ही हो सकता है। 2. एक, हि आदि संख्यावाचक शब्दों से एकल, द्वित्व आदि संख्या के प्रातिपरिमाणे से ही उक्त होने के कारण यहाँ संख्या अर्थ की बोधक प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति] 1 : व्याकरण [67 2. सम्बोधने च--सम्बोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। 'सम्बोधन' (शाब्दिक अर्थ-अच्छी तरह समझना) का अर्थ है वक्ता का श्रोता को अपनी बात सुनने के लिए अपनी ओर आकृष्ट करना / जैसे-हे राम! हे कृष्ण ! यद्यपि सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का रूप कहीं-कही कुछ बदल जाता है परन्तु नियमतः वही प्रथमा विभक्ति ही मानी जाती है। शब्दरूपों में स्पष्टता के लिये सम्बोधन के रूप प्रथमा से पृथक् दिखलाये गये हैं। factor fauft (Second case-ending ) 3. कर्तुरीप्सिततमं कर्म-कर्ता का ईप्सिततम (सर्वाधिक अभीष्ट ) कर्म कहलाता है। अर्थात् कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेषरूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्मसंज्ञा होती है।' कर्मसंज्ञा होने पर अगले सत्र 'कर्मणि द्वितीया' से उस कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे—(क) देवदत्तः पयसा मोदनं भुक्त (देवदत्त दूध से भात खाता है)। यहाँ के को यद्यपि 'मोदन' और 'पयस्' दोनों अभीष्ट हैं परन्तु अभीष्टतम केवल 'मोदन' है। अतः उसी में कर्मअप्राप्त है। ऐसी स्थिति में संख्या अर्थ में जो प्रथमा विभक्ति की गयी है उसका कारण है वैयाकरणों का अभेदान्वय का सिद्धान्त ( इहोक्तार्थत्वाद्विभक्तरप्राप्ती . वचनम् ) / 1. तथायुक्तं चानीप्सितम् [तथा (इप्सिततमव) + युक्तम् (क्रिया से युक्त)+ च (अवधारण)+ अनीसितम् (उपेक्ष्य या द्वेष्य)]-तथा युक्त (जिस प्रकार ईप्सित-तम कर्म क्रिया के साथ युक्त रहता है उसी प्रकार यदि कोई) भनीप्सित भी [क्रिया के साथ क्रियाजन्य फलयुक्त हो तो उसे भी कर्मसंज्ञा हो] अर्थात् कर्ता को अनीप्सित होते हुए भी जो पदार्थ अभी की तरह क्रिया से सम्बद्ध रहते हैं उनकी भी कर्मसंज्ञा होती है। यहाँ इतना विशेष है कि ईप्सिततम तथा अनीप्सित कर्म का कर्ता एक ही हो तथा दोनों का प्रयोग एक काल में हो। यदि अनीप्सित का अन्य क्रिया से योग होगा तो वह क्रिया से पूर्व ही समाप्त होने वाली होगी। जैसे-'ओदनं भुजानो विषं मुड्कते' (भात खाते हुए विष खाता है) / यहाँ कर्ता को 'रोदन' ईप्सिततम है और 'विष' अनीप्सिततम (द्वेष्य) परन्तु मोदन की ही तरह विष भी भोजन-क्रिया से अनिवार्यरूप से सम्बद्ध है। अतः विष की भी कर्मसंज्ञा हुई। इसी तरह 'ग्राम गच्छन् तृणं स्पृशति' (गांव को जाता हुमा तृण को छूता है); यहाँ कर्ता को गमन क्रिया के द्वारा ग्राम ईप्सिततम है / अतः ईप्सिततम ग्राम की तरह अनीप्सित (उपेक्ष्य) 'तृण' की भी कर्मसंज्ञा हुई। यहाँ प्रधान क्रिया (गमन क्रिया) से पूर्व समाप्त होने वाली 'स्पर्श क्रिया' से तृण का योग उसी तरह है जिस तरह गमन के द्वारा