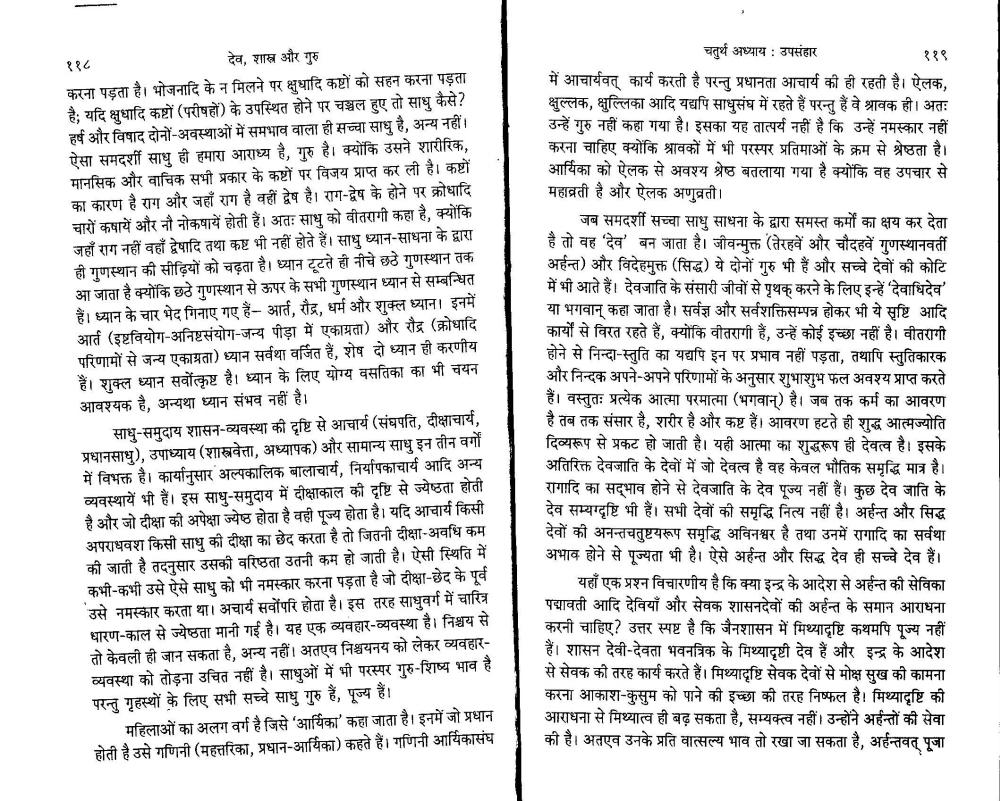________________ 118 देव, शास्त्र और गुरु करना पड़ता है। भोजनादि के न मिलने पर क्षुधादि कष्टों को सहन करना पड़ता है; यदि क्षुधादि कष्टों (परीषहों) के उपस्थित होने पर चञ्चल हुए तो साधु कैसे? हर्ष और विषाद दोनों-अवस्थाओं में समभाव वाला ही सच्चा साधु है, अन्य नहीं। ऐसा समदर्शी साधु ही हमारा आराध्य है, गुरु है। क्योंकि उसने शारीरिक, मानसिक और वाचिक सभी प्रकार के कष्टों पर विजय प्राप्त कर ली है। कष्टों का कारण है राग और जहाँ राग है वहीं द्वेष है। राग-द्वेष के होने पर क्रोधादि चारों कषायें और नौ नोकषायें होती हैं। अतः साधु को वीतरागी कहा है, क्योंकि जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेषादि तथा कष्ट भी नहीं होते हैं। साधु ध्यान-साधना के द्वारा ही गुणस्थान की सीढ़ियों को चढ़ता है। ध्यान टूटते ही नीचे छठे गुणस्थान तक आ जाता है क्योंकि छठे गुणस्थान से ऊपर के सभी गुणस्थान ध्यान से सम्बन्धित हैं। ध्यान के चार भेद गिनाए गए हैं- आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। इनमें आर्त (इष्टवियोग-अनिष्टसंयोग-जन्य पीड़ा में एकाग्रता) और रौद्र (क्रोधादि परिणामों से जन्य एकाग्रता) ध्यान सर्वथा वर्जित हैं, शेष दो ध्यान ही करणीय हैं। शुक्ल ध्यान सर्वोत्कृष्ट है। ध्यान के लिए योग्य वसतिका का भी चयन आवश्यक है, अन्यथा ध्यान संभव नहीं है। साधु-समुदाय शासन-व्यवस्था की दृष्टि से आचार्य (संघपति, दीक्षाचार्य, प्रधानसाधु), उपाध्याय (शास्त्रवेत्ता, अध्यापक) और सामान्य साधु इन तीन वर्गों में विभक्त है। कार्यानुसार अल्पकालिक बालाचार्य, निर्यापकाचार्य आदि अन्य व्यवस्थायें भी हैं। इस साधु-समुदाय में दीक्षाकाल की दृष्टि से ज्येष्ठता होती है और जो दीक्षा की अपेक्षा ज्येष्ठ होता है वही पूज्य होता है। यदि आचार्य किसी अपराधवश किसी साधु की दीक्षा का छेद करता है तो जितनी दीक्षा अवधि कम की जाती है तदनुसार उसकी वरिष्ठता उतनी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में कभी-कभी उसे ऐसे साधु को भी नमस्कार करना पड़ता है जो दीक्षा-छेद के पूर्व 'उसे नमस्कार करता था। अचार्य सवोपरि होता है। इस तरह साधुवर्ग में चारित्र धारण-काल से ज्येष्ठता मानी गई है। यह एक व्यवहार-व्यवस्था है। निश्चय से तो केवली ही जान सकता है, अन्य नहीं। अतएव निश्चयनय को लेकर व्यवहारव्यवस्था को तोड़ना उचित नहीं है। साधुओं में भी परस्पर गुरु-शिष्य भाव है परन्तु गृहस्थों के लिए सभी सच्चे साधु गुरु हैं, पूज्य हैं। महिलाओं का अलग वर्ग है जिसे 'आर्यिका' कहा जाता है। इनमें जो प्रधान होती है उसे गणिनी (महत्तरिका, प्रधान-आर्यिका) कहते हैं। गणिनी आर्यिकासंघ चतुर्थ अध्याय : उपसंहार में आचार्यवत् कार्य करती है परन्तु प्रधानता आचार्य की ही रहती है। ऐलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि यद्यपि साधुसंघ में रहते हैं परन्तु हैं वे श्रावक ही। अतः उन्हें गुरु नहीं कहा गया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उन्हें नमस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि श्रावकों में भी परस्पर प्रतिमाओं के क्रम से श्रेष्ठता है। आर्यिका को ऐलक से अवश्य श्रेष्ठ बतलाया गया है क्योंकि वह उपचार से महाव्रती है और ऐलक अणुव्रती। ___ जब समदर्शी सच्चा साधु साधना के द्वारा समस्त कर्मों का क्षय कर देता है तो वह 'देव' बन जाता है। जीवन्मुक्त (तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती अर्हन्त) और विदेहमुक्त (सिद्ध) ये दोनों गुरु भी हैं और सच्चे देवों की कोटि में भी आते हैं। देवजाति के संसारी जीवों से पृथक् करने के लिए इन्हें 'देवाधिदेव' या भगवान् कहा जाता है। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिसम्पन्न होकर भी ये सृष्टि आदि कार्यों से विरत रहते हैं, क्योंकि वीतरागी हैं, उन्हें कोई इच्छा नहीं है। वीतरागी होने से निन्दा-स्तुति का यद्यपि इन पर प्रभाव नहीं पड़ता, तथापि स्तुतिकारक और निन्दक अपने-अपने परिणामों के अनुसार शुभाशुभ फल अवश्य प्राप्त करते हैं। वस्तुतः प्रत्येक आत्मा परमात्मा (भगवान्) है। जब तक कर्म का आवरण है तब तक संसार है, शरीर है और कष्ट हैं। आवरण हटते ही शुद्ध आत्मज्योति दिव्यरूप से प्रकट हो जाती है। यही आत्मा का शुद्धरूप ही देवत्व है। इसके अतिरिक्त देवजाति के देवों में जो देवत्व है वह केवल भौतिक समृद्धि मात्र है। रागादि का सद्भाव होने से देवजाति के देव पूज्य नहीं हैं। कुछ देव जाति के देव सम्यग्दृष्टि भी हैं। सभी देवों की समृद्धि नित्य नहीं है। अर्हन्त और सिद्ध देवों की अनन्तचतुष्टयरूप समृद्धि अविनश्वर है तथा उनमें रागादि का सर्वथा अभाव होने से पूज्यता भी है। ऐसे अर्हन्त और सिद्ध देव ही सच्चे देव हैं। यहाँ एक प्रश्न विचारणीय है कि क्या इन्द्र के आदेश से अर्हन्त की सेविका पद्मावती आदि देवियाँ और सेवक शासनदेवों की अर्हन्त के समान आराधना करनी चाहिए? उत्तर स्पष्ट है कि जैनशासन में मिथ्यादृष्टि कथमपि पूज्य नहीं हैं। शासन देवी-देवता भवनत्रिक के मिथ्यादृष्टी देव हैं और इन्द्र के आदेश से सेवक की तरह कार्य करते हैं। मिथ्यादृष्टि सेवक देवों से मोक्ष सुख की कामना करना आकाश-कुसुम को पाने की इच्छा की तरह निष्फल है। मिथ्यादृष्टि की आराधना से मिथ्यात्व ही बढ़ सकता है, सम्यक्त्व नहीं। उन्होंने अर्हन्तों की सेवा की है। अतएव उनके प्रति वात्सल्य भाव तो रखा जा सकता है, अर्हन्तवत् पूजा