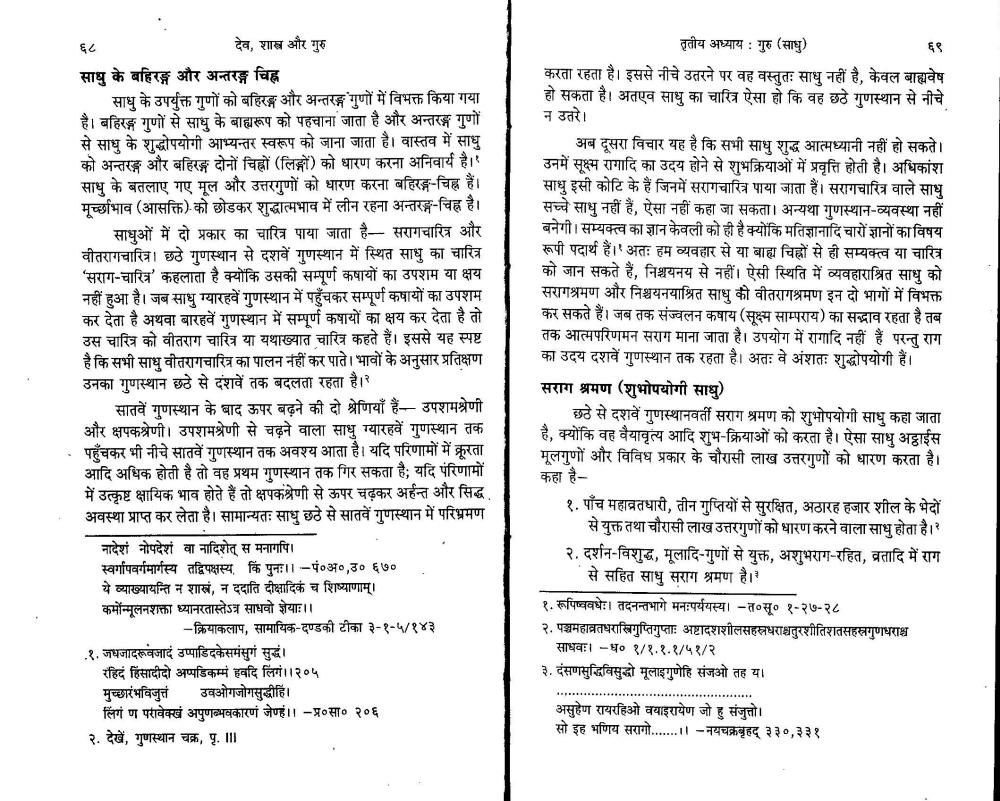________________ 68 देव, शास्त्र और गुरु साधु के बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग चिह्न साधु के उपर्युक्त गुणों को बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग गुणों में विभक्त किया गया है। बहिरङ्ग गुणों से साधु के बाह्यरूप को पहचाना जाता है और अन्तरङ्ग गुणों से साधु के शुद्धोपयोगी आभ्यन्तर स्वरूप को जाना जाता है। वास्तव में साधु को अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों चिह्नों (लिङ्गों) को धारण करना अनिवार्य है। साधु के बतलाए गए मूल और उत्तरगुणों को धारण करना बहिरङ्ग-चिह्न हैं। मूभिाव (आसक्ति) को छोडकर शुद्धात्मभाव में लीन रहना अन्तरङ्ग-चिह्न है। ___ साधुओं में दो प्रकार का चारित्र पाया जाता है- सरागचारित्र और वीतरागचारित्र। छठे गुणस्थान से दशवें गुणस्थान में स्थित साधु का चारित्र 'सराग-चारित्र' कहलाता है क्योंकि उसकी सम्पूर्ण कषायों का उपशम या क्षय नहीं हुआ है। जब साधु ग्यारहवें गुणस्थान में पहुँचकर सम्पूर्ण कषायों का उपशम कर देता है अथवा बारहवें गुणस्थान में सम्पर्ण कषायों का क्षय कर देता है तो उस चारित्र को वीतराग चारित्र या यथाख्यात चारित्र कहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि सभी साधु वीतरागचारित्र का पालन नहीं कर पाते। भावों के अनुसार प्रतिक्षण उनका गुणस्थान छठे से दंशवें तक बदलता रहता है। ___सातवें गुणस्थान के बाद ऊपर बढ़ने की दो श्रेणियाँ हैं- उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी। उपशमश्रेणी से चढ़ने वाला साधु ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुँचकर भी नीचे सातवें गुणस्थान तक अवश्य आता है। यदि परिणामों में क्रूरता आदि अधिक होती है तो वह प्रथम गुणस्थान तक गिर सकता है; यदि परिणामों में उत्कृष्ट क्षायिक भाव होते हैं तो क्षपकश्रेणी से ऊपर चढ़कर अर्हन्त और सिद्ध, अवस्था प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः साधु छठे से सातवें गुणस्थान में परिभ्रमण नादेशं नोपदेशं वा नादिशेत् स मनागपि। स्वर्गापवर्गमार्गस्य तद्विपक्षस्य, किं पुनः।। -पं०अ०,उ० 670 . ये व्याख्यायन्ति न शास्त्रं, न ददाति दीक्षादिकं च शिष्याणाम्। कमोन्मूलनशक्ता ध्यानरतास्तेऽत्र साधवो शेयाः।। -क्रियाकलाप, सामायिक-दण्डकी टीका 3-1-5/143 .1. जधजादरूवजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं सुद्धं। रहिदं हिंसादीदो अप्पडिकम्म हवदि लिंग।।२०५ मुच्छारंभविजुत्तं उवओगजोगसुद्धीहिं। लिंग ण परावेक्खं अपुणब्भवकारणं जेण्हं।। -प्र०सा० 206 2. देखें, गुणस्थान चक्र, पृ. III तृतीय अध्याय : गुरु (साधु) करता रहता है। इससे नीचे उतरने पर वह वस्तुतः साधु नहीं है, केवल बाह्यवेष हो सकता है। अतएव साधु का चारित्र ऐसा हो कि वह छठे गुणस्थान से नीचे न उतरे। अब दूसरा विचार यह है कि सभी साधु शुद्ध आत्मध्यानी नहीं हो सकते। उनमें सूक्ष्म रागादि का उदय होने से शुभक्रियाओं में प्रवृत्ति होती है। अधिकांश साधु इसी कोटि के हैं जिनमें सरागचारित्र पाया जाता है। सरागचारित्र वाले साधु सच्चे साधु नहीं हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अन्यथा गुणस्थान-व्यवस्था नहीं बनेगी। सम्यक्त्व का ज्ञान केवली को ही है क्योंकि मतिज्ञानादि चारों ज्ञानों का विषय रूपी पदार्थ हैं। अतः हम व्यवहार से या बाह्य चिह्नों से ही सम्यक्त्व या चारित्र को जान सकते हैं, निश्शयनय से नहीं। ऐसी स्थिति में व्यवहाराश्रित साधु को सरागश्रमण और निश्चयनयाश्रित साधु को वीतरागश्रमण इन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जब तक संज्वलन कषाय (सक्ष्म साम्पराय) का सद्भाव रहता है तब तक आत्मपरिणमन सराग माना जाता है। उपयोग में रागादि नहीं हैं परन्तु राग का उदय दशवें गुणस्थान तक रहता है। अतः वे अंशतः शुद्धोपयोगी हैं। सराग श्रमण (शुभोपयोगी साधु) छठे से दशवें गुणस्थानवर्ती सराग श्रमण को शुभोपयोगी साधु कहा जाता है, क्योंकि वह वैयावृत्य आदि शुभ-क्रियाओं को करता है। ऐसा साधु अट्ठाईस मूलगुणों और विविध प्रकार के चौरासी लाख उत्तरगुणों को धारण करता है। कहा है१. पाँच महाव्रतधारी, तीन गुप्तियों से सुरक्षित, अठारह हजार शील के भेदों से युक्त तथा चौरासी लाख उत्तरगुणों को धारण करने वाला साधु होता है। 2. दर्शन-विशुद्ध, मूलादि-गुणों से युक्त, अशुभराग-रहित, व्रतादि में राग से सहित साधु सराग श्रमण है। 1. रूपिष्ववधेः। तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य। -त०सू०१-२७-२८ 2. पञ्चमहावतधरास्त्रिगुप्तिगुप्ताः अष्टादशशीलसहस्रधराश्चतुरशीतिशतसहस्रगुणधराच साधवः। -ध० 1/1.1.1/51/2 3. दंसणसुद्धिविसुद्धो मूलाइगुणेहि संजओ तह य। असुहेण रायरहिओ वयाइरायेण जो हु संजुत्तो। सो इह भणिय सरागो.......।। - नयचक्रबृहद् 330,331