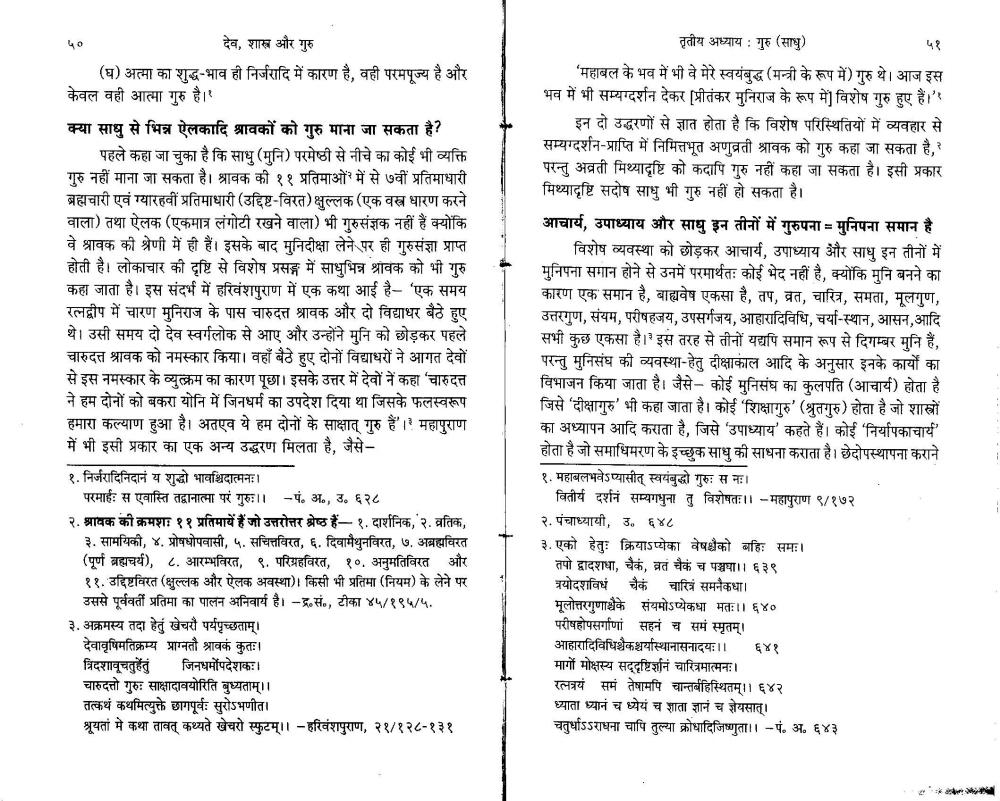________________ देव, शास्त्र और गुरु (घ) अत्मा का शुद्ध-भाव ही निर्जरादि में कारण है, वही परमपूज्य है और केवल वही आत्मा गुरु है। क्या साधु से भिन्न ऐलकादि श्रावकों को गुरु माना जा सकता है? पहले कहा जा चुका है कि साधु (मुनि) परमेष्ठी से नीचे का कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं माना जा सकता है। श्रावक की 11 प्रतिमाओं में से ७वीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी एवं ग्यारहवीं प्रतिमाधारी (उद्दिष्ट-विरत) क्षुल्लक (एक वस्त्र धारण करने वाला) तथा ऐलक (एकमात्र लंगोटी रखने वाला) भी गुरुसंज्ञक नहीं हैं क्योंकि वे श्रावक की श्रेणी में ही हैं। इसके बाद मुनिदीक्षा लेने पर ही गुरुसंज्ञा प्राप्त होती है। लोकाचार की दृष्टि से विशेष प्रसङ्ग में साधुभिन्न श्रावक को भी गुरु कहा जाता है। इस संदर्भ में हरिवंशपुराण में एक कथा आई है- 'एक समय रत्नद्वीप में चारण मुनिराज के पास चारुदत्त श्रावक और दो विद्याधर बैठे हुए थे। उसी समय दो देव स्वर्गलोक से आए और उन्होंने मुनि को छोड़कर पहले चारुदत्त श्रावक को नमस्कार किया। वहाँ बैठे हुए दोनों विद्याधरों ने आगत देवों से इस नमस्कार के व्युत्क्रम का कारण पूछा। इसके उत्तर में देवों ने कहा 'चारुदत्त ने हम दोनों को बकरा योनि में जिनधर्म का उपदेश दिया था जिसके फलस्वरूप हमारा कल्याण हुआ है। अतएव ये हम दोनों के साक्षात् गुरु हैं। महापुराण में भी इसी प्रकार का एक अन्य उद्धरण मिलता है, जैसे१. निर्जरादिनिदानं य शुद्धो भावश्चिदात्मनः। परमाहः स एवास्ति तद्वानात्मा परं गुरुः।। -पं. अ., उ.६२८ 2. श्रावक की क्रमशा 11 प्रतिमायें हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं- 1. दार्शनिक, 2. व्रतिक, 3. सामयिकी, 4. प्रोषधोपवासी, 5. सचित्तविरत, 6. दिवामैथुनविरत, 7. अब्रह्मविरत (पूर्ण ब्रह्मचर्य), 8. आरम्भविरत, 9. परिग्रहविरत, 10. अनुमतिविरत और 11. उद्दिष्टविरत (क्षुल्लक और ऐलक अवस्था)। किसी भी प्रतिमा (नियम) के लेने पर उससे पूर्ववर्ती प्रतिमा का पालन अनिवार्य है। -द्र.सं., टीका 45/195/5. 3. अक्रमस्य तदा हेतुं खेचरौ पर्यपृच्छताम्। देवावृषिमतिक्रम्य प्राग्नतौ श्रावकं कुतः। त्रिदशावूचतुहेतुं जिनधर्मोपदेशकः। चारुदत्तो गुरुः साक्षादावयोरिति बुध्यताम्।। तत्कथं कथमित्युक्ते छागपूर्वः सुरोऽभणीत। श्रूयतां मे कथा तावत् कथ्यते खेचरो स्फुटम्।। - हरिवंशपुराण, 21/128-131 तृतीय अध्याय : गुरु (साधु) 'महाबल के भव में भी वे मेरे स्वयंबुद्ध (मन्त्री के रूप में) गुरु थे। आज इस भव में भी सम्यग्दर्शन देकर [प्रीतंकर मुनिराज के रूप में विशेष गुरु हुए हैं।'' इन दो उद्धरणों से ज्ञात होता है कि विशेष परिस्थितियों में व्यवहार से सम्यग्दर्शन-प्राप्ति में निमित्तभूत अणुव्रती श्रावक को गुरु कहा जा सकता है, परन्तु अवती मिथ्यादृष्टि को कदापि गुरु नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि सदोष साधु भी गुरु नहीं हो सकता है। आचार्य, उपाध्याय और साधु इन तीनों में गुरुपना = मुनिपना समान है विशेष व्यवस्था को छोड़कर आचार्य, उपाध्याय और साधु इन तीनों में मुनिपना समान होने से उनमें परमार्थतः कोई भेद नहीं है, क्योंकि मुनि बनने का कारण एक समान है, बाह्यवेष एकसा है, तप, व्रत, चारित्र, समता, मूलगुण, उत्तरगुण, संयम, परीषहजय, उपसर्गजय, आहारादिविधि, चर्या-स्थान, आसन,आदि सभी कुछ एकसा है। इस तरह से तीनों यद्यपि समान रूप से दिगम्बर मुनि हैं, परन्तु मुनिसंघ की व्यवस्था-हेतु दीक्षाकाल आदि के अनुसार इनके कार्यों का विभाजन किया जाता है। जैसे- कोई मुनिसंघ का कुलपति (आचार्य) होता है जिसे 'दीक्षागुरु' भी कहा जाता है। कोई 'शिक्षागुरु' (श्रुतगुरु) होता है जो शास्त्रों का अध्यापन आदि कराता है, जिसे 'उपाध्याय' कहते हैं। कोई 'निर्यापकाचार्य' होता है जो समाधिमरण के इच्छुक साधु की साधना कराता है। छेदोपस्थापना कराने 1. महाबलभवेऽप्यासीत् स्वयंबुद्धो गुरुः स नः। वितीर्य दर्शनं सम्यगधुना तु विशेषतः।। -महापुराण 9/172 2. पंचाध्यायी, उ. 648 3. एको हेतुः क्रियाऽप्येका वेषश्चैको बहिः समः। तपो द्वादशधा, चैकं, व्रत चैकं च पशघा।। 639 त्रयोदशविधं चैकं चारित्रं समनैकधा। मूलोत्तरगुणाश्चैके संयमोऽप्येकधा मतः।। 640 परीषहोपसर्गाणां सहनं च समं स्मृतम्। आहारादिविधिश्चैकश्चर्यास्थानासनादयः।। 641 मागों मोक्षस्य सदृष्टिनिं चारित्रमात्मनः। रत्नत्रयं समं तेषामपि चान्तर्बहिस्थितम्।। 642 ध्याता ध्यानं च ध्येयं च ज्ञाता ज्ञानं च ज्ञेयसात्। चतुर्धाऽऽराधना चापि तुल्या क्रोधादिजिष्णुता।। -पं. अ. 643