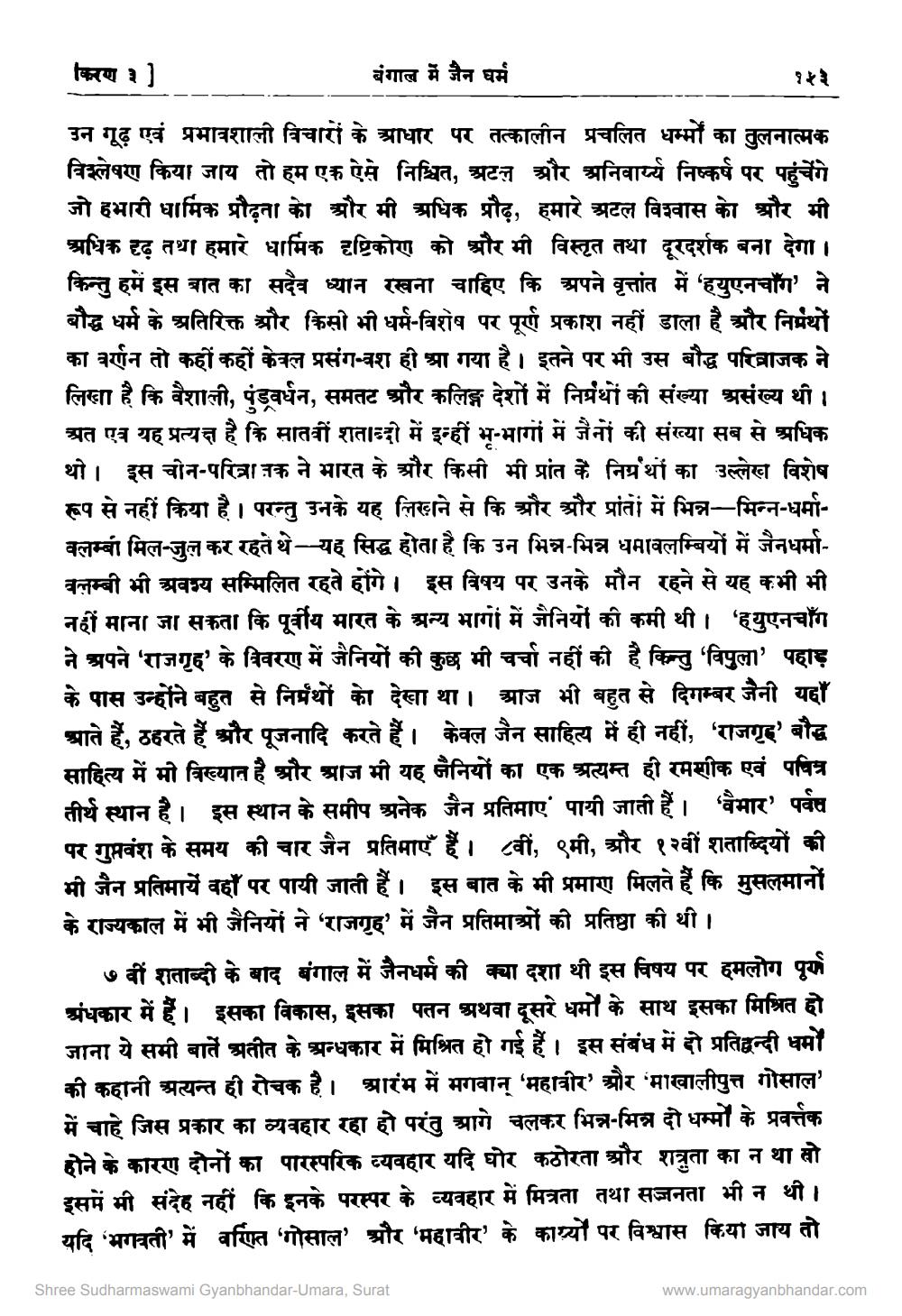________________
किरण ३]
बंगाल में जैन धर्म
उन गूढ़ एवं प्रभावशाली विचारों के आधार पर तत्कालीन प्रचलित धम्मों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाय तो हम एक ऐसे निश्चित, अटल और अनिवार्य्य निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जो हमारी धार्मिक प्रौढ़ता को और भी अधिक प्रौढ़, हमारे अटल विश्वास को और मी अधिक दृढ़ तथा हमारे धार्मिक दृष्टिकोण को और भी विस्तृत तथा दूरदर्शक बना देगा। किन्तु हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने वृत्तांत में 'हयुएनचॉग' ने बौद्ध धर्म के अतिरिक्त और किसी भी धर्म-विशेष पर पूर्ण प्रकाश नहीं डाला है और निग्रंथों का वर्णन तो कहीं कहों केवल प्रसंग-वश ही आ गया है। इतने पर भी उस बौद्ध परिव्राजक ने लिखा है कि वैशाली, पंडवर्धन, समतट और कलिङ्ग देशों में निग्रंथों की संख्या असंख्य थी। अत एव यह प्रत्यक्ष है कि सातवीं शताब्दी में इन्हीं भू-भागों में जैनों की संख्या सब से अधिक थो। इस चीन-परित्रातक ने भारत के और किसी भी प्रांत के निग्रंथों का उल्लेख विशेष रूप से नहीं किया है। परन्तु उनके यह लिखने से कि और और प्रांतों में भिन्न-मिन्न-धर्मावलम्बा मिल-जुल कर रहते थे--यह सिद्ध होता है कि उन भिन्न-भिन्न धमावलम्बियों में जैनधर्मावलम्बी भी अवश्य सम्मिलित रहते होंगे। इस विषय पर उनके मौन रहने से यह कभी भी नहीं माना जा सकता कि पूर्वीय भारत के अन्य भागों में जैनियों की कमी थी। 'हयुएनचाँग ने अपने राजगृह' के विवरण में जैनियों की कुछ भी चर्चा नहीं की है किन्तु 'विपुला' पहाड़ के पास उन्होंने बहुत से निपंथों को देखा था। आज भी बहुत से दिगम्बर जैनी यहाँ आते हैं, ठहरते हैं और पूजनादि करते हैं। केवल जैन साहित्य में ही नहीं, 'राजगृह' बौद्ध साहित्य में मो विख्यात है और आज भी यह जैनियों का एक अत्यन्त ही रमणीक एवं पवित्र तीर्थ स्थान है। इस स्थान के समीप अनेक जैन प्रतिमाए पायी जाती हैं। 'वैमार' पर्वत पर गुप्तवंश के समय की चार जैन प्रतिमाएँ हैं। ८वीं, ९मी, और १२वीं शताब्दियों की मी जैन प्रतिमायें वहाँ पर पायी जाती हैं। इस बात के मी प्रमाण मिलते हैं कि मुसलमानों के राज्यकाल में भी जैनियों ने 'राजगृह' में जैन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की थी।
७ वीं शताब्दी के बाद बंगाल में जैनधर्म की क्या दशा थी इस विषय पर हमलोग पूर्ण अंधकार में हैं। इसका विकास, इसका पतन अथवा दूसरे धर्मों के साथ इसका मिश्रित हो जाना ये समी बातें अतीत के अन्धकार में मिश्रित हो गई हैं। इस संबंध में दो प्रतिद्वन्दी धमों की कहानी अत्यन्त ही रोचक है। प्रारंभ में भगवान महावीर' और 'माखालीपुत्त गोसाल' में चाहे जिस प्रकार का व्यवहार रहा हो परंतु आगे चलकर भिन्न-भिन्न दो धम्मों के प्रवर्तक होने के कारण दोनों का पारस्परिक व्यवहार यदि घोर कठोरता और शत्रुता का न था वो इसमें भी संदेह नहीं कि इनके परस्पर के व्यवहार में मित्रता तथा सजनता भी न थी। यदि भगवती' में वर्णित 'गोसाल' और 'महावीर' के कार्यों पर विश्वास किया जाय तो
Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat
www.umaragyanbhandar.com