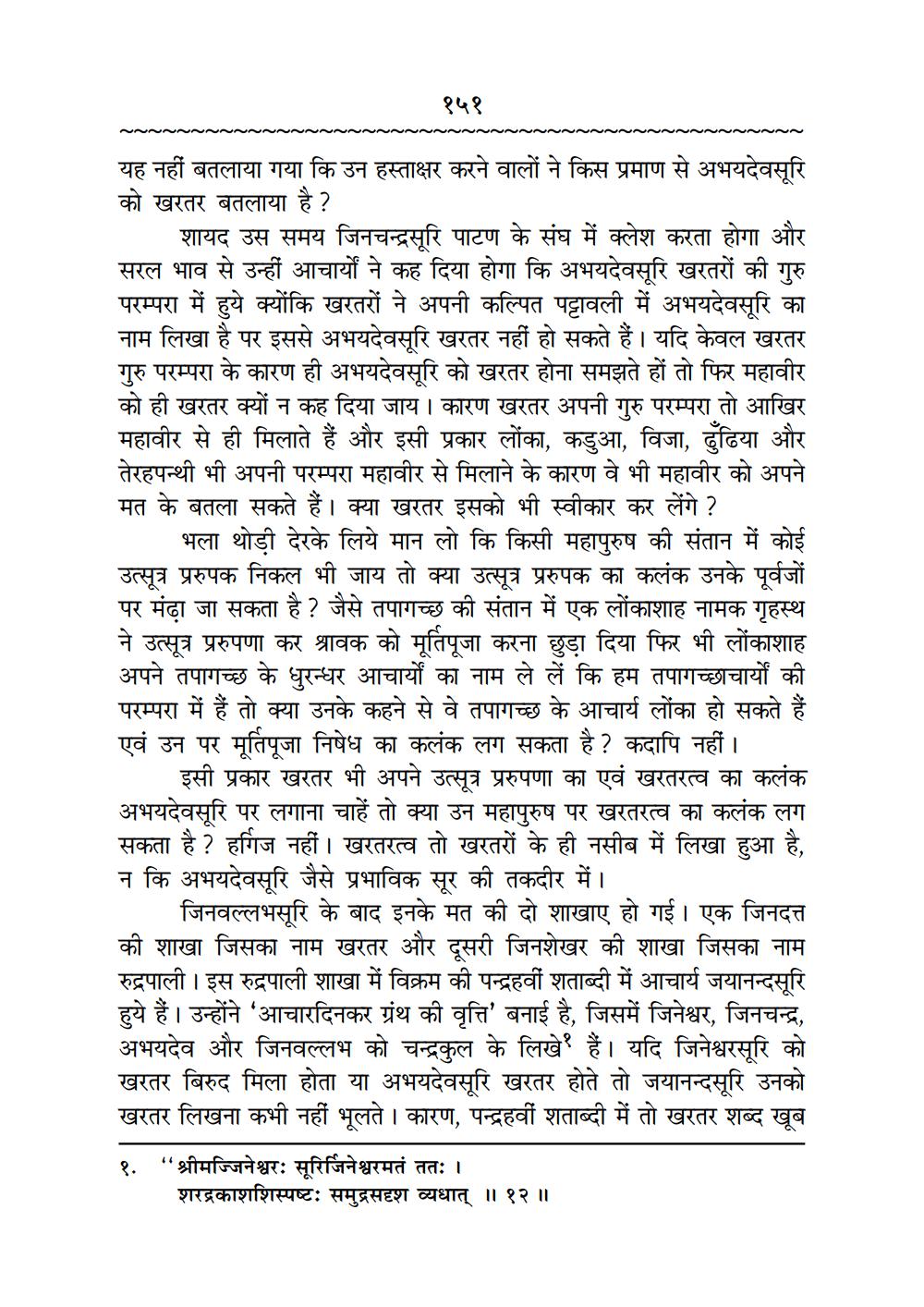________________
१५१
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
यह नहीं बतलाया गया कि उन हस्ताक्षर करने वालों ने किस प्रमाण से अभयदेवसूरि को खरतर बतलाया है? ।
शायद उस समय जिनचन्द्रसूरि पाटण के संघ में क्लेश करता होगा और सरल भाव से उन्हीं आचार्यों ने कह दिया होगा कि अभयदेवसूरि खरतरों की गुरु परम्परा में हुये क्योंकि खरतरों ने अपनी कल्पित पट्टावली में अभयदेवसूरि का नाम लिखा है पर इससे अभयदेवसूरि खरतर नहीं हो सकते हैं। यदि केवल खरतर गुरु परम्परा के कारण ही अभयदेवसूरि को खरतर होना समझते हों तो फिर महावीर को ही खरतर क्यों न कह दिया जाय । कारण खरतर अपनी गुरु परम्परा तो आखिर महावीर से ही मिलाते हैं और इसी प्रकार लोंका, कडुआ, विजा, दुढिया और तेरहपन्थी भी अपनी परम्परा महावीर से मिलाने के कारण वे भी महावीर को अपने मत के बतला सकते हैं। क्या खरतर इसको भी स्वीकार कर लेंगे?
भला थोड़ी देरके लिये मान लो कि किसी महापुरुष की संतान में कोई उत्सूत्र प्ररुपक निकल भी जाय तो क्या उत्सूत्र प्ररुपक का कलंक उनके पूर्वजों पर मंढ़ा जा सकता है? जैसे तपागच्छ की संतान में एक लोंकाशाह नामक गृहस्थ ने उत्सूत्र प्ररुपणा कर श्रावक को मूर्तिपूजा करना छुड़ा दिया फिर भी लोंकाशाह अपने तपागच्छ के धुरन्धर आचार्यों का नाम ले लें कि हम तपागच्छाचार्यों की परम्परा में हैं तो क्या उनके कहने से वे तपागच्छ के आचार्य लोंका हो सकते हैं एवं उन पर मूर्तिपूजा निषेध का कलंक लग सकता है? कदापि नहीं।
इसी प्रकार खरतर भी अपने उत्सूत्र प्ररुपणा का एवं खरतरत्व का कलंक अभयदेवसूरि पर लगाना चाहें तो क्या उन महापुरुष पर खरतरत्व का कलंक लग सकता है? हर्गिज नहीं। खरतरत्व तो खरतरों के ही नसीब में लिखा हुआ है, न कि अभयदेवसूरि जैसे प्रभाविक सूर की तकदीर में।
जिनवल्लभसूरि के बाद इनके मत की दो शाखाए हो गई। एक जिनदत्त की शाखा जिसका नाम खरतर और दूसरी जिनशेखर की शाखा जिसका नाम रुद्रपाली । इस रुद्रपाली शाखा में विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में आचार्य जयानन्दसूरि हुये हैं। उन्होंने 'आचारदिनकर ग्रंथ की वृत्ति' बनाई है, जिसमें जिनेश्वर, जिनचन्द्र, अभयदेव और जिनवल्लभ को चन्द्रकुल के लिखे हैं। यदि जिनेश्वरसूरि को खरतर बिरुद मिला होता या अभयदेवसूरि खरतर होते तो जयानन्दसूरि उनको खरतर लिखना कभी नहीं भूलते । कारण, पन्द्रहवीं शताब्दी में तो खरतर शब्द खूब १. “श्रीमज्जिनेश्वरः सूरिजिनेश्वरमतं ततः ।
शरद्रकाशशिस्पष्टः समुद्रसदृश व्यधात् ॥ १२ ॥