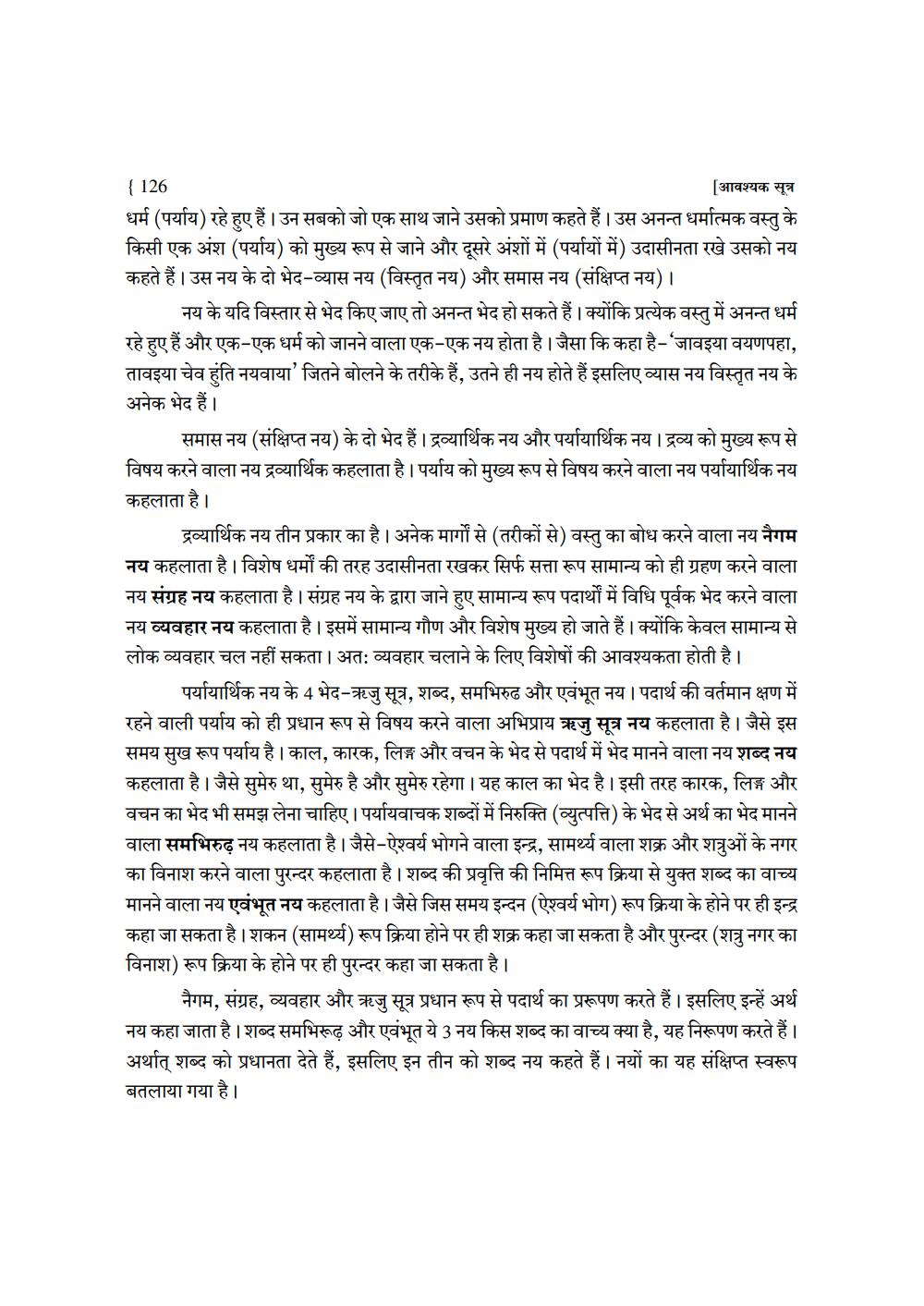________________
{ 126
[आवश्यक सूत्र धर्म (पर्याय) रहे हुए हैं। उन सबको जो एक साथ जाने उसको प्रमाण कहते हैं । उस अनन्त धर्मात्मक वस्तु के किसी एक अंश (पर्याय) को मुख्य रूप से जाने और दूसरे अंशों में (पर्यायों में) उदासीनता रखे उसको नय कहते हैं। उस नय के दो भेद-व्यास नय (विस्तृत नय) और समास नय (संक्षिप्त नय)।
नय के यदि विस्तार से भेद किए जाए तो अनन्त भेद हो सकते हैं । क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म रहे हुए हैं और एक-एक धर्म को जानने वाला एक-एक नय होता है। जैसा कि कहा है-'जावइया वयणपहा, तावइया चेव हुंति नयवाया' जितने बोलने के तरीके हैं, उतने ही नय होते हैं इसलिए व्यास नय विस्तृत नय के अनेक भेद हैं।
समास नय (संक्षिप्त नय) के दो भेद हैं। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय । द्रव्य को मुख्य रूप से विषय करने वाला नय द्रव्यार्थिक कहलाता है। पर्याय को मुख्य रूप से विषय करने वाला नय पर्यायार्थिक नय कहलाता है।
द्रव्यार्थिक नय तीन प्रकार का है। अनेक मार्गों से (तरीकों से) वस्तु का बोध करने वाला नय नैगम नय कहलाता है। विशेष धर्मों की तरह उदासीनता रखकर सिर्फ सत्ता रूप सामान्य को ही ग्रहण करने वाला नय संग्रह नय कहलाता है। संग्रह नय के द्वारा जाने हुए सामान्य रूप पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करने वाला नय व्यवहार नय कहलाता है। इसमें सामान्य गौण और विशेष मुख्य हो जाते हैं। क्योंकि केवल सामान्य से लोक व्यवहार चल नहीं सकता। अत: व्यवहार चलाने के लिए विशेषों की आवश्यकता होती है।
पर्यायार्थिक नय के 4 भेद-ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरुढ और एवंभूत नय । पदार्थ की वर्तमान क्षण में रहने वाली पर्याय को ही प्रधान रूप से विषय करने वाला अभिप्राय ऋजु सूत्र नय कहलाता है। जैसे इस समय सुख रूप पर्याय है। काल, कारक, लिङ्ग और वचन के भेद से पदार्थ में भेद मानने वाला नय शब्द नय कहलाता है। जैसे सुमेरु था, सुमेरु है और सुमेरु रहेगा । यह काल का भेद है। इसी तरह कारक, लिङ्ग और वचन का भेद भी समझ लेना चाहिए । पर्यायवाचक शब्दों में निरुक्ति (व्युत्पत्ति) के भेद से अर्थ का भेद मानने वाला समभिरुढ़ नय कहलाता है। जैसे-ऐश्वर्य भोगने वाला इन्द्र, सामर्थ्य वाला शक्र और शत्रुओं के नगर का विनाश करने वाला पुरन्दर कहलाता है। शब्द की प्रवृत्ति की निमित्त रूप क्रिया से युक्त शब्द का वाच्य मानने वाला नय एवंभूत नय कहलाता है। जैसे जिस समय इन्दन (ऐश्वर्य भोग) रूप क्रिया के होने पर ही इन्द्र कहा जा सकता है। शकन (सामर्थ्य) रूप क्रिया होने पर ही शक्र कहा जा सकता है और पुरन्दर (शत्रु नगर का विनाश) रूप क्रिया के होने पर ही पुरन्दर कहा जा सकता है।
नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र प्रधान रूप से पदार्थ का प्ररूपण करते हैं। इसलिए इन्हें अर्थ नय कहा जाता है। शब्द समभिरूढ़ और एवंभूत ये 3 नय किस शब्द का वाच्य क्या है, यह निरूपण करते हैं। अर्थात् शब्द को प्रधानता देते हैं, इसलिए इन तीन को शब्द नय कहते हैं। नयों का यह संक्षिप्त स्वरूप बतलाया गया है।