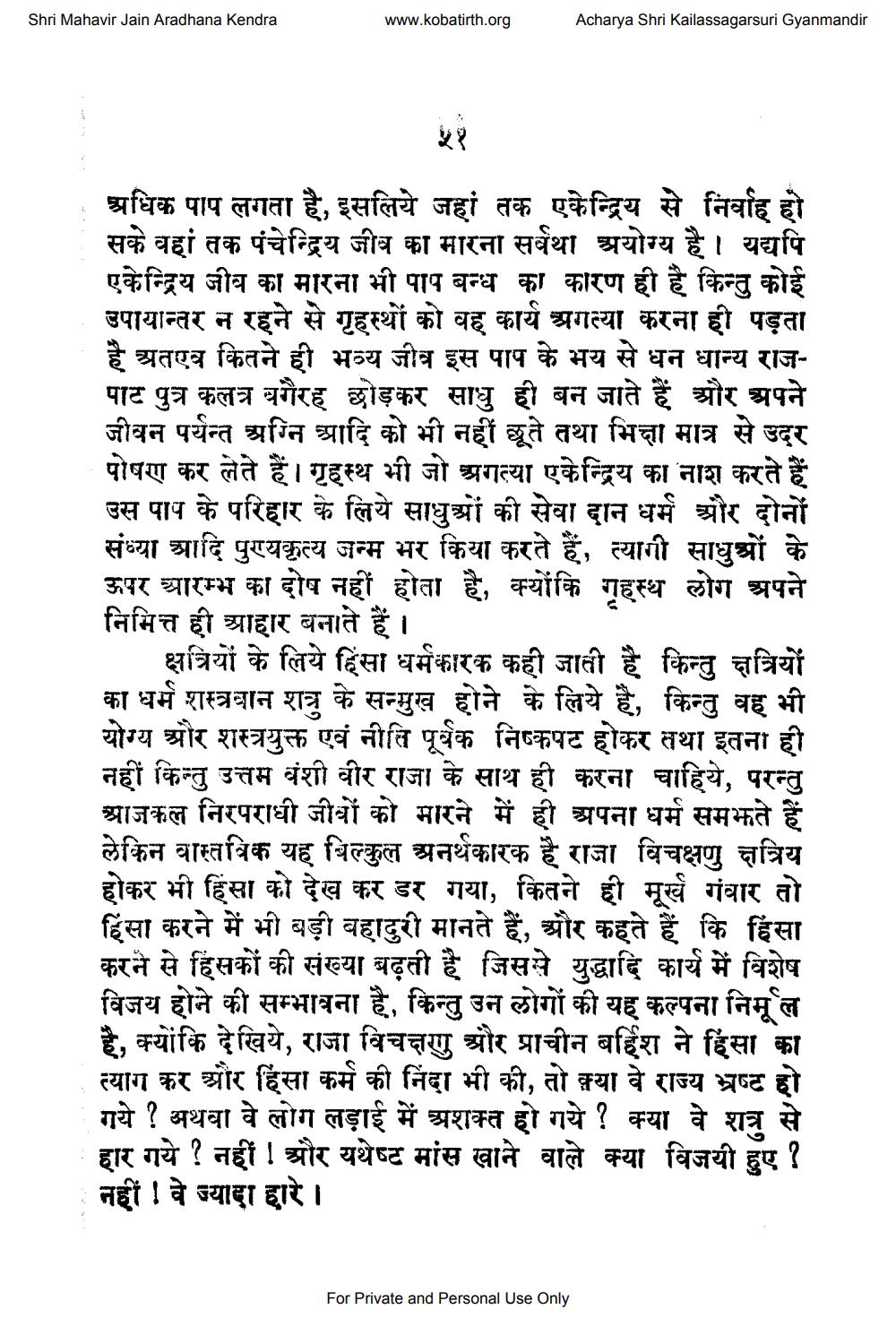________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
अधिक पाप लगता है, इसलिये जहां तक एकेन्द्रिय से निर्वाह हो सके वहां तक पंचेन्द्रिय जीव का मारना सर्वथा अयोग्य है। यद्यपि एकेन्द्रिय जीव का मारना भी पाप बन्ध का कारण ही है किन्तु कोई उपायान्तर न रहने से गृहस्थों को वह कार्य अगत्या करना ही पड़ता है अतएव कितने ही भव्य जीव इस पाप के भय से धन धान्य राजपाट पुत्र कलत्र वगैरह छोड़कर साधु ही बन जाते हैं और अपने जीवन पर्यन्त अग्नि आदि को भी नहीं छूते तथा भिक्षा मात्र से उदर पोषण कर लेते हैं। गृहस्थ भी जो अगत्या एकेन्द्रिय का नाश करते हैं उस पाप के परिहार के लिये साधुओं की सेवा दान धर्म और दोनों संध्या आदि पुण्यकृत्य जन्म भर किया करते हैं, त्यागी साधुओं के ऊपर आरम्भ का दोष नहीं होता है, क्योंकि गृहस्थ लोग अपने निमित्त ही आहार बनाते हैं।
क्षत्रियों के लिये हिंसा धर्मकारक कही जाती है किन्तु क्षत्रियों का धर्म शस्त्रवान शत्रु के सन्मुख होने के लिये है, किन्तु वह भी योग्य और शस्त्रयुक्त एवं नीति पूर्वक निष्कपट होकर तथा इतना ही नहीं किन्तु उत्तम वंशी वीर राजा के साथ ही करना चाहिये, परन्तु अाजकल निरपराधी जीवों को मारने में ही अपना धर्म समझते हैं लेकिन वास्तविक यह बिल्कुल अनर्थकारक है राजा विचक्षणु क्षत्रिय होकर भी हिंसा को देख कर डर गया, कितने ही मूर्ख गंवार तो हिंसा करने में भी बड़ी बहादुरी मानते हैं, और कहते हैं कि हिंसा करने से हिंसकों की संख्या बढ़ती है जिससे युद्धादि कार्य में विशेष विजय होने की सम्भावना है, किन्तु उन लोगों की यह कल्पना निर्मूल है, क्योंकि देखिये, राजा विचक्षणु और प्राचीन बर्हिश ने हिंसा का त्याग कर और हिंसा कर्म की निंदा भी की, तो क्या वे राज्य भ्रष्ट हो गये ? अथवा वे लोग लड़ाई में अशक्त हो गये ? क्या वे शत्रु से हार गये ? नहीं ! और यथेष्ट मांस खाने वाले क्या विजयी हुए ? नहीं ! वे ज्यादा हारे।
For Private and Personal Use Only