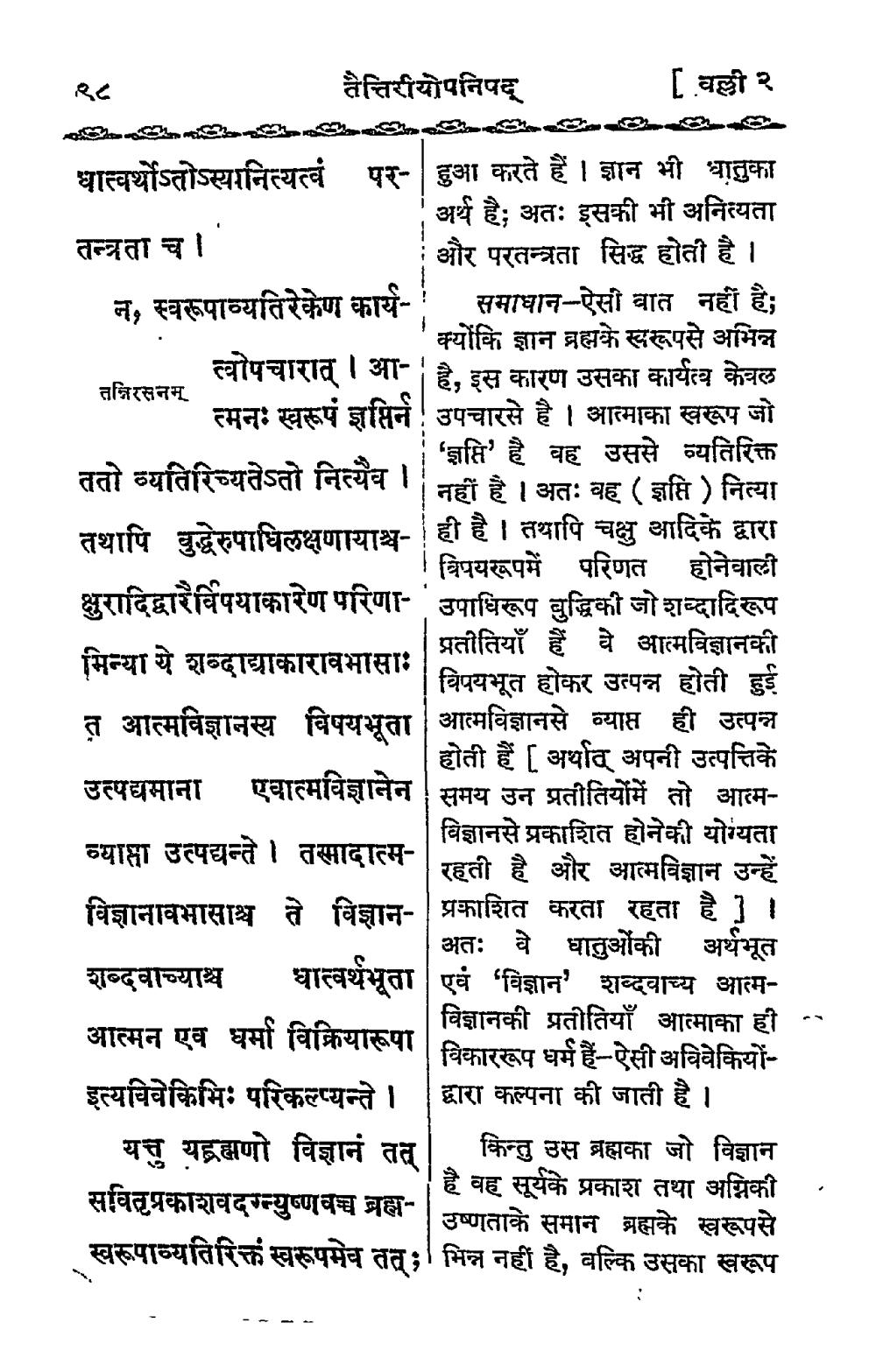________________
तैत्तिरीयोपनिषद्
[ वल्ली २
धात्वर्थोऽतोऽस्यानित्यत्वं पर हुआ करते हैं । ज्ञान भी धातुका
अर्थ है; अतः इसकी भी अनित्यता और परतन्त्रता सिद्ध होती है ।
९८
तन्त्रता च ।
समाधान- ऐसी बात नहीं है; क्योंकि ज्ञान ब्रह्मके स्वरूपसे अभिन्न त्वोपचारात् । आ- है, इस कारण उसका कार्यत्व केवल तन्निरसनम् त्मनः स्वरूपं ज्ञप्तिर्न ! उपचारसे है । आत्माका स्वरूप जो
न, स्वरूपाव्यतिरेकेण कार्य
ततो व्यतिरिच्यतेऽतो नित्यैव ।
तथापि
बुद्धेरुपाधिलक्षणायाश्च
|
क्षुरादिद्वारैर्विपयाकारेण परिणा
'ज्ञप्ति' है वह उससे व्यतिरिक्त नहीं है । अतः वह (ज्ञप्ति ) नित्या ही है। तथापि चक्षु आदिके द्वारा विपयरूपमें परिणत होनेवाली उपाधिरूप बुद्धिकी जो शब्दादिरूप प्रतीतियाँ हैं वे आत्मविज्ञानकी विपयभूत होकर उत्पन्न होती हुई आत्मविज्ञानसे व्याप्त ही उत्पन्न होती हैं [ अर्थात् अपनी उत्पत्तिके समय उन प्रतीतियोंमें तो आत्मविज्ञानसे प्रकाशित होने की योग्यता व्याप्ता उत्पद्यन्ते । तस्मादात्म- रहती है और आत्मविज्ञान उन्हें विज्ञानावभासाथ ते विज्ञान - प्रकाशित करता रहता है ] । अतः वे धातुओंकी अर्थभूत धात्वर्थभूता एवं 'विज्ञान' शब्दवाच्य आत्मविज्ञानकी प्रतीतियाँ आत्माका ही विकाररूप धर्म हैं- ऐसी अविवेकियोंद्वारा कल्पना की जाती है ।
उत्पद्यमाना
शब्दवाच्याच आत्मन एव धर्मा विक्रियारूपा इत्यविवेकिभिः परिकल्प्यन्ते ।
यत्तु यद्ब्रह्मणो विज्ञानं तत् किन्तु उस ब्रह्मका जो विज्ञान सवितृप्रकाशवदग्न्युष्णवच्च ब्रह्म- उष्णताके समान ब्रह्मके स्वरूपसे है वह सूर्यके प्रकाश तथा अग्निकी स्वरूपाव्यतिरिक्तं स्वरूपमेव तत्; भिन्न नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप
मिन्या ये
त आत्मविज्ञानस्य विषयभूता
एवात्मविज्ञानेन
शब्दाद्याकारावभासाः
--