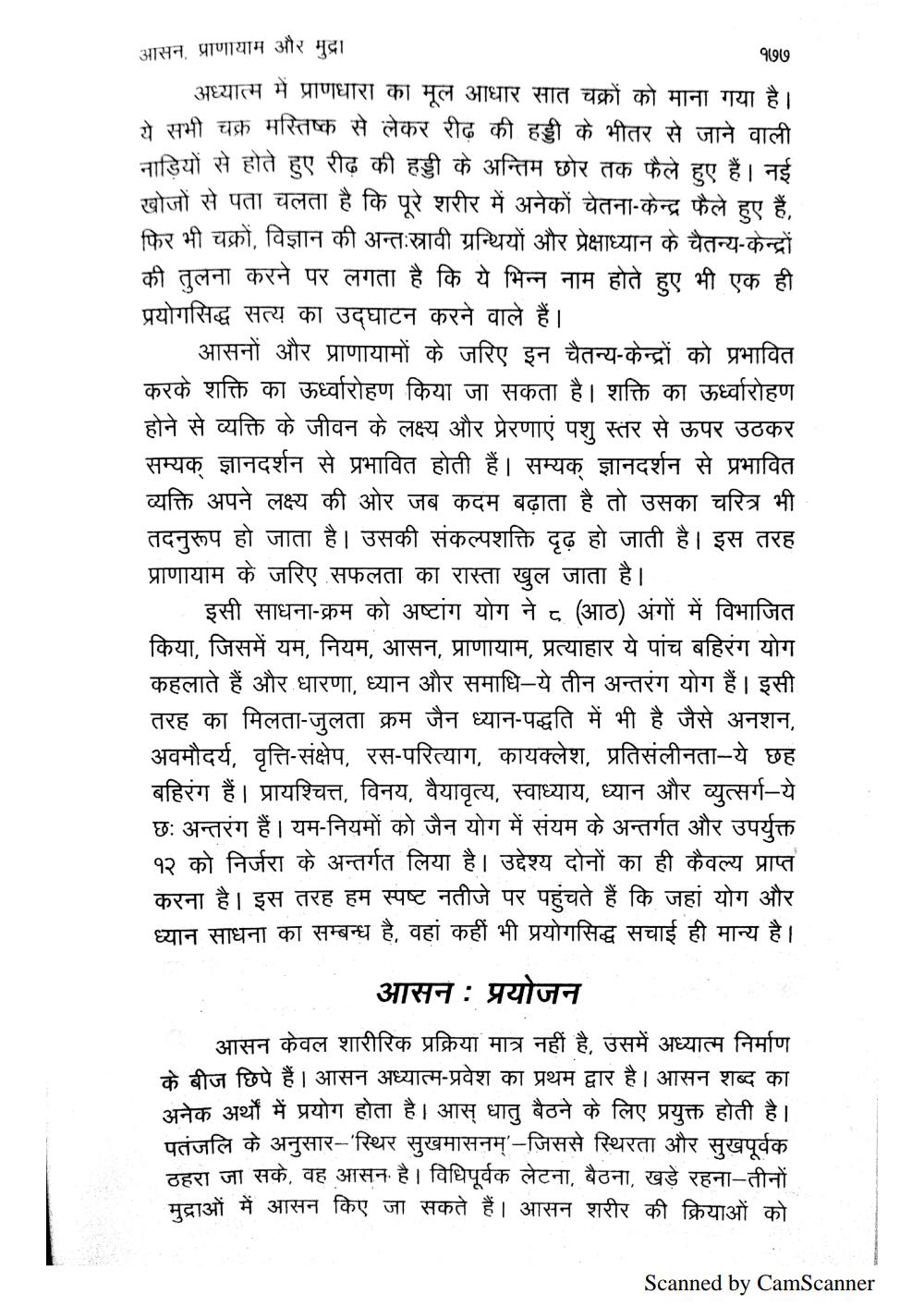________________
आसन, प्राणायाम और मुद्रा
१७७ अध्यात्म में प्राणधारा का मूल आधार सात चक्रों को माना गया है। ये सभी चक्र मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डी के भीतर से जाने वाली नाडियों से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अन्तिम छोर तक फैले हुए हैं। नई खोजों से पता चलता है कि पूरे शरीर में अनेकों चेतना-केन्द्र फैले हुए हैं, फिर भी चक्रों, विज्ञान की अन्तःस्रावी ग्रन्थियों और प्रेक्षाध्यान के चैतन्य-केन्द्रों की तुलना करने पर लगता है कि ये भिन्न नाम होते हुए भी एक ही प्रयोगसिद्ध सत्य का उद्घाटन करने वाले हैं।
आसनों और प्राणायामों के जरिए इन चैतन्य-केन्द्रों को प्रभावित करके शक्ति का ऊर्ध्वारोहण किया जा सकता है। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होने से व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य और प्रेरणाएं पशु स्तर से ऊपर उठकर सम्यक् ज्ञानदर्शन से प्रभावित होती हैं। सम्यक् ज्ञानदर्शन से प्रभावित व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर जब कदम बढ़ाता है तो उसका चरित्र भी तदनुरूप हो जाता है। उसकी संकल्पशक्ति दृढ़ हो जाती है। इस तरह प्राणायाम के जरिए सफलता का रास्ता खुल जाता है।
इसी साधना-क्रम को अष्टांग योग ने ८ (आठ) अंगों में विभाजित किया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये पांच बहिरंग योग कहलाते हैं और धारणा, ध्यान और समाधि-ये तीन अन्तरंग योग हैं। इसी तरह का मिलता-जुलता क्रम जैन ध्यान-पद्धति में भी है जैसे अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति-संक्षेप, रस-परित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंलीनता-ये छह बहिरंग हैं। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग-ये छ: अन्तरंग हैं। यम-नियमों को जैन योग में संयम के अन्तर्गत और उपर्युक्त १२ को निर्जरा के अन्तर्गत लिया है। उद्देश्य दोनों का ही कैवल्य प्राप्त करना है। इस तरह हम स्पष्ट नतीजे पर पहुंचते हैं कि जहां योग और ध्यान साधना का सम्बन्ध है, वहां कहीं भी प्रयोगसिद्ध सचाई ही मान्य है।
आसन : प्रयोजन आसन केवल शारीरिक प्रक्रिया मात्र नहीं है, उसमें अध्यात्म निर्माण के बीज छिपे हैं। आसन अध्यात्म-प्रवेश का प्रथम द्वार है। आसन शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। आस् धातु बैठने के लिए प्रयुक्त होती है। पतंजलि के अनुसार-'स्थिर सुखमासनम्'-जिससे स्थिरता और सुखपूर्वक ठहरा जा सके, वह आसन है। विधिपूर्वक लेटना, बैठना, खड़े रहना-तीनों मद्राओं में आसन किए जा सकते हैं। आसन शरीर की क्रियाओं को
Scanned by CamScanner