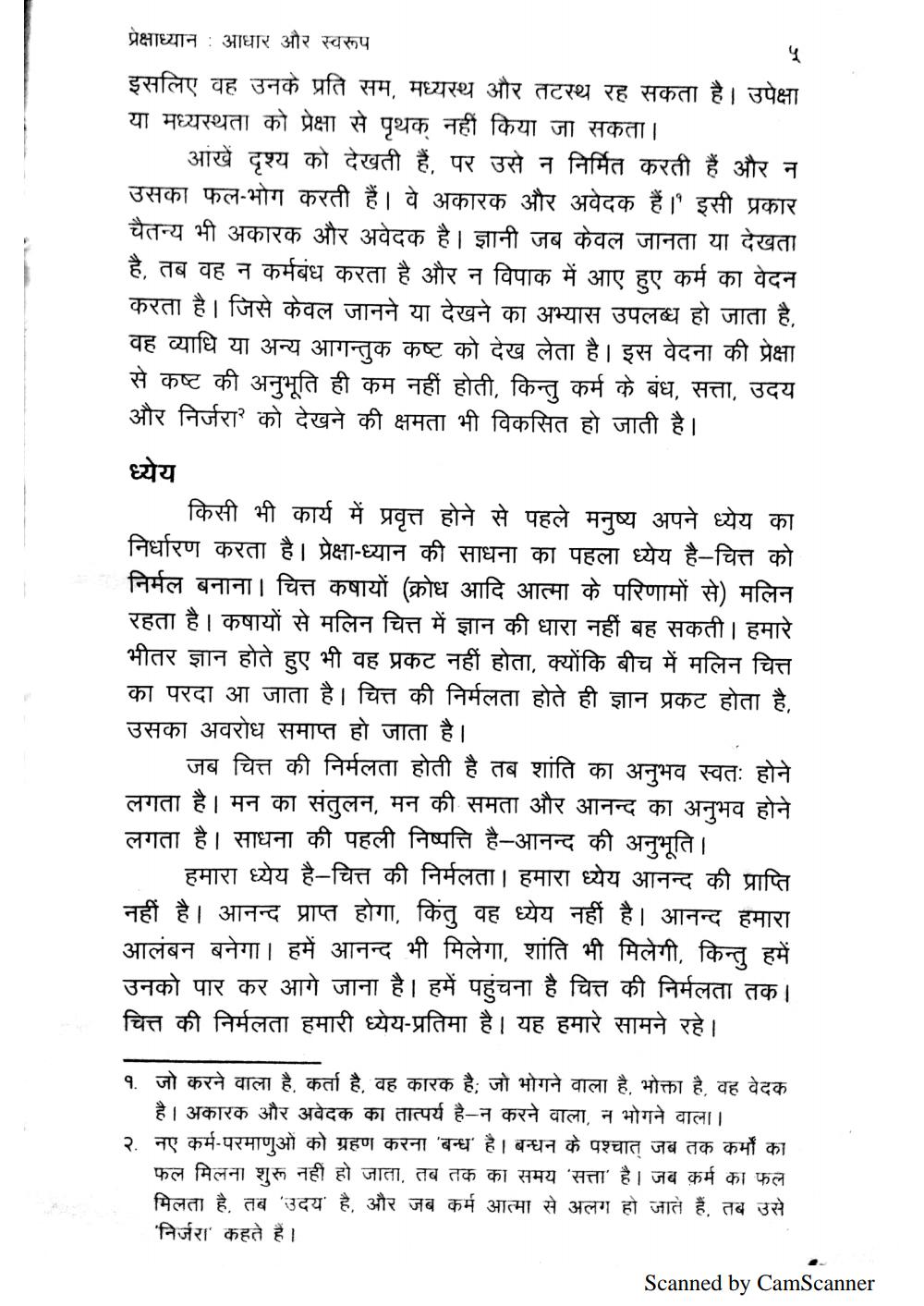________________
प्रेक्षाध्यान : आधार और स्वरूप इसलिए वह उनके प्रति सम, मध्यस्थ और तटस्थ रह सकता है। उपेक्षा या मध्यस्थता को प्रेक्षा से पृथक नहीं किया जा सकता।
आंखें दृश्य को देखती हैं, पर उसे न निर्मित करती हैं और न उसका फल-भोग करती हैं। वे अकारक और अवेदक हैं।' इसी प्रकार चैतन्य भी अकारक और अवेदक है। ज्ञानी जब केवल जानता या देखता है, तब वह न कर्मबंध करता है और न विपाक में आए हुए कर्म का वेदन करता है। जिसे केवल जानने या देखने का अभ्यास उपलब्ध हो जाता है, वह व्याधि या अन्य आगन्तुक कष्ट को देख लेता है। इस वेदना की प्रेक्षा से कष्ट की अनुभूति ही कम नहीं होती, किन्तु कर्म के बंध, सत्ता, उदय और निर्जरा' को देखने की क्षमता भी विकसित हो जाती है।
ध्येय
किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने से पहले मनुष्य अपने ध्येय का निर्धारण करता है। प्रेक्षा-ध्यान की साधना का पहला ध्येय है-चित्त को निर्मल बनाना। चित्त कषायों (क्रोध आदि आत्मा के परिणामों से) मलिन रहता है। कषायों से मलिन चित्त में ज्ञान की धारा नहीं बह सकती। हमारे भीतर ज्ञान होते हुए भी वह प्रकट नहीं होता, क्योंकि बीच में मलिन चित्त का परदा आ जाता है। चित्त की निर्मलता होते ही ज्ञान प्रकट होता है, उसका अवरोध समाप्त हो जाता है।
जब चित्त की निर्मलता होती है तब शांति का अनुभव स्वतः होने लगता है। मन का संतुलन, मन की समता और आनन्द का अनुभव होने लगता है। साधना की पहली निष्पत्ति है-आनन्द की अनुभूति।
हमारा ध्येय है-चित्त की निर्मलता। हमारा ध्येय आनन्द की प्राप्ति नहीं है। आनन्द प्राप्त होगा, किंतु वह ध्येय नहीं है। आनन्द हमारा आलंबन बनेगा। हमें आनन्द भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, किन्तु हमें उनको पार कर आगे जाना है। हमें पहुंचना है चित्त की निर्मलता तक। चित्त की निर्मलता हमारी ध्येय-प्रतिमा है। यह हमारे सामने रहे।
१. जो करने वाला है. कर्ता है, वह कारक है; जो भोगने वाला है, भोक्ता है, वह वेदक
है। अकारक और अवेदक का तात्पर्य है-न करने वाला, न भोगने वाला। २. नए कर्म-परमाणुओं को ग्रहण करना 'बन्ध है। बन्धन के पश्चात् जब तक कर्मों का
फल मिलना शुरू नहीं हो जाता, तब तक का समय 'सत्ता' है। जब कर्म का फल मिलता है. तब 'उदय' है, और जब कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं, तब उसे 'निर्जरा कहते हैं।
Scanned by CamScanner