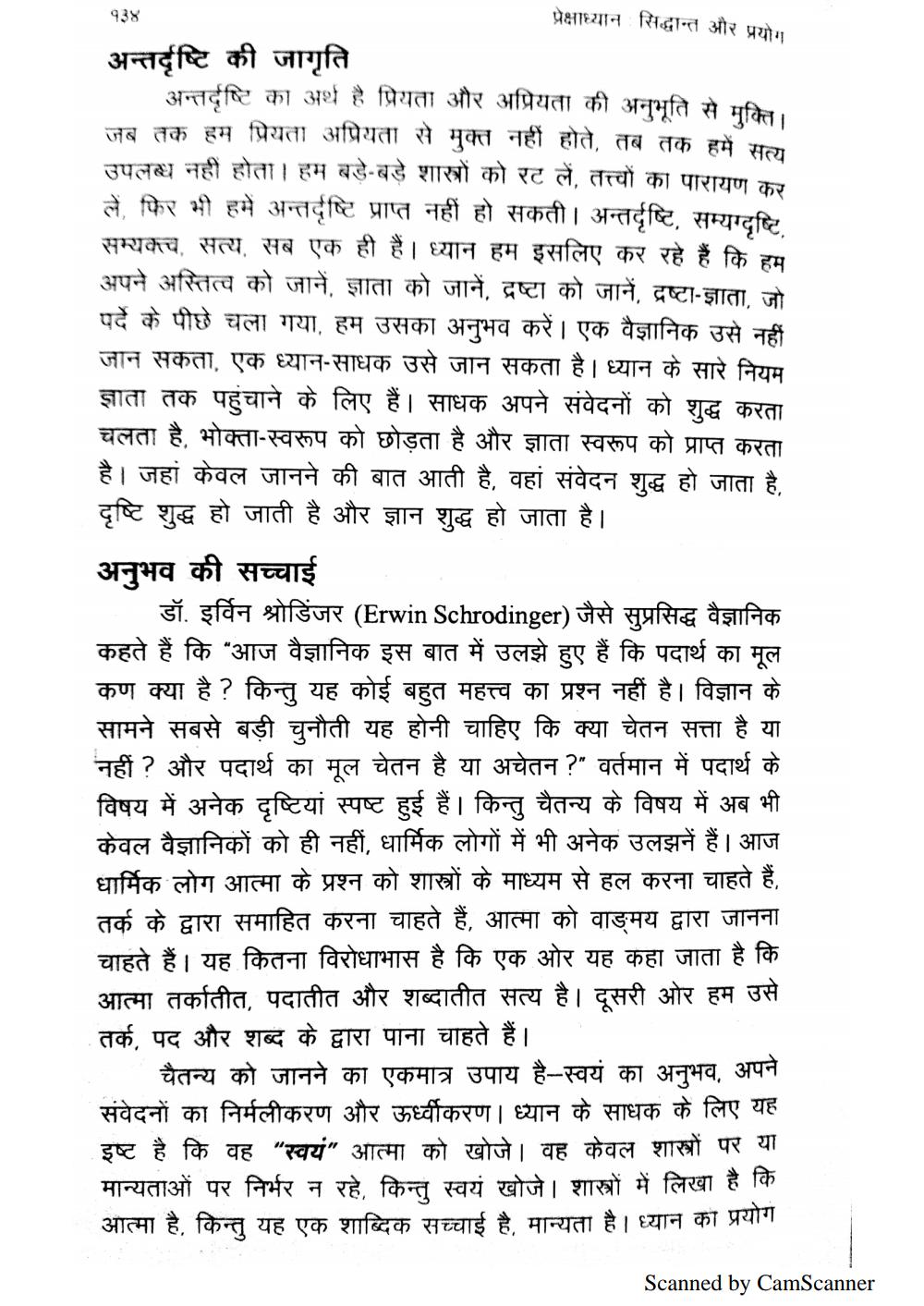________________
प्रेक्षाध्यान सिद्धान्त और प्रयोग
१३४ अन्तर्दृष्टि की जागृति
अन्तर्दष्टि का अर्थ है प्रियता और अप्रियता की अनुभूति से मक्ति। जब तक हम प्रियता अप्रियता से मुक्त नहीं होते, तब तक हमें सत्ता उपलब्ध नहीं होता। हम बड़े-बड़े शास्त्रों को रट लें, तत्त्वों का पारायण कर लें, फिर भी हमें अन्तर्दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। अन्तर्दृष्टि, सम्यग्दष्टि सम्यक्च, सत्य, सब एक ही हैं। ध्यान हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने अस्तित्व को जानें, ज्ञाता को जानें, द्रष्टा को जानें, द्रष्टा-ज्ञाता, जो पर्दे के पीछे चला गया, हम उसका अनुभव करें। एक वैज्ञानिक उसे नहीं जान सकता, एक ध्यान-साधक उसे जान सकता है। ध्यान के सारे नियम ज्ञाता तक पहुंचाने के लिए हैं। साधक अपने संवेदनों को शुद्ध करता चलता है, भोक्ता-स्वरूप को छोड़ता है और ज्ञाता स्वरूप को प्राप्त करता है। जहां केवल जानने की बात आती है, वहां संवेदन शुद्ध हो जाता है, दृष्टि शुद्ध हो जाती है और ज्ञान शुद्ध हो जाता है। अनुभव की सच्चाई
डॉ. इर्विन श्रोडिंजर (Erwin Schrodinger) जैसे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक कहते हैं कि “आज वैज्ञानिक इस बात में उलझे हुए हैं कि पदार्थ का मूल कण क्या है? किन्तु यह कोई बहुत महत्त्व का प्रश्न नहीं है। विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होनी चाहिए कि क्या चेतन सत्ता है या नहीं ? और पदार्थ का मूल चेतन है या अचेतन ?” वर्तमान में पदार्थ के विषय में अनेक दृष्टियां स्पष्ट हुई हैं। किन्तु चैतन्य के विषय में अब भी केवल वैज्ञानिकों को ही नहीं, धार्मिक लोगों में भी अनेक उलझनें हैं। आज धार्मिक लोग आत्मा के प्रश्न को शास्त्रों के माध्यम से हल करना चाहते हैं, तर्क के द्वारा समाहित करना चाहते हैं, आत्मा को वाङ्मय द्वारा जानना चाहते हैं। यह कितना विरोधाभास है कि एक ओर यह कहा जाता है कि आत्मा तर्कातीत, पदातीत और शब्दातीत सत्य है। दूसरी ओर हम उसे तर्क, पद और शब्द के द्वारा पाना चाहते हैं।
___ चैतन्य को जानने का एकमात्र उपाय है-स्वयं का अनुभव, अपने संवेदनों का निर्मलीकरण और ऊर्वीकरण । ध्यान के साधक के लिए यह इष्ट है कि वह "स्वयं" आत्मा को खोजे। वह केवल शास्त्रों पर या मान्यताओं पर निर्भर न रहे, किन्तु स्वयं खोजे। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है, किन्तु यह एक शाब्दिक सच्चाई है, मान्यता है। ध्यान का प्रयोग
Scanned by CamScanner