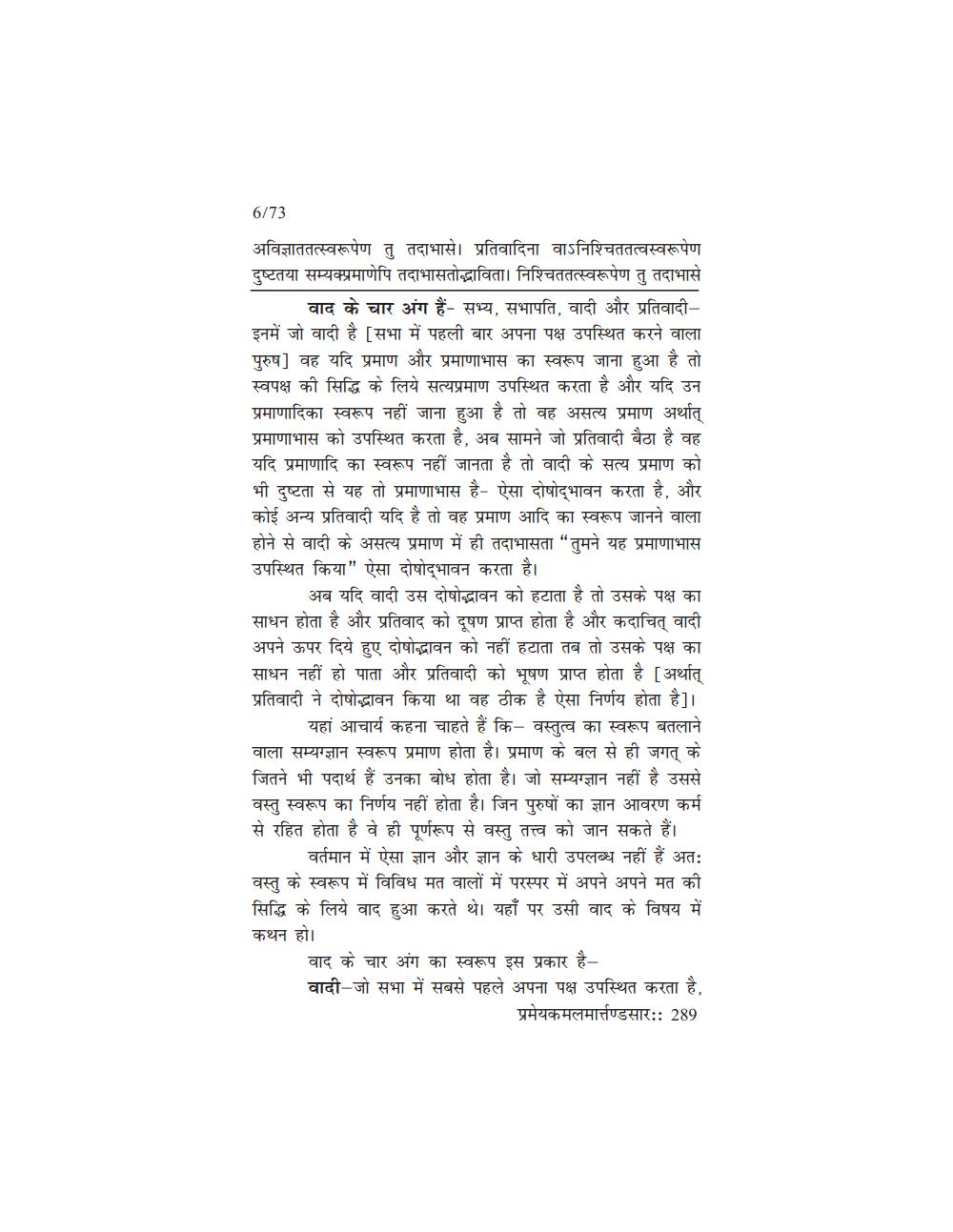________________ 6/73 अविज्ञाततत्स्वरूपेण तु तदाभासे। प्रतिवादिना वाऽनिश्चिततत्वस्वरूपेण दुष्टतया सम्यक्प्रमाणेपि तदाभासतोद्भाविता। निश्चिततत्स्वरूपेण तु तदाभासे वाद के चार अंग हैं- सभ्य, सभापति, वादी और प्रतिवादीइनमें जो वादी है [सभा में पहली बार अपना पक्ष उपस्थित करने वाला पुरुष] वह यदि प्रमाण और प्रमाणाभास का स्वरूप जाना हुआ है तो स्वपक्ष की सिद्धि के लिये सत्यप्रमाण उपस्थित करता है और यदि उन प्रमाणादिका स्वरूप नहीं जाना हुआ है तो वह असत्य प्रमाण अर्थात् प्रमाणाभास को उपस्थित करता है, अब सामने जो प्रतिवादी बैठा है वह यदि प्रमाणादि का स्वरूप नहीं जानता है तो वादी के सत्य प्रमाण को भी दुष्टता से यह तो प्रमाणाभास है- ऐसा दोषोद्भावन करता है, और कोई अन्य प्रतिवादी यदि है तो वह प्रमाण आदि का स्वरूप जानने वाला होने से वादी के असत्य प्रमाण में ही तदाभासता "तुमने यह प्रमाणाभास उपस्थित किया" ऐसा दोषोद्भावन करता है। अब यदि वादी उस दोषोद्भावन को हटाता है तो उसके पक्ष का साधन होता है और प्रतिवाद को दूषण प्राप्त होता है और कदाचित् वादी अपने ऊपर दिये हुए दोषोद्भावन को नहीं हटाता तब तो उसके पक्ष का साधन नहीं हो पाता और प्रतिवादी को भूषण प्राप्त होता है [अर्थात् प्रतिवादी ने दोषोद्भावन किया था वह ठीक है ऐसा निर्णय होता है। यहां आचार्य कहना चाहते हैं कि- वस्तुत्व का स्वरूप बतलाने वाला सम्यग्ज्ञान स्वरूप प्रमाण होता है। प्रमाण के बल से ही जगत् के जितने भी पदार्थ हैं उनका बोध होता है। जो सम्यग्ज्ञान नहीं है उससे वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होता है। जिन पुरुषों का ज्ञान आवरण कर्म से रहित होता है वे ही पूर्णरूप से वस्तु तत्त्व को जान सकते हैं। वर्तमान में ऐसा ज्ञान और ज्ञान के धारी उपलब्ध नहीं हैं अतः वस्तु के स्वरूप में विविध मत वालों में परस्पर में अपने अपने मत की सिद्धि के लिये वाद हुआ करते थे। यहाँ पर उसी वाद के विषय में कथन हो। वाद के चार अंग का स्वरूप इस प्रकार हैवादी-जो सभा में सबसे पहले अपना पक्ष उपस्थित करता है, प्रमेयकमलमार्तण्डसारः: 289