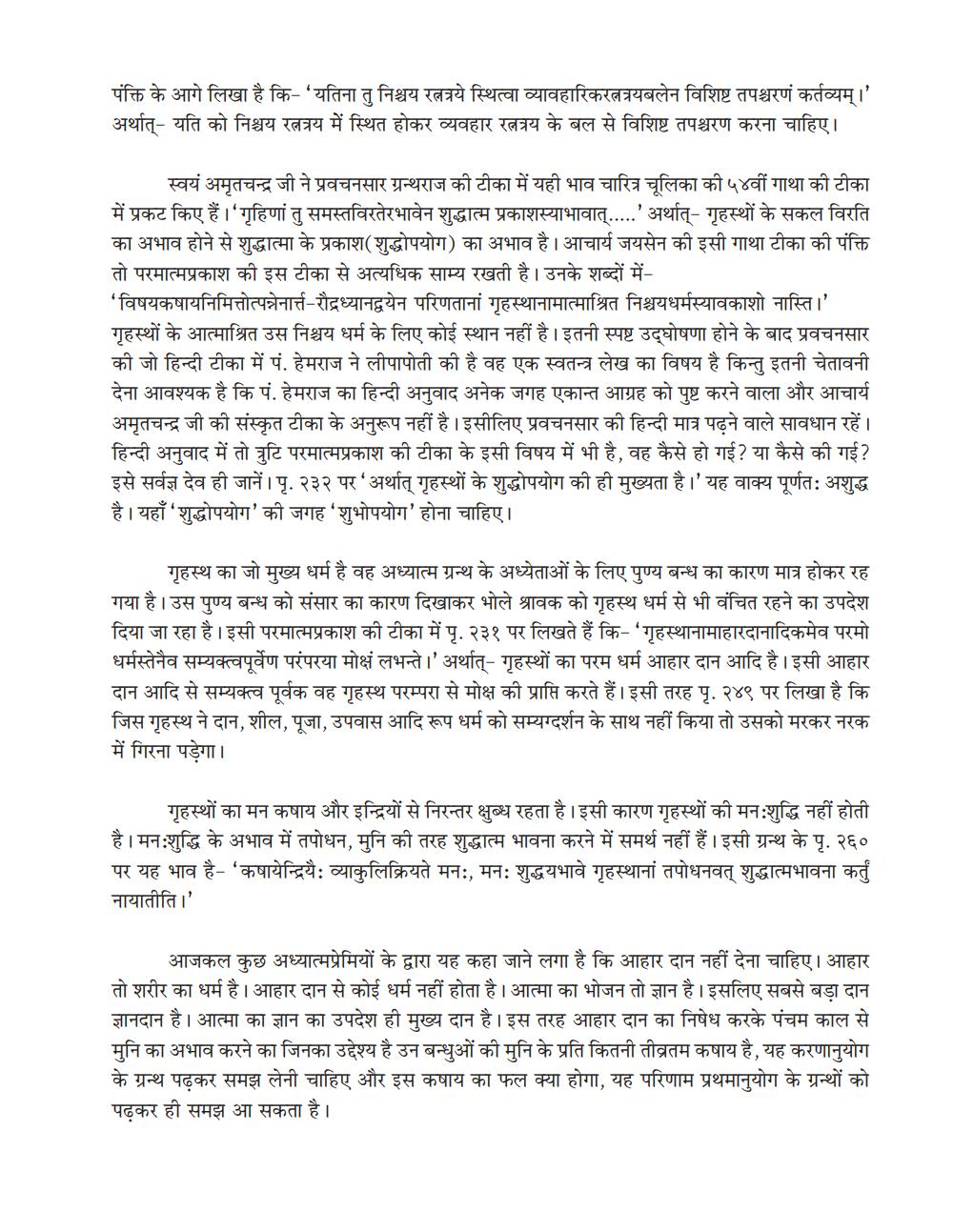________________
पंक्ति के आगे लिखा है कि- 'यतिना तु निश्चय रत्नत्रये स्थित्वा व्यावहारिकरत्नत्रयबलेन विशिष्ट तपश्चरणं कर्तव्यम्।' अर्थात्- यति को निश्चय रत्नत्रय में स्थित होकर व्यवहार रत्नत्रय के बल से विशिष्ट तपश्चरण करना चाहिए।
स्वयं अमृतचन्द्र जी ने प्रवचनसार ग्रन्थराज की टीका में यही भाव चारित्र चूलिका की ५४वीं गाथा की टीका में प्रकट किए हैं। 'गृहिणां तु समस्तविरतेरभावेन शुद्धात्म प्रकाशस्याभावात्.....' अर्थात्- गृहस्थों के सकल विरति का अभाव होने से शद्धात्मा के प्रकाश(शद्धोपयोग) का अभाव है। आचार्य जयसेन की इसी गाथा टीका की पंक्ति तो परमात्मप्रकाश की इस टीका से अत्यधिक साम्य रखती है। उनके शब्दों में'विषयकषायनिमित्तोत्पन्नेनार्त्त-रौद्रध्यानद्वयेन परिणतानां गृहस्थानामात्माश्रित निश्चयधर्मस्यावकाशो नास्ति।' गृहस्थों के आत्माश्रित उस निश्चय धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। इतनी स्पष्ट उद्घोषणा होने के बाद प्रवचनसार की जो हिन्दी टीका में पं. हेमराज ने लीपापोती की है वह एक स्वतन्त्र लेख का विषय है किन्तु इतनी चेतावनी देना आवश्यक है कि पं. हेमराज का हिन्दी अनुवाद अनेक जगह एकान्त आग्रह को पुष्ट करने वाला और आचार्य अमृतचन्द्र जी की संस्कृत टीका के अनुरूप नहीं है। इसीलिए प्रवचनसार की हिन्दी मात्र पढ़ने वाले सावधान रहें। हिन्दी अनुवाद में तो त्रुटि परमात्मप्रकाश की टीका के इसी विषय में भी है, वह कैसे हो गई? या कैसे की गई? इसे सर्वज्ञ देव ही जानें। पृ. २३२ पर 'अर्थात् गृहस्थों के शुद्धोपयोग की ही मुख्यता है।' यह वाक्य पूर्णत: अशुद्ध है। यहाँ 'शुद्धोपयोग' की जगह 'शुभोपयोग' होना चाहिए।
गृहस्थ का जो मुख्य धर्म है वह अध्यात्म ग्रन्थ के अध्येताओं के लिए पुण्य बन्ध का कारण मात्र होकर रह गया है। उस पुण्य बन्ध को संसार का कारण दिखाकर भोले श्रावक को गृहस्थ धर्म से भी वंचित रहने का उपदेश दिया जा रहा है। इसी परमात्मप्रकाश की टीका में पृ. २३१ पर लिखते हैं कि- 'गृहस्थानामाहारदानादिकमेव परमो धर्मस्तेनैव सम्यक्त्वपूर्वेण परंपरया मोक्षं लभन्ते।' अर्थात्- गृहस्थों का परम धर्म आहार दान आदि है। इसी आहार दान आदि से सम्य वह गृहस्थ परम्परा से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसी तरह पृ. २४९ पर लिखा है कि जिस गृहस्थ ने दान, शील, पूजा, उपवास आदि रूप धर्म को सम्यग्दर्शन के साथ नहीं किया तो उसको मरकर नरक में गिरना पड़ेगा।
गृहस्थों का मन कषाय और इन्द्रियों से निरन्तर क्षुब्ध रहता है। इसी कारण गृहस्थों की मन:शुद्धि नहीं होती है। मन:शुद्धि के अभाव में तपोधन, मुनि की तरह शुद्धात्म भावना करने में समर्थ नहीं हैं। इसी ग्रन्थ के पृ. २६० पर यह भाव है- 'कषायेन्द्रियैः व्याकुलिक्रियते मनः, मनः शुद्धयभावे गृहस्थानां तपोधनवत् शुद्धात्मभावना कर्तुं नायातीति।'
आजकल कुछ अध्यात्मप्रेमियों के द्वारा यह कहा जाने लगा है कि आहार दान नहीं देना चाहिए। आहार तो शरीर का धर्म है। आहार दान से कोई धर्म नहीं होता है। आत्मा का भोजन तो ज्ञान है। इसलिए सबसे बड़ा दान ज्ञानदान है। आत्मा का ज्ञान का उपदेश ही मुख्य दान है। इस तरह आहार दान का निषेध करके पंचम काल से मुनि का अभाव करने का जिनका उद्देश्य है उन बन्धुओं की मुनि के प्रति कितनी तीव्रतम कषाय है, यह करणानुयोग के ग्रन्थ पढ़कर समझ लेनी चाहिए और इस कषाय का फल क्या होगा, यह परिणाम प्रथमानुयोग के ग्रन्थों को पढकर ही समझ आ सकता है।