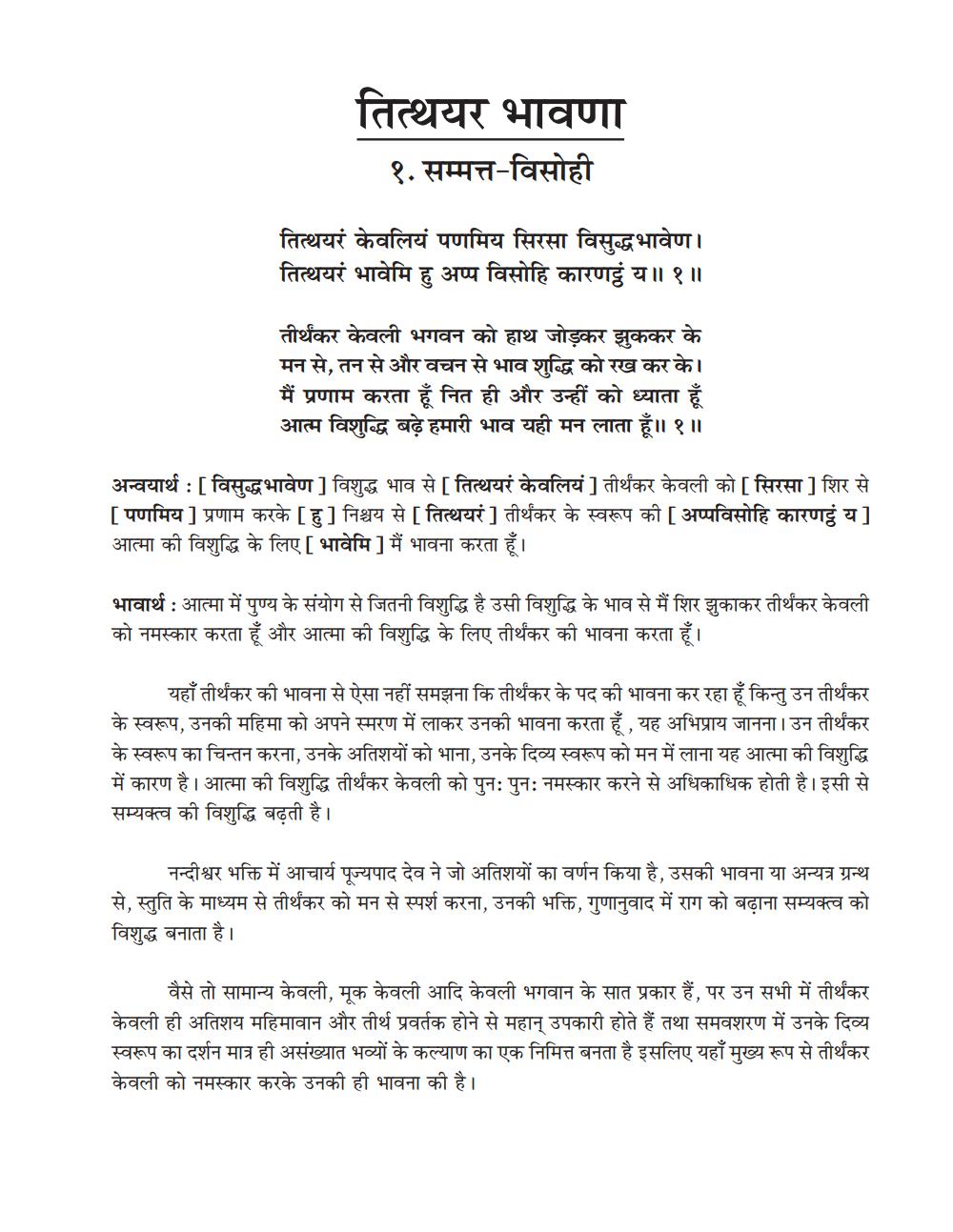________________
तित्थयर भावणा १. सम्मत्त-विसोही
तित्थयरं केवलियं पणमिय सिरसा विसुद्धभावेण। तित्थयरं भावेमि हु अप्प विसोहि कारणटुं य॥१॥
तीर्थंकर केवली भगवन को हाथ जोड़कर झुककर के मन से, तन से और वचन से भाव शुद्धि को रख कर के। मैं प्रणाम करता हूँ नित ही और उन्हीं को ध्याता हूँ आत्म विशुद्धि बढ़े हमारी भाव यही मन लाता हूँ॥१॥
अन्वयार्थ : [विसुद्धभावेण ] विशुद्ध भाव से [ तित्थयरं केवलियं] तीर्थंकर केवली को [ सिरसा ] शिर से [पणमिय] प्रणाम करके [ह] निश्चय से [तित्थयरं] तीर्थंकर के स्वरूप की [अप्पविसोहि कारणटुं य] आत्मा की विशुद्धि के लिए [ भावेमि ] मैं भावना करता हूँ।
भावार्थ : आत्मा में पुण्य के संयोग से जितनी विशुद्धि है उसी विशुद्धि के भाव से मैं शिर झुकाकर तीर्थंकर केवली को नमस्कार करता हूँ और आत्मा की विशुद्धि के लिए तीर्थंकर की भावना करता हूँ।
यहाँ तीर्थंकर की भावना से ऐसा नहीं समझना कि तीर्थंकर के पद की भावना कर रहा हूँ किन्तु उन तीर्थंकर के स्वरूप, उनकी महिमा को अपने स्मरण में लाकर उनकी भावना करता हूँ , यह अभिप्राय जानना। उन तीर्थंकर के स्वरूप का चिन्तन करना, उनके अतिशयों को भाना, उनके दिव्य स्वरूप को मन में लाना यह आत्मा की विशुद्धि में कारण है। आत्मा की विशुद्धि तीर्थंकर केवली को पुनः पुनः नमस्कार करने से अधिकाधिक होती है। इसी से सम्यक्त्व की विशुद्धि बढ़ती है।
नन्दीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्यपाद देव ने जो अतिशयों का वर्णन किया है, उसकी भावना या अन्यत्र ग्रन्थ से, स्तुति के माध्यम से तीर्थंकर को मन से स्पर्श करना, उनकी भक्ति, गुणानुवाद में राग को बढ़ाना सम्यक्त्व को विशुद्ध बनाता है।
वैसे तो सामान्य केवली, मूक केवली आदि केवली भगवान के सात प्रकार हैं, पर उन सभी में तीर्थंकर केवली ही अतिशय महिमावान और तीर्थ प्रवर्तक होने से महान् उपकारी होते हैं तथा समवशरण में उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन मात्र ही असंख्यात भव्यों के कल्याण का एक निमित्त बनता है इसलिए यहाँ मुख्य रूप से तीर्थंकर केवली को नमस्कार करके उनकी ही भावना की है।