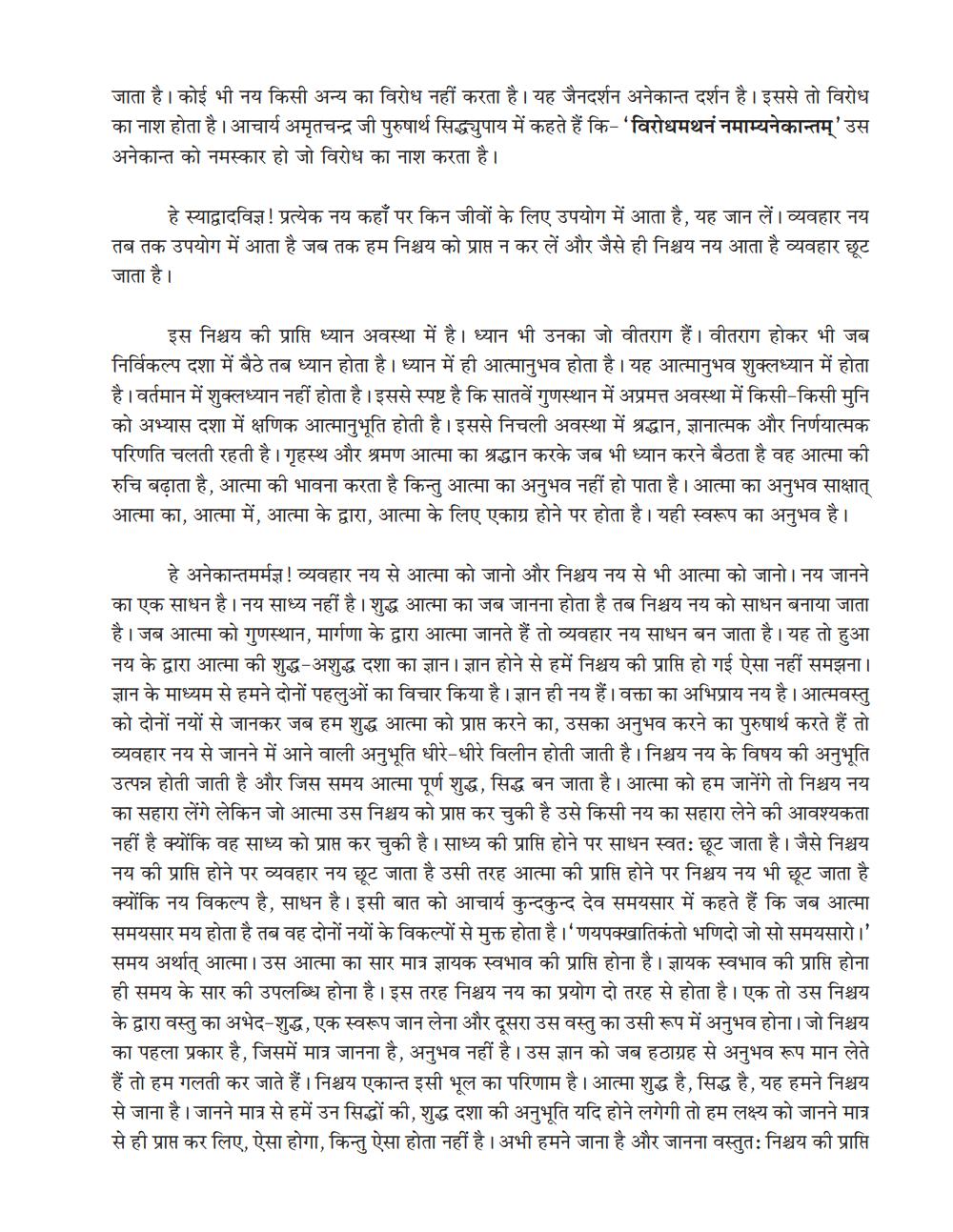________________
जाता है। कोई भी नय किसी अन्य का विरोध नहीं करता है। यह जैनदर्शन अनेकान्त दर्शन है। इससे तो विरोध का नाश होता है। आचार्य अमृतचन्द्र जी पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में कहते हैं कि- 'विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्' उस अनेकान्त को नमस्कार हो जो विरोध का नाश करता है।
हे स्याद्वादविज्ञ! प्रत्येक नय कहाँ पर किन जीवों के लिए उपयोग में आता है, यह जान लें। व्यवहार नय तब तक उपयोग में आता है जब तक हम निश्चय को प्राप्त न कर लें और जैसे ही निश्चय नय आता है व्यवहार छुट जाता है।
इस निश्चय की प्राप्ति ध्यान अवस्था में है। ध्यान भी उनका जो वीतराग हैं। वीतराग होकर भी जब निर्विकल्प दशा में बैठे तब ध्यान होता है। ध्यान में ही आत्मानुभव होता है। यह आत्मानुभव शुक्लध्यान में होता है। वर्तमान में शुक्लध्यान नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि सातवें गुणस्थान में अप्रमत्त अवस्था में किसी-किसी मुनि को अभ्यास दशा में क्षणिक आत्मानुभूति होती है। इससे निचली अवस्था में श्रद्धान, ज्ञानात्मक और निर्णयात्मक परिणति चलती रहती है। गृहस्थ और श्रमण आत्मा का श्रद्धान करके जब भी ध्यान करने बैठता है वह आत्मा की रुचि बढ़ाता है, आत्मा की भावना करता है किन्तु आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता है। आत्मा का अनुभव साक्षात् आत्मा का, आत्मा में, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए एकाग्र होने पर होता है। यही स्वरूप का अनुभव है।
हे अनेकान्तमर्मज्ञ! व्यवहार नय से आत्मा को जानो और निश्चय नय से भी आत्मा को जानो। नय जानने का एक साधन है। नय साध्य नहीं है। शुद्ध आत्मा का जब जानना होता है तब निश्चय नय को साधन बनाया जाता है। जब आत्मा को गुणस्थान, मार्गणा के द्वारा आत्मा जानते हैं तो व्यवहार नय साधन बन जाता है। यह तो हुआ नय के द्वारा आत्मा की शुद्ध-अशुद्ध दशा का ज्ञान । ज्ञान होने से हमें निश्चय की प्राप्ति हो गई ऐसा नहीं समझना। ज्ञान के माध्यम से हमने दोनों पहलुओं का विचार किया है। ज्ञान ही नय हैं। वक्ता का अभिप्राय नय है। आत्मवस्तु को दोनों नयों से जानकर जब हम शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का, उसका अनुभव करने का पुरुषार्थ करते हैं तो व्यवहार नय से जानने में आने वाली अनुभूति धीरे-धीरे विलीन होती जाती है। निश्चय नय के विषय की अनुभूति उत्पन्न होती जाती है और जिस समय आत्मा पूर्ण शुद्ध, सिद्ध बन जाता है। आत्मा को हम जानेंगे तो निश्चय नय का सहारा लेंगे लेकिन जो आत्मा उस निश्चय को प्राप्त कर चुकी है उसे किसी नय का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह साध्य को प्राप्त कर चुकी है। साध्य की प्राप्ति होने पर साधन स्वतः छूट जाता है। जैसे निश्चय नय की प्राप्ति होने पर व्यवहार नय छूट जाता है उसी तरह आत्मा की प्राप्ति होने पर निश्चय नय भी छूट जाता है क्योंकि नय विकल्प है, साधन है। इसी बात को आचार्य कुन्दकुन्द देव समयसार में कहते हैं कि जब आत्मा समयसार मय होता है तब वह दोनों नयों के विकल्पों से मुक्त होता है। ‘णयपक्खातिकतो भणिदो जो सो समयसारो।' समय अर्थात् आत्मा। उस आत्मा का सार मात्र ज्ञायक स्वभाव की प्राप्ति होना है। ज्ञायक स्वभाव की प्राप्ति होना ही समय के सार की उपलब्धि होना है। इस तरह निश्चय नय का प्रयोग दो तरह से होता है। एक तो उस निश्चय के द्वारा वस्तु का अभेद-शुद्ध, एक स्वरूप जान लेना और दूसरा उस वस्तु का उसी रूप में अनुभव होना। जो निश्चय का पहला प्रकार है, जिसमें मात्र जानना है, अनुभव नहीं है। उस ज्ञान को जब हठाग्रह से अनुभव रूप मान लेते हैं तो हम गलती कर जाते हैं। निश्चय एकान्त इसी भूल का परिणाम है। आत्मा शुद्ध है, सिद्ध है, यह हमने निश्चय से जाना है। जानने मात्र से हमें उन सिद्धों की, शुद्ध दशा की अनुभूति यदि होने लगेगी तो हम लक्ष्य को जानने मात्र से ही प्राप्त कर लिए, ऐसा होगा, किन्तु ऐसा होता नहीं है। अभी हमने जाना है और जानना वस्तुत: निश्चय की प्राप्ति