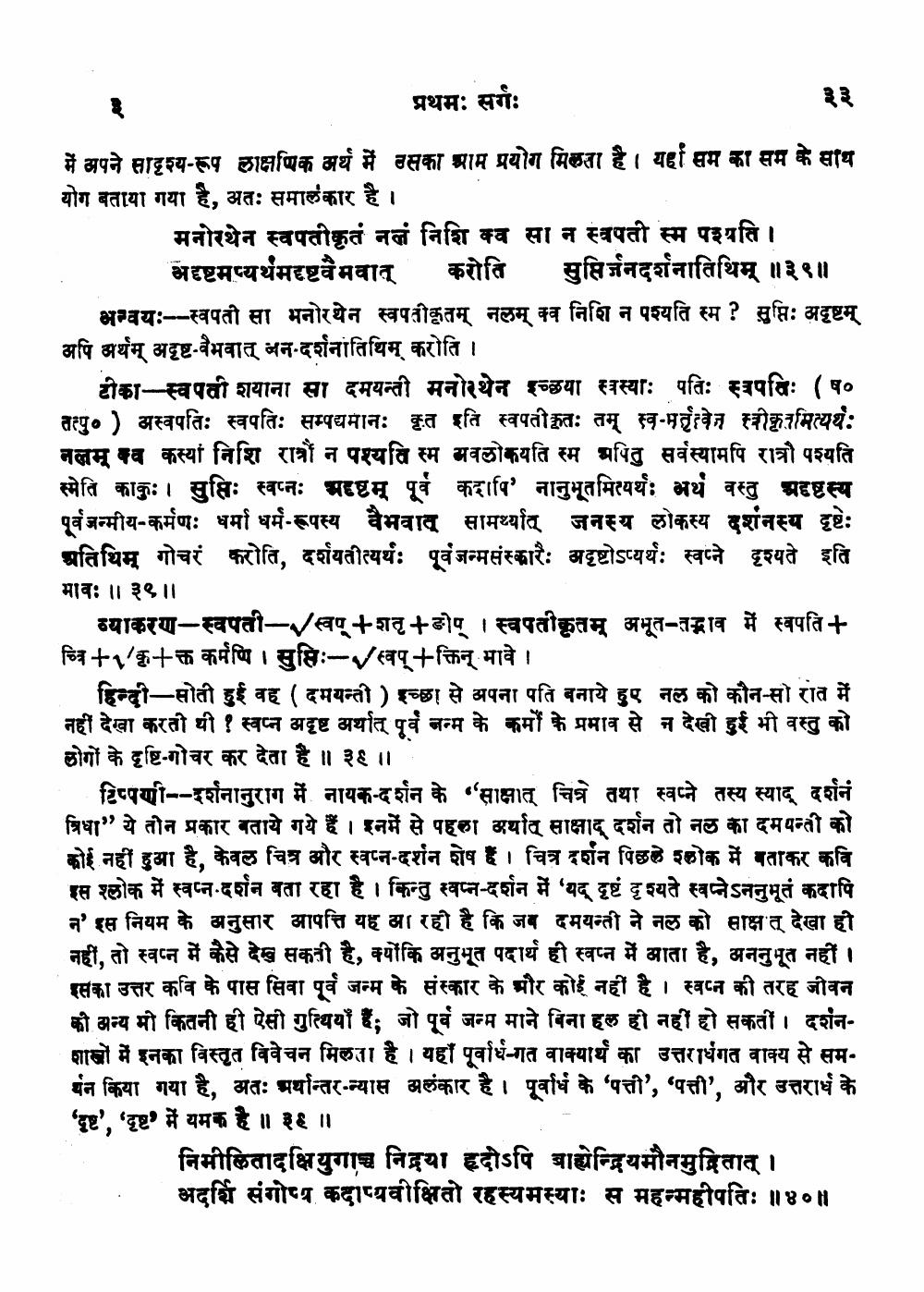________________ प्रथमः सर्गः में अपने सादृश्य-रूप लाक्षणिक अर्थ में उसका नाम प्रयोग मिलता है। यहां सम का सम के साथ योग बताया गया है, अतः समालंकार है। मनोरथेन स्वपतीकृतं नलं निशि क्व सा न स्वपती स्म पश्यति / अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवैमवात् करोति सुप्तिर्जनदर्शनातिथिम् // 39 // भन्वयः--स्वपती सा मनोरथेन स्वपतीकृतम् नलम् क्व निशि न पश्यति स्म ? सुप्तिः अदृष्टम् अपि अर्थम् अदृष्ट-वैभवात् जन-दर्शनातिथिम् करोति / टीका-स्वपती शयाना सा दमयन्ती मनोरथेन इच्छया स्वस्याः पतिः स्वपतिः (10 तत्पु०) अस्वपतिः स्वपतिः सम्पद्यमानः कृत इति स्वपतीकृतः तम् स्व-मर्तृत्वेन स्वीकृतमित्यर्थः नलम् क्व कस्यां निशि रात्रौं न पश्यति स्म अवलोकयति स्म अपितु सर्वस्यामपि रात्रौ पश्यति स्मेति काकुः। सुप्तिः स्वप्नः अदृष्टम् पूर्व कदापि नानुभूतमित्यर्थः अर्थ वस्तु अदृष्टस्य पूर्वजन्मीय-कर्मणः धर्मा धर्म-रूपस्य वैभवात् सामर्थ्यात् जनस्य लोकस्य दर्शनस्य दृष्टः अतिथिम गोचरं करोति, दर्शयतीत्यर्थः पूर्वजन्मसंस्कारैः अदृष्टोऽप्यर्थः स्वप्ने दृश्यते इति मावः / / 39 // व्याकरण-स्वपती- स्वप् +शत+डोप / स्वपतीकृतम् अभूत-तद्भाव में स्वपति+ चि+ +क्त कर्मणि / सुप्तिः- स्वप्+क्तिन् मावे / हिन्दी सोती हुई वह ( दमयन्ती ) इच्छा से अपना पति बनाये हुए नल को कौन-सो रात में नहीं देखा करती थी ? स्वप्न अदृष्ट अर्थात् पूर्व नन्म के कर्मों के प्रमाव से न देखी हुई भी वस्तु को लोगों के दृष्टि-गोचर कर देता है // 36 / / टिप्पणी--दर्शनानुराग में नायक-दर्शन के "साक्षात् चित्रे तथा स्वप्ने तस्य स्याद् दर्शनं विधा" ये तीन प्रकार बताये गये हैं। इनमें से पहला अर्थात् साक्षाद् दर्शन तो नल का दमयन्ती को कोई नहीं हुआ है, केवल चित्र और स्वप्न-दर्शन शेष है। चित्र दर्शन पिछले लोक में बताकर कवि इस श्लोक में स्वप्न दर्शन बता रहा है / किन्तु स्वप्न-दर्शन में 'यद् दृष्टं दृश्यते स्वप्नेऽननुभूतं कदापि न' इस नियम के अनुसार आपत्ति यह आ रही है कि जब दमयन्ती ने नल को साक्षात् देखा ही नहीं, तो स्वप्न में कैसे देख सकती है, क्योंकि अनुभूत पदार्थ ही स्वप्न में आता है, अननुभूत नहीं। इसका उत्तर कवि के पास सिवा पूर्व जन्म के संस्कार के और कोई नहीं है / स्वप्न की तरह जीवन की अन्य मी कितनी ही ऐसी गुत्थियाँ हैं, जो पूर्व जन्म माने विना हल ही नहीं हो सकतीं। दर्शनशाखों में इनका विस्तृत विवेचन मिलता है / यहाँ पूर्वार्ध-गत वाक्यार्थ का उत्तरार्धगत वाक्य से समयंन किया गया है, अतः अर्थान्तर-न्यास अलंकार है। पूर्वार्ध के 'पत्ती', 'पत्ती', और उत्तरार्ध के 'दृष्ट', 'दृष्ट में यमक है // 39 // निमीलितादक्षियुगाच निद्रया हृदोऽपि बाह्येन्द्रियमौनमुद्रितात् / . अदर्शि संगोप्य कदाप्यवीक्षितो रहस्यमस्याः स महन्महीपतिः // 40 //