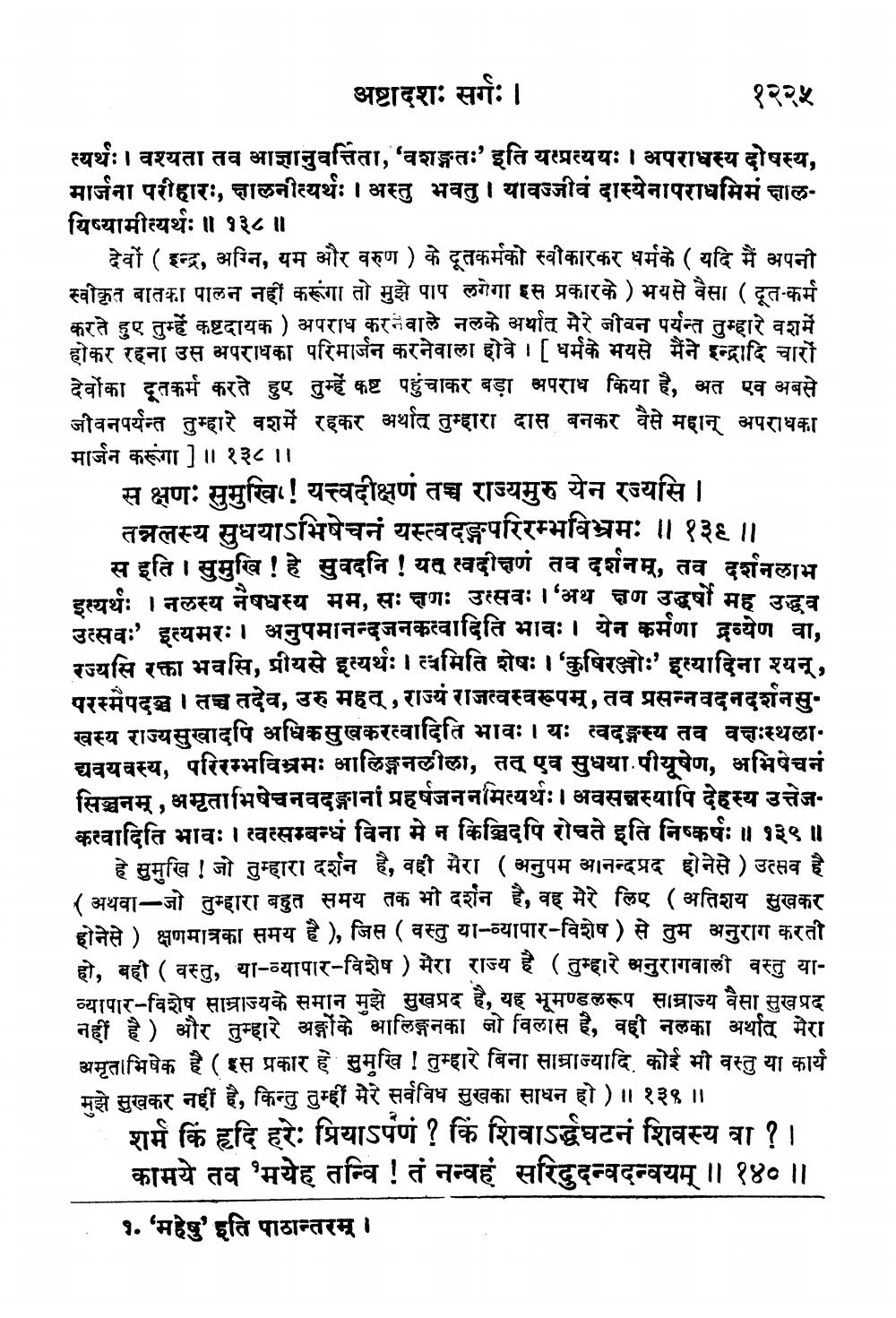________________ अष्टादशः सर्गः। 1225 त्यर्थः / वश्यता तव आज्ञानुवर्तिता, 'वशङ्गतः' इति यस्प्रत्ययः / अपराधस्य दोषस्य, मार्जना परीहारः, क्षालनीत्यर्थः / अस्तु भवतु / यावज्जीवं दास्येनापराधमिमं क्षाल. यिष्यामीत्यर्थः // 138 // देवों ( इन्द्र, अग्नि, यम और वरुण ) के दूतकर्मको स्वीकारकर धर्मके ( यदि मैं अपनी स्वीकृत बातका पालन नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा इस प्रकारके) भयसे वैसा ( दूत-कर्म करते हुए तुम्हें कष्टदायक ) अपराध करनेवाले नलके अर्थात् मेरे जीवन पर्यन्त तम्हारे वश में होकर रहना उस अपराधका परिमार्जन करनेवाला होवे / [ धर्मके मयसे मैंने इन्द्रादि चारों देवोंका दूतकर्म करते हुए तुम्हें कष्ट पहुंचाकर बड़ा अपराध किया है, अत एव अबसे जीवनपर्यन्त तुम्हारे वशमें रहकर अर्थात् तुम्हारा दास बनकर वैसे महान् अपराधका मार्जन करूंगा] // 138 / / स क्षणः सुमुखिः! यत्त्वदीक्षणं तच्च राज्यमुरु येन रज्यसि | तन्नलस्य सुधयाऽभिषेचनं यस्त्वदङ्गपरिरम्भविभ्रमः / / 136 / / स इति / सुमुखि ! हे सुवदनि ! यत् स्वदीक्षणं तव दर्शनम्, तव दर्शनलाभ इत्यर्थः / नलस्य नेषधस्य मम, सः क्षणः उत्सवः / अथ क्षण उद्धर्षो मह अनार उत्सवः' इत्यमरः। अनुपमानन्दजनकत्वादिति भावः। येन कर्मणा द्रव्येण वा, रज्यसि रक्ता भवसि, प्रीयसे इत्यर्थः / त्वमिति शेषः / 'कुषिरोः' इत्यादिना श्यन, परस्मैपदश्च / तच्च तदेव, उरु महत् , राज्यं राजत्वस्वरूपम्, तव प्रसन्नवदनदर्शनसु. खस्य राज्यसुखादपि अधिक सुखकरत्वादिति भावः / यः त्वदङ्गस्य तव वक्षःस्थला. द्यवयवस्य, परिरम्भविभ्रमः आलिङ्गनलीला, तत् एव सुधया.पीयूषेण, अभिषेचनं सिजनम् , अमृताभिषेचनवदङ्गानां प्रहर्षजननमित्यर्थः। अवसन्नस्यापि देहस्य उत्तेजकत्वादिति भावः / त्वत्सम्बन्धं विना मे न किञ्चिदपि रोचते इति निष्कर्षः॥ 139 // हे सुमुखि ! जो तुम्हारा दर्शन है, वही मैरा ( अनुपम आनन्दप्रद होनेसे ) उत्सव है ( अथवा-जो तुम्हारा बहुत समय तक भी दर्शन है, वह मेरे लिए (अतिशय सुखकर होनेसे ) क्षणमात्रका समय है ), जिस ( वस्तु या-व्यापार-विशेष ) से तुम अनुराग करती हो, बही ( वस्तु, या-व्यापार-विशेष ) मेरा राज्य है ( तुम्हारे अनुरागवाली वस्तु याव्यापार-विशेष साम्राज्यके समान मुझे सुखप्रद है, यह भूमण्डलरूप साम्राज्य वैसा सुखप्रद नहीं है) और तुम्हारे अङ्गोंके आलिङ्गनका जो विलास है, वही नलका अर्थात् मेरा अमृताभिषेक है (इस प्रकार हे सुमुखि ! तुम्हारे बिना साम्राज्यादि कोई भी वस्तु या कार्य मझे सुखकर नहीं है, किन्तु तुम्हीं मेरे सर्वविध सुखका साधन हो ) // 139 / / शर्म किं हृदि हरेः प्रियाऽपणं ? किं शिवाऽर्द्धघटनं शिवस्य वा ? | कामये तव 'मयेह तन्वि ! तं नन्वहं सरिदुदन्वदन्वयम् // 140 // 1. 'महेषु' इति पाठान्तरम्।