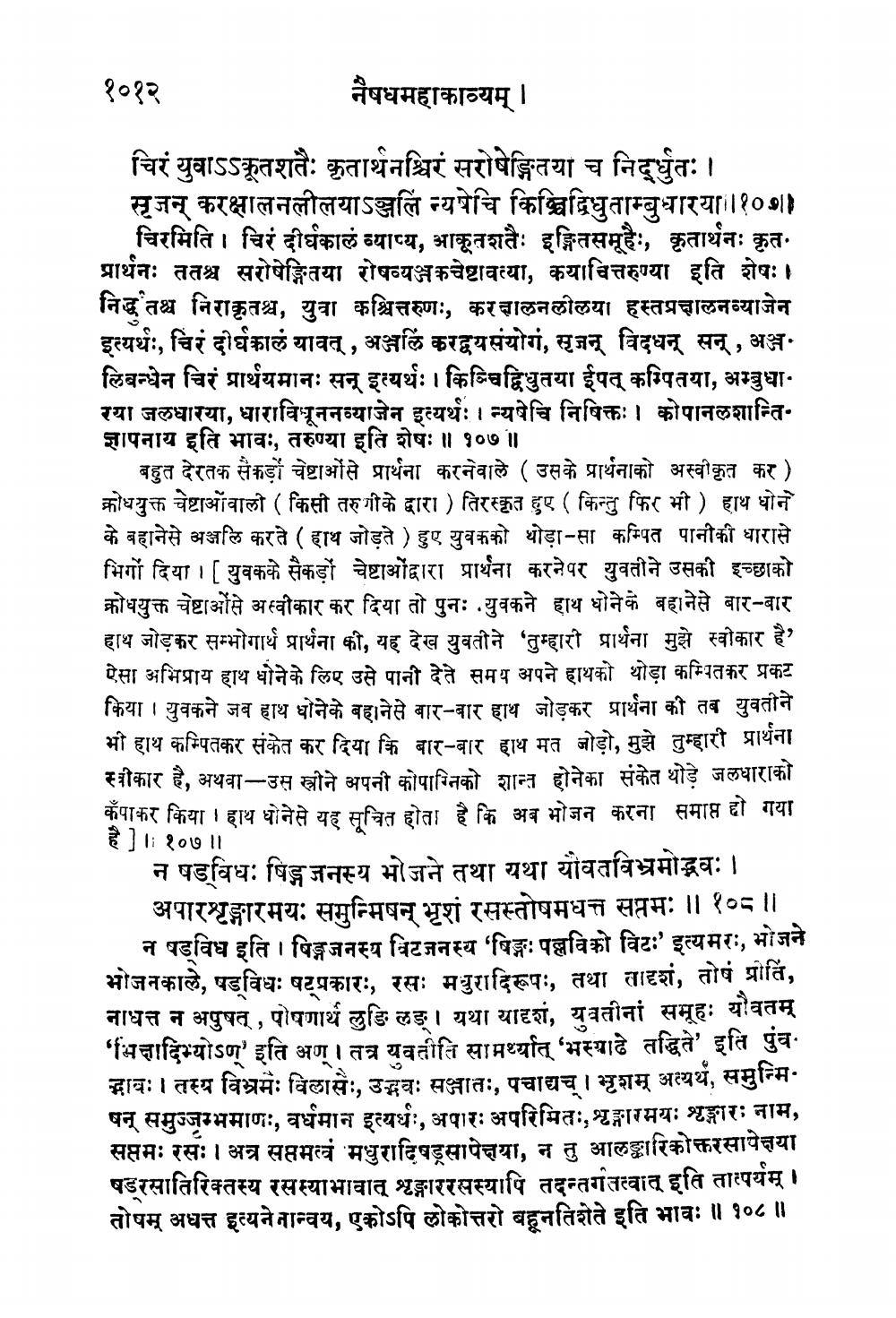________________ 1012 नैषधमहाकाव्यम् / चिरं युवाऽऽकूतशतैः कृतार्थनश्चिरं सरोषेङ्गितया च निर्बुतः। सृजन करक्षालनलीलयाऽञ्जलिं न्यषेचि किश्चिद्विधुताम्बुधारया।।१०७॥ चिरमिति। चिरं दीर्घकालं व्याप्य, आकूतशतैः इङ्गितसमूहैः, कृतार्थनः कृत. प्रार्थनः ततश्च सरोषेतिया रोषव्यञ्जकचेष्टावत्या, कयाचित्तरुण्या इति शेषः / निद्धतश्च निराकृतश्च, युवा कश्चित्तरुणः, करक्षालनलीलया हस्तप्रक्षालनव्याजेन इत्यर्थः, चिरं दीर्घकालं यावत् , अञ्जलिं करद्वयसंयोगं, सृजन् विदधन् सन् , अञ्ज. लिबन्धेन चिरं प्रार्थयमानः सन् इत्यर्थः / किञ्चिद्विधुतया ईपत् कम्पितया, अम्बुधा. रया जलधारया, धाराविधूननव्याजेन इत्यर्थः / न्यषेचि निषिक्तः। कोपानलशान्ति. ज्ञापनाय इति भावः, तरुण्या इति शेषः // 107 // बहुत देरतक सैकड़ों चेष्टाओंसे प्रार्थना करनेवाले ( उसके प्रार्थनाको अस्वीकृत कर ) क्रोधयुक्त चेष्टाओंवाली ( किसी तरु गीके द्वारा ) तिरस्कृत हुए ( किन्तु फिर भी ) हाथ धोने के बहानेसे अञ्जलि करते ( हाथ जोड़ते ) हुए युवकको थोड़ा-सा कम्पित पानीकी धारासे भिगों दिया। [युवकके सैकड़ों चेष्टाओंद्वारा प्रार्थना करने पर युवतीने उसकी इच्छाको क्रोधयुक्त चेष्टाओंसे अस्वीकार कर दिया तो पुनः .युवकने हाथ धोने के बहानेसे बार-बार हाथ जोड़कर सम्भोगार्थ प्रार्थना की, यह देख युवतीने 'तुम्हारी प्रार्थना मुझे स्वीकार है' ऐसा अभिप्राय हाथ धोने के लिए उसे पानी देते समय अपने हाथको थोड़ा कम्पितकर प्रकट किया / युवकने जब हाथ धोने के बहानेसे बार-बार हाथ जोड़कर प्रार्थना की तब युवतीने भी हाथ कम्पितकर संकेत कर दिया कि बार-बार हाथ मत जोड़ो, मुझे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है, अथवा-उस स्त्रीने अपनी कोपाग्निको शान्त होनेका संकेत थोड़े जलधाराको कपाकर किया / हाथ धोनेसे यह सूचित होता है कि अब भोजन करना समाप्त हो गया है ] || 107 // न षड्विधः षिगजनस्य भोजने तथा यथा यौवतविभ्रमोद्भवः / / अपारशृङ्गारमयः समुन्मिषन भृशं रसस्तोषमधत्त सप्तमः / / 108 / / / न षड्विध इति / पिङ्गजनस्य विटजनस्य 'षिङ्गः पल्लविको विटः' इत्यमरः, भोजने भोजनकाले, षड़विधः षटप्रकारः, रसः मधुरादिरूपः, तथा तादृशं, तोषं प्रीति, नाधत्त न अपुषत् , पोषणार्थ लुडि लङ। यथा यादृशं, यवतीनां समूहः यौवतम् 'मिक्षादिभ्योऽण' इति अण / तत्र यवतीति सामर्थ्यात् 'भस्थाढे तद्धिते' इति पुव द्भावः / तस्य विभ्रमः विलासैः, उद्भवः सञ्जातः, पचाद्यच / भृशम् अत्यर्थ, समुन्मि. षन् समुज्जम्भमाणः, वर्धमान इत्यर्थः, अपारः अपरिमितः,शृङ्गारमयः शृङ्गारा नाम, सप्तमः रसः / अत्र सप्तमत्वं मधुरादिषड्सापेक्षया, न तु आलङ्कारिकोक्तरसापेक्षया षडरसातिरिक्तस्य रसस्याभावात् शृङ्गाररसस्यापि तदन्तर्गतत्वात् इति तात्पर्यम् / तोषम् अधत्त इत्यने नान्वय, एकोऽपि लोकोत्तरो बहूनतिशेते इति भावः // 108 //