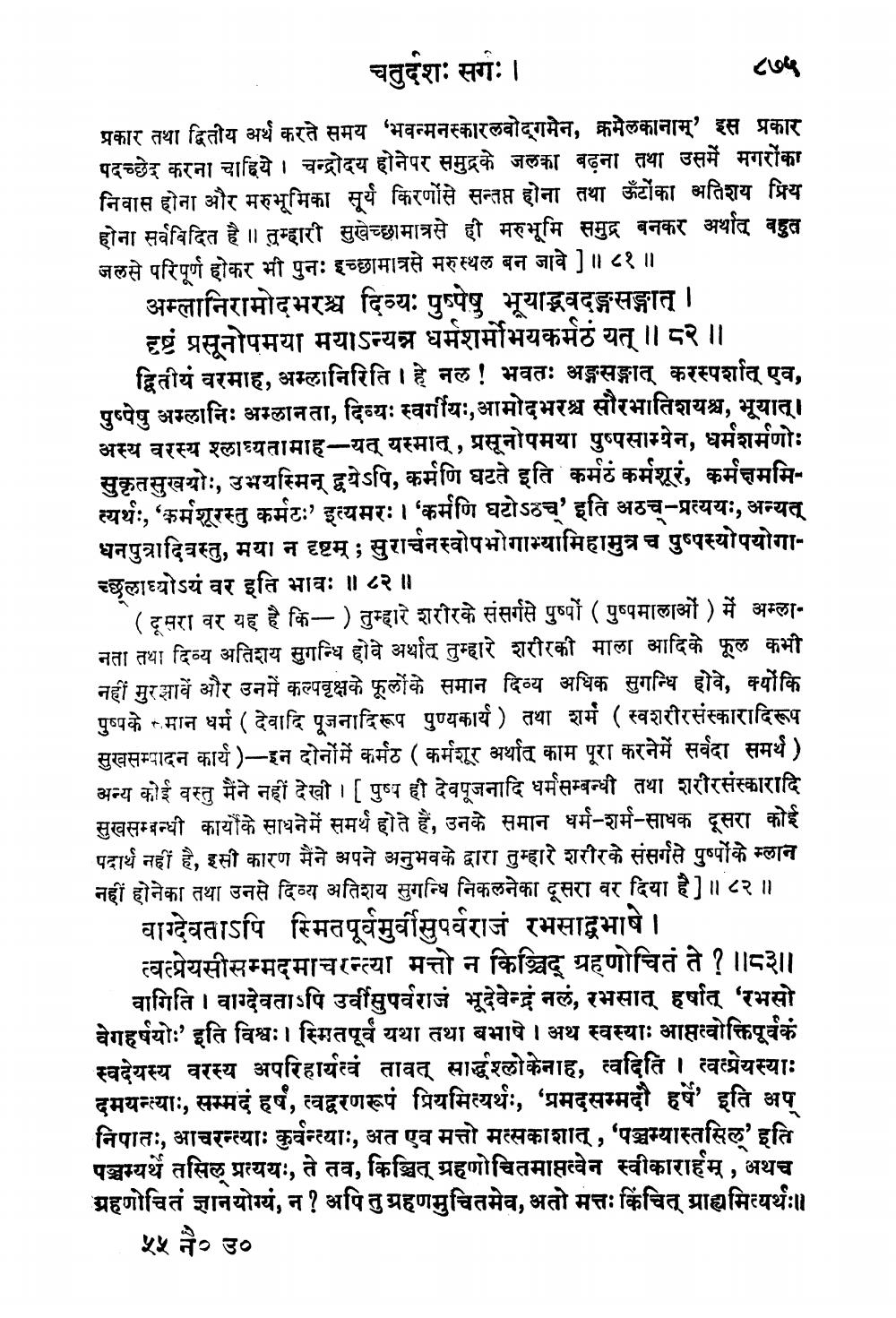________________ चतुर्दशः सर्गः। 875 प्रकार तथा द्वितीय अर्थ करते समय 'भवन्मनस्कारलवोद्गमेन, क्रमेलकानाम्' इस प्रकार पदच्छेद करना चाहिये / चन्द्रोदय होनेपर समुद्रके जलका बढ़ना तथा उसमें मगरोंका निवास होना और मरुभूमिका सूर्य किरणोंसे सन्तप्त होना तथा ऊँटोंका अतिशय प्रिय होना सर्वविदित है / तुम्हारी सुखेच्छामात्रसे ही मरुभूमि समुद्र बनकर अर्थात् बहुत जलसे परिपूर्ण होकर भी पुनः इच्छामात्रसे मरुस्थल बन जावे ] // 81 // अम्लानिरामोदभरश्च दिव्यः पुष्पेषु भूयाद्भवदङ्गसङ्गात् / दृष्टं प्रसूनोपमया मयाऽन्यन्न धमेशर्मोभयकमेठं यत् / / 2 / / द्वितीयं वरमाह, अम्लानिरिति / हे नल! भवतः अङ्गसङ्गात् करस्पर्शात् एव, पुष्पेषु अम्लानिः अम्लानता, दिव्यः स्वर्गीयः,आमोदभरश्च सौरभातिशयश्च, भूयात्। अस्य वरस्य श्लाध्यतामाह-यत् यस्मात् , प्रसूनोपमया पुष्पसाम्येन, धर्मशर्मणोः सुकृतसुखयोः, उभयस्मिन् द्वयेऽपि, कर्मणि घटते इति कर्मठं कर्मशूरं, कर्मक्षममित्यर्थः, 'कर्मशूरस्तु कर्मटः' इत्यमरः / 'कर्मणि घटोऽठच' इति अठच-प्रत्ययः, अन्यत् धनपुत्रादिवस्तु, मया न दृष्टम् ; सुरार्चनस्वोपभोगाभ्यामिहामुत्र च पुष्पस्योपयोगाच्छलाध्योऽयं वर इति भावः // 82 // (दूसरा वर यह है कि-) तुम्हारे शरीरके संसर्गसे पुष्पों ( पुष्पमालाओं ) में अम्लानता तथा दिव्य अतिशय सुगन्धि होवे अर्थात् तुम्हारे शरीरकी माला आदिके फूल कभी नहीं मुरझावें और उनमें कल्पवृक्षके फूलों के समान दिव्य अधिक सुगन्धि होवे, क्योंकि पुष्पके + मान धर्म ( देवादि पूजनादिरूप पुण्यकार्य) तथा शर्म (स्वशरीरसंस्कारादिरूप सुखसम्पादन कार्य)-इन दोनों में कर्मठ ( कर्मशूर अर्थात् काम पूरा करनेमें सर्वदा समर्थ ) अन्य कोई वस्तु मैंने नहीं देखी। [ पुष्य ही देवपूजनादि धर्मसम्बन्धी तथा शरीरसंस्कारादि सुखसम्बन्धी कार्यों के साधने में समर्थ होते हैं, उनके समान धर्म-शर्म-साधक दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, इसी कारण मैंने अपने अनुभवके द्वारा तुम्हारे शरीरके संसर्गसे पुष्पों के म्लान नहीं होनेका तथा उनसे दिव्य अतिशय सुगन्धि निकलनेका दूसरा वर दिया है ] // 82 // वाग्देवताऽपि स्मितपूर्वमुर्वीसुपर्वराजं रभसाद्वभाषे / त्वत्प्रेयसीसम्मदमाचरन्त्या मत्तो न किञ्चिद ग्रहणोचितं ते ? // 23 // वागिति / वाग्देवताऽपि उर्वीसुपर्वराजं भूदेवेन्द्रं नलं, रभसात् हर्षात् 'रभसो वेगहर्षयोः' इति विश्वः। स्मितपूर्वं यथा तथा बभाषे / अथ स्वस्याः आप्तत्वोक्तिपूर्वकं स्वदेयस्य वरस्य अपरिहार्यत्वं तावत् सार्द्धश्लोकेनाह, त्वदिति / त्वत्प्रेयस्याः दमयन्त्याः , सम्मदं हर्ष, त्वद्वरणरूपं प्रियमित्यर्थः, 'प्रमदसम्मदी हर्षे' इति अप् निपातः, आचरन्त्याः कुर्वन्त्याः, अत एव मत्तो मत्सकाशात् , 'पञ्चम्यास्तसिल' इति पञ्चम्यर्थे तसिल प्रत्ययः, ते तव, किञ्चित् ग्रहणोचितमाप्तत्वेन स्वीकाराहम् , अथच ग्रहणोचितं ज्ञानयोग्यं, न ? अपि तु ग्रहणमुचितमेव, अतो मत्तः किंचित् ग्राह्यमित्यर्थः॥ 55 नै० उ०