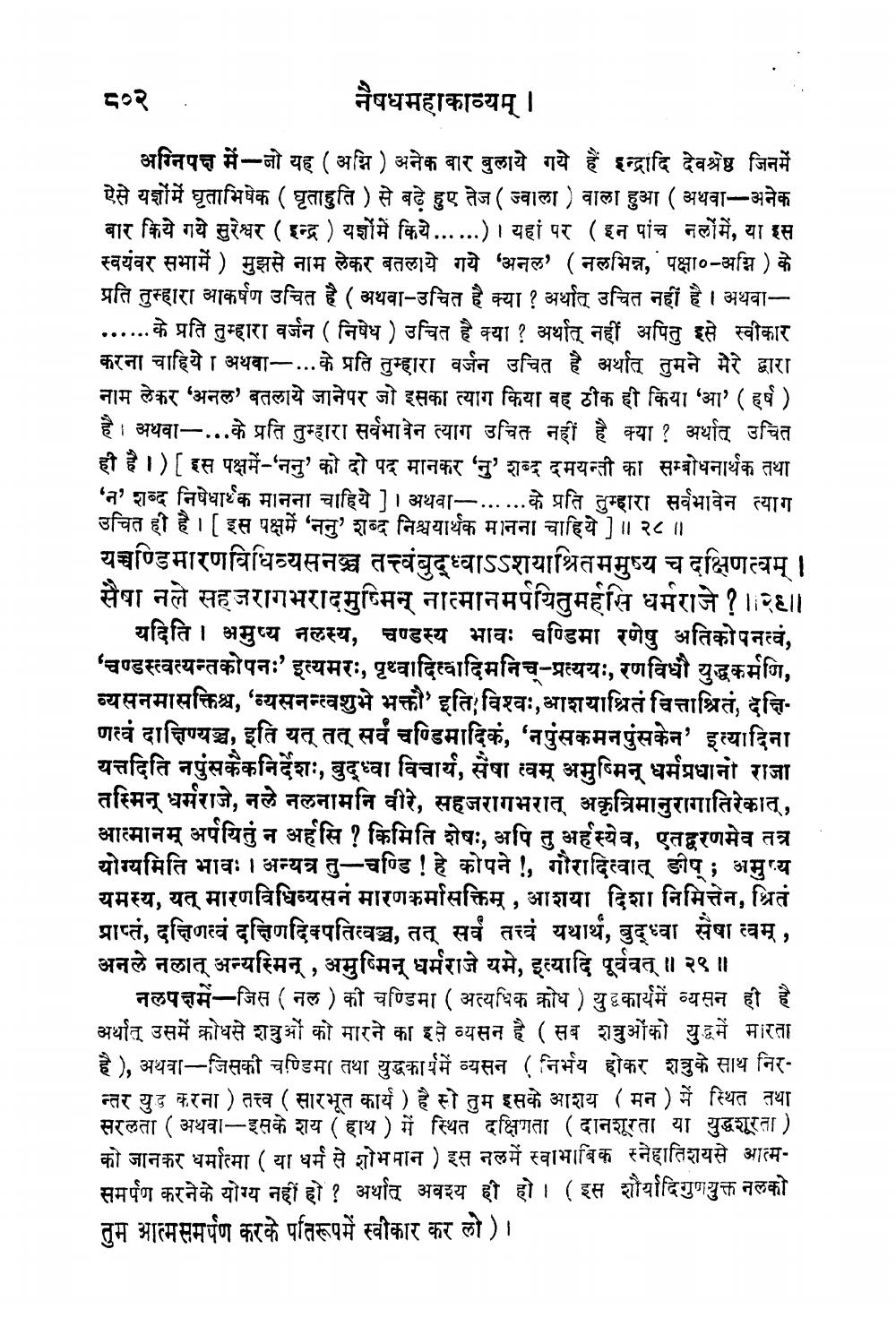________________ 802 . नैषधमहाकाव्यम् / अग्निपक्ष में जो यह ( अग्नि ) अनेक बार बुलाये गये हैं इन्द्रादि देवश्रेष्ठ जिनमें ऐसे यज्ञोंमें घृताभिषेक (घृताहुति ) से बढ़े हुए तेज ( ज्वाला) वाला हुआ ( अथवा-अनेक बार किये गये सुरेश्वर (इन्द्र ) यज्ञोंमें किये......)। यहां पर ( इन पांच नलों में, या इस स्वयंवर सभामें) मुझसे नाम लेकर बतलाये गये 'अनल' (नलभिन्न, पक्षा०-अग्नि ) के प्रति तुम्हारा आकर्षण उचित है ( अथवा-उचित है क्या ? अर्थात् उचित नहीं है / अथवा...... के प्रति तुम्हारा वर्जन ( निषेध ) उचित है क्या ? अर्थात् नहीं अपितु इसे स्वीकार करना चाहिये / अथवा-...के प्रति तुम्हारा वर्जन उचित है अर्थात् तुमने मेरे द्वारा नाम लेकर 'अनल' बतलाये जानेपर जो इसका त्याग किया वह ठीक ही किया 'आ' ( हर्ष ) है। अथवा-...के प्रति तुम्हारा सर्वभावेन त्याग उचित नहीं है क्या ? अर्थात् उचित ही है। ) [ इस पक्षमें-'ननु' को दो पद मानकर 'नु' शब्द दमयन्ती का सम्बोधनार्थक तथा 'न' शब्द निषेधार्थक मानना चाहिये ] / अथवा-...... के प्रति तुम्हारा सर्वभावेन त्याग उचित ही है / [ इस पक्षमें 'ननु' शब्द निश्चयार्थक मानना चाहिये ] // 28 // यच्चण्डिमारणविधिव्यसनञ्च तत्त्वंबुद्ध्वाऽऽशयाश्रितममुष्य च दक्षिणत्वम् / सैषा नले सहजरागभरादमुष्मिन् नात्मानमर्पयितुमर्हसि धर्मराजे ? / 26 / / ___यदिति / अमुष्य नलस्य, चण्डस्य भावः चण्डिमा रणेषु अतिको पनत्वं, 'चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः' इत्यमरः, पृथ्वादित्वादिमनिच-प्रत्ययः, रणविधौ युद्धकर्मणि, व्यसनमासक्तिश्च, 'व्यसनन्त्वशुभे भक्तौ' इति विश्वः,आशयाश्रितं चित्ताश्रितं, दक्षिणत्वं दाक्षिण्यञ्च, इति यत् तत् सर्व चण्डिमादिकं, 'नपुंसकमनपुंसकेन' इत्यादिना यत्तदिति नपुंसकैकनिर्देशः, बुद्ध्वा विचार्य, सैषा स्वम् अमुष्मिन् धर्मप्रधानी राजा तस्मिन् धर्मराजे, नले नलनामनि वीरे, सहजरागभरात् अकृत्रिमानुरागातिरेकात्, आत्मानम् अर्पयितुं न अर्हसि ? किमिति शेषः, अपि तु अर्हस्येव, एतद्वरणमेव तत्र योग्यमिति भावः / अन्यत्र तु-चण्डि ! हे कोपने !, गौरादित्वात् ङीप ; अमुग्य यमस्य, यत् मारणविधिव्यसनं मारणकर्मासक्तिम् , आशया दिशा निमित्तेन, श्रितं प्राप्तं, दक्षिणत्वं दक्षिणदिक्पतित्वञ्च, तत् सर्वं तत्त्वं यथार्थ, बुद्ध्वा सैषा त्वम् , अनले नलात् अन्यस्मिन् , अमुग्मिन् धर्मराजे यमे, इत्यादि पूर्ववत् // 29 // ___ नलपक्षमें-जिस ( नल ) की चण्डिमा ( अत्यधिक क्रोध ) युद्ध कार्यमें व्यसन ही है अर्थात् उसमें क्रोधसे शत्रुओं को मारने का इसे व्यसन है ( सब शत्रुओंको युद्ध में मारता है), अथवा-जिसकी चण्डिमा तथा युद्धकार्यमें व्यसन (निर्भय होकर शत्रुके साथ निरन्तर युद्ध करना ) तत्त्व ( सारभूत कार्य ) है सो तुम इसके आशय (मन) में स्थित तथा सरलता ( अथवा-इसके शय (हाथ ) में स्थित दक्षिगता (दानशूरता या युद्धशूरता) को जानकर धर्मात्मा ( या धर्म से शोभमान ) इस नल में स्वाभाबिक स्नेहातिशयसे आत्मसमर्पण करने के योग्य नहीं हो ? अर्थात् अवश्य ही हो। ( इस शौर्यादिगुणयुक्त नलको तुम आत्मसमर्पण करके पतिरूपमें स्वीकार कर लो)।