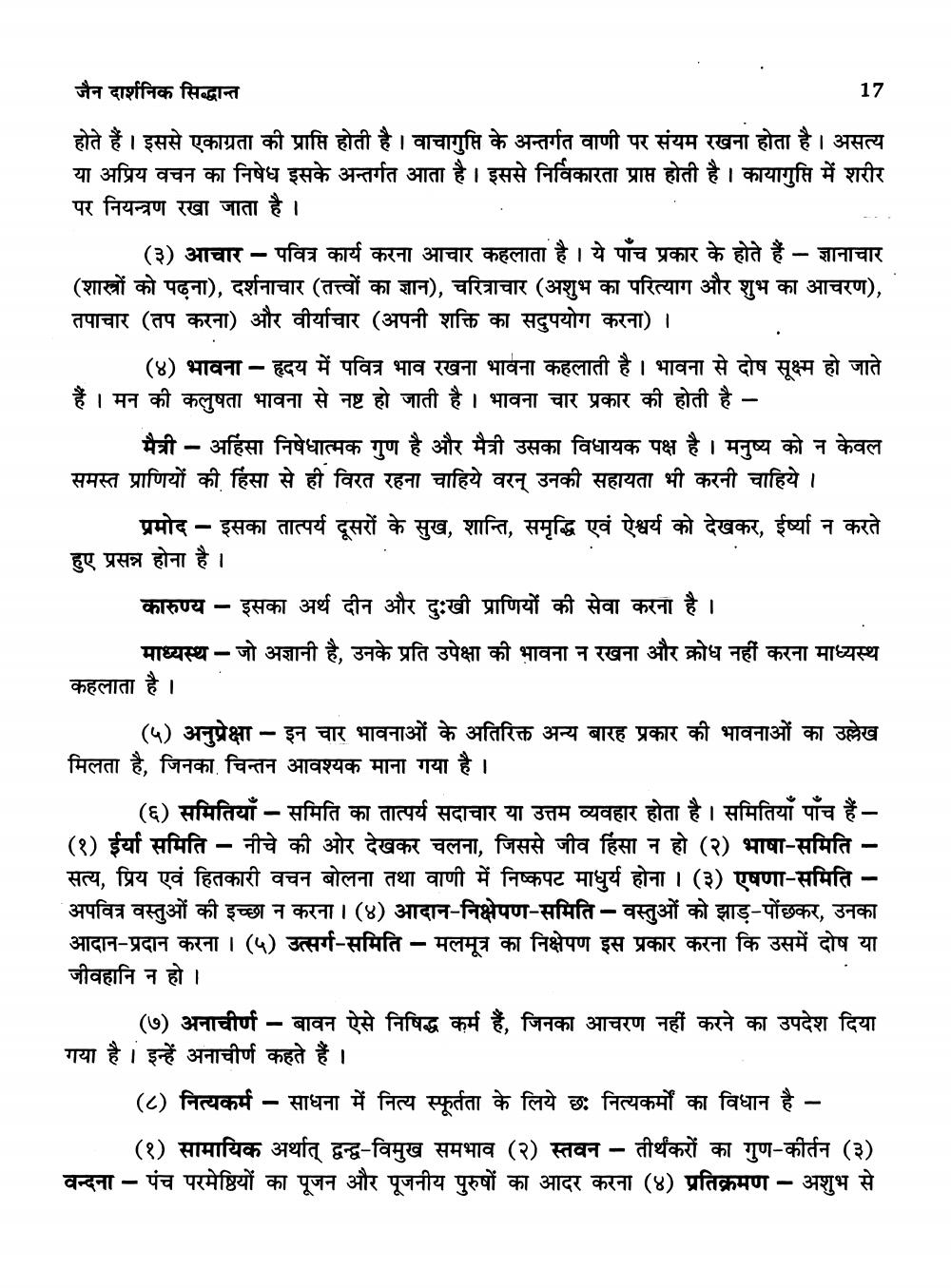________________ ___ 17 जैन दार्शनिक सिद्धान्त होते हैं। इससे एकाग्रता की प्राप्ति होती है। वाचागुप्ति के अन्तर्गत वाणी पर संयम रखना होता है। असत्य या अप्रिय वचन का निषेध इसके अन्तर्गत आता है। इससे निर्विकारता प्राप्त होती है। कायागुप्ति में शरीर पर नियन्त्रण रखा जाता है / (3) आचार - पवित्र कार्य करना आचार कहलाता है। ये पाँच प्रकार के होते हैं - ज्ञानाचार (शास्त्रों को पढ़ना), दर्शनाचार (तत्त्वों का ज्ञान), चरित्राचार (अशुभ का परित्याग और शुभ का आचरण), तपाचार (तप करना) और वीर्याचार (अपनी शक्ति का सदुपयोग करना)। (4) भावना - हृदय में पवित्र भाव रखना भावना कहलाती है। भावना से दोष सूक्ष्म हो जाते हैं / मन की कलुषता भावना से नष्ट हो जाती है / भावना चार प्रकार की होती है - मैत्री - अहिंसा निषेधात्मक गुण है और मैत्री उसका विधायक पक्ष है / मनुष्य को न केवल समस्त प्राणियों की हिंसा से ही विरत रहना चाहिये वरन् उनकी सहायता भी करनी चाहिये / ___ प्रमोद - इसका तात्पर्य दूसरों के सुख, शान्ति, समृद्धि एवं ऐश्वर्य को देखकर, ईर्ष्या न करते हुए प्रसन्न होना है। कारुण्य - इसका अर्थ दीन और दुःखी प्राणियों की सेवा करना है / माध्यस्थ - जो अज्ञानी है, उनके प्रति उपेक्षा की भावना न रखना और क्रोध नहीं करना माध्यस्थ कहलाता है। (5) अनुप्रेक्षा - इन चार भावनाओं के अतिरिक्त अन्य बारह प्रकार की भावनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनका चिन्तन आवश्यक माना गया है / (6) समितियाँ - समिति का तात्पर्य सदाचार या उत्तम व्यवहार होता है। समितियाँ पाँच हैं(१) ईर्या समिति - नीचे की ओर देखकर चलना, जिससे जीव हिंसा न हो (2) भाषा-समिति - सत्य, प्रिय एवं हितकारी वचन बोलना तथा वाणी में निष्कपट माधुर्य होना / (3) एषणा-समिति - अपवित्र वस्तुओं की इच्छा न करना / (4) आदान-निक्षेपण-समिति- वस्तुओं को झाड़-पोंछकर, उनका आदान-प्रदान करना / (5) उत्सर्ग-समिति - मलमूत्र का निक्षेपण इस प्रकार करना कि उसमें दोष या जीवहानि न हो। (7) अनाचीर्ण - बावन ऐसे निषिद्ध कर्म हैं, जिनका आचरण नहीं करने का उपदेश दिया गया है। इन्हें अनाचीर्ण कहते हैं। (8) नित्यकर्म - साधना में नित्य स्फूर्तता के लिये छ: नित्यकर्मों का विधान है - (1) सामायिक अर्थात् द्वन्द्व-विमुख समभाव (2) स्तवन - तीर्थंकरों का गुण-कीर्तन (3) वन्दना - पंच परमेष्ठियों का पूजन और पूजनीय पुरुषों का आदर करना (4) प्रतिक्रमण - अशुभ से