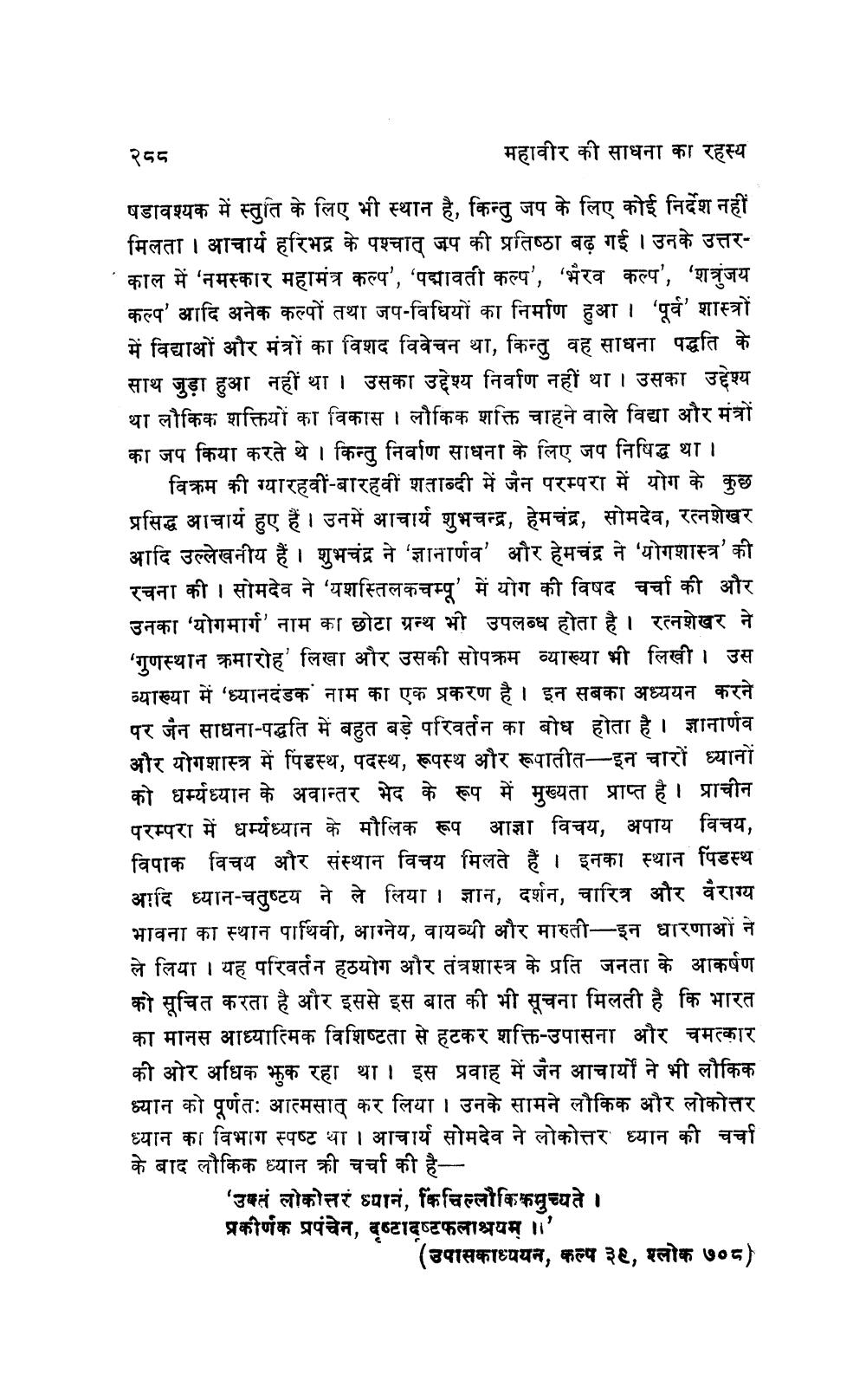________________
२८८
महावीर की साधना का रहस्य
षडावश्यक में स्तुति के लिए भी स्थान है, किन्तु जप के लिए कोई निर्देश नहीं मिलता । आचार्य हरिभद्र के पश्चात् जप की प्रतिष्ठा बढ़ गई । उनके उत्तरकाल में 'नमस्कार महामंत्र कल्प', 'पद्मावती कल्प', 'भैरव कल्प', 'शत्रुजय कल्प' आदि अनेक कल्पों तथा जप-विधियों का निर्माण हुआ। 'पूर्व' शास्त्रों में विद्याओं और मंत्रों का विशद विवेचन था, किन्तु वह साधना पद्धति के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। उसका उद्देश्य निर्वाण नहीं था। उसका उद्देश्य था लौकिक शक्तियों का विकास । लौकिक शक्ति चाहने वाले विद्या और मंत्रों का जप किया करते थे। किन्तु निर्वाण साधना के लिए जप निषिद्ध था।
विक्रम की ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में जैन परम्परा में योग के कुछ प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। उनमें आचार्य शुभचन्द्र, हेमचंद्र, सोमदेव, रत्नशेखर आदि उल्लेखनीय हैं। शुभचंद्र ने 'ज्ञानार्णव' और हेमचंद्र ने 'योगशास्त्र' की रचना की । सोमदेव ने 'यशस्तिलकचम्पू' में योग की विषद चर्चा की और उनका 'योगमार्ग' नाम का छोटा ग्रन्थ भी उपलब्ध होता है। रत्नशेखर ने 'गुणस्थान क्रमारोह' लिखा और उसकी सोपक्रम व्याख्या भी लिखी। उस व्याख्या में 'ध्यानदंडक नाम का एक प्रकरण है। इन सबका अध्ययन करने पर जैन साधना-पद्धति में बहुत बड़े परिवर्तन का बोध होता है। ज्ञानार्णव और योगशास्त्र में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत-इन चारों ध्यानों को धर्म्यध्यान के अवान्तर भेद के रूप में मुख्यता प्राप्त है। प्राचीन परम्परा में धर्म्यध्यान के मौलिक रूप आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय मिलते हैं । इनका स्थान पिंडस्थ आदि ध्यान-चतुष्टय ने ले लिया। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वैराग्य भावना का स्थान पार्थिवी, आग्नेय, वायव्यी और मारुती-इन धारणाओं ने ले लिया । यह परिवर्तन हठयोग और तंत्रशास्त्र के प्रति जनता के आकर्षण को सूचित करता है और इससे इस बात की भी सूचना मिलती है कि भारत का मानस आध्यात्मिक विशिष्टता से हटकर शक्ति-उपासना और चमत्कार की ओर अधिक झुक रहा था। इस प्रवाह में जैन आचार्यों ने भी लौकिक ध्यान को पूर्णत: आत्मसात् कर लिया। उनके सामने लौकिक और लोकोत्तर ध्यान का विभाग स्पष्ट था । आचार्य सोमदेव ने लोकोत्तर ध्यान की चर्चा के बाद लौकिक ध्यान की चर्चा की है
'उक्तं लोकोत्तरं ध्यानं, किचिल्लौकिकमुच्यते । प्रकीर्णक प्रपंचेन, दृष्टादृष्टफलाश्रयम् ॥'
(उपासकाध्ययन, कल्प ३६, श्लोक ७०८)