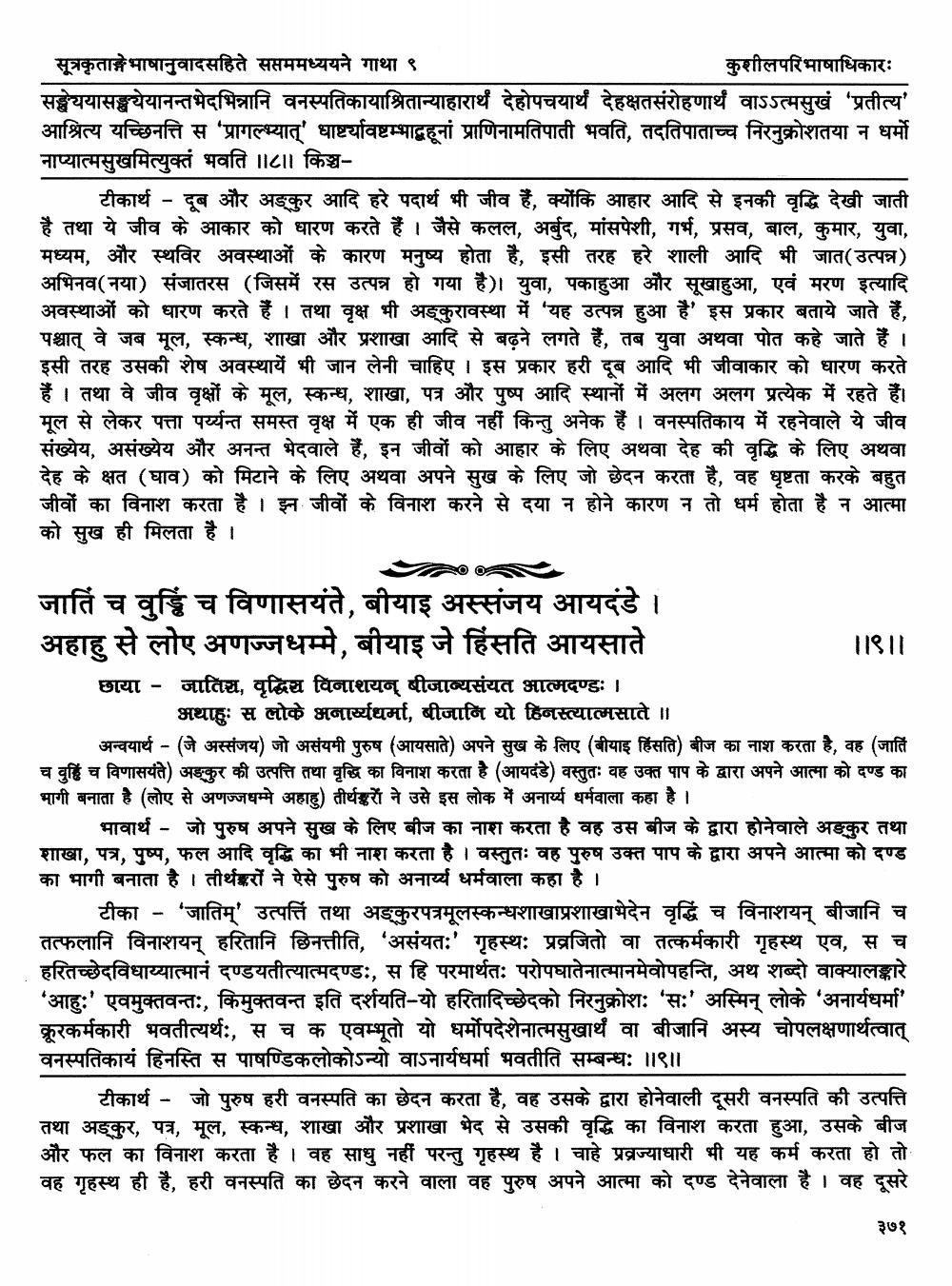________________
सूत्रकृताङ्गे भाषानुवादसहिते सप्तममध्ययने गाथा ९
कुशीलपरिभाषाधिकारः
सङ्ख्ययासङ्ख्येयानन्तभेदभिन्नानि वनस्पतिकायाश्रितान्याहारार्थं देहोपचयार्थं देहक्षतसंरोहणार्थं वाऽऽत्मसुखं 'प्रतीत्य' आश्रित्य यच्छित्तिस 'प्रागल्भ्यात्' धाष्टर्थ्यावष्टम्भाद्बहूनां प्राणिनामतिपाती भवति, तदतिपाताच्च निरनुक्रोशतया न धर्मो नाप्यात्मसुखमित्युक्तं भवति ॥८॥ किञ्च
टीकार्थ दूब और अङ्कुर आदि हरे पदार्थ भी जीव हैं, क्योंकि आहार आदि से इनकी वृद्धि देखी जाती है तथा ये जीव के आकार को धारण करते हैं। जैसे कलल, अर्बुद, मांसपेशी, गर्भ, प्रसव, बाल, कुमार, युवा, मध्यम, और स्थविर अवस्थाओं के कारण मनुष्य होता है, इसी तरह हरे शाली आदि भी जात (उत्पन्न) अभिनव (नया) संजातरस (जिसमें रस उत्पन्न हो गया है) । युवा, पकाहुआ और सूखाहुआ, एवं मरण इत्यादि अवस्थाओं को धारण करते हैं । तथा वृक्ष भी अङ्कुरावस्था में 'यह उत्पन्न हुआ है' इस प्रकार बताये जाते हैं, पश्चात् वे जब मूल, स्कन्ध, शाखा और प्रशाखा आदि से बढ़ने लगते हैं, तब युवा अथवा पोत कहे जाते हैं । इसी तरह उसकी शेष अवस्थायें भी जान लेनी चाहिए । इस प्रकार हरी दूब आदि भी जीवाकार को धारण करते हैं । तथा वे जीव वृक्षों के मूल, स्कन्ध, शाखा, पत्र और पुष्प आदि स्थानों में अलग अलग प्रत्येक में रहते हैं। मूल से लेकर पत्ता पर्य्यन्त समस्त वृक्ष में एक ही जीव नहीं किन्तु अनेक हैं । वनस्पतिकाय में रहनेवाले ये जीव संख्येय, असंख्येय और अनन्त भेदवाले हैं, इन जीवों को आहार के लिए अथवा देह की वृद्धि के लिए अथवा देह के क्षत (घाव) को मिटाने के लिए अथवा अपने सुख के लिए जो छेदन करता है, वह धृष्टता करके बहुत जीवों का विनाश करता है। इन जीवों के विनाश करने से दया न होने कारण न तो धर्म होता है न आत्मा को सुख ही मिलता है ।
-
जातिं च वुड्विं च विणासयंते, बीयाइ अस्संजय आयदंडे । अहाहु से लोए अणज्जधम्मे, बीयाइ जे हिंसति आयसाते
छाया - जातिश, वृद्धि विनाशयन् बीजान्यसंयत आत्मदण्डः । अथाहुः स लोके अनार्य्यधर्मा, बीजानि यो हिनस्त्यात्मसाते ॥
अन्वयार्थ - (जे अस्संजय ) जो असंयमी पुरुष (आयसाते) अपने सुख के लिए ( बीयाइ हिंसति) बीज का नाश करता है, वह (जातिं च वुद्धिं च विणासयंते) अङ्कुर की उत्पत्ति तथा वृद्धि का विनाश करता है (आयदंडे ) वस्तुतः वह उक्त पाप के द्वारा अपने आत्मा को दण्ड का भागी बनाता है (लोए से अणज्जधम्मे अहाहु) तीर्थङ्करों ने उसे इस लोक में अनार्य्य धर्मवाला कहा है ।
11811
भावार्थ जो पुरुष अपने सुख के लिए बीज का नाश करता वह उस बीज के द्वारा होनेवाले अङ्कुर तथा शाखा, पत्र, पुष्प, फल आदि वृद्धि का भी नाश करता है । वस्तुतः वह पुरुष उक्त पाप के द्वारा अपने आत्मा को दण्ड का भागी बनाता है । तीर्थकरों ने ऐसे पुरुष को अनार्य्य धर्मवाला कहा है ।
-
टीका – 'जातिम्' उत्पत्तिं तथा अङ्कुरपत्रमूलस्कन्धशाखाप्रशाखाभेदेन वृद्धिं च विनाशयन् बीजानि च तत्फलानि विनाशयन् हरितानि छिनत्तीति, 'असंयतः ' गृहस्थः प्रव्रजितो वा तत्कर्मकारी गृहस्थ एव, स च हरितच्छेदविधाय्यात्मानं दण्डयतीत्यात्मदण्डः, स हि परमार्थतः परोपघातेनात्मानमेवोपहन्ति, अथ शब्दो वाक्यालङ्कारे 'आहु:' एवमुक्तवन्तः, किमुक्तवन्त इति दर्शयति-यो हरितादिच्छेदको निरनुक्रोशः 'सः' अस्मिन् लोके 'अनार्यधर्मा' क्रूरकर्मकारी भवतीत्यर्थः, स च क एवम्भूतो यो धर्मोपदेशेनात्मसुखार्थं वा बीजानि अस्य चोपलक्षणार्थत्वात् वनस्पतिकायं हिनस्ति स पाषण्डिकलोकोऽन्यो वाऽनार्यधर्मा भवतीति सम्बन्धः ॥ ९ ॥
टीकार्थ जो पुरुष हरी वनस्पति का छेदन करता है, वह उसके द्वारा होनेवाली दूसरी वनस्पति की उत्पत्ति तथा अङ्कुर, पत्र, मूल, स्कन्ध, शाखा और प्रशाखा भेद से उसकी वृद्धि का विनाश करता हुआ, उसके बीज और फल का विनाश करता है । वह साधु नहीं परन्तु गृहस्थ है। चाहे प्रव्रज्याधारी भी यह कर्म करता हो तो वह गृहस्थ ही है, हरी वनस्पति का छेदन करने वाला वह पुरुष अपने आत्मा को दण्ड देनेवाला है । वह दूसरे
३७१
-