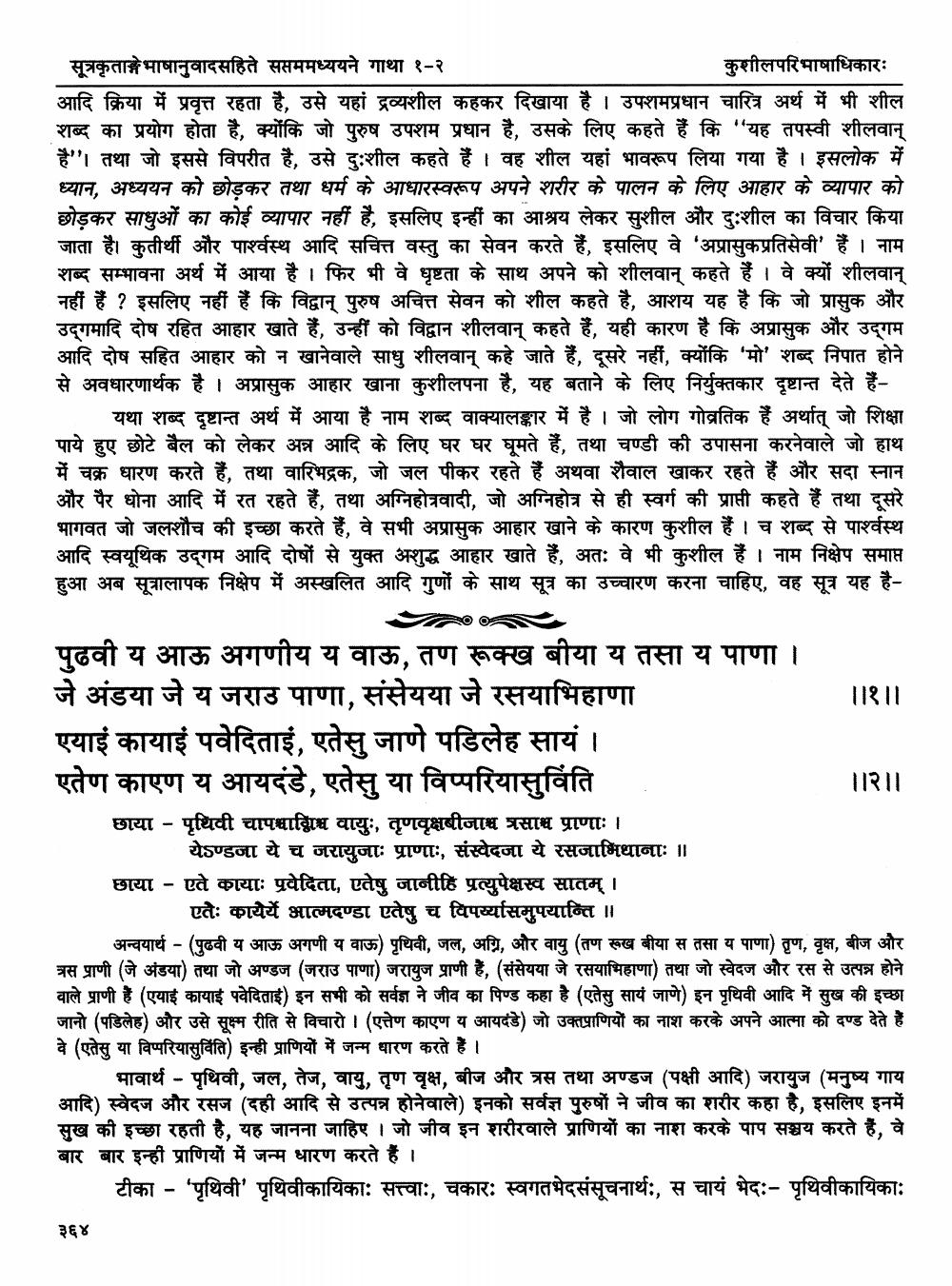________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते ससममध्ययने गाथा १-२
कुशीलपरिभाषाधिकारः आदि क्रिया में प्रवृत्त रहता है, उसे यहां द्रव्यशील कहकर दिखाया है। उपशमप्रधान चारित्र अर्थ में भी शील शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि जो पुरुष उपशम प्रधान है, उसके लिए कहते हैं कि "यह तपस्वी शीलवान् है"। तथा जो इससे विपरीत है, उसे दुःशील कहते हैं । वह शील यहां भावरूप लिया गया है । इसलोक में ध्यान, अध्ययन को छोड़कर तथा धर्म के आधारस्वरूप अपने शरीर के पालन के लिए आहार के व्यापार को छोड़कर साधुओं का कोई व्यापार नहीं है, इसलिए इन्हीं का आश्रय लेकर सुशील और दुःशील का विचार किया जाता है। कुतीर्थी और पार्श्वस्थ आदि सचित्त वस्तु का सेवन करते हैं, इसलिए वे 'अप्रासुकप्रतिसेवी' हैं । नाम शब्द सम्भावना अर्थ में आया है । फिर भी वे धृष्टता के साथ अपने को शीलवान् कहते हैं । वे क्यों शीलवान् नहीं हैं ? इसलिए नहीं हैं कि विद्वान् पुरुष अचित्त सेवन को शील कहते है, आशय यह है कि जो प्रासुक और उद्गमादि दोष रहित आहार खाते हैं, उन्हीं को विद्वान शीलवान् कहते हैं, यही कारण है कि अप्रासुक और उद्गम आदि दोष सहित आहार को न खानेवाले साधु शीलवान् कहे जाते हैं, दूसरे नहीं, क्योंकि 'मो' शब्द निपात होने से अवधारणार्थक है । अप्रासुक आहार खाना कुशीलपना है, यह बताने के लिए निर्युक्तकार दृष्टान्त देते हैं
यथा शब्द दृष्टान्त अर्थ में आया है नाम शब्द वाक्यालङ्कार में है। जो लोग गोव्रतिक हैं अर्थात् जो शिक्षा पाये हुए छोटे बैल को लेकर अन्न आदि के लिए घर घर घूमते हैं, तथा चण्डी की उपासना करनेवाले जो हाथ में चक्र धारण करते हैं, तथा वारिभद्रक, जो जल पीकर रहते हैं अथवा शैवाल खाकर रहते हैं और सदा स्नान और पैर धोना आदि में रत रहते हैं, तथा अग्निहोत्रवादी, जो अग्निहोत्र से ही स्वर्ग की प्राप्ती कहते हैं तथा दूसरे भागवत जो जलशौच की इच्छा करते हैं, वे सभी अप्रासुक आहार खाने के कारण कुशील हैं। च शब्द से पार्श्वस्थ
उदगम आदि दोषों से यक्त अशद्ध आहार खाते हैं, अतः वे भी कशील हैं। नाम निक्षेप समाप्त हुआ अब सूत्रालापक निक्षेप में अस्खलित आदि गुणों के साथ सूत्र का उच्चारण करना चाहिए, वह सूत्र यह है
पढवी य आऊ अगणीय य वाऊ, तण रूक्ख बीया य तसा य पाणा। जे अंडया जे य जराउ पाणा, संसेयया जे रसयाभिहाणा
॥१॥ एयाई कायाई पवेदिताई, एतेसु जाणे पडिलेह सायं । एतेण कारण य आयदंडे, एतेसु या विप्परियासुविंति
॥२॥ छाया - पृथिवी चापश्चादिश्च वायुः, तृणवृक्षबीजाच त्रसाश्च प्राणाः ।
येऽण्डजा ये च जरायुजाः प्राणाः, संस्वेदजा ये रसजाभिधानाः ॥ छाया - एते कायाः प्रवेदिता, एतेषु जानीहि प्रत्युपेक्षस्व सातम् ।
एतेः कायर्ये भात्मदण्डा एतेषु च विपर्यासमुपयान्ति ॥ अन्वयार्थ - (पुढवी य आऊ अगणी य वाऊ) पृथिवी, जल, अग्रि, और वायु (तण रूख बीया स तसा य पाणा) तृण, वृक्ष, बीज और त्रस प्राणी (जे अंडया) तथा जो अण्डज (जराउ पाणा) जरायुज प्राणी हैं, (संसेयया जे रसयाभिहाणा) तथा जो स्वेदज और रस से उत्पन्न होने वाले प्राणी है (एयाई कायाई पवेदिताई) इन सभी को सर्वज्ञ ने जीव का पिण्ड कहा है (एतेसु सायं जाणे) इन पृथिवी आदि में सुख की इच्छा जानो (पडिलेह) और उसे सूक्ष्म रीति से विचारो । (एत्तेण कारण य आयदंडे) जो उक्तप्राणियों का नाश करके अपने आत्मा को दण्ड देते हैं वे (एतेसु या विपरियासुर्विति) इन्ही प्राणियों में जन्म धारण करते है।
भावार्थ- पृथिवी, जल, तेज, वायु, तृण वृक्ष, बीज और त्रस तथा अण्डज (पक्षी आदि) जरायुज (मनुष्य गाय आदि) स्वेदज और रसज (दही आदि से उत्पन्न होनेवाले) इनको सर्वज्ञ पुरुषों ने जीव का शर सुख की इच्छा रहती है, यह जानना जाहिए । जो जीव इन शरीरवाले प्राणियों का नाश करके पाप सञ्चय करते हैं, वे बार बार इन्ही प्राणियों में जन्म धारण करते हैं।
टीका - 'पृथिवी' पृथिवीकायिकाः सत्त्वाः, चकारः स्वगतभेदसंसूचनार्थः, स चायं भेदः- पृथिवीकायिकाः
३६४