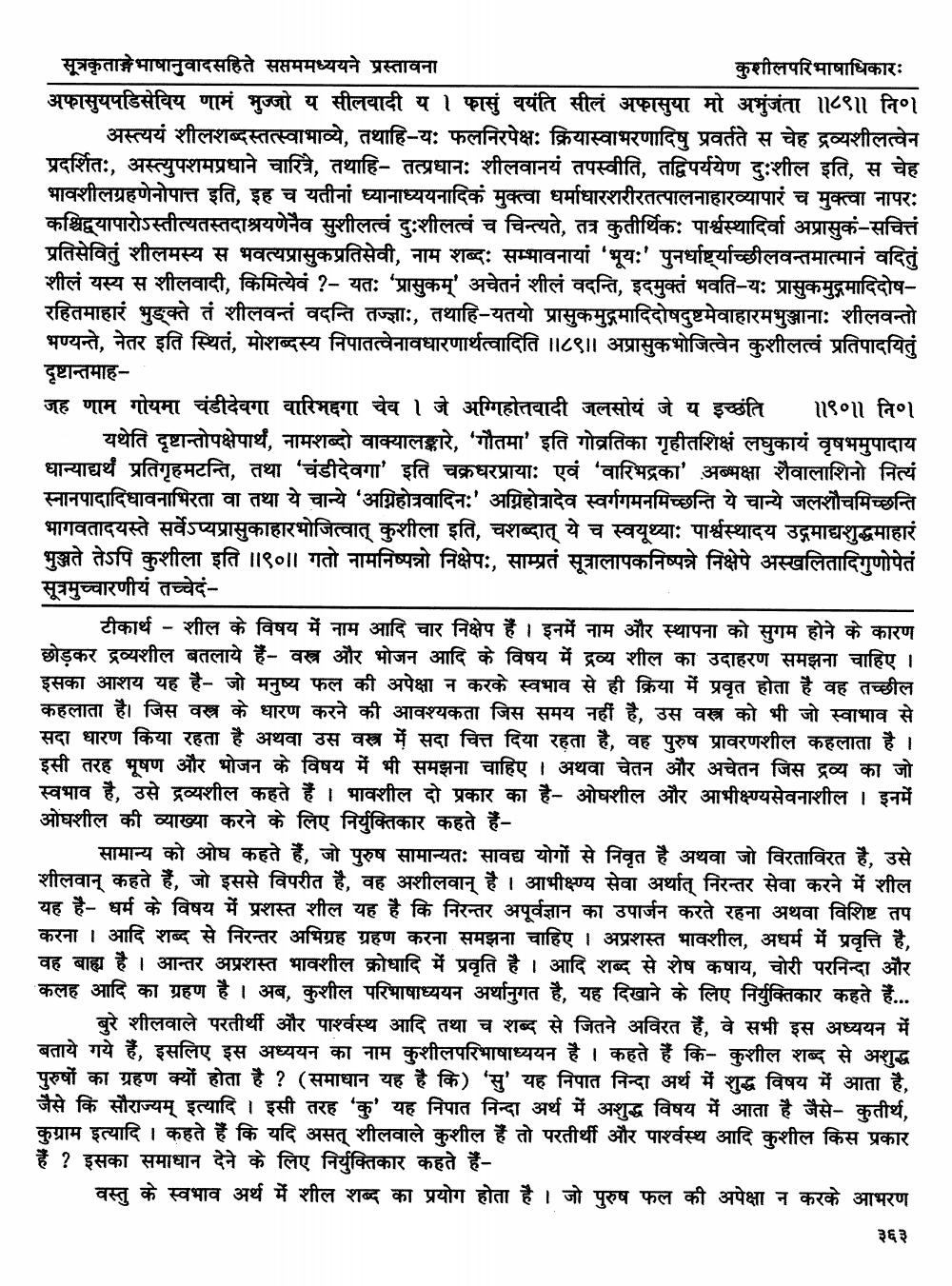________________
सूत्रकृताङ्गे भाषानुवादसहिते सप्तममध्ययने प्रस्तावना
कुशीलपरिभाषाधिकारः अफासुयपडिसेविय णामं भुज्जो य सीलयादी य । कासुं वयंति सीलं अफासुया मो अजंता ॥८९॥ नि०
अस्त्ययं शीलशब्दस्तत्स्वाभाव्ये, तथाहि यः फलनिरपेक्षः क्रियास्वाभरणादिषु प्रवर्तते स चेह द्रव्यशीलत्वेन प्रदर्शितः, अस्त्युपशमप्रधाने चारित्रे, तथाहि तत्प्रधानः शीलवानयं तपस्वीति, तद्विपर्ययेण दुःशील इति, स चेह भावशीलग्रहणेनोपात्त इति, इह च यतीनां ध्यानाध्ययनादिकं मुक्त्वा धर्माधारशरीरतत्पालनाहारव्यापारं च मुक्त्वा नापर: कश्चिद्व्यापारोऽस्तीत्यतस्तदाश्रयणेनैव सुशीलत्वं दुःशीलत्वं च चिन्त्यते, तत्र कुतीर्थिकः पार्श्वस्थादिर्वा अप्रासुकं - सचित्तं प्रतिसेवितुं शीलमस्य स भवत्यप्रासुकप्रतिसेवी, नाम शब्दः सम्भावनायां 'भूयः' पुनर्धाष्टर्थ्याच्छीलवन्तमात्मानं वदितुं शीलं यस्य स शीलवादी, किमित्येवं ? - यत: 'प्रासुकम्' अचेतनं शीलं वदन्ति, इदमुक्तं भवति यः प्रासुकमुद्गमादिदोषरहितमाहारं भुङ्क्ते तं शीलवन्तं वदन्ति तज्ज्ञाः, तथाहि यतयो प्रासुकमुद्गमादिदोषदुष्टमेवाहारमभुञ्जानाः शीलवन्तो भण्यन्ते, नेतर इति स्थितं, मोशब्दस्य निपातत्वेनावधारणार्थत्वादिति ॥ ८९ ॥ अप्रासुकभोजित्वेन कुशीलत्वं प्रतिपादयितुं दृष्टान्तमाह
जह णाम गोयमा चंडीदेवगा वारिभद्दगा चेव । जे अग्गिहोत्तयादी जलसोयं जे य इच्छंति ॥९०॥ नि०
यथेति दृष्टान्तोपक्षेपार्थं, नामशब्दो वाक्यालङ्कारे, 'गौतमा' इति गोव्रतिका गृहीतशिक्षं लघुकायं वृषभमुपादाय धान्याद्यर्थं प्रतिगृहमटन्ति, तथा 'चंडीदेवगा' इति चक्रधरप्रायाः एवं 'वारिभद्रका' अब्भक्षा शैवालाशिनो नित्यं स्नानपादादिधावनाभिरता वा तथा ये चान्ये 'अग्निहोत्रवादिनः' अग्निहोत्रादेव स्वर्गगमनमिच्छन्ति ये चान्ये जलशौचमिच्छन्ति भागवतादयस्ते सर्वेऽप्यप्रासुकाहार भोजित्वात् कुशीला इति, चशब्दात् ये च स्वयूथ्याः पार्श्वस्थादय उद्गमाद्यशुद्धमाहारं भुञ्जतेऽपि कुशीला इति ॥ ९०॥ गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः, साम्प्रतं सूत्रालापकनिष्पन्ने निक्षेपे अस्खलितादिगुणोपेतं सूत्रमुच्चारणीयं तच्चेदं
टीकार्थ शील के विषय में नाम आदि चार निक्षेप हैं। इनमें नाम और स्थापना को सुगम होने के कारण छोड़कर द्रव्यशील बतलाये हैं- वस्त्र और भोजन आदि के विषय में द्रव्य शील का उदाहरण समझना चाहिए । इसका आशय यह है- जो मनुष्य फल की अपेक्षा न करके स्वभाव से ही क्रिया में प्रवृत होता है वह तच्छील कहलाता है। जिस वस्त्र के धारण करने की आवश्यकता जिस समय नहीं है, उस वस्त्र को भी जो स्वाभाव से सदा धारण किया रहता है अथवा उस वस्त्र में सदा चित्त दिया रहता है, वह पुरुष प्रावरणशील कहलाता है । इसी तरह भूषण और भोजन के विषय में भी समझना चाहिए । अथवा चेतन और अचेतन जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, उसे द्रव्यशील कहते हैं । भावशील दो प्रकार का है- ओघशील और आभीक्ष्ण्यसेवनाशील । इनमें अघशील की व्याख्या करने के लिए नियुक्तिकार कहते हैं
सामान्य को ओघ कहते हैं, जो पुरुष सामान्यतः सावद्य योगों से निवृत है अथवा जो विरताविरत है, उसे शीलवान् कहते हैं, जो इससे विपरीत है, वह अशीलवान् है । आभीक्ष्ण्य सेवा अर्थात् निरन्तर सेवा करने में शील यह है- धर्म के विषय में प्रशस्त शील यह है कि निरन्तर अपूर्वज्ञान का उपार्जन करते रहना अथवा विशिष्ट तप करना । आदि शब्द से निरन्तर अभिग्रह ग्रहण करना समझना चाहिए। अप्रशस्त भावशील अधर्म में प्रवृत्ति है, वह बाह्य है । आन्तर अप्रशस्त भावशील क्रोधादि में प्रवृति है । आदि शब्द से शेष कषाय, चोरी परनिन्दा और कलह आदि का ग्रहण है । अब, कुशील परिभाषाध्ययन अर्थानुगत है, यह दिखाने के लिए नियुक्तिकार कहते हैं...
बुरे शीलवाले परतीर्थी और पार्श्वस्थ आदि तथा च शब्द से जितने अविरत हैं, वे सभी इस अध्ययन में बताये गये हैं, इसलिए इस अध्ययन का नाम कुशीलपरिभाषाध्ययन है । कहते हैं कि- कुशील शब्द से अशुद्ध पुरुषों का ग्रहण क्यों होता है ? (समाधान यह है कि) 'सु' यह निपात निन्दा अर्थ में शुद्ध विषय में आता है, जैसे कि सौराज्यम् इत्यादि । इसी तरह 'कु' यह निपात निन्दा अर्थ में अशुद्ध विषय में आता है जैसे- कुतीर्थ, कुग्राम इत्यादि । कहते हैं कि यदि असत् शीलवाले कुशील हैं तो परतीर्थी और पार्श्वस्थ आदि कुशील किस प्रकार हैं ? इसका समाधान देने के लिए नियुक्तिकार कहते हैं
वस्तु के स्वभाव अर्थ में शील शब्द का प्रयोग होता है । जो पुरुष फल की अपेक्षा न करके आभरण
३६३