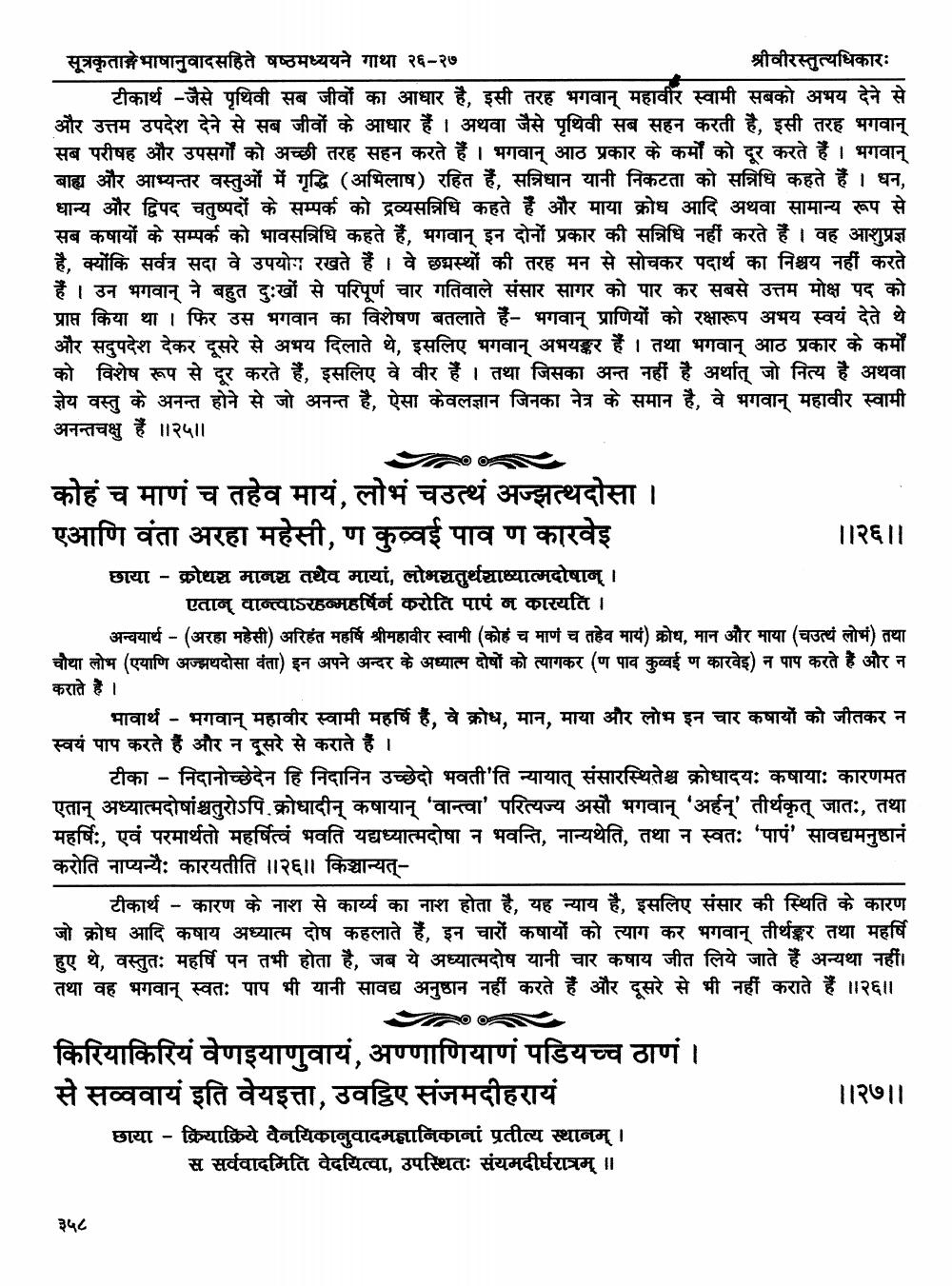________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते षष्ठमध्ययने गाथा २६-२७
श्रीवीरस्तुत्यधिकारः टीकार्थ -जैसे पृथिवी सब जीवों का आधार है, इसी तरह भगवान् महावीर स्वामी सबको अभय देने से और उत्तम उपदेश देने से सब जीवों के आधार हैं । अथवा जैसे पृथिवी सब सहन करती है, इसी तरह भगवान् सब परीषह और उपसर्गों को अच्छी तरह सहन करते हैं । भगवान् आठ प्रकार के कर्मों को दूर करते हैं। भगवान् बाह्य और आभ्यन्तर वस्तुओं में गृद्धि (अभिलाष) रहित हैं, सन्निधान यानी निकटता को सन्निधि कहते हैं । धन, धान्य और द्विपद चतुष्पदों के सम्पर्क को द्रव्यसन्निधि कहते हैं और माया क्रोध आदि अथवा सामान्य रूप से सब कषायों के सम्पर्क को भावसन्निधि कहते हैं, भगवान् इन दोनों प्रकार की सन्निधि नहीं करते हैं। वह आशुप्रज्ञ है, क्योंकि सर्वत्र सदा वे उपयोग रखते हैं । वे छद्मस्थों की तरह मन से सोचकर पदार्थ का निश्चय नहीं करते हैं । उन भगवान् ने बहुत दुःखों से परिपूर्ण चार गतिवाले संसार सागर को पार कर सबसे उत्तम मोक्ष पद को प्राप्त किया था । फिर उस भगवान का विशेषण बतलाते हैं- भगवान् प्राणियों को रक्षारूप अभय स्वयं देते थे
और सदुपदेश देकर दूसरे से अभय दिलाते थे, इसलिए भगवान् अभयङ्कर हैं। तथा भगवान् आठ प्रकार के कर्मों को विशेष रूप से दर करते हैं. इसलिए वे वीर हैं। तथा जिसका अन्त नहीं है अर्थात जो नित्य है अथवा ज्ञेय वस्तु के अनन्त होने से जो अनन्त है, ऐसा केवलज्ञान जिनका नेत्र के समान है, वे भगवान् महावीर स्वामी अनन्तचक्षु हैं ॥२५॥
कोहं च माणं च तहेव मायं, लोभं चउत्थं अज्झत्थदोसा । एआणि वंता अरहा महेसी, ण कुव्वई पाव ण कारवेइ
॥२६॥ छाया - क्रोधच मानव तथैव मायां, लोभशतुर्थशाध्यात्मदोषान् ।
एतान् वान्त्वाऽरहन्महर्षिन करोति पापं न कारयति । अन्वयार्थ - (अरहा महेसी) अरिहंत महर्षि श्रीमहावीर स्वामी (कोहं च माणं च तहेव माय) क्रोध, मान और माया (चउत्थं लोभ) तथा चौथा लोभ (एयाणि अज्झथदोसा वंता) इन अपने अन्दर के अध्यात्म दोषों को त्यागकर (ण पाव कुब्बई ण कारवेइ) न पाप करते हैं और न कराते हैं।
भावार्थ - भगवान् महावीर स्वामी महर्षि हैं, वे क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायों को जीतकर न स्वयं पाप करते हैं और न दूसरे से कराते हैं।
टीका - निदानोच्छेदेन हि निदानिन उच्छेदो भवतीति न्यायात् संसारस्थितेश्च क्रोधादयः कषायाः कारणमत एतान् अध्यात्मदोषांश्चतुरोऽपि क्रोधादीन् कषायान् 'वान्त्वा' परित्यज्य असौ भगवान् 'अर्हन्' तीर्थकृत् जातः, तथा महर्षिः, एवं परमार्थतो महर्षित्वं भवति यद्यध्यात्मदोषा न भवन्ति, नान्यथेति, तथा न स्वतः 'पाप' सावधमनुष्ठानं करोति नाप्यन्यैः कारयतीति ॥२६।। किञ्चान्यत्
टीकार्थ - कारण के नाश से कार्य का नाश होता है, यह न्याय है, इसलिए संसार की स्थिति के कारण जो क्रोध आदि कषाय अध्यात्म दोष कहलाते हैं, इन चारों कषायों को त्याग कर भगवान् तीर्थङ्कर तथा महर्षि हुए थे, वस्तुतः महर्षि पन तभी होता है, जब ये अध्यात्मदोष यानी चार कषाय जीत लिये जाते हैं अन्यथा नहीं। तथा वह भगवान स्वतः पाप भी यानी सावध अनुष्ठान नहीं करते हैं और दूसरे से भी नहीं कराते हैं ॥२६॥
किरियाकिरियं वेणइयाणवायं, अण्णाणियाणं पडियच्च ठाणं । से सव्ववायं इति वेयइत्ता, उवट्ठिए संजमदीहरायं छाया - क्रियाक्रिये वैनयिकानुवादमहानिकानां प्रतीत्य स्थानम् ।
स सर्ववादमिति वेदयित्वा, उपस्थितः संयमदीर्घरात्रम् ॥
॥२७॥
३५८