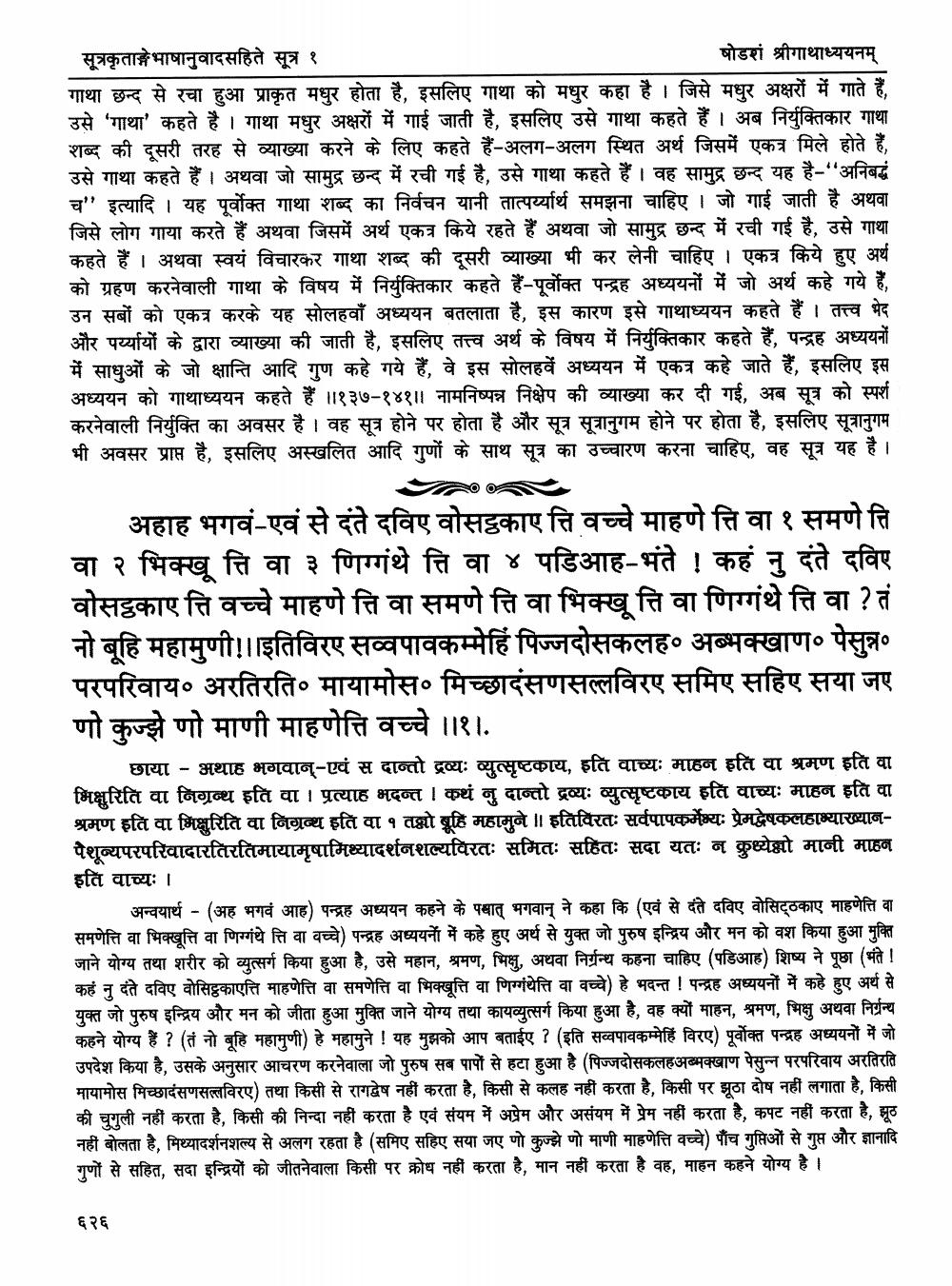________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते सूत्र १
षोडशं श्रीगाथाध्ययनम् गाथा छन्द से रचा हुआ प्राकृत मधुर होता है, इसलिए गाथा को मधुर कहा है । जिसे मधुर अक्षरों में गाते हैं, उसे 'गाथा' कहते है । गाथा मधुर अक्षरों में गाई जाती है, इसलिए उसे गाथा कहते हैं । अब निर्युक्तिकार गाथा शब्द की दूसरी तरह से व्याख्या करने के लिए कहते हैं अलग-अलग स्थित अर्थ जिसमें एकत्र मिले होते हैं, उसे गाथा कहते हैं । अथवा जो सामुद्र छन्द में रची गई है, उसे गाथा कहते हैं । वह सामुद्र छन्द यह है - " अनिबद्धं च" इत्यादि । यह पूर्वोक्त गाथा शब्द का निर्वचन यानी तात्पर्य्यार्थ समझना चाहिए । जो गाई जाती है अथवा जिसे लोग गाया करते हैं अथवा जिसमें अर्थ एकत्र किये रहते हैं अथवा जो सामुद्र छन्द में रची गई है, उसे गाथा कहते हैं । अथवा स्वयं विचारकर गाथा शब्द की दूसरी व्याख्या भी कर लेनी चाहिए । एकत्र किये हुए अर्थ को ग्रहण करनेवाली गाथा के विषय में नियुक्तिकार कहते हैं- पूर्वोक्त पन्द्रह अध्ययनों में जो अर्थ कहे गये हैं, उन सबों को एकत्र करके यह सोलहवाँ अध्ययन बतलाता है, इस कारण इसे गाथाध्ययन कहते हैं । तत्त्व भेद और पर्य्यायों के द्वारा व्याख्या की जाती है, इसलिए तत्त्व अर्थ के विषय में नियुक्तिकार कहते हैं, पन्द्रह अध्ययनों में साधुओं के जो क्षान्ति आदि गुण कहे गये हैं, वे इस सोलहवें अध्ययन में एकत्र कहे जाते हैं, इसलिए इस अध्ययन को गाथाध्ययन कहते हैं ।। १३७ - १४१ ॥ नामनिष्पन्न निक्षेप की व्याख्या कर दी गई, अब सूत्र को स्पर्श करनेवाली नियुक्ति का अवसर है। वह सूत्र होने पर होता है और सूत्र सूत्रानुगम होने पर होता है, इसलिए सूत्रानुगम भी अवसर प्राप्त है, इसलिए अस्खलित आदि गुणों के साथ सूत्र का उच्चारण करना चाहिए, वह सूत्र यह है ।
अहाह भगवं एवं से दंते दविए वोसट्टकाए त्ति वच्चे माहणे त्ति वा १ समणे त्ति वा २ भिक्खू त्ति वा ३ णिग्गंथे त्ति वा ४ पडिआह- भंते ! कहं नु दंते दविए वोसट्टकाए त्ति वच्चे माहणे त्ति वा समणे त्ति वा भिक्खू त्ति वा णिग्गंथे त्ति वा ? तं नो बूहि महामुणी! ।। इतिविरए सव्वपावकम्मेहिं पिज्जदोसकलह • अब्भक्खाण० पेसुन्न० परपरिवाय० अरतिरति • मायामोस० मिच्छादंसणसल्लविरए समिए सहिए सया जए
कुणी माणी माहणेत्ति वच्चे ॥ १ ॥ .
छाया - अथाह भगवान् एवं स दान्तो द्रव्यः व्युत्सृष्टकाय, इति वाच्यः माहन इति वा श्रमण इति वा भिक्षुरिति वा निग्रन्थ इति वा । प्रत्याह भदन्त । कथं नु दान्तो द्रव्यः व्युत्सृष्टकाय इति वाच्यः माहन इति वा श्रमण इति वा भिक्षुरिति वा निग्रन्थ इति वा १ तल्लो ब्रूहि महामुने || इतिविरतः सर्वपापकर्मेभ्यः प्रेमद्वेषकलहाभ्याख्यानपैशून्यपरपरिवादारतिरतिमायामृषामिध्यादर्शनशल्यविरतः समितः सहितः सदा यतः न क्रुध्येलो मानी माहन
इति वाच्यः ।
अन्वयार्थ - ( अह भगवं आह) पन्द्रह अध्ययन कहने के पश्चात् भगवान् ने कहा कि ( एवं से दंते दविए वोसिट्ठकाए माहणेत्ति वा समणेत्ति वा भिक्खुत्ति वा णिग्गंथे त्ति वा बच्चे) पन्द्रह अध्ययनों में कहे हुए अर्थ से युक्त जो पुरुष इन्द्रिय और मन को वश किया हुआ मुक्ति जाने योग्य तथा शरीर को व्युत्सर्ग किया हुआ है, उसे महान, श्रमण, भिक्षु, अथवा निर्ग्रन्थ कहना चाहिए (पडिआह ) शिष्य ने पूछा ( भंते ! कहं नु दंते दविए वोसिकाएत्ति माहणेत्ति वा समणेत्ति वा भिक्खूत्ति वा णिग्गंथेत्ति वा वच्चे) हे भदन्त । पन्द्रह अध्ययनों में कहे हुए अर्थ से युक्त जो पुरुष इन्द्रिय और मन को जीता हुआ मुक्ति जाने योग्य तथा कायव्युत्सर्ग किया हुआ है, वह क्यों माहन, श्रमण, भिक्षु अथवा निर्ग्रन्थ कहने योग्य हैं ? (तं नो बूहि महामुणी) हे महामुने ! यह मुझको आप बताईए ? (इति सव्वपावकम्मेहिं विरए) पूर्वोक्त पन्द्रह अध्ययनों में जो उपदेश किया है, उसके अनुसार आचरण करनेवाला जो पुरुष सब पापों से हटा हुआ है (पिज्जदोसकलहअब्मक्खाण पेसुन्न परपरिवाय अरतिरति मायामोस मिच्छादंसणसत्तविरए) तथा किसी से रागद्वेष नहीं करता है, किसी से कलह नहीं करता है, किसी पर झूठा दोष नहीं लगाता है, किसी की चुगुली नहीं करता है, किसी की निन्दा नहीं करता है एवं संयम में अप्रेम और असंयम में प्रेम नहीं करता है, कपट नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, मिथ्यादर्शनशल्य से अलग रहता है ( समिए सहिए सया जए णो कुज्झे णो माणी माहणेत्ति वच्चे) पाँच गुप्तिओं से गुप्त और ज्ञानादि गुणों से सहित, सदा इन्द्रियों को जीतनेवाला किसी पर क्रोध नहीं करता है, मान नहीं करता है वह, माहन कहने योग्य है ।
६२६