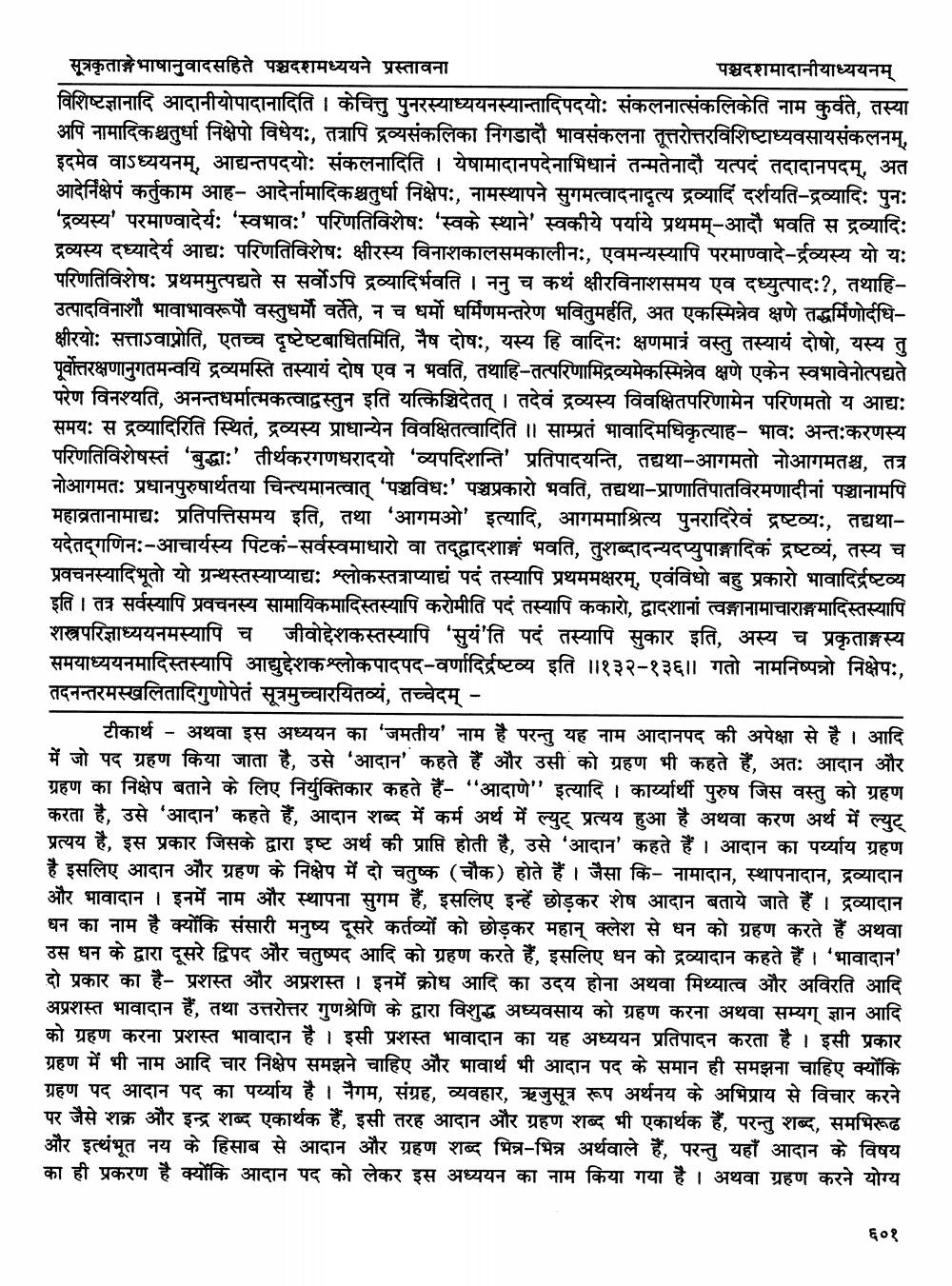________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते पञ्चदशमध्ययने प्रस्तावना
पञ्चदशमादानीयाध्ययनम् विशिष्टज्ञानादि आदानीयोपादानादिति । केचित्तु पुनरस्याध्ययनस्यान्तादिपदयोः संकलनात्संकलिकेति नाम कुर्वते, तस्या अपि नामादिकश्चतुर्धा निक्षेपो विधेयः, तत्रापि द्रव्यसंकलिका निगडादौ भावसंकलना तूत्तरोत्तरविशिष्टाध्यवसायसंकलनम्, इदमेव वाऽध्ययनम्, आद्यन्तपदयोः संकलनादिति । येषामादानपदेनाभिधानं तन्मतेनादौ यत्पदं तदादानपदम्, अत आदेनिक्षेपं कर्तुकाम आह- आदेर्नामादिकश्चतुर्धा निक्षेपः, नामस्थापने सुगमत्वादनादृत्य द्रव्यादि दर्शयति-द्रव्यादिः पुनः 'द्रव्यस्य' परमाण्वादेर्यः ‘स्वभावः' परिणतिविशेषः 'स्वके स्थाने' स्वकीये पर्याये प्रथमम्-आदौ भवति स द्रव्यादिः द्रव्यस्य दध्यादेर्य आद्यः परिणतिविशेषः क्षीरस्य विनाशकालसमकालीनः, एवमन्यस्यापि परमाण्वादे-द्रव्यस्य यो यः परिणतिविशेषः प्रथममुत्पद्यते स सर्वोऽपि द्रव्यादिर्भवति । ननु च कथं क्षीरविनाशसमय एव दध्युत्पादः?, तथाहिउत्पादविनाशौ भावाभावरूपौ वस्तुधर्मो वर्तेते, न च धर्मो धर्मिणमन्तरेण भवितुमर्हति, अत एकस्मिन्नेव क्षणे तद्धर्मिणोर्दधिक्षीरयोः सत्ताऽवाप्नोति, एतच्च दृष्टेष्टबाधितमिति, नैष दोषः, यस्य हि वादिनः क्षणमात्र वस्तु तस्यायं दोषो, यस्य तु पूर्वोत्तरक्षणानुगतमन्वयि द्रव्यमस्ति तस्यायं दोष एव न भवति, तथाहि-तत्परिणामिद्रव्यमेकस्मिन्नेव क्षणे एकेन स्वभावेनोत्पद्यते परेण विनश्यति, अनन्तधर्मात्मकत्वाद्वस्तुन इति यत्किञ्चिदेतत् । तदेवं द्रव्यस्य विवक्षितपरिणामेन परिणमतो य आद्यः समयः स द्रव्यादिरिति स्थितं, द्रव्यस्य प्राधान्येन विवक्षितत्वादिति ॥ साम्प्रतं भावादिमधिकृत्याह- भावः अन्तःकरणस्य परिणतिविशेषस्तं 'बुद्धाः' तीर्थकरगणधरादयो 'व्यपदिशन्ति' प्रतिपादयन्ति, तद्यथा-आगमतो नोआगमतश्च, तत्र नोआगमतः प्रधानपुरुषार्थतया चिन्त्यमानत्वात् 'पञ्चविधः' पञ्चप्रकारो भवति, तद्यथा-प्राणातिपातविरमणादीनां पञ्चानामपि महाव्रतानामाद्यः प्रतिपत्तिसमय इति, तथा 'आगमओ' इत्यादि, आगममाश्रित्य पुनरादिरेवं द्रष्टव्यः, तद्यथायदेतद्गणिन:-आचार्यस्य पिटकं-सर्वस्वमाधारो वा तद्द्वादशाङ्गं भवति, तुशब्दादन्यदप्युपाङ्गादिकं द्रष्टव्यं, तस्य च प्रवचनस्यादिभूतो यो ग्रन्थस्तस्याप्याद्यः श्लोकस्तत्राप्याद्यं पदं तस्यापि प्रथममक्षरम्, एवंविधो बहु प्रकारो भावादिर्द्रष्टव्य इति । तत्र सर्वस्यापि प्रवचनस्य सामायिकमादिस्तस्यापि करोमीति पदं तस्यापि ककारो, द्वादशानां त्वङ्गानामाचाराङ्गमादिस्तस्यापि शस्त्रपरिज्ञाध्ययनमस्यापि च जीवोद्देशकस्तस्यापि 'सुर्य'ति पदं तस्यापि सुकार इति, अस्य च प्रकृताङ्गस्य समयाध्ययनमादिस्तस्यापि आधुद्देशकश्लोकपादपद-वर्णादिष्टव्य इति ॥१३२-१३६।। गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः, तदनन्तरमस्खलितादिगुणोपेतं सूत्रमुच्चारयितव्यं, तच्चेदम् -
टीकार्थ - अथवा इस अध्ययन का 'जमतीय' नाम है परन्तु यह नाम आदानपद की अपेक्षा से है। आदि में जो पद ग्रहण किया जाता है, उसे 'आदान' कहते हैं और उसी को ग्रहण भी कहते हैं, अतः आदान और ग्रहण का निक्षेप बताने के लिए नियुक्तिकार कहते हैं- "आदाणे" इत्यादि । कार्यार्थी पुरुष जिस वस्तु को ग्रहण करता है, उसे 'आदान' कहते हैं, आदान शब्द में कर्म अर्थ में ल्युट् प्रत्यय हुआ है अथवा करण अर्थ में ल्युट् प्रत्यय है, इस प्रकार जिसके द्वारा इष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे 'आदान' कहते हैं । आदान का पर्याय ग्रहण है इसलिए आदान और ग्रहण के निक्षेप में दो चतुष्क (चौक) होते हैं। जैसा कि- नामादान, स्थापनादान, द्रव्यादान और भावादान । इनमें नाम और स्थापना सुगम हैं, इसलिए इन्हें छोड़कर शेष आदान बताये जाते हैं । द्रव्यादान धन का नाम है क्योंकि संसारी मनुष्य दूसरे कर्तव्यों को छोड़कर महान् क्लेश से धन को ग्रहण करते हैं अथवा उस धन के द्वारा दूसरे द्विपद और चतुष्पद आदि को ग्रहण करते हैं, इसलिए धन को द्रव्यादान कहते हैं । 'भावादान' दो प्रकार का है- प्रशस्त और अप्रशस्त । इनमें क्रोध आदि का उदय होना अथवा मिथ्यात्व और अविरति आदि अप्रशस्त भावादान हैं, तथा उत्तरोत्तर गुणश्रेणि के द्वारा विशुद्ध अध्यवसाय को ग्रहण करना अथवा सम्यग् ज्ञान आदि को ग्रहण करना प्रशस्त भावादान है। इसी प्रशस्त भावादान का यह अध्ययन प्रतिपादन करता है। इसी प्रकार ग्रहण में भी नाम आदि चार निक्षेप समझने चाहिए और भावार्थ भी आदान पद के समान ही समझना चाहिए क्योंकि ग्रहण पद आदान पद का पर्याय है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र रूप अर्थनय के अभिप्राय से विचार करने पर जैसे शक्र और इन्द्र शब्द एकार्थक हैं, इसी तरह आदान और ग्रहण शब्द भी एकार्थक हैं, परन्तु शब्द, समभिरूढ और इत्थंभूत नय के हिसाब से आदान और ग्रहण शब्द भिन्न-भिन्न अर्थवाले हैं, परन्तु यहाँ आदान के विषय का ही प्रकरण है क्योंकि आदान पद को लेकर इस अध्ययन का नाम किया गया है। अथवा ग्रहण करने योग्य
६०१