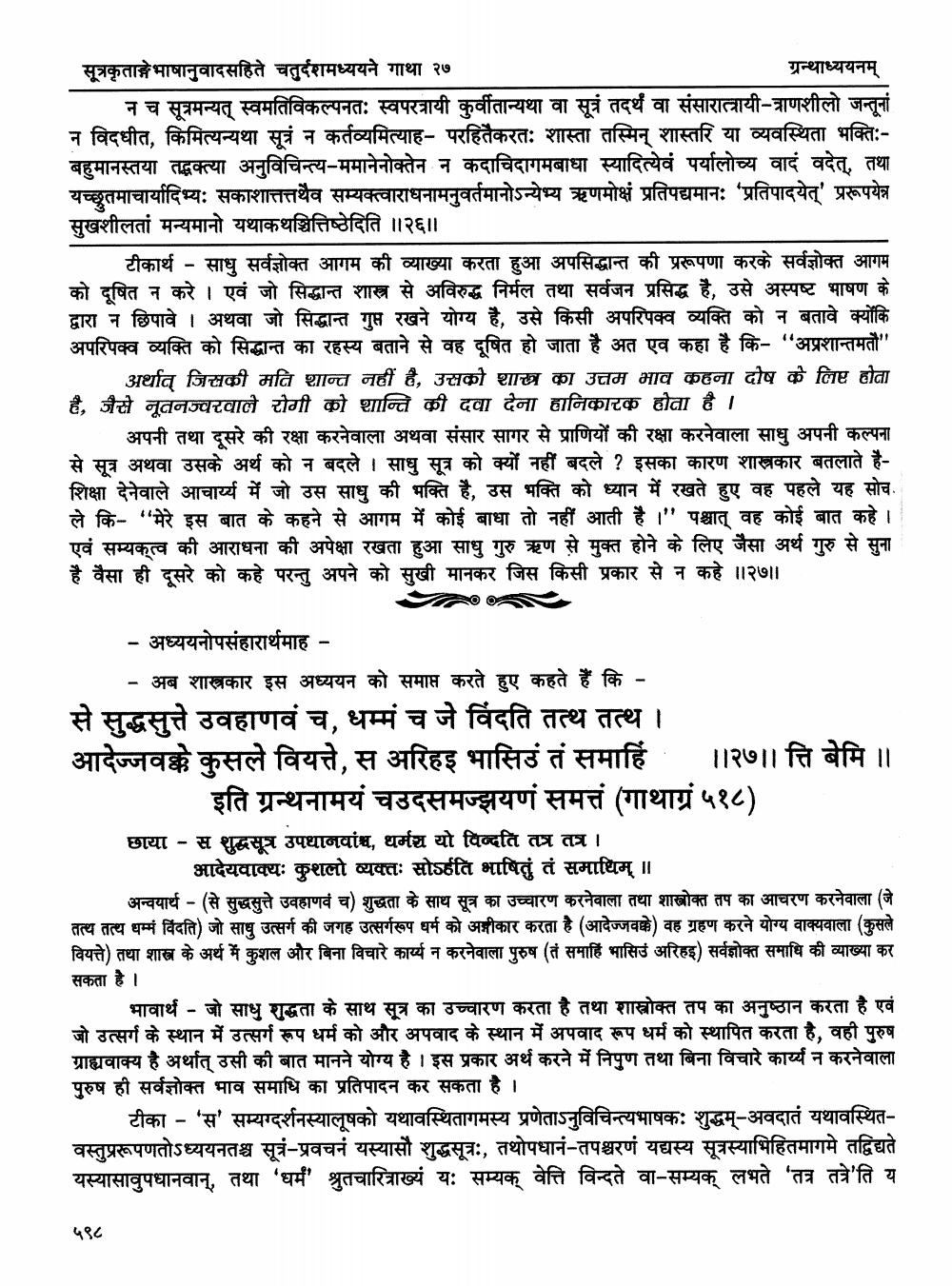________________
सूत्रकृताङ्गे भाषानुवादसहिते चतुर्दशमध्ययने गाथा २७
ग्रन्थाध्ययनम्
न च सूत्रमन्यत् स्वमतिविकल्पनतः स्वपरत्रायी कुर्वीतान्यथा वा सूत्रं तदर्थं वा संसारात्त्रायी - त्राणशीलो जन्तूनां न विदधीत, किमित्यन्यथा सूत्रं न कर्तव्यमित्याह - परहितैकरतः शास्ता तस्मिन् शास्तरि या व्यवस्थिता भक्ति:बहुमानस्तया तद्भक्त्या अनुविचिन्त्य - ममानेनोक्तेन न कदाचिदागमबाधा स्यादित्येवं पर्यालोच्य वादं वदेत्, तथा यच्छ्रुतमाचार्यादिभ्यः सकाशात्तत्तथैव सम्यक्त्वाराधनामनुवर्तमानोऽन्येभ्य ऋणमोक्षं प्रतिपद्यमानः 'प्रतिपादयेत्' प्ररूपयेन्न सुखशीलतां मन्यमानो यथाकथञ्चित्तिष्ठेदिति ॥ २६॥
-
टीकार्थ साधु सर्वज्ञोक्त आगम की व्याख्या करता हुआ अपसिद्धान्त की प्ररूपणा करके सर्वज्ञोक्त आगम को दूषित न करे । एवं जो सिद्धान्त शास्त्र से अविरुद्ध निर्मल तथा सर्वजन प्रसिद्ध है, उसे अस्पष्ट भाषण के द्वारा न छिपावे । अथवा जो सिद्धान्त गुप्त रखने योग्य है, उसे किसी अपरिपक्व व्यक्ति को न बतावे क्योंकि अपरिपक्व व्यक्ति को सिद्धान्त का रहस्य बताने से वह दूषित हो जाता अत एव कहा कि- "अप्रशान्तमतौ"
अर्थात् जिसकी मति शान्त नहीं है, उसको शास्त्र का उत्तम भाव कहना दोष के लिए होता है, जैसे नूतनज्वरवाले रोगी को शान्ति की दवा देना हानिकारक होता है ।
अपनी तथा दूसरे की रक्षा करनेवाला अथवा संसार सागर से प्राणियों की रक्षा करनेवाला साधु अपनी कल्पना से सूत्र अथवा उसके अर्थ को न बदले । साधु सूत्र को क्यों नहीं बदले ? इसका कारण शास्त्रकार बतलाते हैशिक्षा देनेवाले आचार्य्य में जो उस साधु की भक्ति है, उस भक्ति को ध्यान में रखते हुए वह पहले यह सोच. ले कि- "मेरे इस बात के कहने से आगम में कोई बाधा तो नहीं आती है ।" पश्चात् वह कोई बात कहे । एवं सम्यक्त्व की आराधना की अपेक्षा रखता हुआ साधु गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए जैसा अर्थ गुरु से सुना है वैसा ही दूसरे को कहे परन्तु अपने को सुखी मानकर जिस किसी प्रकार से न कहे ||२७||
अध्ययनोपसंहारार्थमाह
अब शास्त्रकार इस अध्ययन को समाप्त करते हुए कहते हैं कि से सुद्धसुत्ते उवहाणवं च, धम्मं च जे विंदति तत्थ तत्थ । आदेज्जवक्के कुसले वियत्ते, स अरिहइ भासिउं तं समाहिं
।। २७ ।। त्ति बेमि ॥ इति ग्रन्थनामयं चउदसमज्झयणं समत्तं (गाथाग्रं ५१८ ) छाया - स शुद्धसूत्र उपधानवांश्च, धर्मश यो विन्दति तत्र तत्र । आदेयवाक्यः कुशलो व्यक्तः सोऽर्हति भाषितुं तं समाधिम् ॥
अन्वयार्थ - (से सुद्धसुत्ते उवहाणवं च ) शुद्धता के साथ सूत्र का उच्चारण करनेवाला तथा शास्त्रोक्त तप का आचरण करनेवाला (जे तत्थ तत्थ धम्मं विंदति) जो साधु उत्सर्ग की जगह उत्सर्गरूप धर्म को अङ्गीकार करता है (आदेज्जवक्के) वह ग्रहण करने योग्य वाक्यवाला (कुसले वियत्ते) तथा शास्त्र के अर्थ में कुशल और बिना विचारे कार्य्य न करनेवाला पुरुष ( तं समाहिं भासिउं अरिहइ) सर्वज्ञोक्त समाधि की व्याख्या कर सकता है ।
-
-
५९८
-
-
भावार्थ जो साधु शुद्धता के साथ सूत्र का उच्चारण करता है तथा शास्त्रोक्त तप का अनुष्ठान करता है एवं जो उत्सर्ग के स्थान में उत्सर्ग रूप धर्म को और अपवाद के स्थान में अपवाद रूप धर्म को स्थापित करता है, वही पुरुष ग्राह्यवाक्य है अर्थात् उसी की बात मानने योग्य है। इस प्रकार अर्थ करने में निपुण तथा बिना विचारे कार्य्यं न करनेवाला पुरुष ही सर्वज्ञोक्त भाव समाधि का प्रतिपादन कर सकता है ।
टीका- 'स' सम्यग्दर्शनस्यालूषको यथावस्थितागमस्य प्रणेताऽनुविचिन्त्यभाषकः शुद्धम् अवदातं यथावस्थितवस्तुप्ररूपणतोऽध्ययनतश्च सूत्रं - प्रवचनं यस्यासौ शुद्धसूत्रः, तथोपधानं - तपश्चरणं यद्यस्य सूत्रस्याभिहितमागमे तद्विद्य यस्यासावुपधानवान्, तथा 'धर्म' श्रुतचारित्राख्यं यः सम्यक् वेत्ति विन्दते वा सम्यक् लभते 'तत्र तत्रे'ति य