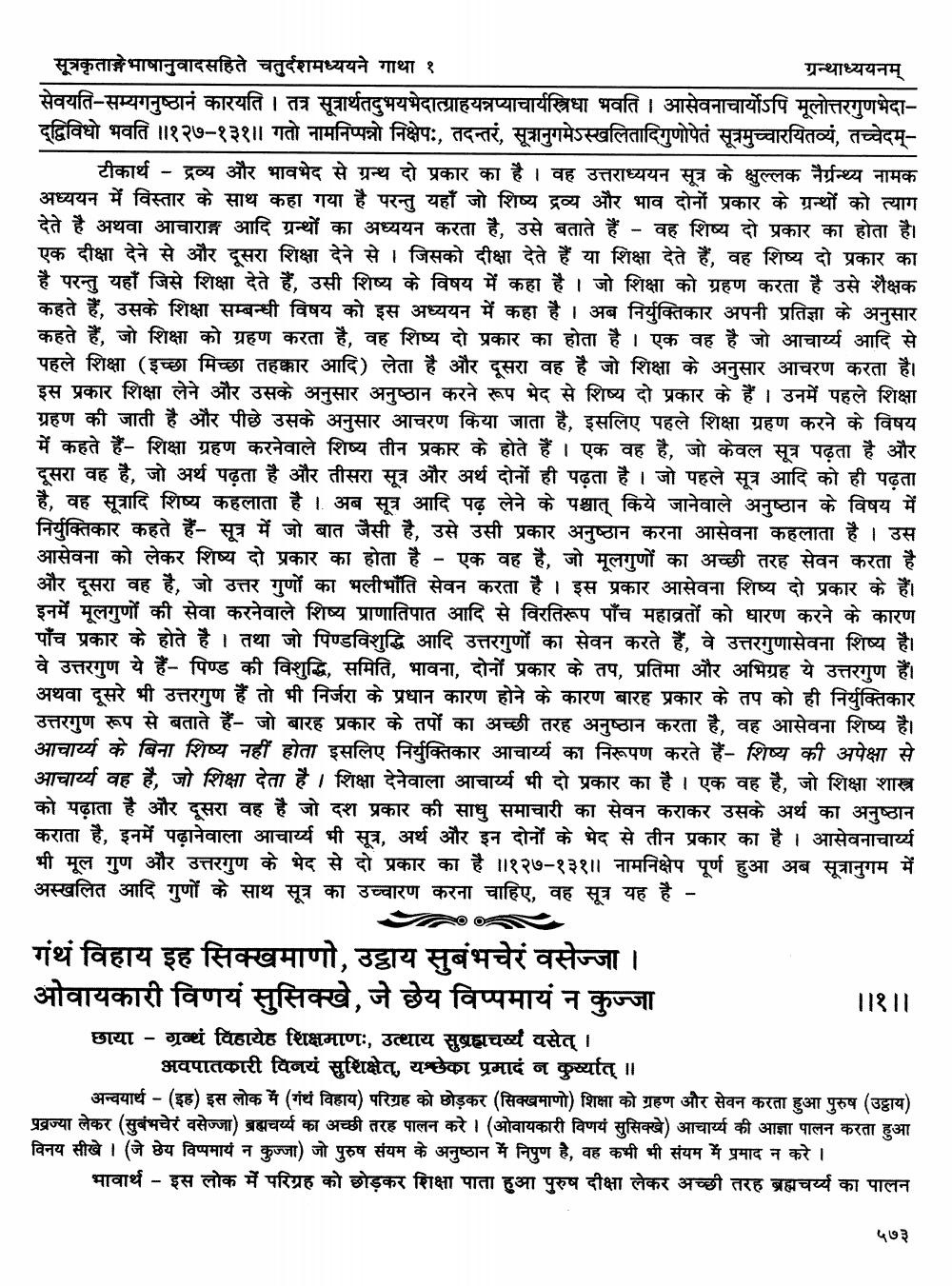________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते चतुर्दशमध्ययने गाथा १
ग्रन्थाध्ययनम् सेवयति-सम्यगनुष्ठानं कारयति । तत्र सूत्रार्थतदुभयभेदात्ग्राहयनप्याचार्यस्त्रिधा भवति । आसेवनाचार्योऽपि मूलोत्तरगुणभेदाद्विविधो भवति ॥१२७-१३१।। गतो नामनिप्पन्नो निक्षेपः, तदन्तरं, सूत्रानुगमेऽस्खलितादिगुणोपेतं सूत्रमुच्चारयितव्यं, तच्चेदम्
टीकार्थ - द्रव्य और भावभेद से ग्रन्थ दो प्रकार का है। वह उत्तराध्ययन सूत्र के क्षुल्लक नैर्ग्रन्थ्य नामक अध्ययन में विस्तार के साथ कहा गया है परन्तु यहाँ जो शिष्य द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के ग्रन्थों को त्याग देते है अथवा आचाराङ्ग आदि ग्रन्थों का अध्ययन करता है, उसे बताते हैं - वह शिष्य दो प्रकार का होता है। एक दीक्षा देने से और दूसरा शिक्षा देने से । जिसको दीक्षा देते हैं या शिक्षा देते हैं, वह शिष्य दो प्रकार का है परन्तु यहाँ जिसे शिक्षा देते हैं, उसी शिष्य के विषय में कहा है । जो शिक्षा को ग्रहण करता है उसे शैक्षक कहते हैं, उसके शिक्षा सम्बन्धी विषय को इस अध्ययन में कहा है। अब निर्यक्तिकार अपनी प्रति कहते हैं, जो शिक्षा को ग्रहण करता है, वह शिष्य दो प्रकार का होता है । एक वह है जो आचार्य आदि से पहले शिक्षा (इच्छा मिच्छा तहक्कार आदि) लेता है और दूसरा वह है जो शिक्षा के अनुसार आचरण करता है। इस प्रकार शिक्षा लेने और उसके अनुसार अनुष्ठान करने रूप भेद से शिष्य दो प्रकार के हैं। उनमें पहले शिक्षा ग्रहण की जाती है और पीछे उसके अनुसार आचरण किया जाता है, इसलिए पहले शिक्षा ग्रहण करने के विषय में कहते हैं- शिक्षा ग्रहण करनेवाले शिष्य तीन प्रकार के होते हैं । एक वह है, जो केवल सूत्र पढ़ता है और दूसरा वह है, जो अर्थ पढ़ता है और तीसरा सूत्र और अर्थ दोनों ही पढ़ता है । जो पहले सूत्र आदि को ही पढ़ता है, वह सूत्रादि शिष्य कहलाता है । अब सूत्र आदि पढ़ लेने के पश्चात् किये जानेवाले अनुष्ठान के विषय में नियुक्तिकार कहते हैं- सूत्र में जो बात जैसी है, उसे उसी प्रकार अनुष्ठान करना आसेवना कहलाता है। उस आसेवना को लेकर शिष्य दो प्रकार का होता है - एक वह है, जो मूलगुणों का अच्छी तरह सेवन करता है
और दूसरा वह है, जो उत्तर गुणों का भलीभाँति सेवन करता है । इस प्रकार आसेवना शिष्य दो प्रकार के हैं। इनमें मूलगुणों की सेवा करनेवाले शिष्य प्राणातिपात आदि से विरतिरूप पाँच महाव्रतों को धारण करने के कारण पाँच प्रकार के होते है । तथा जो पिण्डविशुद्धि आदि उत्तरगुणों का सेवन करते हैं, वे उत्तरगुणासेवना शिष्य है। वे उत्तरगुण ये हैं- पिण्ड की विशुद्धि, समिति, भावना, दोनों प्रकार के तप, प्रतिमा और अभिग्रह ये उत्तरगुण हैं। अथवा दूसरे भी उत्तरगुण हैं तो भी निर्जरा के प्रधान कारण होने के कारण बारह प्रकार के तप को ही नियुक्तिकार उत्तरगुण रूप से बताते हैं- जो बारह प्रकार के तपों का अच्छी तरह अनुष्ठान करता है, वह आसेवना शिष्य है। आचार्य के बिना शिष्य नहीं होता इसलिए नियुक्तिकार आचार्य का निरूपण करते हैं- शिष्य की अपेक्षा से आचार्य्य वह है, जो शिक्षा देता है। शिक्षा देनेवाला आचार्य भी दो प्रकार का है। एक वह है, जो शिक्षा शास्त्र को पढ़ाता है और दूसरा वह है जो दश प्रकार की साधु समाचारी का सेवन कराकर उसके अर्थ का अनुष्ठान कराता है, इनमें पढ़ानेवाला आचार्य भी सूत्र, अर्थ और इन दोनों के भेद से तीन प्रकार का है। आसेवनाचार्य भी मूल गुण और उत्तरगुण के भेद से दो प्रकार का है ॥१२७-१३१॥ नामनिक्षेप पूर्ण हुआ अब सूत्रानुगम में अस्खलित आदि गुणों के साथ सूत्र का उच्चारण करना चाहिए, वह सूत्र यह है -
गंथं विहाय इह सिक्खमाणो, उट्ठाय सुबंभचेरं वसेज्जा । ओवायकारी विणयं सुसिक्खे, जे छेय विप्पमायं न कुज्जा
॥१॥ छाया - ग्रन्थं विहायेह शिक्षमाणः, उत्थाय सुब्रह्मचयं वसेत् ।
अवपातकारी विनयं सुशिक्षेत्, यश्छेका प्रमादं न कुर्य्यात् ।। अन्वयार्थ - (इह) इस लोक में (गंथं विहाय) परिग्रह को छोड़कर (सिक्खमाणो) शिक्षा को ग्रहण और सेवन करता हुआ पुरुष (उठाय) प्रव्रज्या लेकर (सुबंभचेरं वसेज्जा) ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह पालन करे । (ओवायकारी विणयं सुसिक्खे) आचार्य की आज्ञा पालन करता हुआ विनय सीखे । (जे छेय विष्पमायं न कुज्जा) जो पुरुष संयम के अनुष्ठान में निपुण है, वह कभी भी संयम में प्रमाद न करे ।
भावार्थ - इस लोक में परिग्रह को छोड़कर शिक्षा पाता हुआ पुरुष दीक्षा लेकर अच्छी तरह ब्रह्मचर्य का पालन
५७३