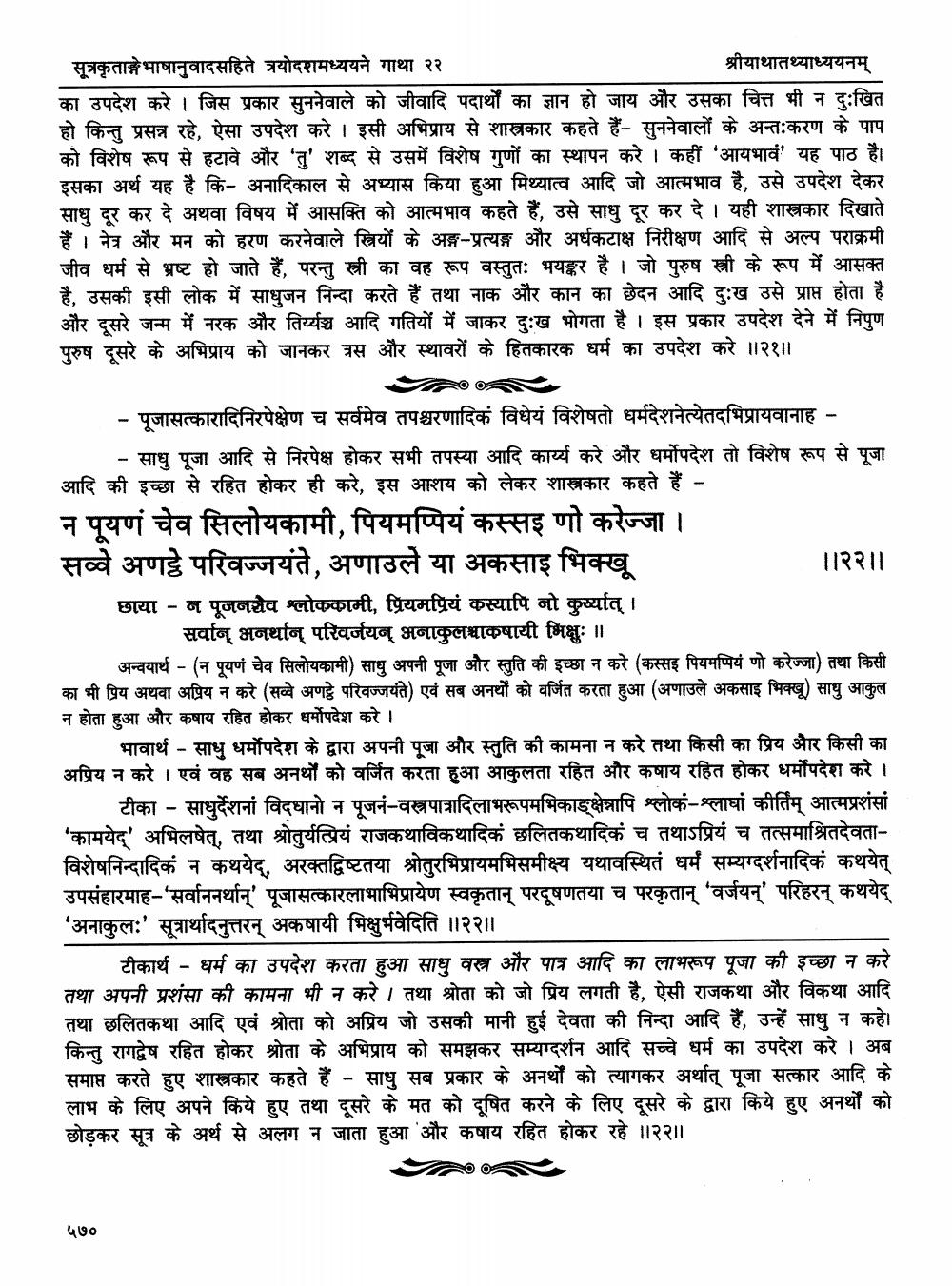________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते त्रयोदशमध्ययने गाथा २२
श्रीयाथातथ्याध्ययनम् का उपदेश करे । जिस प्रकार सुननेवाले को जीवादि पदार्थों का ज्ञान हो जाय और उसका चित्त भी न दुःखित हो किन्तु प्रसन्न रहे, ऐसा उपदेश करे । इसी अभिप्राय से शास्त्रकार कहते हैं- सुननेवालों के अन्तःकरण के पाप को विशेष रूप से हटावे और 'तु' शब्द से उसमें विशेष गुणों का स्थापन करे । कहीं 'आयभावं' यह पाठ है। इसका अर्थ यह है कि- अनादिकाल से अभ्यास किया हुआ मिथ्यात्व आदि जो आत्मभाव है, उसे उपदेश देकर साधु दूर कर दे अथवा विषय में आसक्ति को आत्मभाव कहते हैं, उसे साधु दूर कर दे । यही शास्त्रकार दिखाते हैं । नेत्र और मन को हरण करनेवाले स्त्रियों के अङ्ग-प्रत्यङ्ग और अर्धकटाक्ष निरीक्षण आदि से अल्प पराक्रमी जीव धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, परन्तु स्त्री का वह रूप वस्तुतः भयङ्कर है । जो पुरुष स्त्री के रूप में आसक्त है, उसकी इसी लोक में साधुजन निन्दा करते हैं तथा नाक और कान का छेदन आदि दुःख उसे प्राप्त होता है
और दूसरे जन्म में नरक और तिर्यश्च आदि गतियों में जाकर दुःख भोगता है । इस प्रकार उपदेश देने में निपुण पुरुष दूसरे के अभिप्राय को जानकर त्रस और स्थावरों के हितकारक धर्म का उपदेश करे ॥२१॥
- पूजासत्कारादिनिरपेक्षेण च सर्वमेव तपश्चरणादिकं विधेयं विशेषतो धर्मदेशनेत्येतदभिप्रायवानाह -
- साधु पूजा आदि से निरपेक्ष होकर सभी तपस्या आदि कार्य करे और धर्मोपदेश तो विशेष रूप से पूजा आदि की इच्छा से रहित होकर ही करे, इस आशय को लेकर शास्त्रकार कहते हैं - न पूयणं चेव सिलोयकामी, पियमप्पियं कस्सइ णो करेज्जा। सव्वे अणटे परिवज्जयंते, अणाउले या अकसाइ भिक्खू
|॥२२॥ छाया - न पूजनशेव श्लोककामी, प्रियमप्रियं कस्यापि नो कुर्यात् ।
सर्वान् अनर्थान् परिवर्जयन् अनाकुलश्चाकषायी भिक्षुः । अन्वयार्थ - (न पूयणं चेव सिलोयकामी) साधु अपनी पूजा और स्तुति की इच्छा न करे (कस्सइ पियमप्पियं णो करेज्जा) तथा किसी का भी प्रिय अथवा अप्रिय न करे (सव्वे अणट्टे परिवज्जयंते) एवं सब अनर्थों को वर्जित करता हुआ (अणाउले अकसाइ भिक्खू) साधु आकुल न होता हुआ और कषाय रहित होकर धर्मोपदेश करे ।
भावार्थ - साधु धर्मोपदेश के द्वारा अपनी पूजा और स्तुति की कामना न करे तथा किसी का प्रिय और किसी का अप्रिय न करे । एवं वह सब अनथों को वर्जित करता हुआ आकुलता रहित और कषाय रहित होकर धर्मोपदेश करे ।
टीका - साधुर्देशनां विदधानो न पूजन-वस्त्रपात्रादिलाभरूपमभिकाक्षेन्नापि श्लोकं-श्लाघां कीर्तिम् आत्मप्रशंसां 'कामयेद्' अभिलषेत्, तथा श्रोतुर्यत्प्रियं राजकथाविकथादिकं छलितकथादिकं च तथाऽप्रियं च तत्समाश्रितदेवताविशेषनिन्दादिकं न कथयेद्, अरक्तद्विष्टतया श्रोतुरभिप्रायमभिसमीक्ष्य यथावस्थितं धर्म सम्यग्दर्शनादिकं कथयेत् उपसंहारमाह-'सर्वाननर्थान्' पूजासत्कारलाभाभिप्रायेण स्वकृतान् परदूषणतया च परकृतान् ‘वर्जयन्' परिहरन् कथयेद् 'अनाकुलः' सूत्रार्थादनुत्तरन् अकषायी भिक्षुर्भवेदिति ॥२२॥
टीकार्थ - धर्म का उपदेश करता हुआ साधु वस्त्र और पात्र आदि का लाभरूप पूजा की इच्छा न करे तथा अपनी प्रशंसा की कामना भी न करे । तथा श्रोता को जो प्रिय लगती है, ऐसी राजकथा और विकथा आदि तथा छलितकथा आदि एवं श्रोता को अप्रिय जो उसकी मानी हुई देवता की निन्दा आदि हैं, उन्हें साधु न कहे। किन्तु रागद्वेष रहित होकर श्रोता के अभिप्राय को समझकर सम्यग्दर्शन आदि सच्चे धर्म का उपदेश करे । अब समाप्त करते हुए शास्त्रकार कहते हैं - साधु सब प्रकार के अनर्थों को त्यागकर अर्थात् पूजा सत्कार आदि के
| के लिए अपने किये हुए तथा दूसरे के मत को दूषित करने के लिए दूसरे के द्वारा किये हुए अनर्थों को छोड़कर सूत्र के अर्थ से अलग न जाता हुआ और कषाय रहित होकर रहे ॥२२॥
५७०