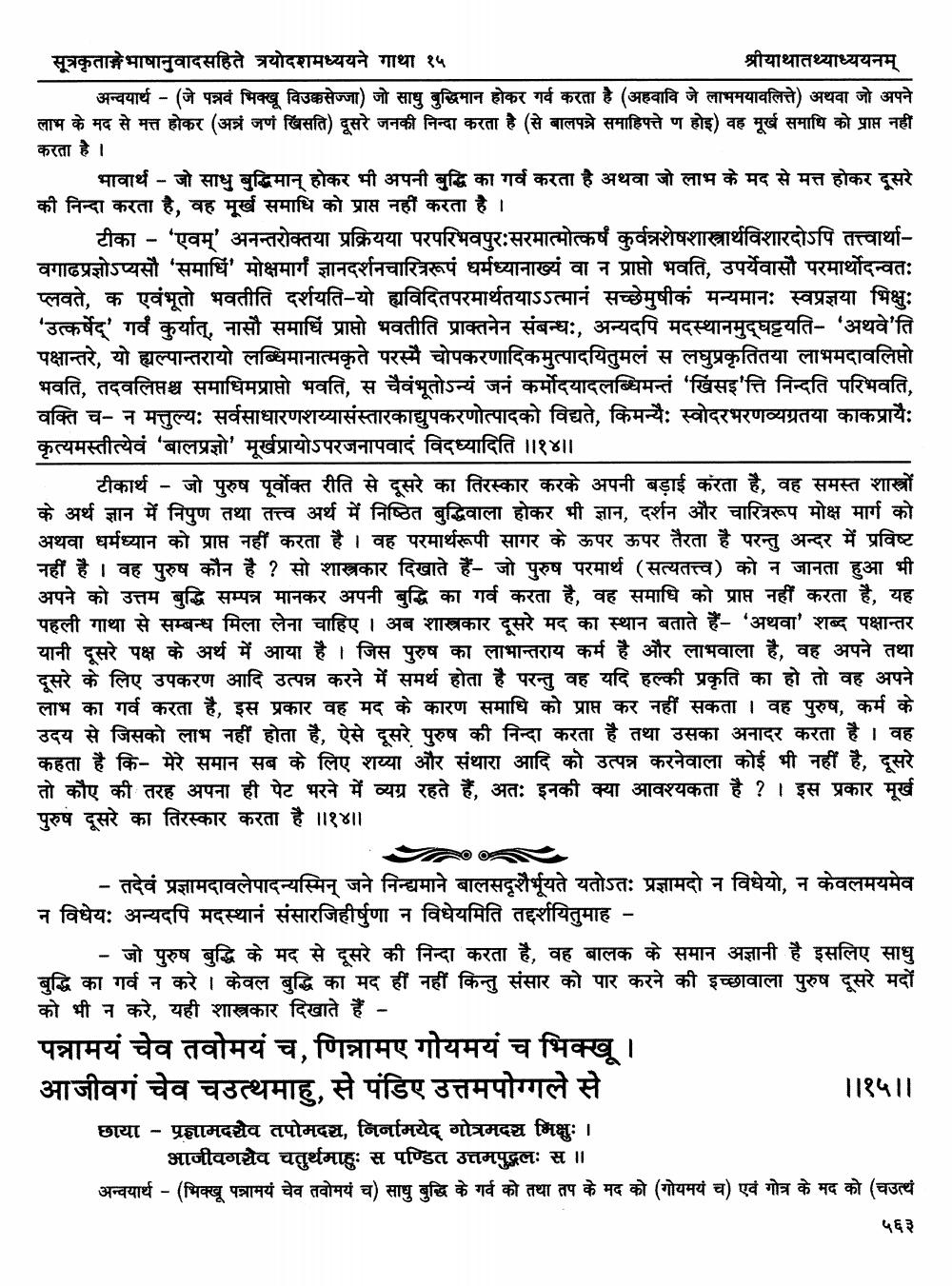________________
सूत्रकृताङ्गे भाषानुवादसहिते त्रयोदशमध्ययने गाथा १५
श्रीयाथातथ्याध्ययनम्
अन्वयार्थ - (जे पन्नवं भिक्खू विउक्कसेज्जा) जो साधु बुद्धिमान होकर गर्व करता है ( अहवावि जे लाभमयावलित्ते) अथवा जो अपने लाभ के मद से मत्त होकर (अन्नं जणं खिंसति) दूसरे जनकी निन्दा करता है ( से बालपन्ने समाहिपत्ते ण होइ) वह मूर्ख समाधि को प्राप्त नहीं करता है ।
भावार्थ - जो साधु बुद्धिमान् होकर भी अपनी बुद्धि का गर्व करता है अथवा जो लाभ के मद से मत्त होकर दूसरे की निन्दा करता है, वह मूर्ख समाधि को प्राप्त नहीं करता है ।
टीका – 'एवम्' अनन्तरोक्तया प्रक्रियया परपरिभवपुर : सरमात्मोत्कर्षं कुर्वन्नशेषशास्त्रार्थविशारदोऽपि तत्त्वार्थावगाढप्रज्ञोऽप्यसौ ‘समाधिं' मोक्षमार्गं ज्ञानदर्शनचारित्ररूपं धर्मध्यानाख्यं वा न प्राप्तो भवति, उपर्येवासौ परमार्थोदन्वतः प्लवते, क एवंभूतो भवतीति दर्शयति-यो ह्यविदितपरमार्थतयाऽऽत्मानं सच्छेमुषीकं मन्यमानः स्वप्रज्ञया भिक्षुः 'उत्कर्षेद्' गर्वं कुर्यात्, नासौ समाधिं प्राप्तो भवतीति प्राक्तनेन संबन्ध:, अन्यदपि मदस्थानमुद्घट्टयति- ' अथवे 'ति पक्षान्तरे, यो ह्यल्पान्तरायो लब्धिमानात्मकृते परस्मै चोपकरणादिकमुत्पादयितुमलं स लघुप्रकृतितया लाभमदावलिप्तो भवति, तदवलिप्तश्च समाधिमप्राप्तो भवति, स चैवंभूतोऽन्यं जनं कर्मोदयादलब्धिमन्तं 'खिसइ 'त्ति निन्दति परिभवति, वक्ति च- न मत्तुल्यः सर्वसाधारणशय्यासंस्तारकाद्युपकरणोत्पादको विद्यते, किमन्यैः स्वोदरभरणव्यग्रतया काकप्रायैः कृत्यमस्तीत्येवं 'बालप्रज्ञो' मूर्खप्रायोऽपरजनापवादं विदध्यादिति ||१४||
टीकार्थ जो पुरुष पूर्वोक्त रीति से दूसरे का तिरस्कार करके अपनी बड़ाई करता है, वह समस्त शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण तथा तत्त्व अर्थ में निष्ठित बुद्धिवाला होकर भी ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप मोक्ष मार्ग को अथवा धर्मध्यान को प्राप्त नहीं करता है । वह परमार्थरूपी सागर के ऊपर ऊपर तैरता है परन्तु अन्दर में प्रविष्ट नहीं है । वह पुरुष कौन है ? सो शास्त्रकार दिखाते हैं- जो पुरुष परमार्थ (सत्यतत्त्व) को न जानता हुआ भी अपने को उत्तम बुद्धि सम्पन्न मानकर अपनी बुद्धि का गर्व करता है, वह समाधि को प्राप्त नहीं करता है, यह पहली गाथा से सम्बन्ध मिला लेना चाहिए । अब शास्त्रकार दूसरे मद का स्थान बताते हैं- ' अथवा ' शब्द पक्षान्तर यानी दूसरे पक्ष के अर्थ में आया है। जिस पुरुष का लाभान्तराय कर्म है और लाभवाला है, वह अपने तथा दूसरे लिए उपकरण आदि उत्पन्न करने में समर्थ होता है परन्तु वह यदि हल्की प्रकृति का हो तो वह अपने लाभ का गर्व करता है, इस प्रकार वह मद के कारण समाधि को प्राप्त कर नहीं सकता । वह पुरुष, कर्म के उदय से जिसको लाभ नहीं होता है, ऐसे दूसरे पुरुष की निन्दा करता है तथा उसका अनादर करता है । वह कहता है कि- मेरे समान सब के लिए शय्या और संथारा आदि को उत्पन्न करनेवाला कोई भी नहीं है, दूसरे तो कौए की तरह अपना ही पेट भरने में व्यग्र रहते हैं, अतः इनकी क्या आवश्यकता है ? । इस प्रकार मूर्ख पुरुष दूसरे का तिरस्कार करता है || १४ ||
-
तदेवं प्रज्ञामदावलेपादन्यस्मिन् जने निन्द्यमाने बालसदृशैर्भूयते यतोऽतः प्रज्ञामदो न विधेयो, न केवलमयमेव न विधेयः अन्यदपि मदस्थानं संसारजिहीर्षुणा न विधेयमिति तद्दर्शयितुमाह
जो पुरुष बुद्धि के मद से दूसरे की निन्दा करता है, वह बालक के समान अज्ञानी है इसलिए साधु बुद्धि का गर्व न करे । केवल बुद्धि का मद हीं नहीं किन्तु संसार को पार करने की इच्छावाला पुरुष दूसरे मदों को भी न करे, यही शास्त्रकार दिखाते हैं
-
पन्नामयं चेव तवोमयं च णिन्नामए गोयमयं च भिक्खू ।
आजीवगं चेव चउत्थमाहु, से पंडिए उत्तमपोग्गले से
छाया -
।।१५।।
प्रज्ञामदञ्चैव तपोमदश, निर्नामयेद् गोत्रमदश भिक्षुः । आजीवगशैव चतुर्थमाहुः स पण्डित उत्तमपुद्गलः स ॥
अन्वयार्थ – (भिक्खू पन्नामयं चेव तवोमयं च ) साधु बुद्धि के गर्व को तथा तप के मद को (गोयमयं च ) एवं गोत्र के मद को (चउत्थं
-
५६३