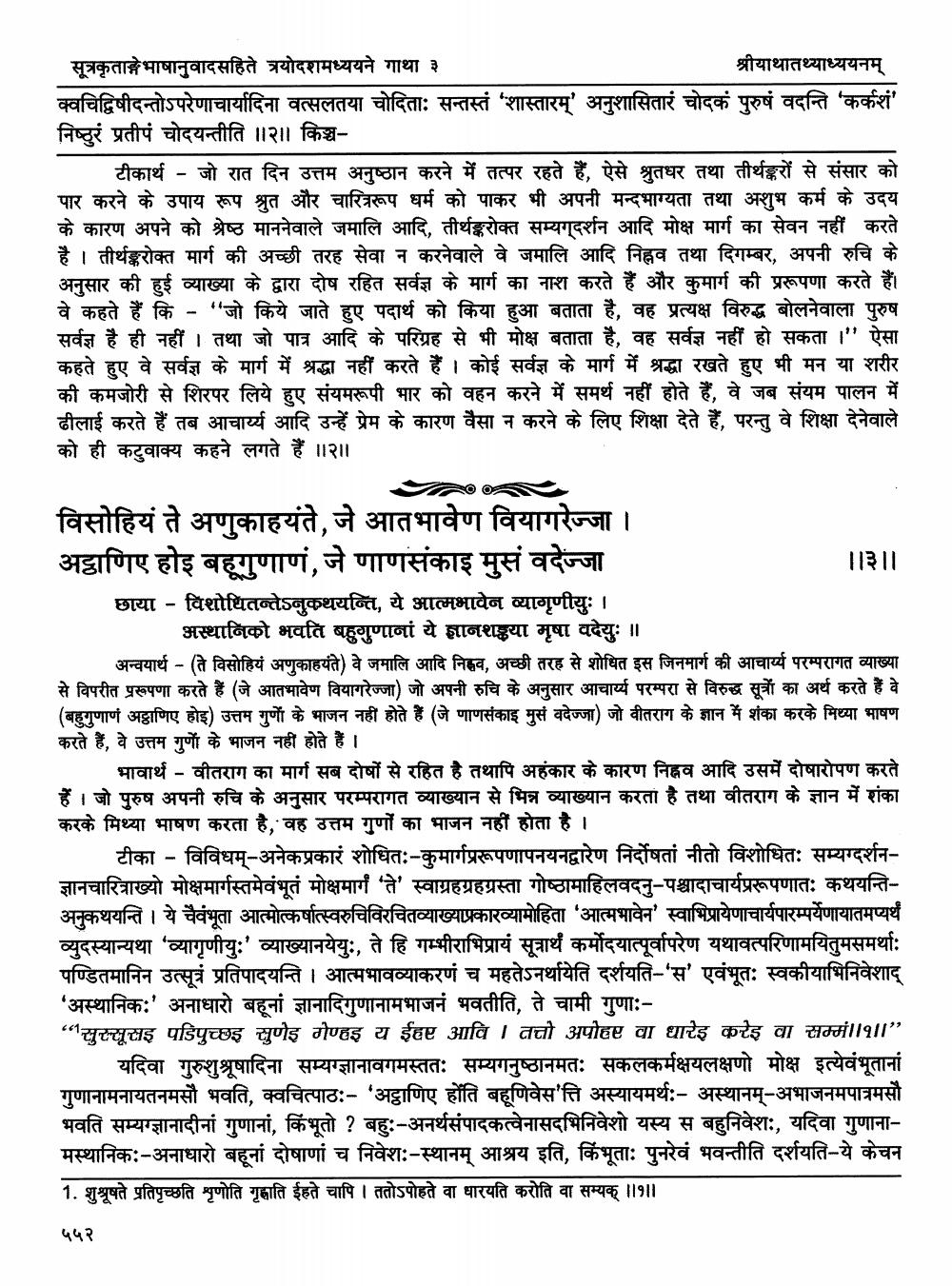________________
सूत्रकृताङ्गे भाषानुवादसहिते त्रयोदशमध्ययने गाथा ३ श्रीयाथातथ्याध्ययनम् क्वचिद्विषीदन्तोऽपरेणाचार्यादिना वत्सलतया चोदिताः सन्तस्तं 'शास्तारम्' अनुशासितारं चोदकं पुरुषं वदन्ति 'कर्कशं' निष्ठुरं प्रतीपं चोदयन्तीति ॥२॥ किञ्च -
टीकार्थ जो रात दिन उत्तम अनुष्ठान करने में तत्पर रहते हैं, ऐसे श्रुतधर तथा तीर्थङ्करों से संसार को पार करने के उपाय रूप श्रुत और चारित्ररूप धर्म को पाकर भी अपनी मन्दभाग्यता तथा अशुभ कर्म के उदय के कारण अपने को श्रेष्ठ माननेवाले जमालि आदि, तीर्थङ्करोक्त सम्यग्दर्शन आदि मोक्ष मार्ग का सेवन नहीं करते है । तीर्थङ्करोक्त मार्ग की अच्छी तरह सेवा न करनेवाले वे जमालि आदि निह्नव तथा दिगम्बर, अपनी रुचि के अनुसार की हुई व्याख्या के द्वारा दोष रहित सर्वज्ञ के मार्ग का नाश करते हैं और कुमार्ग की प्ररूपणा करते हैं। वे कहते हैं कि - "जो किये जाते हुए पदार्थ को किया हुआ बताता है, वह प्रत्यक्ष विरुद्ध बोलनेवाला पुरुष सर्वज्ञ है ही नहीं । तथा जो पात्र आदि के परिग्रह से भी मोक्ष बताता है, वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता ।" ऐसा कहते हुए वे सर्वज्ञ के मार्ग में श्रद्धा नहीं करते हैं । कोई सर्वज्ञ के मार्ग में श्रद्धा रखते हुए भी मन या शरीर की कमजोरी से शिरपर लिये हुए संयमरूपी भार को वहन करने में समर्थ नहीं होते हैं, वे जब संयम पालन में ढीलाई करते हैं तब आचार्य्य आदि उन्हें प्रेम के कारण वैसा न करने के लिए शिक्षा देते हैं, परन्तु वे शिक्षा देनेवाले को ही कटुवाक्य कहने लगते हैं ||२||
-
विसोहियं ते अणुकाहयंते, जे आतभावेण वियागरेज्जा । अाणि होइ बहूगुणाणं, जे णाणसंकाइ मुसं वदेज्जा
छाया
-
विशोधितन्तेऽनुकथयन्ति ये आत्मभावेन व्यागृणीयुः ।
अस्थानिको भवति बहुगुणानां ये ज्ञानशङ्कया मृषा वदेयुः ॥
॥३॥
अन्वयार्थ - (ते विसोहियं अणुकाहयंते) वे जमालि आदि निसव, अच्छी तरह से शोधित इस जिनमार्ग की आचार्य्य परम्परागत व्याख्या से विपरीत प्ररूपणा करते हैं (जे आतभावेण वियागरेज्जा) जो अपनी रुचि के अनुसार आचार्य्य परम्परा से विरुद्ध सूत्रों का अर्थ करते हैं वे ( बहुगुणाणं अट्ठाणिए होइ) उत्तम गुणों के भाजन नहीं होते हैं (जे णाणसंकाइ मुसं वदेज्जा) जो वीतराग के ज्ञान में शंका करके मिथ्या भाषण करते हैं, वे उत्तम गुणों के भाजन नहीं होते हैं ।
भावार्थ - वीतराग का मार्ग सब दोषों से रहित है तथापि अहंकार के कारण निह्नव आदि उसमें दोषारोपण करते हैं। जो पुरुष अपनी रुचि के अनुसार परम्परागत व्याख्यान से भिन्न व्याख्यान करता है तथा वीतराग के ज्ञान में शंका करके मिथ्या भाषण करता है, वह उत्तम गुणों का भाजन नहीं होता है ।
टीका - विविधम्-अनेकप्रकारं शोधितः कुमार्गप्ररूपणापनयनद्वारेण निर्दोषतां नीतो विशोधितः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राख्यो मोक्षमार्गस्तमेवंभूतं मोक्षमार्गं 'ते' स्वाग्रहग्रहग्रस्ता गोष्ठामाहिलवदनु - पश्चादाचार्यप्ररूपणातः कथयन्ति - अनुकथयन्ति । ये चैवंभूता आत्मोत्कर्षात्स्वरुचिविरचितव्याख्याप्रकारव्यामोहिता 'आत्मभावेन' स्वाभिप्रायेणाचार्यपारम्पर्येणायातमप्यर्थं व्युदस्यान्यथा 'व्यागृणीयुः' व्याख्यानयेयुः, ते हि गम्भीराभिप्रायं सूत्रार्थं कर्मोदयात्पूर्वापरेण यथावत्परिणामयितुमसमर्थाः पण्डितमानिन उत्सूत्रं प्रतिपादयन्ति । आत्मभावव्याकरणं च महतेऽनर्थायेति दर्शयति- 'स' एवंभूतः स्वकीयाभिनिवेशाद् 'अस्थानिकः' अनाधारो बहूनां ज्ञानादिगुणानामभाजनं भवतीति, ते चामी गुणा:""सुरसूसइ पडिपुच्छइ सुणेइ गेण्हइ य ईहए आवि । तत्तो अपोहर वा धारेइ करेइ वा सम्म ||१||” यदिवा गुरुशुश्रूषादिना सम्यग्ज्ञानावगमस्ततः सम्यगनुष्ठानमतः सकलकर्मक्षयलक्षणो मोक्ष इत्येवंभूतानां गुणानामनायतनमसौ भवति, क्वचित्पाठः - 'अट्ठाणिए होंति बहूणिवेस' त्ति अस्यायमर्थ:- अस्थानम् - अभाजनमपात्रमसौ भवति सम्यग्ज्ञानादीनां गुणानां, किंभूतो ? बहुः - अनर्थसंपादकत्वेनासदभिनिवेशो यस्य स बहुनिवेशः, यदिवा गुणानामस्थानिक:- अनाधारो बहूनां दोषाणां च निवेश: स्थानम् आश्रय इति, किंभूताः पुनरेवं भवन्तीति दर्शयति- ये केचन 1. शुश्रूषते प्रतिपृच्छति शृणोति गृह्णाति ईहते चापि । ततोऽपोहते वा धारयति करोति वा सम्यक् ||१|
५५२