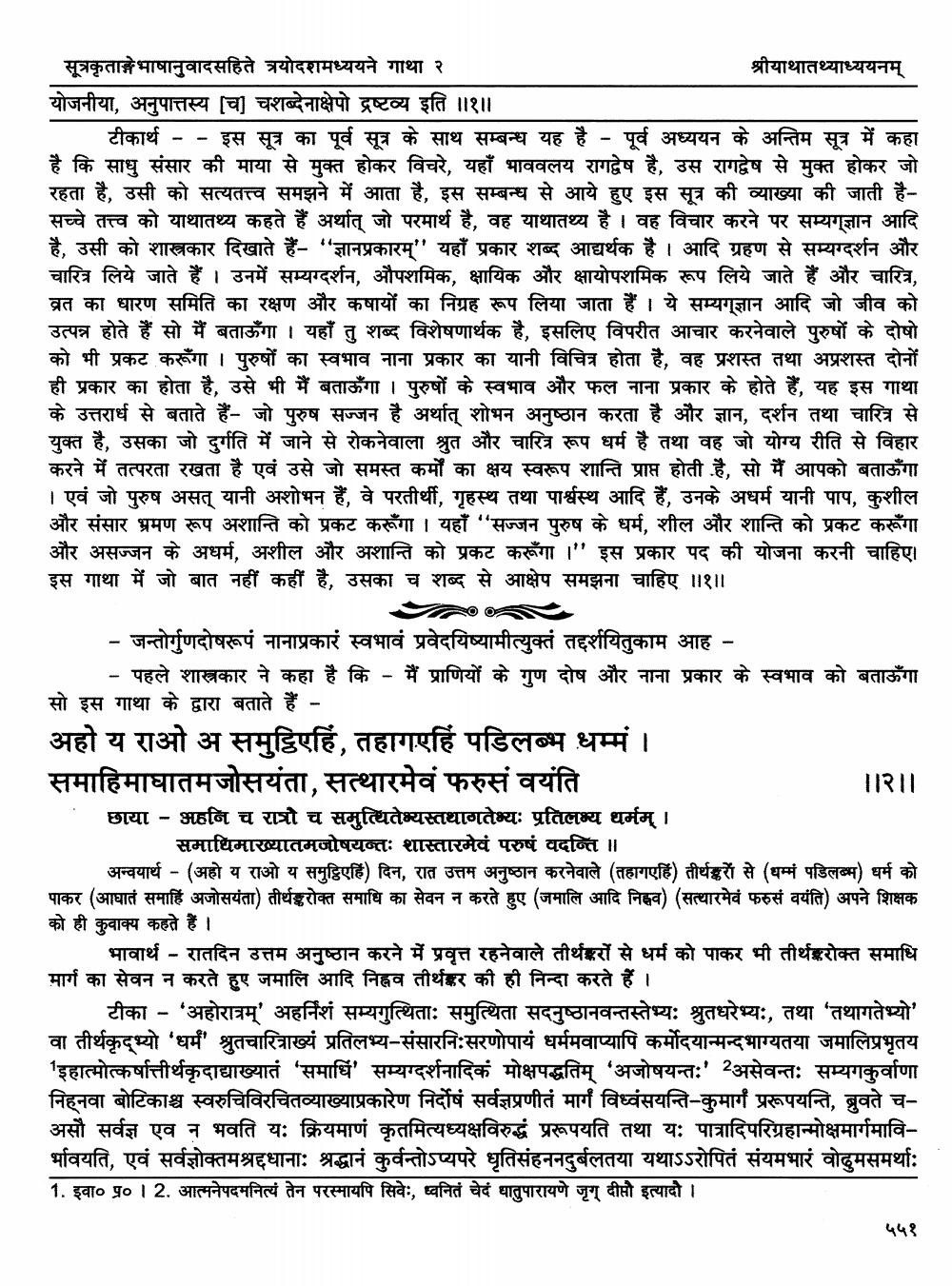________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते त्रयोदशमध्ययने गाथा २
श्रीयाथातथ्याध्ययनम् योजनीया, अनुपात्तस्य [च] चशब्देनाक्षेपो द्रष्टव्य इति ॥१॥
टीकार्थ - - इस सूत्र का पूर्व सूत्र के साथ सम्बन्ध यह है - पूर्व अध्ययन के अन्तिम सूत्र में कहा है कि साधु संसार की माया से मुक्त होकर विचरे, यहाँ भाववलय रागद्वेष है, उस रागद्वेष से मुक्त होकर जो रहता है, उसी को सत्यतत्त्व समझने में आता है, इस सम्बन्ध से आये हुए इस सूत्र की व्याख्या की जाती हैसच्चे तत्त्व को याथातथ्य कहते हैं अर्थात् जो परमार्थ है, वह याथातथ्य है । वह विचार करने पर सम्यग्ज्ञान आदि है, उसी को शास्त्रकार दिखाते हैं- "ज्ञानप्रकारम्" यहाँ प्रकार शब्द आद्यर्थक है। आदि ग्रहण से सम्यग्दर्शन और चारित्र लिये जाते हैं। उनमें सम्यग्दर्शन, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक रूप लिये जाते हैं और चारित्र, व्रत का धारण समिति का रक्षण और कषायों का निग्रह रूप लिया जाता हैं । ये सम्यग्ज्ञान आदि जो जीव को उत्पन्न होते हैं सो मैं बताऊँगा । यहाँ तु शब्द विशेषणार्थक है, इसलिए विपरीत आचार करनेवाले पुरुषों के दोषो को भी प्रकट करूँगा । पुरुषों का स्वभाव नाना प्रकार का यानी विचित्र होता है, वह प्रशस्त तथा अप्रशस्त दोनों ही प्रकार का होता है, उसे भी मैं बताऊँगा । पुरुषों के स्वभाव और फल नाना प्रकार के होते हैं, यह इस गाथा के उत्तरार्ध से बताते हैं- जो पुरुष सज्जन है अर्थात् शोभन अनुष्ठान करता है और ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र से युक्त है, उसका जो दुर्गति में जाने से रोकनेवाला श्रुत और चारित्र रूप धर्म है तथा वह जो योग्य रीति से विहार करने में तत्परता रखता है एवं उसे जो समस्त कर्मों का क्षय स्वरूप शान्ति प्राप्त होती है, सो मैं आपको बताऊँगा । एवं जो पुरुष असत् यानी अशोभन हैं, वे परतीर्थी, गृहस्थ तथा पार्श्वस्थ आदि हैं, उनके अधर्म यानी पाप, कुशील और संसार भ्रमण रूप अशान्ति को प्रकट करूँगा । यहाँ "सज्जन पुरुष के धर्म, शील और शान्ति को प्रकट करूँगा और असज्जन के अधर्म, अशील और अशान्ति को प्रकट करूँगा ।" इस प्रकार पद की योजना करनी चाहिए। इस गाथा में जो बात नहीं कहीं है, उसका च शब्द से आक्षेप समझना चाहिए ॥१॥
- जन्तोर्गुणदोषरूपं नानाप्रकारं स्वभावं प्रवेदयिष्यामीत्युक्तं तदर्शयितुकाम आह -
- पहले शास्त्रकार ने कहा है कि - मैं प्राणियों के गुण दोष और नाना प्रकार के स्वभाव को बताऊँगा सो इस गाथा के द्वारा बताते हैं - अहो य राओ अ समुट्ठिएहि, तहागएहिं पडिलब्भ धम्म । समाहिमाघातमजोसयंता, सत्थारमेवं फरुसं वयंति
॥२॥ छाया - अहनि च रात्री च समुत्थितेभ्यस्तथागतेभ्यः प्रतिलभ्य धर्मम् ।
समाधिमाख्यातमजोषयन्तः शास्तारमेवं परुषं वदन्ति ।। अन्वयार्थ - (अहो य राओ य समुट्ठिएहिं) दिन, रात उत्तम अनुष्ठान करनेवाले (तहागएहिं) तीर्थङ्करों से (धम्म पडिलब्म) धर्म को पाकर (आघातं समाहिं अजोसयंता) तीर्थङ्करोक्त समाधि का सेवन न करते हुए (जमालि आदि निहव) (सत्थारमेवं फरुसं वयंति) अपने शिक्षक को ही कुवाक्य कहते हैं।
भावार्थ - रातदिन उत्तम अनुष्ठान करने में प्रवृत्त रहनेवाले तीर्थकरों से धर्म को पाकर भी तीर्थङ्करोक्त समाधि मार्ग का सेवन न करते हुए जमालि आदि निह्नव तीर्थक्कर की ही निन्दा करते हैं।
टीका - 'अहोरात्रम्' अहर्निशं सम्यगुत्थिताः समुत्थिता सदनुष्ठानवन्तस्तेभ्यः श्रुतधरेभ्यः, तथा 'तथागतेभ्यो' वा तीर्थकृद्भ्यो 'धर्म' श्रुतचारित्राख्यं प्रतिलभ्य-संसारनिःसरणोपायं धर्ममवाप्यापि कर्मोदयान्मन्दभाग्यतया जमालिप्रभृतय इहात्मोत्कर्षात्तीर्थकृदाद्याख्यातं 'समाधि' सम्यग्दर्शनादिकं मोक्षपद्धतिम् 'अजोषयन्तः' असेवन्तः सम्यगकुर्वाणा निह्नवा बोटिकाश्च स्वरुचिविरचितव्याख्याप्रकारेण निर्दोषं सर्वज्ञप्रणीतं मागं विध्वंसयन्ति-कुमार्ग प्ररूपयन्ति, ब्रुवते चअसौ सर्वज्ञ एव न भवति यः क्रियमाणं कृतमित्यध्यक्षविरुद्धं प्ररूपयति तथा यः पात्रादिपरिग्रहान्मोक्षमार्गमाविर्भावयति, एवं सर्वज्ञोक्तमश्रद्दधानाः श्रद्धानं कुर्वन्तोऽप्यपरे धृतिसंहननदुर्बलतया यथाऽऽरोपितं संयमभारं वोढुमसमर्थाः 1. इवा० प्र०। 2. आत्मनेपदमनित्यं तेन परस्मायपि सिवेः, ध्वनितं चेदं धातुपारायणे जृग् दीप्तौ इत्यादौ ।