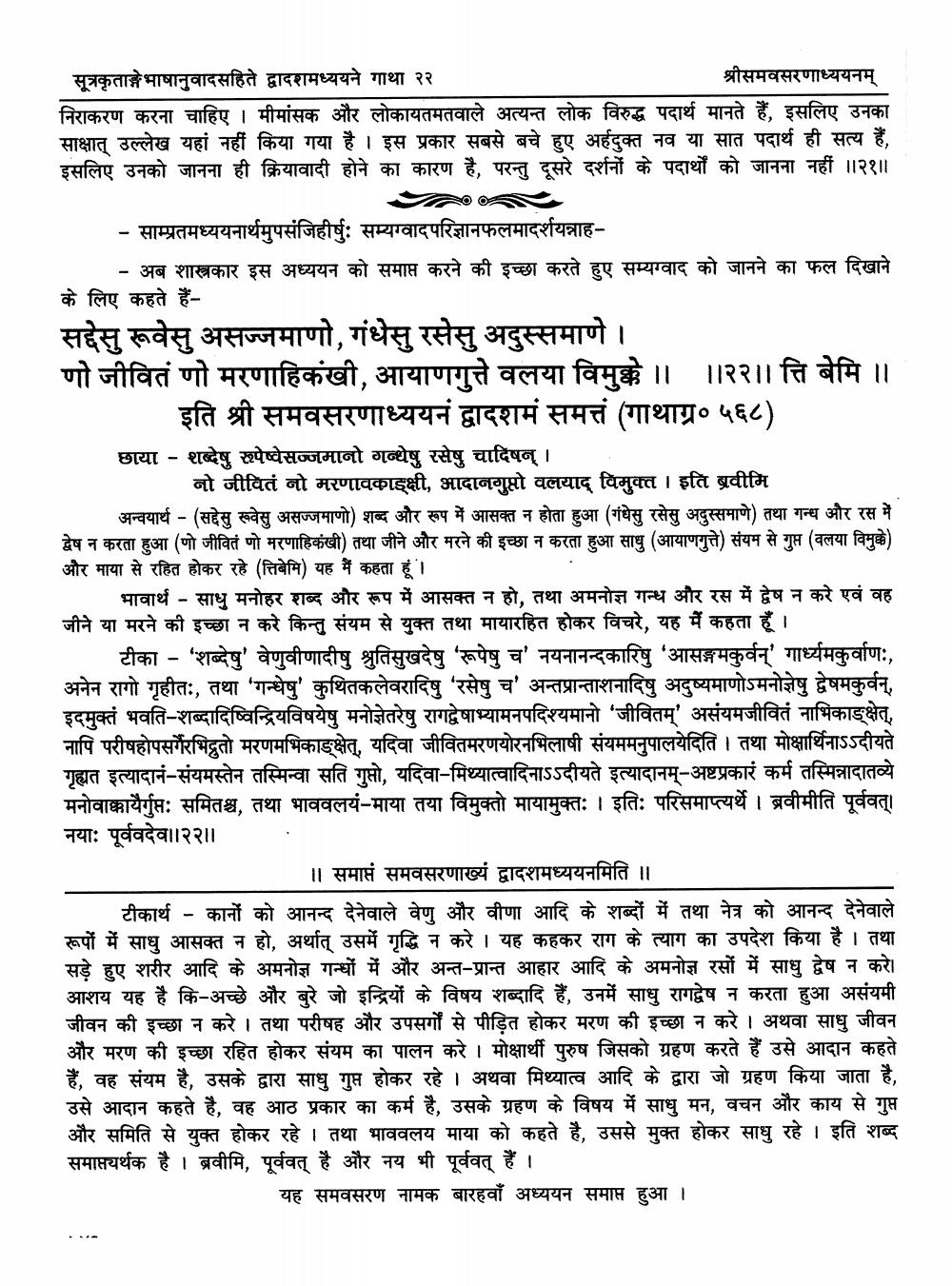________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते द्वादशमध्ययने गाथा २२
श्रीसमवसरणाध्ययनम् निराकरण करना चाहिए । मीमांसक और लोकायतमतवाले अत्यन्त लोक विरुद्ध पदार्थ मानते हैं, इसलिए उनका साक्षात् उल्लेख यहां नहीं किया गया है । इस प्रकार सबसे बचे हुए अर्हदुक्त नव या सात पदार्थ ही सत्य हैं, इसलिए उनको जानना ही क्रियावादी होने का कारण है, परन्तु दूसरे दर्शनों के पदार्थों को जानना नहीं ॥२१॥
- साम्प्रतमध्ययनार्थमुपसंजिहीर्षुः सम्यग्वादपरिज्ञानफलमादर्शयन्नाह
- अब शास्त्रकार इस अध्ययन को समाप्त करने की इच्छा करते हुए सम्यग्वाद को जानने का फल दिखाने के लिए कहते हैंसद्देसु रूवेसु असज्जमाणो, गंधेसु रसेसु अदुस्समाणे । णो जीवितं णो मरणाहिकंखी, आयाणगुत्ते वलया विमुक्के ।। ॥२२।। त्ति बेमि ॥
इति श्री समवसरणाध्ययनं द्वादशमं समत्तं (गाथाग्र० ५६८) छाया - शब्देषु रूपेष्वेसज्जमानो गन्धेषु रसेषु चादिषन् ।
___ नो जीवितं नो मरणावकाङ्क्षी, आदानगुप्तो वलयाद् विमुक्त । इति ब्रवीमि
अन्वयार्थ - (सद्देसु रुवेसु असज्जमाणो) शब्द और रूप में आसक्त न होता हुआ (गंधेसु रसेसु अदुस्समाणे) तथा गन्ध और रस में द्वेष न करता हुआ (णो जीवितं णो मरणाहिकंखी) तथा जीने और मरने की इच्छा न करता हुआ साधु (आयाणगुत्ते) संयम से गुप्त (वलया विमुक्के) और माया से रहित होकर रहे (त्तिबेमि) यह मैं कहता हूं।
भावार्थ- साधु मनोहर शब्द और रूप में आसक्त न हो, तथा अमनोज्ञ गन्ध और रस में द्वेष न करे एवं वह जीने या मरने की इच्छा न करे किन्तु संयम से युक्त तथा मायारहित होकर विचरे, यह मैं कहता हूँ। ___टीका - 'शब्देषु' वेणुवीणादीषु श्रुतिसुखदेषु 'रूपेषु च' नयनानन्दकारिषु 'आसङ्गमकुर्वन्' गाय॑मकुर्वाणः, अनेन रागो गृहीतः, तथा 'गन्धेषु' कुथितकलेवरादिषु 'रसेषु च' अन्तप्रान्ताशनादिषु अदुष्यमाणोऽमनोज्ञेषु द्वेषमकुर्वन्, इदमुक्तं भवति-शब्दादिष्विन्द्रियविषयेषु मनोज्ञेतरेषु रागद्वेषाभ्यामनपदिश्यमानो 'जीवितम्' असंयमजीवितं नाभिकाक्षेत्, नापि परीषहोपसर्गेरभिद्रुतो मरणमभिकाक्षेत्, यदिवा जीवितमरणयोरनभिलाषी संयममनुपालयेदिति । तथा मोक्षार्थिनाऽऽदीयते गृह्यत इत्यादानं-संयमस्तेन तस्मिन्वा सति गुप्तो, यदिवा-मिथ्यात्वादिनाऽऽदीयते इत्यादानम्-अष्टप्रकारं कर्म तस्मिन्नादातव्ये मनोवाक्कायैर्गुप्तः समितश्च, तथा भाववलयं-माया तया विमुक्तो मायामुक्तः । इतिः परिसमाप्त्यर्थे । ब्रवीमीति पूर्ववत्। नयाः पूर्ववदेव।।२२॥
॥ समाप्तं समवसरणाख्यं द्वादशमध्ययनमिति ॥ टीकार्थ - कानों को आनन्द देनेवाले वेणु और वीणा आदि के शब्दों में तथा नेत्र को आनन्द देनेवाले रूपों में साधु आसक्त न हो, अर्थात् उसमें गृद्धि न करे । यह कहकर राग के त्याग का उपदेश किया है । तथा सड़े हुए शरीर आदि के अमनोज्ञ गन्धों में और अन्त-प्रान्त आहार आदि के अमनोज्ञ रसों में साधु द्वेष न करे। आशय यह है कि-अच्छे और बुरे जो इन्द्रियों के विषय शब्दादि हैं, उनमें साधु रागद्वेष न करता हुआ असंयमी जीवन की इच्छा न करे । तथा परीषह और उपसर्गों से पीड़ित होकर मरण की इच्छा न करे । अथवा साधु जीवन
और मरण की इच्छा रहित होकर संयम का पालन करे । मोक्षार्थी पुरुष जिसको ग्रहण करते हैं उसे आदान कहते हैं, वह संयम है, उसके द्वारा साधु गुप्त होकर रहे । अथवा मिथ्यात्व आदि के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, उसे आदान कहते है, वह आठ प्रकार का कर्म है, उसके ग्रहण के विषय में साधु मन, वचन और काय से गुप्त और समिति से युक्त होकर रहे । तथा भाववलय माया को कहते है, उससे मुक्त होकर साधु रहे । इति शब्द समाप्तयर्थक है । ब्रवीमि, पूर्ववत् है और नय भी पूर्ववत् हैं।
यह समवसरण नामक बारहवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।