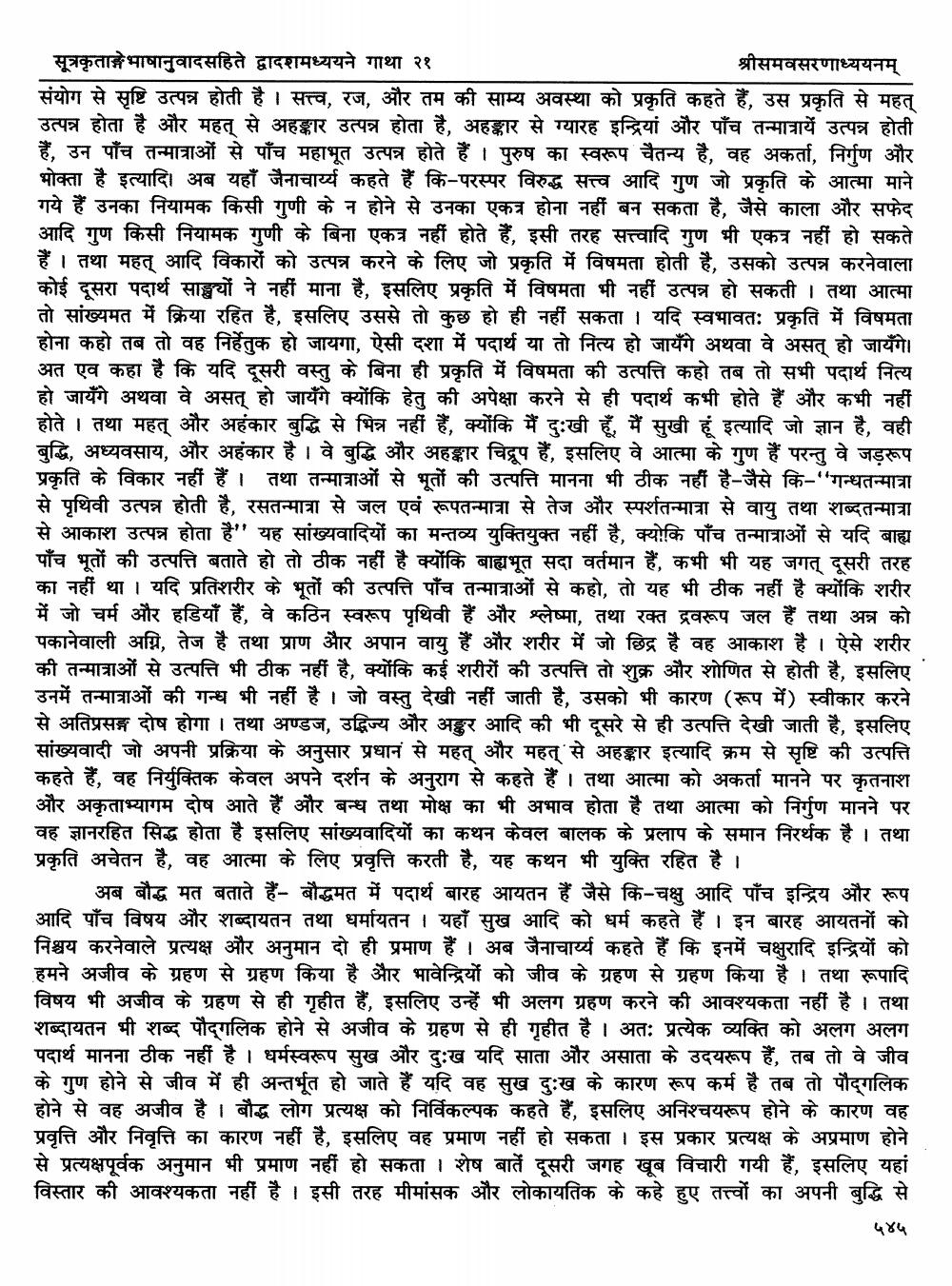________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते द्वादशमध्ययने गाथा २१
श्रीसमवसरणाध्ययनम् संयोग से सष्टि उत्पन्न होती है। सत्त्व, रज, और तम की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं, उस प्रकृति से महत् उत्पन्न होता है और महत् से अहङ्कार उत्पन्न होता है, अहङ्कार से ग्यारह इन्द्रियां और पाँच तन्मात्रायें उत्पन्न होती हैं, उन पाँच तन्मात्राओं से पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं । पुरुष का स्वरूप चैतन्य है, वह अकर्ता, निर्गुण और भोक्ता है इत्यादि। अब यहाँ जैनाचार्य कहते हैं कि-परस्पर विरुद्ध सत्त्व आदि गुण जो प्रकृति के आत्मा माने गये हैं उनका नियामक किसी गुणी के न होने से उनका एकत्र होना नहीं बन सकता है, जैसे काला और सफेद आदि गुण किसी नियामक गुणी के बिना एकत्र नहीं होते हैं, इसी तरह सत्त्वादि गुण भी एकत्र नहीं हो सकते हैं । तथा महत् आदि विकारों को उत्पन्न करने के लिए जो प्रकृति में विषमता होती है, उसको उत्पन्न करनेवाला कोई दूसरा पदार्थ साङ्खयों ने नहीं माना है, इसलिए प्रकृति में विषमता भी नहीं उत्पन्न हो सकती । तथा आत्मा तो सांख्यमत में क्रिया रहित है, इसलिए उससे तो कुछ हो ही नहीं सकता । यदि स्वभावतः प्रकृति में विषमता होना कहो तब तो वह निर्हेतुक हो जायगा, ऐसी दशा में पदार्थ या तो नित्य हो जायँगे अथवा वे असत् हो जायँगे। अत एव कहा है कि यदि दूसरी वस्तु के बिना ही प्रकृति में विषमता की उत्पत्ति कहो तब तो सभी पदार्थ नित्य हो जायँगे अथवा वे असत् हो जायेंगे क्योंकि हेतु की अपेक्षा करने से ही पदार्थ कभी होते हैं और कभी नहीं होते । तथा महत् और अहंकार बुद्धि से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि मैं दुःखी हूँ, मैं सुखी हूं इत्यादि जो ज्ञान है, वही बुद्धि, अध्यवसाय, और अहंकार है । वे बुद्धि और अहङ्कार चिद्रूप हैं, इसलिए वे आत्मा के गुण हैं परन्तु वे जड़रूप प्रकृति के विकार नहीं हैं। तथा तन्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है-जैसे कि-"गन्धतन्मात्रा से पृथिवी उत्पन्न होती है, रसतन्मात्रा से जल एवं रूपतन्मात्रा से तेज और स्पर्शतन्मात्रा से वायु तथा शब्दतन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है" यह सांख्यवादियों का मन्तव्य युक्तियुक्त नहीं है, क्योकि पाँच तन्मात्राओं से यदि बाह्य पाँच भूतों की उत्पत्ति बताते हो तो ठीक नहीं है क्योंकि बाह्यभूत सदा वर्तमान हैं, कभी भी यह जगत् दूसरी तरह का नहीं था । यदि प्रतिशरीर के भूतों की उत्पत्ति पाँच तन्मात्राओं से कहो, तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि शरीर में जो चर्म और हडियाँ हैं, वे कठिन स्वरूप पृथिवी हैं और श्लेष्मा, तथा रक्त द्रवरूप जल हैं तथा अन्न को पकानेवाली अग्नि, तेज है तथा प्राण और अपान वायु हैं और शरीर में जो छिद्र है वह आकाश है । ऐसे शरीर की तन्मात्राओं से उत्पत्ति भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई शरीरों की उत्पत्ति तो शुक्र और शोणित से होती है, इसलिए उनमें तन्मात्राओं की गन्ध भी नहीं है । जो वस्तु देखी नहीं जाती है, उसको भी कारण (रूप में) स्वीकार करने से अतिप्रसङ्ग दोष होगा । तथा अण्डज, उद्भिज्य और अङ्कुर आदि की भी दूसरे से ही उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए सांख्यवादी जो अपनी प्रक्रिया के अनुसार प्रधान से महत् और महत् से अहङ्कार इत्यादि क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति कहते हैं, वह नियुक्तिक केवल अपने दर्शन के अनुराग से कहते हैं । तथा आत्मा को अकर्ता मानने पर कृतनाश
और अकृताभ्यागम दोष आते हैं और बन्ध तथा मोक्ष का भी अभाव होता है तथा आत्मा को निर्गुण मानने पर वह ज्ञानरहित सिद्ध होता है इसलिए सांख्यवादियों का कथन केवल बालक के प्रलाप के समान निरर्थक है। तथा प्रकृति अचेतन है, वह आत्मा के लिए प्रवृत्ति करती है, यह कथन भी युक्ति रहित है ।
अब बौद्ध मत बताते हैं- बौद्धमत में पदार्थ बारह आयतन हैं जैसे कि-चक्षु आदि पाँच इन्द्रिय और रूप आदि पाँच विषय और शब्दायतन तथा धर्मायतन । यहाँ सख आदि को धर्म कहते हैं। निश्चय करनेवाले प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण हैं। अब जैनाचार्या कहते हैं कि इनमें चक्षुरादि इन्द्रियों को हमने अजीव के ग्रहण से ग्रहण किया है और भावेन्द्रियों को जीव के ग्रहण से ग्रहण किया है। तथा रूपादि विषय भी अजीव के ग्रहण से ही गृहीत हैं, इसलिए उन्हें भी अलग ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है । तथा शब्दायतन भी शब्द पौद्गलिक होने से अजीव के ग्रहण से ही गृहीत है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग पदार्थ मानना ठीक नहीं है। धर्मस्वरूप सुख और दुःख यदि साता और असाता के उदयरूप हैं, तब तो वे जीव के गुण होने से जीव में ही अन्तर्भूत हो जाते हैं यदि वह सुख दुःख के कारण रूप कर्म है तब तो पौद्गलिक होने से वह अजीव है । बौद्ध लोग प्रत्यक्ष को निर्विकल्पक कहते हैं, इसलिए अनिश्चयरूप होने के कारण वह प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण नहीं है, इसलिए वह प्रमाण नहीं हो सकता । इस प्रकार प्रत्यक्ष के अप्रमाण होने से प्रत्यक्षपूर्वक अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकता । शेष बातें दूसरी जगह खूब विचारी गयी हैं, इसलिए यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह मीमांसक और लोकायतिक के कहे हए तत्त्वों का अपनी बुद्धि से