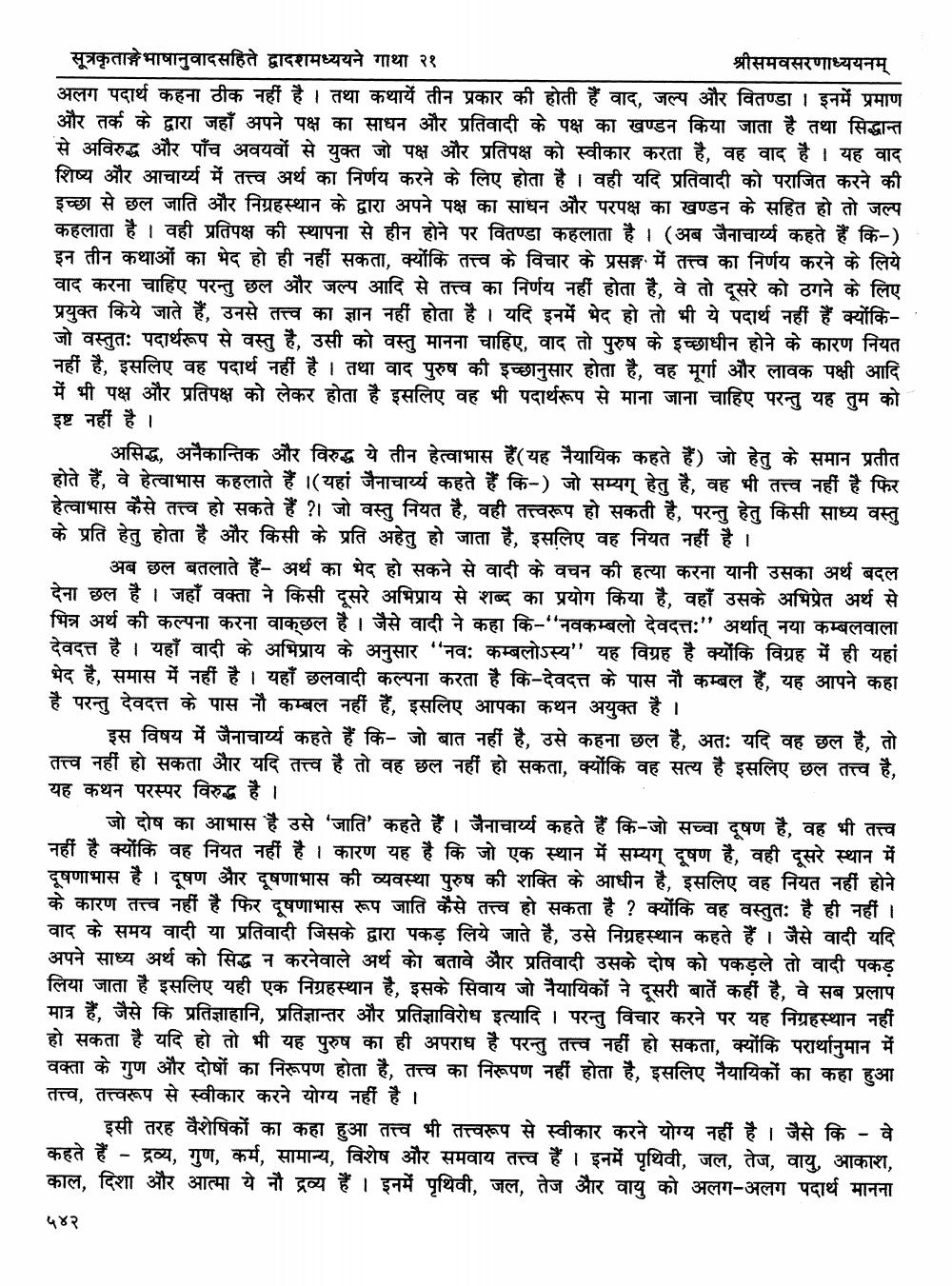________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते द्वादशमध्ययने गाथा २१
श्रीसमवसरणाध्ययनम् अलग पदार्थ कहना ठीक नहीं है। तथा कथायें तीन प्रकार की होती हैं वाद, जल्प और वितण्डा । इनमें प्रमाण
और तर्क के द्वारा जहाँ अपने पक्ष का साधन और प्रतिवादी के पक्ष का खण्डन किया जाता है तथा सिद्धान्त से अविरुद्ध और पाँच अवयवों से युक्त जो पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार करता है, वह वाद है । यह वाद शिष्य और आचार्य में तत्त्व अर्थ का निर्णय करने के लिए होता है । वही यदि प्रतिवादी को पराजित करने की इच्छा से छल जाति और निग्रहस्थान के द्वारा अपने पक्ष का साधन और परपक्ष का खण्डन के सहित हो तो जल्प कहलाता है । वही प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन होने पर वितण्डा कहलाता है। (अब जैनाचार्य कहते हैं कि-) इन तीन कथाओं का भेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि तत्त्व के विचार के प्रसङ्ग में तत्त्व का निर्णय करने के लिये वाद करना चाहिए परन्तु छल और जल्प आदि से तत्त्व का निर्णय नहीं होता है, वे तो दूसरे को ठगने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं, उनसे तत्त्व का ज्ञान नहीं होता है। यदि इनमें भेद हो तो भी ये पदार्थ नहीं हैं क्योंकि- ' जो वस्तुतः पदार्थरूप से वस्तु है, उसी को वस्तु मानना चाहिए, वाद तो पुरुष के इच्छाधीन होने के कारण नियत नहीं है, इसलिए वह पदार्थ नहीं है । तथा वाद पुरुष की इच्छानुसार होता है, वह मूर्गा और लावक पक्षी आदि में भी पक्ष और प्रतिपक्ष को लेकर होता है इसलिए वह भी पदार्थरूप से माना जाना चाहिए परन्तु यह तुम को इष्ट नहीं है।
असिद्ध, अनैकान्तिक और विरुद्ध ये तीन हेत्वाभास हैं(यह नैयायिक कहते हैं) जो हेतु के समान प्रतीत होते हैं, वे हेत्वाभास कहलाते हैं ।(यहां जैनाचार्या कहते हैं कि-) जो सम्यग् हेतु है, वह भी तत्त्व नहीं है फिर
सकते हैं ?। जो वस्तु नियत है, वही तत्त्वरूप हो सकती है, परन्तु हेतु किसी साध्य वस्तु के प्रति हेतु होता है और किसी के प्रति अहेतु हो जाता है, इसलिए वह नियत नहीं है ।
अब छल बतलाते हैं- अर्थ का भेद हो सकने से वादी के वचन की हत्या करना यानी उसका अर्थ बदल देना छल है । जहाँ वक्ता ने किसी दूसरे अभिप्राय से शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ उसके अभिप्रेत अर्थ से भिन्न अर्थ की कल्पना करना वाक्छल है। जैसे वादी ने कहा कि-"नवकम्बलो देवदत्तः" अर्थात् नया कम्बलवाला देवदत्त है। यहाँ वादी के अभिप्राय के अनुसार "नवः कम्बलोऽस्य" यह विग्रह है क्योंकि विग्रह में ही यहां भेद है, समास में नहीं है। यहाँ छलवादी कल्पना करता है कि-देवदत्त के पास नौ कम्बल हैं, यह आपने कहा है परन्तु देवदत्त के पास नौ कम्बल नहीं हैं, इसलिए आपका कथन अयुक्त है।
इस विषय में जैनाचार्य कहते हैं कि- जो बात नहीं है, उसे कहना छल है, अतः यदि वह छल है, तो तत्त्व नहीं हो सकता और यदि तत्त्व है तो वह छल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सत्य है इसलिए छल तत्त्व है, यह कथन परस्पर विरुद्ध है।
जो दोष का आभास है उसे 'जाति' कहते हैं। जैनाचार्या कहते हैं कि-जो सच्चा दूषण है, वह भी तत्त्व नहीं है क्योंकि वह नियत नहीं है । कारण यह है कि जो एक स्थान में सम्यग् दूषण है, वही दूसरे स्थान में दूषणाभास है । दूषण और दूषणाभास की व्यवस्था पुरुष की शक्ति के आधीन है, इसलिए वह नियत नहीं होने के कारण तत्त्व नहीं है फिर दूषणाभास रूप जाति कैसे तत्त्व हो सकता है ? क्योंकि वह वस्तुतः है ही नहीं। वाद के समय वादी या प्रतिवादी जिसके द्वारा पकड़ लिये जाते है, उसे निग्रहस्थान कहते हैं। जैसे वादी यदि अपने साध्य अर्थ को सिद्ध न करनेवाले अर्थ को बतावे और प्रतिवादी उसके दोष को पकड़ले तो वादी पकड़ लिया जाता है इसलिए यही एक निग्रहस्थान है, इसके सिवाय जो नैयायिकों ने दूसरी बातें कहीं है, वे सब प्रलाप मात्र हैं, जैसे कि प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर और प्रतिज्ञाविरोध इत्यादि । परन्तु विचार करने पर यह निग्रहस्थान नहीं हो सकता है यदि हो तो भी यह पुरुष का ही अपराध है परन्तु तत्त्व नहीं हो सकता, क्योंकि परार्थानुमान में वक्ता के गुण और दोषों का निरूपण होता है, तत्त्व का निरूपण नहीं होता है, इसलिए नैयायिकों का कहा हआ तत्त्व, तत्त्वरूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है।
इसी तरह वैशेषिकों का कहा हुआ तत्त्व भी तत्त्वरूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है। जैसे कि - वे कहते हैं - द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय तत्त्व हैं। इनमें पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा और आत्मा ये नौ द्रव्य हैं । इनमें पृथिवी, जल, तेज और वायु को अलग-अलग पदार्थ मानना
५४२