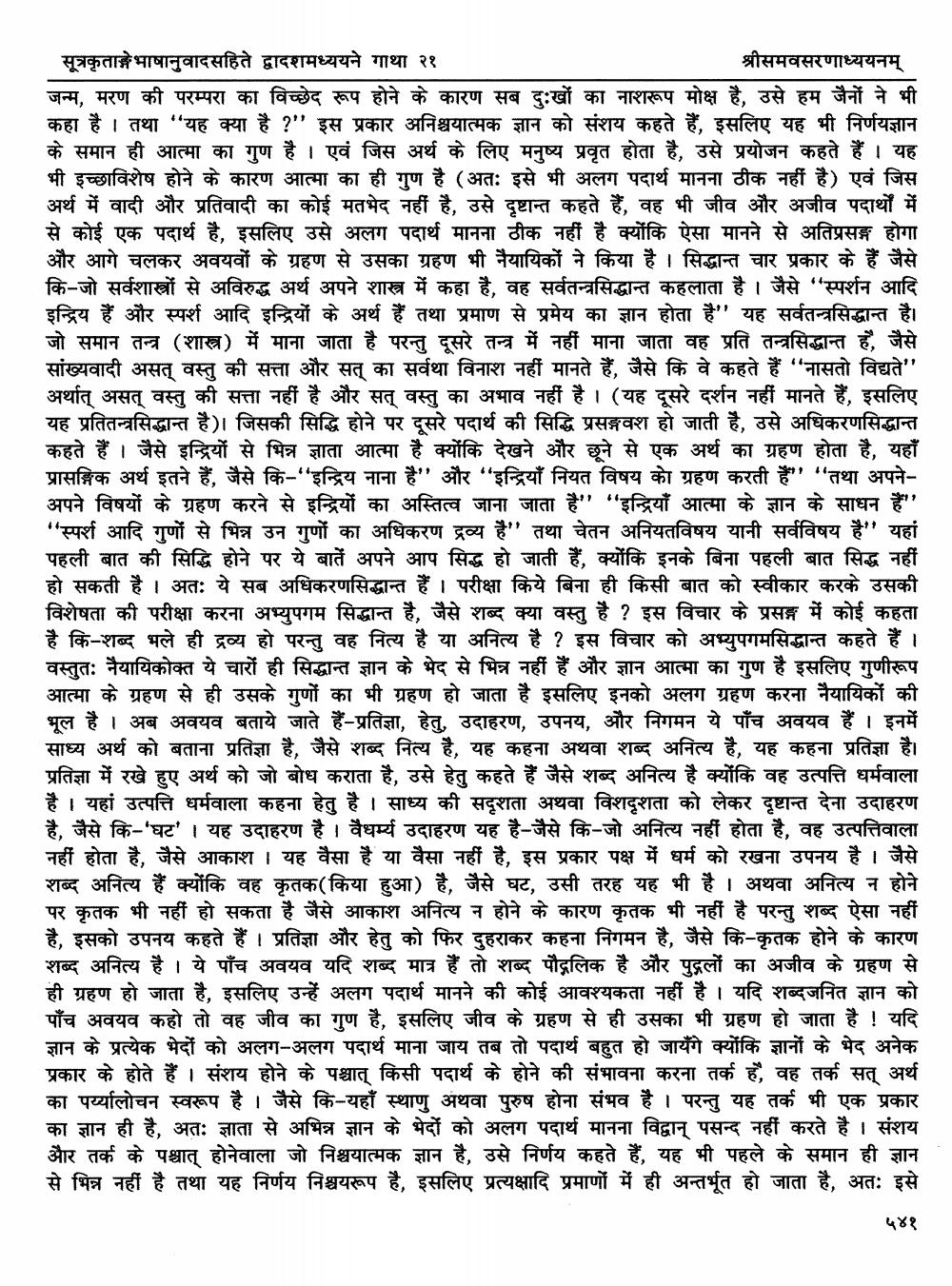________________
सूत्रकृताङ्गे भाषानुवादसहिते द्वादशमध्ययने गाथा २१
श्रीसमवसरणाध्ययनम् जन्म, मरण की परम्परा का विच्छेद रूप होने के कारण सब दुःखों का नाशरूप मोक्ष है, उसे हम जैनों ने भी कहा है । तथा "यह क्या है ?" इस प्रकार अनिश्चयात्मक ज्ञान को संशय कहते हैं, इसलिए यह भी निर्णयज्ञान के समान ही आत्मा का गुण है । एवं जिस अर्थ के लिए मनुष्य प्रवृत होता है, उसे प्रयोजन कहते हैं । यह भी इच्छाविशेष होने के कारण आत्मा का ही गुण है ( अत: इसे भी अलग पदार्थ मानना ठीक नहीं है) एवं जिस अर्थ में वादी और प्रतिवादी का कोई मतभेद नहीं है, उसे दृष्टान्त कहते हैं, वह भी जीव और अजीव पदार्थों में से कोई एक पदार्थ है, इसलिए उसे अलग पदार्थ मानना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने से अतिप्रसङ्ग होगा और आगे चलकर अवयवों के ग्रहण उसका ग्रहण भी नैयायिकों ने किया है । सिद्धान्त चार प्रकार के हैं जैसे कि- जो सर्वशास्त्रों से अविरुद्ध अर्थ अपने शास्त्र में कहा है, वह सर्वतन्त्रसिद्धान्त कहलाता है । जैसे "स्पर्शन आदि इन्द्रिय हैं और स्पर्श आदि इन्द्रियों के अर्थ हैं तथा प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान होता है" यह सर्वतन्त्रसिद्धान्त है। जो समान तन्त्र (शास्त्र) में माना जाता है परन्तु दूसरे तन्त्र में नहीं माना जाता वह प्रति तन्त्रसिद्धान्त है, जैसे सांख्यवादी असत् वस्तु की सत्ता और सत् का सर्वथा विनाश नहीं मानते हैं, जैसे कि वे कहते हैं "नासतो विद्यते" अर्थात् असत् वस्तु की सत्ता नहीं है और सत् वस्तु का अभाव नहीं है । (यह दूसरे दर्शन नहीं मानते हैं, इसलिए यह प्रतितन्त्रसिद्धान्त है ) । जिसकी सिद्धि होने पर दूसरे पदार्थ की सिद्धि प्रसङ्गवश हो जाती है, उसे अधिकरणसिद्धान्त कहते हैं । जैसे इन्द्रियों से भिन्न ज्ञाता आत्मा है क्योंकि देखने और छूने से एक अर्थ का ग्रहण होता है, यहाँ प्रासङ्गिक अर्थ इतने हैं, जैसे कि - "इन्द्रिय नाना है" और "इन्द्रियाँ नियत विषय को ग्रहण करती हैं" "तथा अपनेअपने विषयों के ग्रहण करने से इन्द्रियों का अस्तित्व जाना जाता है " " इन्द्रियाँ आत्मा के ज्ञान के साधन हैं " "स्पर्श आदि गुणों से भिन्न उन गुणों का अधिकरण द्रव्य है" तथा चेतन अनियतविषय यानी सर्वविषय है" यहां पहली बात की सिद्धि होने पर ये बातें अपने आप सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि इनके बिना पहली बात सिद्ध नहीं हो सकती है । अतः ये सब अधिकरणसिद्धान्त हैं । परीक्षा किये बिना ही किसी बात को स्वीकार करके उसकी विशेषता की परीक्षा करना अभ्युपगम सिद्धान्त है, जैसे शब्द क्या वस्तु ? इस विचार के प्रसङ्ग में कोई कहता है कि-शब्द भले ही द्रव्य हो परन्तु वह नित्य है या अनित्य है ? इस विचार को अभ्युपगमसिद्धान्त कहते हैं । वस्तुतः नैयायिकोक्त ये चारों ही सिद्धान्त ज्ञान के भेद से भिन्न नहीं हैं और ज्ञान आत्मा का गुण है इसलिए गुणीरूप आत्मा के ग्रहण से ही उसके गुणों का भी ग्रहण हो जाता है इसलिए इनको अलग ग्रहण करना नैयायिकों की भूल । अब अवयव बताये जाते हैं-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, और निगमन ये पाँच अवयव हैं । इनमें साध्य अर्थ को बताना प्रतिज्ञा है, जैसे शब्द नित्य है, यह कहना अथवा शब्द अनित्य है, यह कहना प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा में रखे हुए अर्थ को जो बोध कराता है, उसे हेतु कहते हैं जैसे शब्द अनित्य है क्योंकि वह उत्पत्ति धर्मवाला हैं । यहां उत्पत्ति धर्मवाला कहना हेतु है । साध्य की सदृशता अथवा विशदृशता को लेकर दृष्टान्त देना उदाहरण है, जैसे कि - 'घट' । यह उदाहरण है । वैधर्म्य उदाहरण यह है-जैसे कि जो अनित्य नहीं होता है, वह उत्पत्तिवाला नहीं होता है, जैसे आकाश । यह वैसा है या वैसा नहीं है, इस प्रकार पक्ष में धर्म को रखना उपनय है । जैसे शब्द अनित्य हैं क्योंकि वह कृतक ( किया हुआ) है, जैसे घट, उसी तरह यह भी है । अथवा अनित्य न होने पर कृतक भी नहीं हो सकता है जैसे आकाश अनित्य न होने के कारण कृतक भी नहीं है परन्तु शब्द ऐसा नहीं है, इसको उपनय कहते हैं । प्रतिज्ञा और हेतु को फिर दुहराकर कहना निगमन है, जैसे कि कृतक होने के कारण शब्द अनित्य है । ये पाँच अवयव यदि शब्द मात्र हैं तो शब्द पौद्गलिक है और पुद्गलों का अजीव के ग्रहण से ही ग्रहण हो जाता है, इसलिए उन्हें अलग पदार्थ मानने की कोई आवश्यकता नहीं हैं । यदि शब्दजनित ज्ञान को पाँच अवयव कहो तो वह जीव का गुण हैं, इसलिए जीव के ग्रहण से ही उसका भी ग्रहण हो जाता है ! यदि ज्ञान के प्रत्येक भेदों को अलग-अलग पदार्थ माना जाय तब तो पदार्थ बहुत हो जायँगे क्योंकि ज्ञानों के भेद अनेक प्रकार के होते हैं । संशय होने के पश्चात् किसी पदार्थ के होने की संभावना करना तर्क है, वह तर्क सत् अर्थ का पर्य्यालोचन स्वरूप हैं । जैसे कि यहाँ स्थाणु अथवा पुरुष होना संभव है । परन्तु यह तर्क भी एक प्रकार का ज्ञान ही है, अतः ज्ञाता से अभिन्न ज्ञान के भेदों को अलग पदार्थ मानना विद्वान् पसन्द नहीं करते है । संशय और तर्क के पश्चात् होनेवाला जो निश्चयात्मक ज्ञान है, उसे निर्णय कहते हैं, यह भी पहले के समान ही ज्ञान से भिन्न नहीं है तथा यह निर्णय निश्चयरूप है, इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों में ही अन्तर्भूत हो जाता है, अतः इसे
५४१