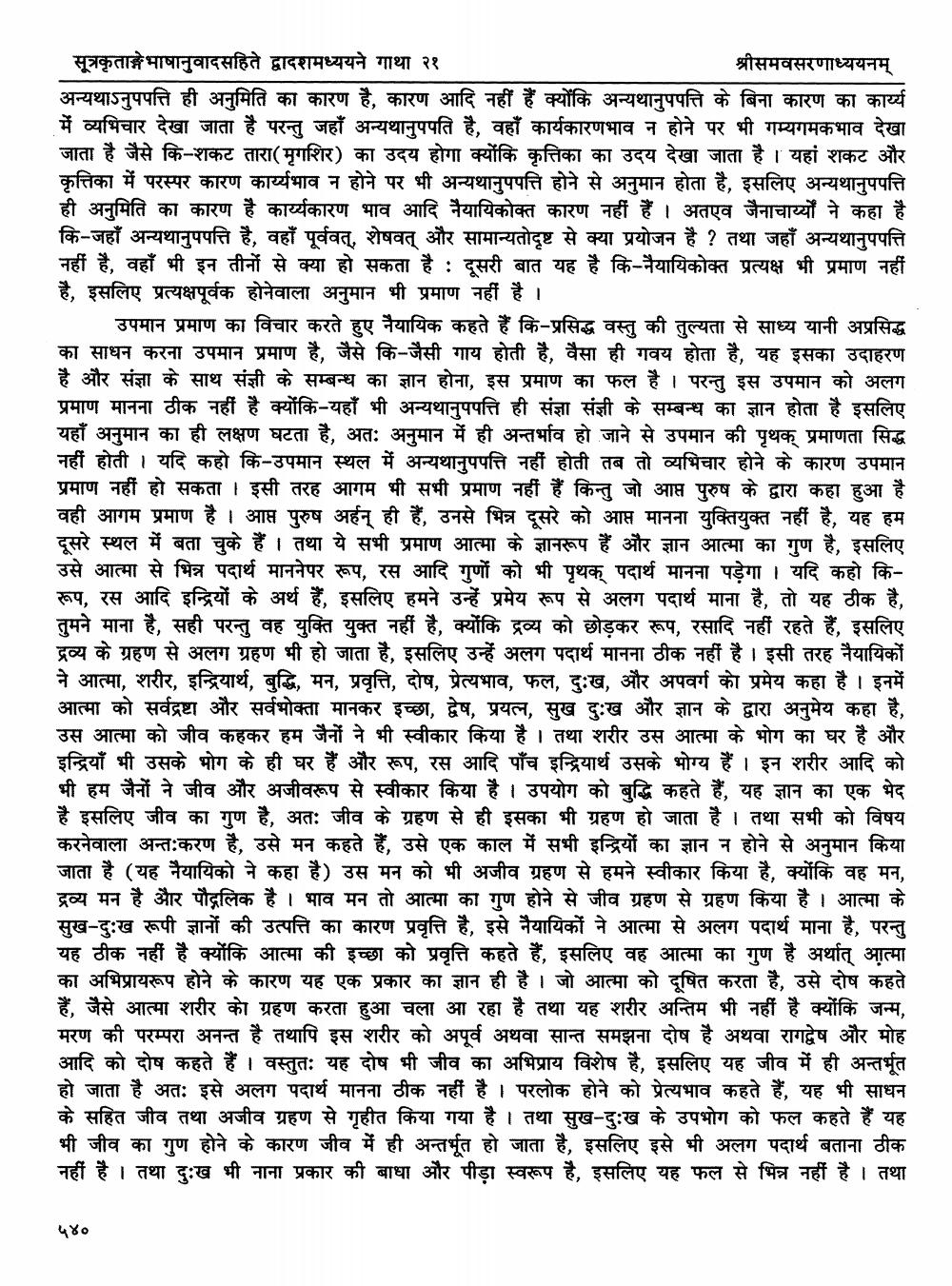________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते द्वादशमध्ययने गाथा २१
श्रीसमवसरणाध्ययनम् अन्यथाऽनुपपत्ति ही अनुमिति का कारण है, कारण आदि नहीं हैं क्योंकि अन्यथानुपपत्ति के बिना कारण का कार्य में व्यभिचार देखा जाता है परन्तु जहाँ अन्यथानुपपति है, वहाँ कार्यकारणभाव न होने पर भी गम्यगमकभाव देखा जाता है जैसे कि-शकट तारा(मृगशिर) का उदय होगा क्योंकि कृत्तिका का उदय देखा जाता है। यहां शकट और कृत्तिका में परस्पर कारण कार्यभाव न होने पर भी अन्यथानुपपत्ति होने से अनुमान होता है, इसलिए अन्यथानुपपत्ति ही अनुमिति का कारण है कार्यकारण भाव आदि नैयायिकोक्त कारण नहीं हैं । अतएव जैनाचार्यों ने कहा है कि-जहाँ अन्यथानुपपत्ति है, वहाँ पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यतोदृष्ट से क्या प्रयोजन है ? तथा जहाँ अन्यथानुपपत्ति नहीं है, वहाँ भी इन तीनों से क्या हो सकता है : दूसरी बात यह है कि-नैयायिकोक्त प्रत्यक्ष भी प्रमाण नहीं है, इसलिए प्रत्यक्षपूर्वक होनेवाला अनुमान भी प्रमाण नहीं है।
उपमान प्रमाण का विचार करते हुए नैयायिक कहते हैं कि-प्रसिद्ध वस्तु की तुल्यता से साध्य यानी अप्रसिद्ध का साधन करना उपमान प्रमाण है, जैसे कि-जैसी गाय होती है, वैसा ही गवय होता है, यह इसका उदाहरण है और संज्ञा के साथ संज्ञी के सम्बन्ध का ज्ञान होना, इस प्रमाण का फल है । परन्तु इस उपमान को अलग प्रमाण मानना ठीक नहीं है क्योंकि-यहाँ भी अन्यथानुपपत्ति ही संज्ञा संज्ञी के सम्बन्ध का ज्ञान होता है इसलिए यहाँ अनुमान का ही लक्षण घटता है, अतः अनुमान में ही अन्तर्भाव हो जाने से उपमान की पृथक प्रमाणता सिद्ध नहीं होती । यदि कहो कि-उपमान स्थल में अन्यथानुपपत्ति नहीं होती तब तो व्यभिचार होने के कारण उपमान प्रमाण नहीं हो सकता । इसी तरह आगम भी सभी प्रमाण नहीं हैं किन्तु जो आप्त पुरुष के द्वारा कहा हुआ है वही आगम प्रमाण है। आप्त पुरुष अर्हन् ही हैं, उनसे भिन्न दूसरे को आप्त मानना युक्तियुक्त नहीं है, यह हम दूसरे स्थल में बता चुके हैं। तथा ये सभी प्रमाण आत्मा के ज्ञानरूप हैं और ज्ञान आत्मा का गुण है, इसलिए उसे आत्मा से भिन्न पदार्थ माननेपर रूप, रस आदि गुणों को भी पृथक् पदार्थ मानना पड़ेगा । यदि कहो किरूप, रस आदि इन्द्रियों के अर्थ हैं, इसलिए हमने उन्हें प्रमेय रूप से अलग पदार्थ माना है, तो यह ठीक है, तुमने माना है, सही परन्तु वह युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि द्रव्य को छोड़कर रूप, रसादि नहीं रहते हैं, इसलिए द्रव्य के ग्रहण से अलग ग्रहण भी हो जाता है, इसलिए उन्हें अलग पदार्थ मानना ठीक नहीं है । इसी तरह नैयायिकों ने आत्मा, शरीर, इन्द्रियार्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख, और अपवर्ग को प्रमेय कहा है। इनमें आत्मा को सर्वद्रष्टा और सर्वभोक्ता मानकर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुःख और ज्ञान के द्वारा अनुमेय कहा है, उस आत्मा को जीव कहकर हम जैनों ने भी स्वीकार किया है । तथा शरीर उस आत्मा के भोग का घर है और इन्द्रियाँ भी उसके भोग के ही घर हैं और रूप, रस आदि पाँच इन्द्रियार्थ उसके भोग्य हैं । इन शरीर आदि को भी हम जैनों ने जीव और अजीवरूप से स्वीकार किया है । उपयोग को बुद्धि कहते हैं, यह ज्ञान का एक भेद है इसलिए जीव का गुण है, अतः जीव के ग्रहण से ही इसका भी ग्रहण हो जाता है । तथा सभी को विषय करनेवाला अन्तःकरण है, उसे मन कहते हैं, उसे एक काल में सभी इन्द्रियों का ज्ञान न होने से अनुमान किया जाता है (यह नैयायिको ने कहा है) उस मन को भी अजीव ग्रहण से हमने स्वीकार किया है, क्योंकि वह मन, द्रव्य मन है और पौगलिक है। भाव मन तो आत्मा का गुण होने से जीव ग्रहण से ग्रहण किया है। आत्मा के सुख-दुःख रूपी ज्ञानों की उत्पत्ति का कारण प्रवृत्ति है, इसे नैयायिकों ने आत्मा से अलग पदार्थ माना है, परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा की इच्छा को प्रवृत्ति कहते हैं, इसलिए वह आत्मा का गुण है अर्थात् आत्मा का अभिप्रायरूप होने के कारण यह एक प्रकार का ज्ञान ही है । जो आत्मा को दूषित करता है, उसे दोष कहते हैं, जैसे आत्मा शरीर को ग्रहण करता हुआ चला आ रहा है तथा यह शरीर अन्तिम भी नहीं है क्योंकि जन्म, मरण की परम्परा अनन्त है तथापि इस शरीर को अपूर्व अथवा सान्त समझना दोष है अथवा रागद्वेष और मोह आदि को दोष कहते हैं । वस्तुतः यह दोष भी जीव का अभिप्राय विशेष है, इसलिए यह जीव में ही अन्तर्भूत हो जाता है अतः इसे अलग पदार्थ मानना ठीक नहीं है । परलोक होने को प्रेत्यभाव कहते हैं, यह भी साधन के सहित जीव तथा अजीव ग्रहण से गृहीत किया गया है । तथा सुख-दुःख के उपभोग को फल कहते हैं यह भी जीव का गुण होने के कारण जीव में ही अन्तर्भूत हो जाता है, इसलिए इसे भी अलग पदार्थ बताना ठीक नहीं है । तथा दुःख भी नाना प्रकार की बाधा और पीड़ा स्वरूप है, इसलिए यह फल से भिन्न नहीं है । तथा