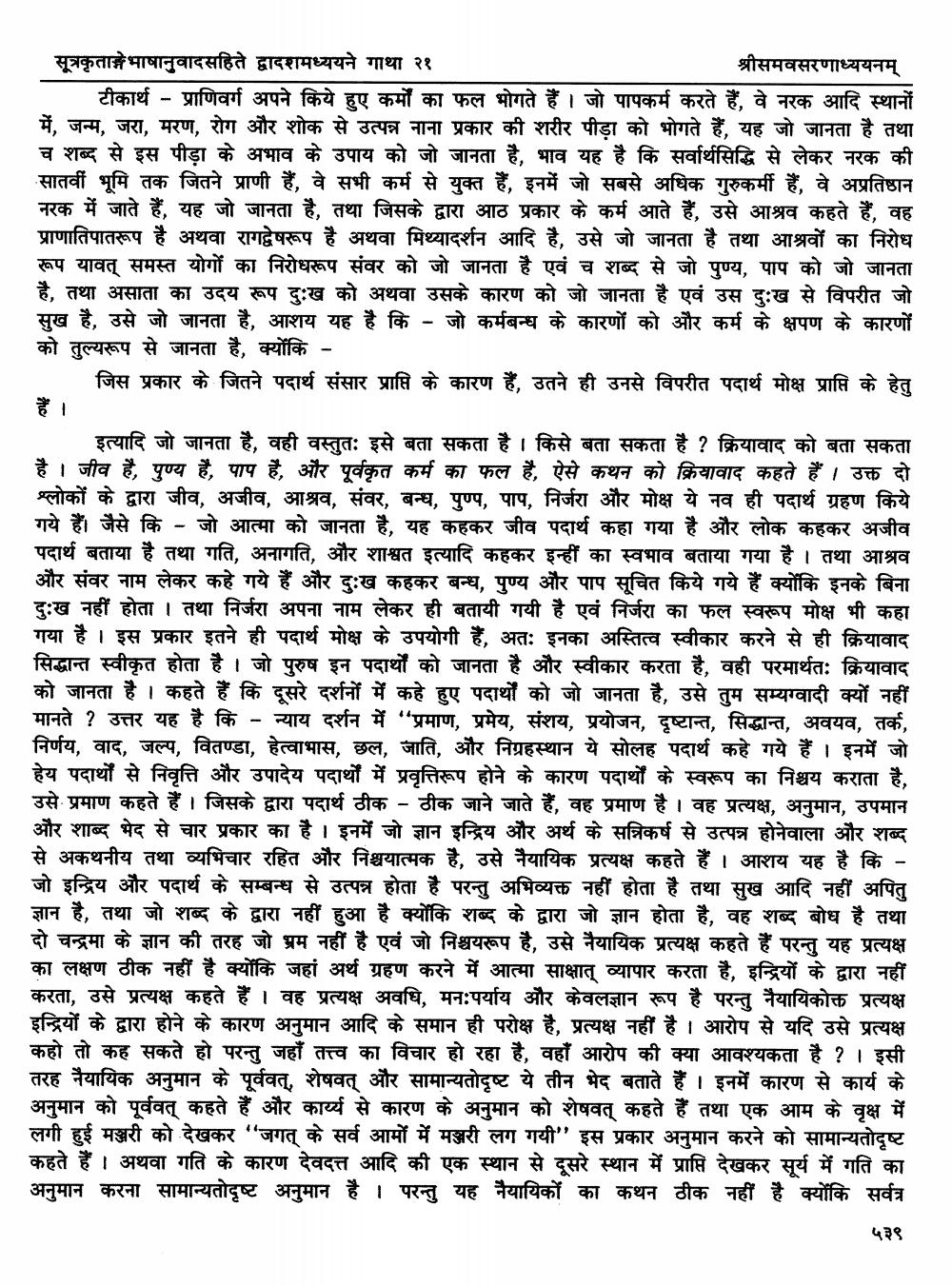________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते द्वादशमध्ययने गाथा २१
श्रीसमवसरणाध्ययनम् टीकार्थ - प्राणिवर्ग अपने किये हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जो पापकर्म करते हैं, वे नरक आदि स्थानों में, जन्म, जरा, मरण, रोग और शोक से उत्पन्न नाना प्रकार की शरीर पीड़ा को भोगते हैं, यह जो जानता है तथा च शब्द से इस पीड़ा के अभाव के उपाय को जो जानता है, भाव यह है कि सर्वार्थसिद्धि से लेकर नरक की सातवीं भूमि तक जितने प्राणी हैं, वे सभी कर्म से युक्त हैं, इनमें जो सबसे अधिक गुरुकर्मी हैं, वे अप्रतिष्ठान नरक में जाते हैं, यह जो जानता है, तथा जिसके द्वारा आठ प्रकार के कर्म आते हैं, उसे आश्रव कहते हैं, वह प्राणातिपातरूप है अथवा रागद्वेषरूप है अथवा मिथ्यादर्शन आदि है, उसे जो जानता है तथा आश्रवों का निरोध रूप यावत् समस्त योगों का निरोधरूप संवर को जो जानता है एवं च शब्द से जो पुण्य, पाप को जो जानता है, तथा असाता का उदय रूप दुःख को अथवा उसके कारण को जो जानता है एवं उस दुःख से विपरीत जो सुख है, उसे जो जानता है, आशय यह है कि - जो कर्मबन्ध के कारणों को और कर्म के क्षपण के कारणों को तुल्यरूप से जानता है, क्योंकि -
जिस प्रकार के जितने पदार्थ संसार प्राप्ति के कारण हैं, उतने ही उनसे विपरीत पदार्थ मोक्ष प्राप्ति के हेतु
इत्यादि जो जानता है, वही वस्तुतः इसे बता सकता है । किसे बता सकता है ? क्रियावाद को बता सकता है । जीव है, पुण्य है, पाप है, और पूर्वकृत कर्म का फल है, ऐसे कथन को क्रियावाद कहते हैं । उक्त दो श्लोकों के द्वारा जीव, अजीव, आश्रव, संवर, बन्ध, पुष्प, पाप, निर्जरा और मोक्ष ये नव ही पदार्थ ग्रहण किये गये हैं। जैसे कि - जो आत्मा को जानता है, यह कहकर जीव पदार्थ कहा गया है और लोक कहकर अजीव पदार्थ बताया है तथा गति, अनागति, और शाश्वत इत्यादि कहकर इन्हीं का स्वभाव बताया गया है। तथा आश्रव
और संवर नाम लेकर कहे गये हैं और दुःख कहकर बन्ध, पुण्य और पाप सूचित किये गये हैं क्योंकि इनके बिना दुःख नहीं होता । तथा निर्जरा अपना नाम लेकर ही बतायी गयी है एवं निर्जरा का फल स्वरूप मोक्ष भी कहा गया है । इस प्रकार इतने ही पदार्थ मोक्ष के उपयोगी हैं, अतः इनका अस्तित्व स्वीकार करने से ही क्रियावाद सिद्धान्त स्वीकृत होता है । जो पुरुष इन पदार्थों को जानता है और स्वीकार करता है, वही परमार्थतः क्रियावाद को जानता है । कहते हैं कि दूसरे दर्शनों में कहे हुए पदार्थों को जो जानता है, उसे तुम सम्यग्वादी क्यों नहीं मानते ? उत्तर यह है कि - न्याय दर्शन में "प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, और निग्रहस्थान ये सोलह पदार्थ कहे गये हैं। इनमें जो हेय पदार्थों से निवृत्ति और उपादेय पदार्थों में प्रवृत्तिरूप होने के कारण पदार्थों के स्वरूप का निश्चय कराता है, उसे प्रमाण कहते हैं। जिसके द्वारा पदार्थ ठीक - ठीक जाने जाते हैं, वह प्रमाण है। वह प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाब्द भेद से चार प्रकार का है। इनमें जो ज्ञान इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होनेवाला और शब्द से अकथनीय तथा व्यभिचार रहित और निश्चयात्मक है, उसे नैयायिक प्रत्यक्ष कहते हैं । आशय यह है कि - जो इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है परन्तु अभिव्यक्त नहीं होता है तथा सुख आदि नहीं अपितु ज्ञान है, तथा जो शब्द के द्वारा नहीं हुआ है क्योंकि शब्द के द्वारा जो ज्ञान होता है, वह शब्द बोध है तथा दो चन्द्रमा के ज्ञान की तरह जो भ्रम नहीं है एवं जो निश्चयरूप है, उसे नैयायिक प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु यह प्रत्यक्ष का लक्षण ठीक नहीं है क्योंकि जहां अर्थ ग्रहण करने में आत्मा साक्षात् व्यापार करता है, इन्द्रियों के द्वारा नहीं करता, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। वह प्रत्यक्ष अवधि, मनःपर्याय और केवलज्ञान रूप है परन्तु नैयायिकोक्त प्रत्यक्ष इन्द्रियों के द्वारा होने के कारण अनुमान आदि के समान ही परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। आरोप से यदि उसे प्रत्यक्ष कहो तो कह सकते हो परन्तु जहाँ तत्त्व का विचार हो रहा है, वहाँ आरोप की क्या आवश्यकता है ? । इसी तरह नैयायिक अनुमान के पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यतोदृष्ट ये तीन भेद बताते हैं । इनमें कारण से कार्य के अनुमान को पूर्ववत् कहते हैं और कार्य से कारण के अनुमान को शेषवत् कहते हैं तथा एक आम के वृक्ष में लगी हुई मञ्जरी को देखकर "जगत् के सर्व आमों में मञ्जरी लग गयी" इस प्रकार अनुमान करने को सामान्यतोदृष्ट कहते हैं । अथवा गति के कारण देवदत्त आदि की एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राप्ति देखकर सर्य में गति का अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट अनुमान है । परन्तु यह नैयायिकों का कथन ठीक नहीं है क्योंकि सर्वत्र
५३९