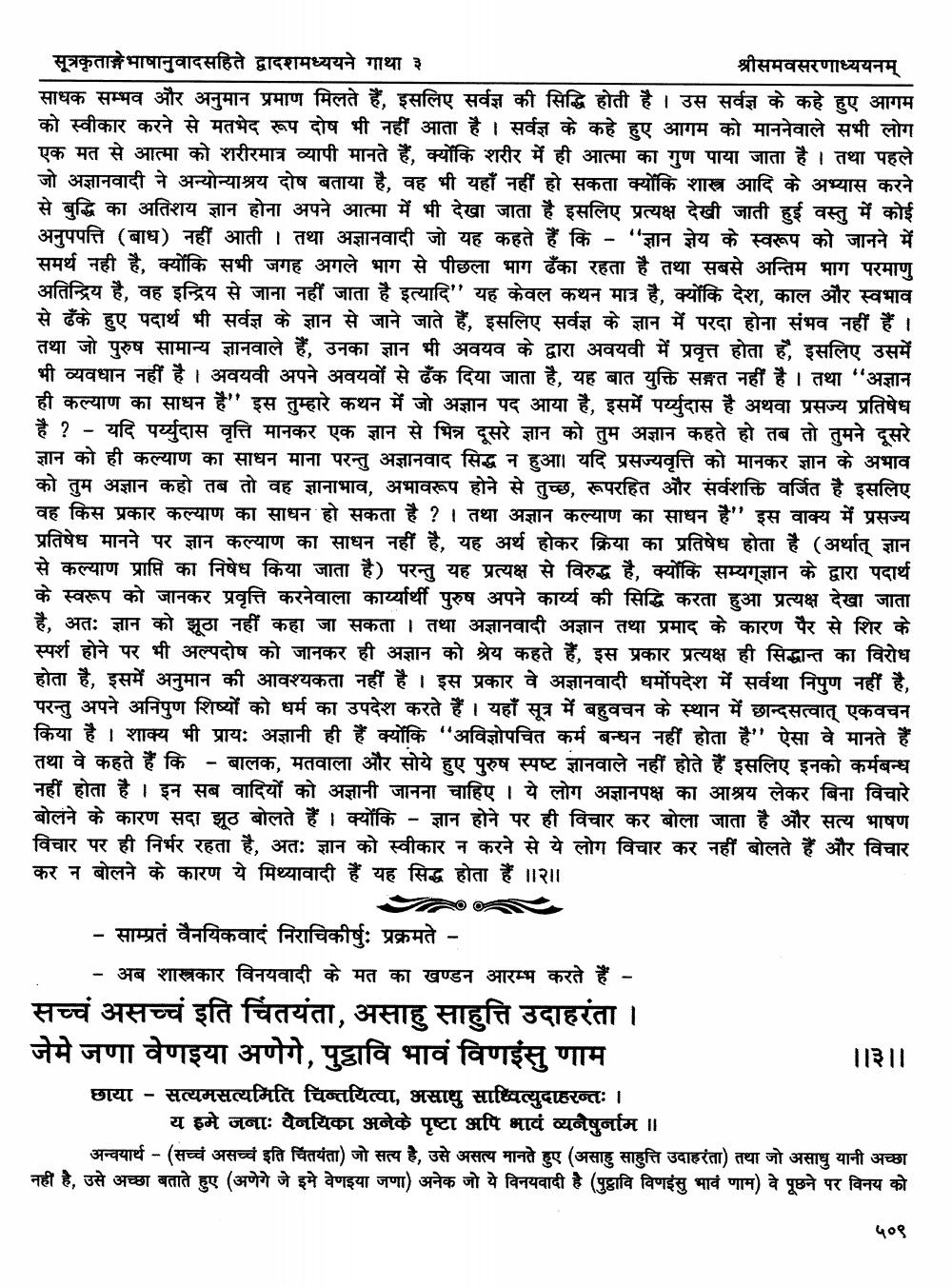________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते द्वादशमध्ययने गाथा ३
श्रीसमवसरणाध्ययनम् साधक सम्भव और अनुमान प्रमाण मिलते हैं, इसलिए सर्वज्ञ की सिद्धि होती है । उस सर्वज्ञ के कहे हुए आग को स्वीकार करने से मतभेद रूप दोष भी नहीं आता है । सर्वज्ञ के कहे हुए आगम को माननेवाले सभी लोग एक मत से आत्मा को शरीरमात्र व्यापी मानते हैं, क्योंकि शरीर में ही आत्मा का गुण पाया जाता है । तथा पहले जो अज्ञानवादी ने अन्योन्याश्रय दोष बताया है, वह भी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि शास्त्र आदि के अभ्यास करने से बुद्धि का अतिशय ज्ञान होना अपने आत्मा में भी देखा जाता है इसलिए प्रत्यक्ष देखी जाती हुई वस्तु में कोई अनुपपत्ति (बाध) नहीं आती । तथा अज्ञानवादी जो यह कहते हैं कि "ज्ञान ज्ञेय के स्वरूप को जानने में समर्थ नही है, क्योंकि सभी जगह अगले भाग से पीछला भाग ढँका रहता है तथा सबसे अन्तिम भाग परमाणु अतिन्द्रिय है, वह इन्द्रिय से जाना नहीं जाता है इत्यादि" यह केवल कथन मात्र है, क्योंकि देश, काल और स्वभाव से ढँके हुए पदार्थ भी सर्वज्ञ के ज्ञान से जाने जाते हैं, इसलिए सर्वज्ञ के ज्ञान में परदा होना संभव नहीं हैं । तथा जो पुरुष सामान्य ज्ञानवाले हैं, उनका ज्ञान भी अवयव के द्वारा अवयवी में प्रवृत्त होता है, इसलिए उसमें भी व्यवधान नहीं है। अवयवी अपने अवयवों से ढँक दिया जाता है, यह बात युक्ति सङ्गत नहीं है । तथा "अज्ञान ही कल्याण का साधन है" इस तुम्हारे कथन में जो अज्ञान पद आया है, इसमें पर्य्युदास है अथवा प्रसज्य प्रतिषेध है ? यदि पर्युदास वृत्ति मानकर एक ज्ञान से भिन्न दूसरे ज्ञान को तुम अज्ञान कहते हो तब तो तुमने दूसरे ज्ञान को ही कल्याण का साधन माना परन्तु अज्ञानवाद सिद्ध न हुआ। यदि प्रसज्यवृत्ति को मानकर ज्ञान के अभाव को तुम अज्ञान कहो तब तो वह ज्ञानाभाव, अभावरूप होने से तुच्छ, रूपरहित और सर्वशक्ति वर्जित है इसलिए वह किस प्रकार कल्याण का साधन हो सकता है ? । तथा अज्ञान कल्याण का साधन है" इस वाक्य में प्रसज्य प्रतिषेध मानने पर ज्ञान कल्याण का साधन नहीं है, यह अर्थ होकर क्रिया का प्रतिषेध होता है ( अर्थात् ज्ञान से कल्याण प्राप्ति का निषेध किया जाता है) परन्तु यह प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, क्योंकि सम्यग्ज्ञान के द्वारा पदार्थ के स्वरूप को जानकर प्रवृत्ति करनेवाला कार्य्यार्थी पुरुष अपने कार्य्य की सिद्धि करता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है, अतः ज्ञान को झूठा नहीं कहा जा सकता । तथा अज्ञानवादी अज्ञान तथा प्रमाद के कारण पैर से शिर के स्पर्श होने पर भी अल्पदोष को जानकर ही अज्ञान को श्रेय कहते हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष ही सिद्धान्त का विरोध होता है, इसमें अनुमान की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार वे अज्ञानवादी धर्मोपदेश में सर्वथा निपुण नहीं है, परन्तु अपने अनिपुण शिष्यों को धर्म का उपदेश करते हैं । यहाँ सूत्र में बहुवचन के स्थान में छान्दसत्वात् एकवचन किया है । शाक्य भी प्रायः अज्ञानी ही हैं क्योंकि "अविज्ञोपचित कर्म बन्धन नहीं होता है" ऐसा वे मानते हैं तथा वे कहते हैं कि बालक, मतवाला और सोये हुए पुरुष स्पष्ट ज्ञानवाले नहीं होते हैं इसलिए इनको कर्मबन्ध नहीं होता है । इन सब वादियों को अज्ञानी जानना चाहिए। ये लोग अज्ञानपक्ष का आश्रय लेकर बिना विचारे बोलने के कारण सदा झूठ बोलते हैं। क्योंकि ज्ञान होने पर ही विचार कर बोला जाता है और सत्य भाषण विचार पर ही निर्भर रहता है, अतः ज्ञान को स्वीकार न करने से ये लोग विचार कर नहीं बोलते हैं और विचार कर न बोलने के कारण ये मिथ्यावादी हैं यह सिद्ध होता हैं ||२||
साम्प्रतं वैनयिकवादं निराचिकीर्षुः प्रक्रम
अब शास्त्रकार विनयवादी के मत का खण्डन आरम्भ करते हैं
सच्चं असच्चं इति चिंतयंता, असाहु साहुत्ति उदाहरंता ।
जेमे जणा वेणइया अणेगे, पुट्ठावि भावं विणईंसु णाम
छाया
---
-
-
सत्यमसत्यमिति चिन्तयित्वा, असाधु साध्वित्युदाहरन्तः । य हमे जनाः वैनयिका अनेके पृष्टा अपि भावं व्यनेषुर्नाम ||
॥३॥
अन्वयार्थ - ( सच्चं असच्चं इति चिंतयंता) जो सत्य है, उसे असत्य मानते हुए (असाहु साहुत्ति उदाहरंता) तथा जो असाधु यानी अच्छा नहीं है, उसे अच्छा बताते हुए (अणेगे जे इमे वेणइया जणा ) अनेक जो ये विनयवादी है ( पुट्ठावि विणइंसु भावं णाम) वे पूछने पर विनय को
५०९