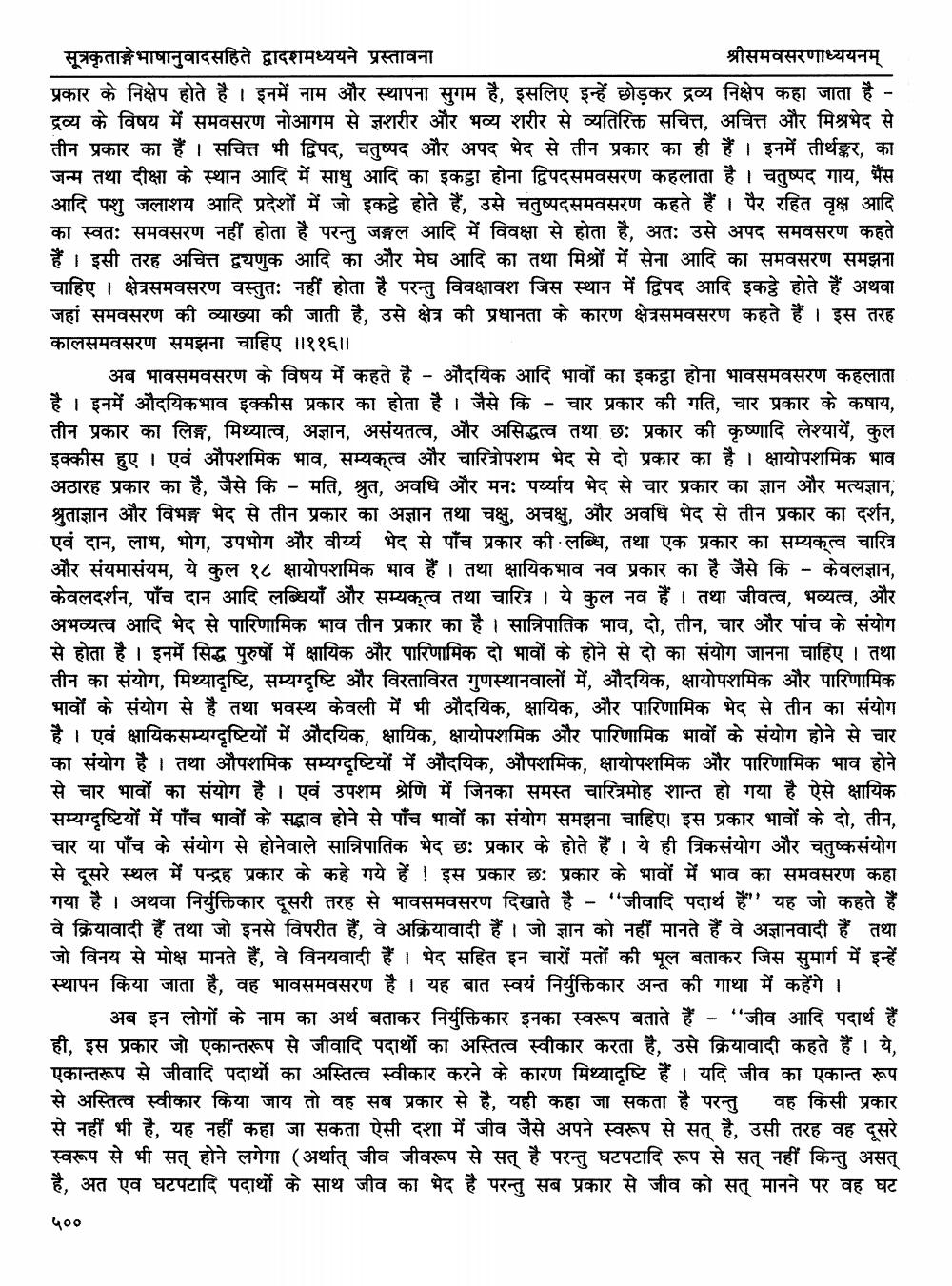________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते द्वादशमध्ययने प्रस्तावना
श्रीसमवसरणाध्ययनम् प्रकार के निक्षेप होते है । इनमें नाम और स्थापना सुगम है, इसलिए इन्हें छोड़कर द्रव्य निक्षेप कहा जाता है - द्रव्य के विषय में समवसरण नोआगम से ज्ञशरीर और भव्य शरीर से व्यतिरिक्त सचित्त, अचित्त और मिश्रभेद से तीन प्रकार का हैं । सचित्त भी द्विपद, चतुष्पद और अपद भेद से तीन प्रकार का ही हैं। इनमें तीर्थङ्कर, का जन्म तथा दीक्षा के स्थान आदि में साधु आदि का इकट्ठा होना द्विपदसमवसरण कहलाता है । चतुष्पद गाय, भैंस आदि पशु जलाशय आदि प्रदेशों में जो इकट्ठे होते हैं, उसे चतुष्पदसमवसरण कहते हैं । पैर रहित वृक्ष आदि का स्वतः समवसरण नहीं होता है परन्तु जङ्गल आदि में विवक्षा से होता है, अतः उसे अपद समवसरण कहते हैं । इसी तरह अचित्त द्वयणुक आदि का और मेघ आदि का तथा मिश्रों में सेना आदि का समवसरण समझना चाहिए । क्षेत्रसमवसरण वस्तुतः नहीं होता है परन्तु विवक्षावश जिस स्थान में द्विपद आदि इकट्ठे होते हैं अथवा जहां समवसरण की व्याख्या की जाती है, उसे क्षेत्र की प्रधानता के कारण क्षेत्रसमवसरण कहते हैं । इस तरह कालसमवसरण समझना चाहिए ॥११६।।
अब भावसमवसरण के विषय में कहते है - औदयिक आदि भावों का इकट्ठा होना भावसमवसरण कहलाता है । इनमें औदयिकभाव इक्कीस प्रकार का होता है। जैसे कि - चार प्रकार की गति, चार प्रकार के कषाय, तीन प्रकार का लिङ्ग, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयतत्व, और असिद्धत्व तथा छः प्रकार की कृष्णादि लेश्यायें, कुल इक्कीस हुए । एवं औपशमिक भाव, सम्यक्त्व और चारित्रोपशम भेद से दो प्रकार का है । क्षायोपशमिक भाव अठारह प्रकार का है, जैसे कि - मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्याय भेद से चार प्रकार का ज्ञान और मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान और विभङ्ग भेद से तीन प्रकार का अज्ञान तथा चक्षु, अचक्षु, और अवधि भेद से तीन प्रकार का दर्शन, एवं दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य्य भेद से पाँच प्रकार की लब्धि, तथा एक प्रकार का सम्यक्त्व चारित्र
और संयमासंयम, ये कुल १८ क्षायोपशमिक भाव हैं। तथा क्षायिकभाव नव प्रकार का है जैसे कि - केवलज्ञान, केवलदर्शन, पाँच दान आदि लब्धियाँ और सम्यक्त्व तथा चारित्र । ये कुल नव हैं । तथा जीवत्व, भव्यत्व, और अभव्यत्व आदि भेद से पारिणामिक भाव तीन प्रकार का है। सान्निपातिक भाव, दो, तीन, चार और पांच के संयोग से होता है। इनमें सिद्ध पुरुषों में क्षायिक और पारिणामिक दो भावों के होने से दो का संयोग जानना चाहिए । तथा तीन का संयोग, मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि और विरताविरत गुणस्थानवालों में, औदयिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक भावों के संयोग से है तथा भवस्थ केवली में भी औदयिक, क्षायिक, और पारिणामिक भेद से तीन का संयोग है । एवं क्षायिकसम्यग्दृष्टियों में औदयिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक भावों के संयोग होने से चार का संयोग है । तथा औपशमिक सम्यग्दृष्टियों में औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक भाव होने से चार भावों का संयोग है । एवं उपशम श्रेणि में जिनका समस्त चारित्रमोह शान्त हो गया है ऐसे क्षायिक सम्यग्दृष्टियों में पाँच भावों के सद्भाव होने से पाँच भावों का संयोग समझना चाहिए। इस प्रकार भावों के दो, तीन,
संयोग से होनेवाले सान्निपातिक भेद छः प्रकार के होते हैं । ये ही त्रिकसंयोग और चतुष्कसंयोग से दूसरे स्थल में पन्द्रह प्रकार के कहे गये हैं ! इस प्रकार छः प्रकार के भावों में भाव का समवसरण कहा गया है । अथवा नियुक्तिकार दूसरी तरह से भावसमवसरण दिखाते है - "जीवादि पदार्थ हैं" यह जो कहते हैं वे क्रियावादी हैं तथा जो इनसे विपरीत हैं, वे अक्रियावादी हैं। जो ज्ञान को नहीं मानते हैं वे अज्ञानवादी हैं तथा जो विनय से मोक्ष मानते हैं, वे विनयवादी हैं । भेद सहित इन चारों मतों की भूल बताकर जिस सुमार्ग में इन्हें स्थापन किया जाता है, वह भावसमवसरण है । यह बात स्वयं नियुक्तिकार अन्त की गाथा में कहेंगे।
अब इन लोगों के नाम का अर्थ बताकर नियुक्तिकार इनका स्वरूप बताते हैं - "जीव आदि पदार्थ हैं ही, इस प्रकार जो एकान्तरूप से जीवादि पदार्थो का अस्तित्व स्वीकार करता है, उसे क्रियावादी कहते हैं । ये, एकान्तरूप से जीवादि पदार्थो का अस्तित्व स्वीकार करने के कारण मिथ्यादृष्टि हैं । यदि जीव का एकान्त रूप से अस्तित्व स्वीकार किया जाय तो वह सब प्रकार से है, यही कहा जा सकता है परन्तु वह किसी प्रकार से नहीं भी है, यह नहीं कहा जा सकता ऐसी दशा में जीव जैसे अपने स्वरूप से सत् है, उसी तरह वह दूसरे स्वरूप से भी सत् होने लगेगा (अर्थात् जीव जीवरूप से सत् है परन्तु घटपटादि रूप से सत् नहीं किन्तु असत् है, अत एव घटपटादि पदार्थो के साथ जीव का भेद है परन्तु सब प्रकार से जीव को सत् मानने पर वह घट
५००