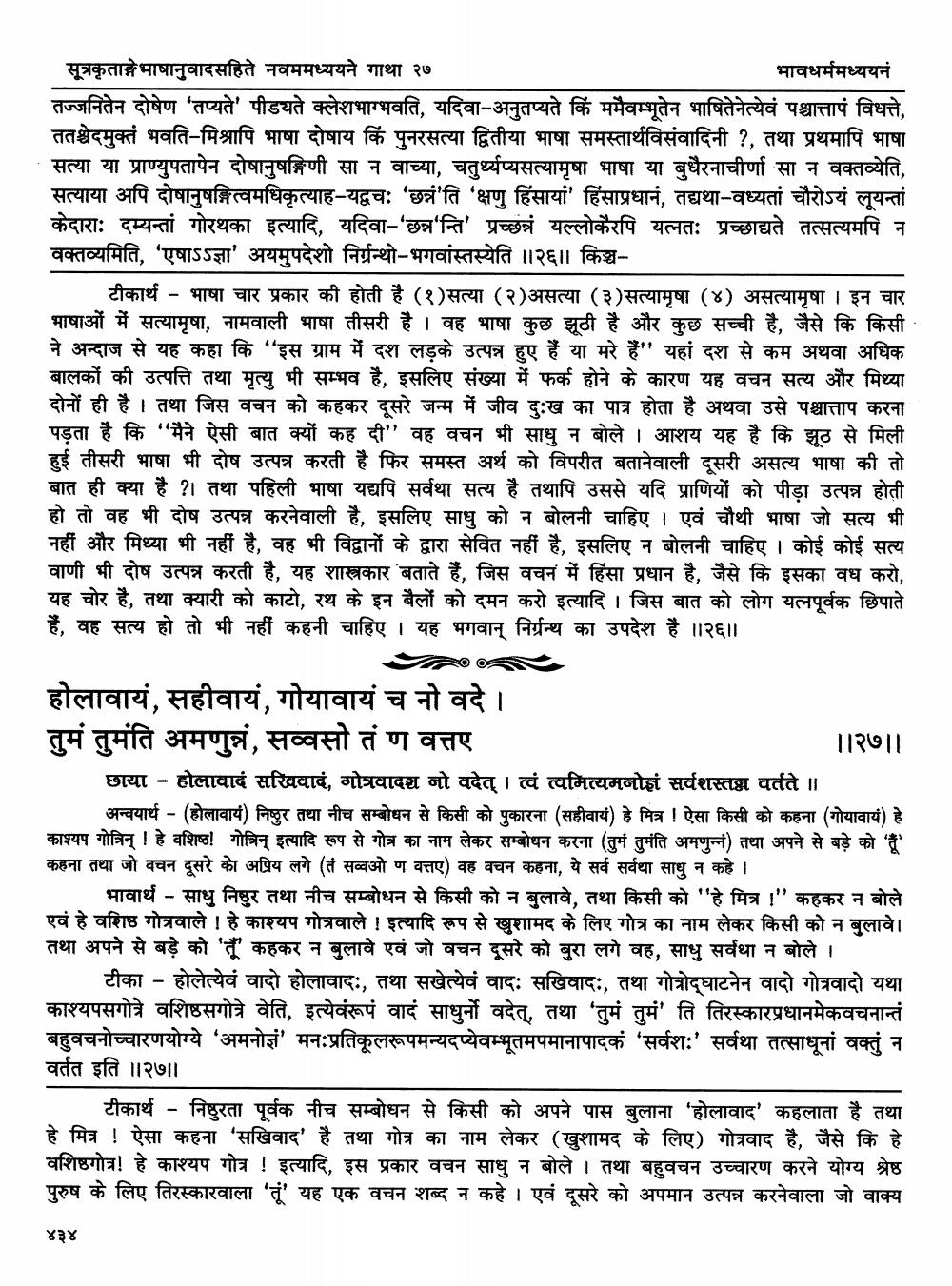________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते नवममध्ययने गाथा २७
भावधर्ममध्ययनं तज्जनितेन दोषेण 'तप्यते' पीडयते क्लेशभाग्भवति, यदिवा-अनुतप्यते किं ममैवम्भूतेन भाषितेनेत्येवं पश्चात्तापं विधत्ते, ततश्चेदमुक्तं भवति-मिश्रापि भाषा दोषाय किं पुनरसत्या द्वितीया भाषा समस्तार्थविसंवादिनी ?, तथा प्रथमापि भाषा सत्या या प्राण्युपतापेन दोषानुषङ्गिणी सा न वाच्या, चतुर्थ्यप्यसत्यामृषा भाषा या बुधैरनाचीर्णा सा न वक्तव्येति, सत्याया अपि दोषानुषङ्गित्वमधिकृत्याह-यद्वचः 'छन्नं'ति 'क्षणु हिंसायां' हिंसाप्रधानं, तद्यथा-वध्यतां चौरोऽयं लूयन्तां केदाराः दम्यन्तां गोरथका इत्यादि, यदिवा-'छन्न'न्ति' प्रच्छन्नं यल्लोकैरपि यत्नतः प्रच्छाद्यते तत्सत्यमपि न वक्तव्यमिति, 'एषाऽऽज्ञा' अयमुपदेशो निर्ग्रन्थो-भगवांस्तस्येति ॥२६।। किञ्च
टीकार्थ - भाषा चार प्रकार की होती है (१)सत्या (२)असत्या (३)सत्यामृषा (४) असत्यामृषा । इन चार भाषाओं में सत्यामृषा, नामवाली भाषा तीसरी है । वह भाषा कुछ झूठी है और कुछ सच्ची है, जैसे कि किसी। ने अन्दाज से यह कहा कि "इस ग्राम में दश लड़के उत्पन्न हुए हैं या मरे हैं" यहां दश से कम अथवा अधिक बालकों की उत्पत्ति तथा मृत्यु भी सम्भव है, इसलिए संख्या में फर्क होने के कारण यह वचन सत्य और मिथ्या दोनों ही है। तथा जिस वचन को कहकर दूसरे जन्म में जीव दुःख का पात्र होता है अथवा उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है कि "मैने ऐसी बात क्यों कह दी" वह वचन भी साधु न बोले । आशय यह है कि झूठ से मिली हुई तीसरी भाषा भी दोष उत्पन्न करती है फिर समस्त अर्थ को विपरीत बतानेवाली दूसरी असत्य भाषा की तो बात ही क्या है ?। तथा पहिली भाषा यद्यपि सर्वथा सत्य है तथापि उससे यदि प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न होती हो तो वह भी दोष उत्पन्न करनेवाली है, इसलिए साधु को न बोलनी चाहिए । एवं चौथी भाषा जो सत्य भी नहीं और मिथ्या भी नहीं है, वह भी विद्वानों के द्वारा सेवित नहीं है, इसलिए न बोलनी चाहिए । कोई कोई सत्य वाणी भी दोष उत्पन्न करती है, यह शास्त्रकार बताते हैं, जिस वचन में हिंसा प्रधान है, जैसे कि इसका वध करो, यह चोर है, तथा क्यारी को काटो, रथ के इन बैलों को दमन करो इत्यादि । जिस बात को लोग यत्नपर्वक छिपाते हैं, वह सत्य हो तो भी नहीं कहनी चाहिए । यह भगवान् निर्ग्रन्थ का उपदेश है ॥२६॥
होलावायं, सहीवायं, गोयावायं च नो वदे। तुमं तुमंति अमणुन्नं, सव्वसो तं ण वत्तए
॥२७॥ छाया - होलावादं सरिखवादं, गोत्रवादश नो वदेत् । त्वं त्वमित्यमनोखं सर्वशस्तन वर्तते ॥
अन्वयार्थ - (होलावाय) निष्ठुर तथा नीच सम्बोधन से किसी को पुकारना (सहीवायं) हे मित्र ! ऐसा किसी को कहना (गोयावायं) हे काश्यप गोत्रिन् । हे वशिष्ठ! गोत्रिन् इत्यादि रूप से गोत्र का नाम लेकर सम्बोधन करना (तुमं तुर्मति अमणुन्न) तथा अपने से बड़े को 'हूं' कहना तथा जो वचन दूसरे को अप्रिय लगे (तं सव्वओ ण वत्तए) वह वचन कहना, ये सर्व सर्वथा साधु न कहे।
भावार्थ - साधु निष्ठुर तथा नीच सम्बोधन से किसी को न बुलावे, तथा किसी को "हे मित्र ।" कहकर न बोले एवं हे वशिष्ठ गोत्रवाले । हे काश्यप गोत्रवाले ! इत्यादि रूप से खुशामद के लिए गोत्र का नाम लेकर किसी को न बुलावे। तथा अपने से बड़े को 'तू' कहकर न बुलावे एवं जो वचन दूसरे को बुरा लगे वह, साधु सर्वथा न बोले ।
टीका - होलेत्येवं वादो होलावादः, तथा सखेत्येवं वादः सखिवादः, तथा गोत्रोद्घाटनेन वादो गोत्रवादो यथा काश्यपसगोत्रे वशिष्ठसगोत्रे वेति, इत्येवंरूपं वादं साधु! वदेत्, तथा 'तुमं तुम' ति तिरस्कारप्रधानमेकवचनान्तं बहुवचनोच्चारणयोग्ये 'अमनोज्ञं' मनःप्रतिकूलरूपमन्यदप्येवम्भूतमपमानापादकं 'सर्वशः' सर्वथा तत्साधूनां वक्तुं न वर्तत इति ॥२७॥
टीकार्थ - निष्ठुरता पूर्वक नीच सम्बोधन से किसी को अपने पास बुलाना 'होलावाद' कहलाता है तथा हे मित्र ! ऐसा कहना 'सखिवाद' है तथा गोत्र का नाम लेकर (खुशामद के लिए) गोत्रवाद है, जैसे कि हे वशिष्ठगोत्र! हे काश्यप गोत्र ! इत्यादि, इस प्रकार वचन साधु न बोले । तथा बहुवचन उच्चारण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष के लिए तिरस्कारवाला 'तूं' यह एक वचन शब्द न कहे । एवं दूसरे को अपमान उत्पन्न करनेवाला जो वाक्य
४३४