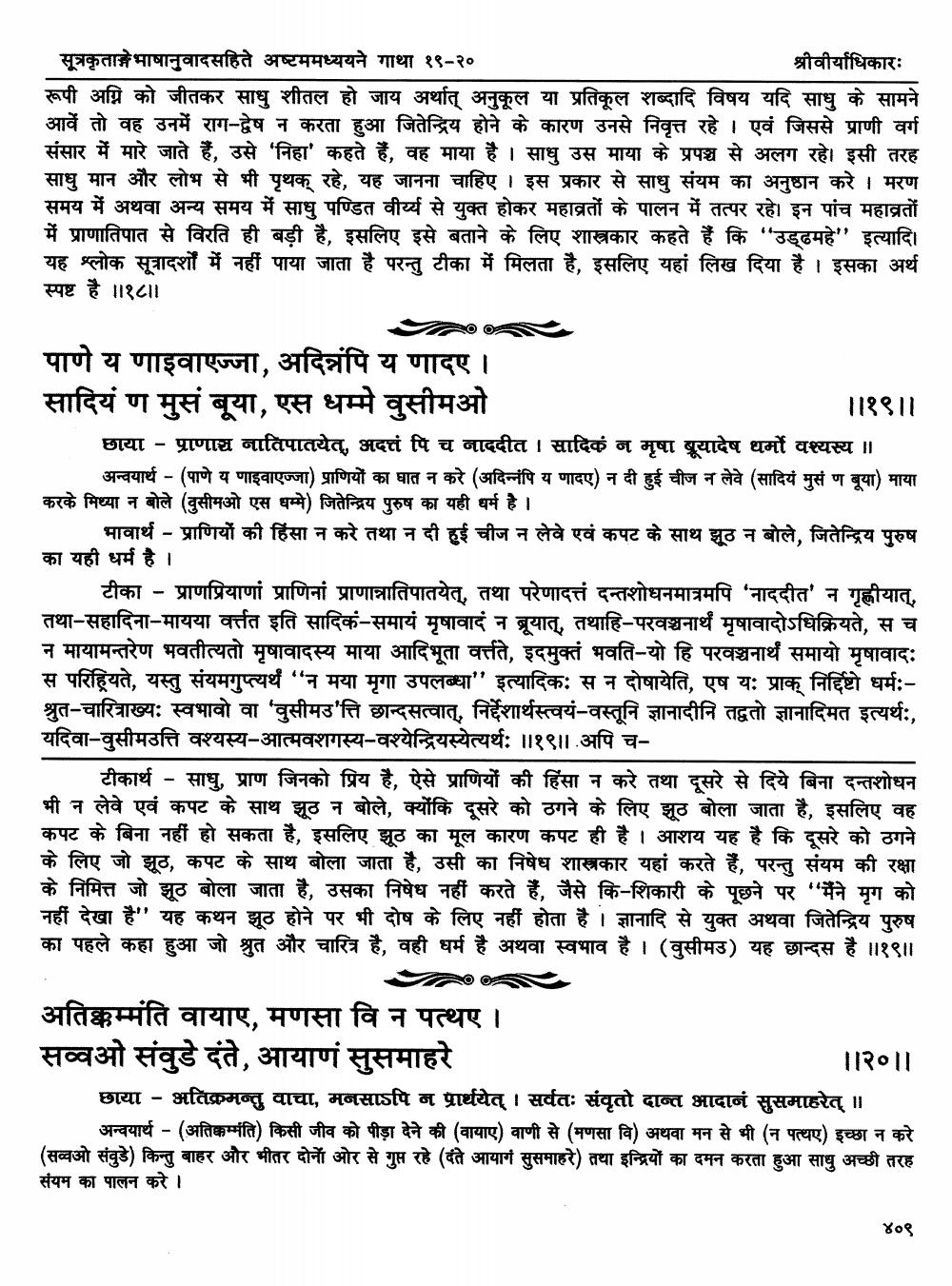________________
सूत्रकृताङ्गे भाषानुवादसहिते अष्टममध्ययने गाथा १९ - २०
श्रीवीर्याधिकारः
रूपी अग्नि को जीतकर साधु शीतल हो जाय अर्थात् अनुकूल या प्रतिकूल शब्दादि विषय यदि साधु के सामने आवें तो वह उनमें राग-द्वेष न करता हुआ जितेन्द्रिय होने के कारण उनसे निवृत्त रहे । एवं जिससे प्राणी वर्ग संसार में मारे जाते हैं, उसे 'निहा' कहते हैं, वह माया है । साधु उस माया के प्रपञ्च से अलग रहे। इसी तरह साधु मान और लोभ से भी पृथक् रहे, यह जानना चाहिए। इस प्रकार से साधु संयम का अनुष्ठान करे । मरण समय में अथवा अन्य समय में साधु पण्डित वीर्य्य से युक्त होकर महाव्रतों के पालन में तत्पर रहे। इन पांच महाव्रतों में प्राणातिपात से विरति ही बड़ी है, इसलिए इसे बताने के लिए शास्त्रकार कहते हैं कि "उड्ढमहे" इत्यादि । यह श्लोक सूत्रादर्शों में नहीं पाया जाता है परन्तु टीका में मिलता है, इसलिए यहां लिख दिया है । इसका अर्थ स्पष्ट है ||१८||
पाणे य णाइवाज्जा, अदिन्नपि य णादए ।
सादियं ण मु बूया, एस धम्मे वसीमओ
।।१९।।
छाया - प्राणाञ्च नातिपातयेत्, अदत्तं पि च नाददीत । सादिकं न मृषा ब्रूयादेष धर्मो वश्यस्य ॥ अन्वयार्थ - (पाणे य णाइवाएज्जा) प्राणियों का घात न करे ( अदिन्नंपि य णादए ) न दी हुई चीज न लेवे ( सादियं मुसं ण बूया) माया करके मिथ्या न बोले ( वुसीमओ एस धम्मे) जितेन्द्रिय पुरुष का यही धर्म है ।
भावार्थ - प्राणियों की हिंसा न करे तथा न दी हुई चीज न लेवे एवं कपट के साथ झूठ न बोले, जितेन्द्रिय पुरुष का यही धर्म है ।
टीका
प्राणप्रियाणां प्राणिनां प्राणान्नातिपातयेत्, तथा परेणादत्तं दन्तशोधनमात्रमपि 'नाददीत' न गृह्णीयात्, तथा - सहादिना - मायया वर्त्तत इति सादिकं समायं मृषावादं न ब्रूयात्, तथाहि परवञ्चनार्थं मृषावादोऽधिक्रियते, स च न मायामन्तरेण भवतीत्यतो मृषावादस्य माया आदिभूता वर्त्तते, इदमुक्तं भवति -यो हि परवञ्चनार्थं समायो मृषावादः स परिड्रियते, यस्तु संयमगुप्त्यर्थं "न मया मृगा उपलब्धा" इत्यादिकः स न दोषायेति, एष यः प्राक् निद्दिष्टो धर्मःश्रुत - चारित्राख्यः स्वभावो वा 'वुसीमउ'त्ति छान्दसत्वात्, निर्देशार्थस्त्वयं - वस्तूनि ज्ञानादीनि तद्वतो ज्ञानादिमत इत्यर्थः, यदिवा - वसीमउत्ति वश्यस्य - आत्मवशगस्य- वश्येन्द्रियस्येत्यर्थः ||१९|| अपि च
टीकार्थ साधु, प्राण जिनको प्रिय है, ऐसे प्राणियों की हिंसा न करे तथा दूसरे से दिये बिना दन्तशोधन भी न लेवे एवं कपट के साथ झूठ न बोले, क्योंकि दूसरे को ठगने के लिए झूठ बोला जाता है, इसलिए वह कपट के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए झूठ का मूल कारण कपट ही है। आशय यह है कि दूसरे को ठगने के लिए जो झूठ, कपट के साथ बोला जाता है, उसी का निषेध शास्त्रकार यहां करते हैं, परन्तु संयम की रक्षा के निमित्त जो झूठ बोला जाता है, उसका निषेध नहीं करते हैं, जैसे कि शिकारी के पूछने पर "मैंने मृग को नहीं देखा है" यह कथन झूठ होने पर भी दोष के लिए नहीं होता है। ज्ञानादि से युक्त अथवा जितेन्द्रिय पुरुष का पहले कहा हुआ जो श्रुत और चारित्र है, वही धर्म है अथवा स्वभाव । ( वुसीमउ ) यह छान्दस है ||१९||
-
अतिक्कम्मंति वायाए, मणसा वि न पत्थए । सव्वओ संवुडे दंते, आयाणं सुसमाहरे
112011
छाया - अतिक्रमन्तु वाचा, मनसाऽपि न प्रार्थयेत् । सर्वतः संवृतो दान्त भादानं सुसमाहरेत् ॥ अन्वयार्थ - (अतिक्कम्मंति) किसी जीव को पीड़ा देने की (वायाए) वाणी से (मणसा वि) अथवा मन से भी ( न पत्थए ) इच्छा न करे ( सव्वओ संवुडे ) किन्तु बाहर और भीतर दोनों ओर से गुप्त रहे (दंते आयागं सुसमाहरे) तथा इन्द्रियों का दमन करता हुआ साधु अच्छी तरह संयम का पालन करे ।
४०९