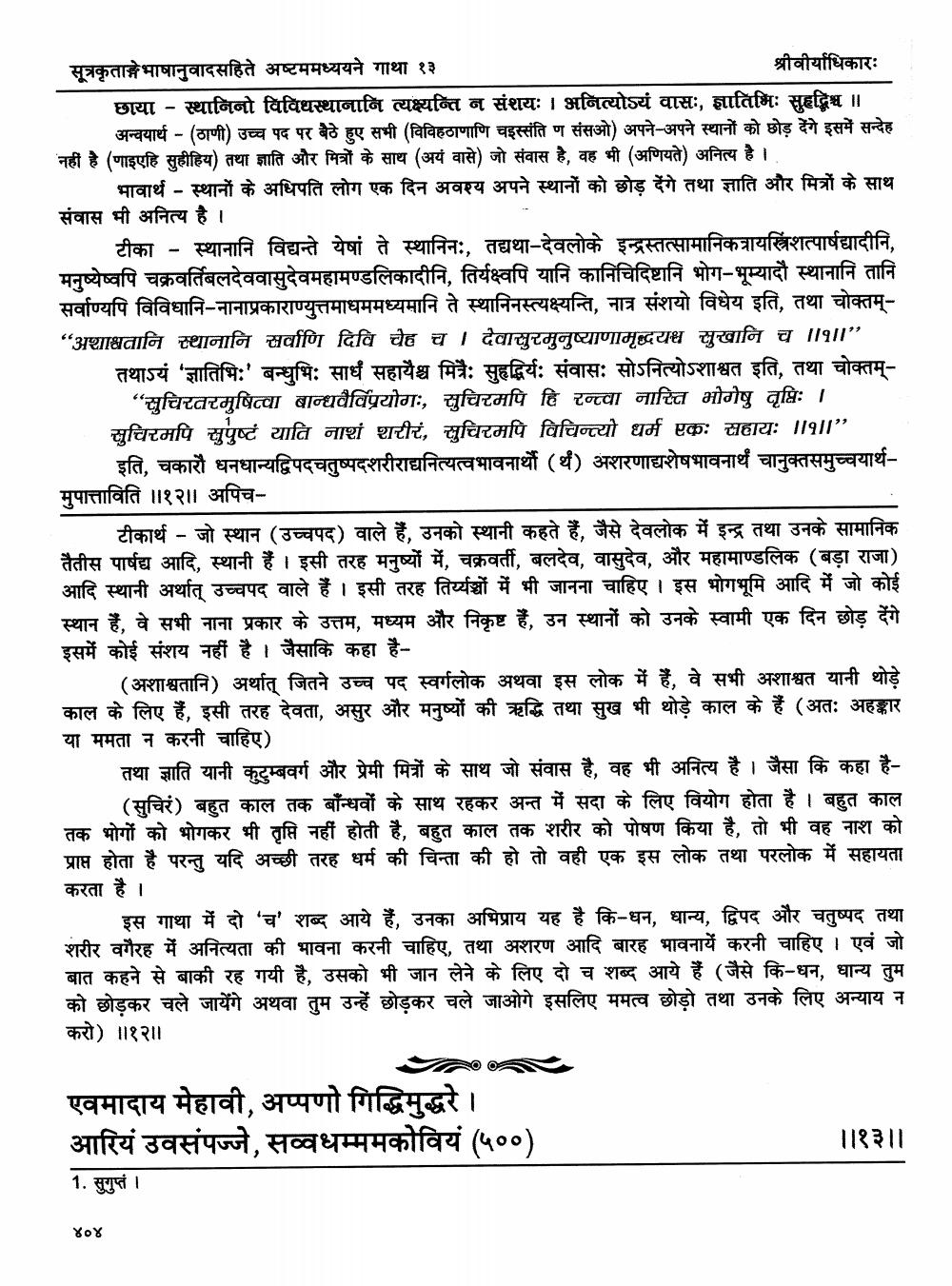________________
सूत्रकृताने भाषानुवादसहिते अष्टममध्ययने गाथा १३
श्रीवीर्याधिकारः
छाया स्थानिनो विविधस्थानानि त्यक्ष्यन्ति न संशयः । अनित्योऽयं वासः, ज्ञातिभिः सुहृद्भिश्च ॥ अन्वयार्थ - ( ठाणी) उच्च पद पर बैठे हुए सभी (विविहठाणाणि चइस्संति ण संसओ) अपने-अपने स्थानों को छोड़ देंगे इसमें सन्देह नहीं है ( गाइएहि सुहीहिय) तथा ज्ञाति और मित्रों के साथ (अयं वासे) जो संवास है, वह भी ( अणियते) अनित्य है ।
-
भावार्थ- स्थानों के अधिपति लोग एक दिन अवश्य अपने स्थानों को छोड़ देंगे तथा ज्ञाति और मित्रों के साथ संवास भी अनित्य है ।
टीका स्थानानि विद्यन्ते येषां ते स्थानिनः, तद्यथा - देवलोके इन्द्रस्तत्सामानिकत्रायस्त्रिंशत्पार्षद्यादीनि, मनुष्येष्वपि चक्रवर्तिबलदेववासुदेवमहामण्डलिकादीनि, तिर्यक्ष्वपि यानि कानिचिदिष्टानि भोग- भूम्यादौ स्थानानि तानि सर्वाण्यपि विविधानि-नानाप्रकाराण्युत्तमाधममध्यमानि ते स्थानिनस्त्यक्ष्यन्ति, नात्र संशयो विधेय इति, तथा चोक्तम्" अशाधतानि स्थानानि सर्वाणि दिवि चेह च । देवासुरमुनुष्याणामृद्धयश्च सुखानि च ||9||” तथाऽयं 'ज्ञातिभिः' बन्धुभिः सार्धं सहायैश्च मित्रैः सुहृद्भिर्यः संवासः सोऽनित्योऽशाश्वत इति, तथा चोक्तम्“सुचिरतरमुषित्वा बान्धवैर्विप्रयोगः, सुचिरमपि हि रन्त्वा नास्ति भोगेषु तृप्तिः । सुचिरमपि सुपुष्टं याति नाशं शरीरं, सुचिरमपि विचिन्त्यो धर्म एकः सहायः ||१||” इति, चकारौ धनधान्यद्विपदचतुष्पदशरीराद्यनित्यत्वभावनार्थों (थं) अशरणाद्यशेषभावनार्थं चानुक्तसमुच्चयार्थमुपात्ताविति ॥ १२ ॥ अपिच
टीकार्थ - जो स्थान (उच्चपद) वाले हैं, उनको स्थानी कहते हैं, जैसे देवलोक में इन्द्र तथा उनके सामानिक तैतीस पार्षद्य आदि, स्थानी हैं। इसी तरह मनुष्यों में, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, और महामाण्डलिक (बड़ा राजा) आदि स्थानी अर्थात् उच्चपद वाले हैं। इसी तरह तिर्य्यञ्चों में भी जानना चाहिए । इस भोगभूमि आदि में जो कोई स्थान हैं, वे सभी नाना प्रकार के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट हैं, उन स्थानों को उनके स्वामी एक दिन छोड़ देंगे इसमें कोई संशय नहीं है । जैसाकि कहा है
( अशाश्वतानि) अर्थात् जितने उच्च पद स्वर्गलोक अथवा इस लोक में हैं, वे सभी अशाश्वत यानी थोड़े काल के लिए हैं, इसी तरह देवता, असुर और मनुष्यों की ऋद्धि तथा सुख भी थोड़े काल के हैं (अतः अहङ्कार या ममता न करनी चाहिए )
तथा ज्ञाति यानी कुटुम्बवर्ग और प्रेमी मित्रों के साथ जो संवास है, वह भी अनित्य है । जैसा कि कहा है
1
(सुचिरं ) बहुत काल तक बाँन्धवों के साथ रहकर अन्त में सदा के लिए वियोग होता है । बहुत काल तक भोगों को भोगकर भी तृप्ति नहीं होती है, बहुत काल तक शरीर को पोषण किया है, तो भी वह नाश को प्राप्त होता है परन्तु यदि अच्छी तरह धर्म की चिन्ता की हो तो वही एक इस लोक तथा परलोक में सहायता करता है ।
इस गाथा में दो 'च' शब्द आये हैं, उनका अभिप्राय यह है कि- धन, धान्य, द्विपद और चतुष्पद तथा शरीर वगैरह में अनित्यता की भावना करनी चाहिए, तथा अशरण आदि बारह भावनायें करनी चाहिए । एवं जो बात कहने से बाकी रह गयी है, उसको भी जान लेने के लिए दो च शब्द आये हैं (जैसे कि-धन, धान्य तुम को छोड़कर चले जायेंगे अथवा तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे इसलिए ममत्व छोड़ो तथा उनके लिए अन्याय न करो ) ॥१२॥
४०४
एवमादाय मेहावी, अप्पणो गिद्धिमुद्धरे । आरियं उवसंपज्जे, सव्वधम्ममकोवियं (५००)
1. सुगुप्तं ।
।।१३॥