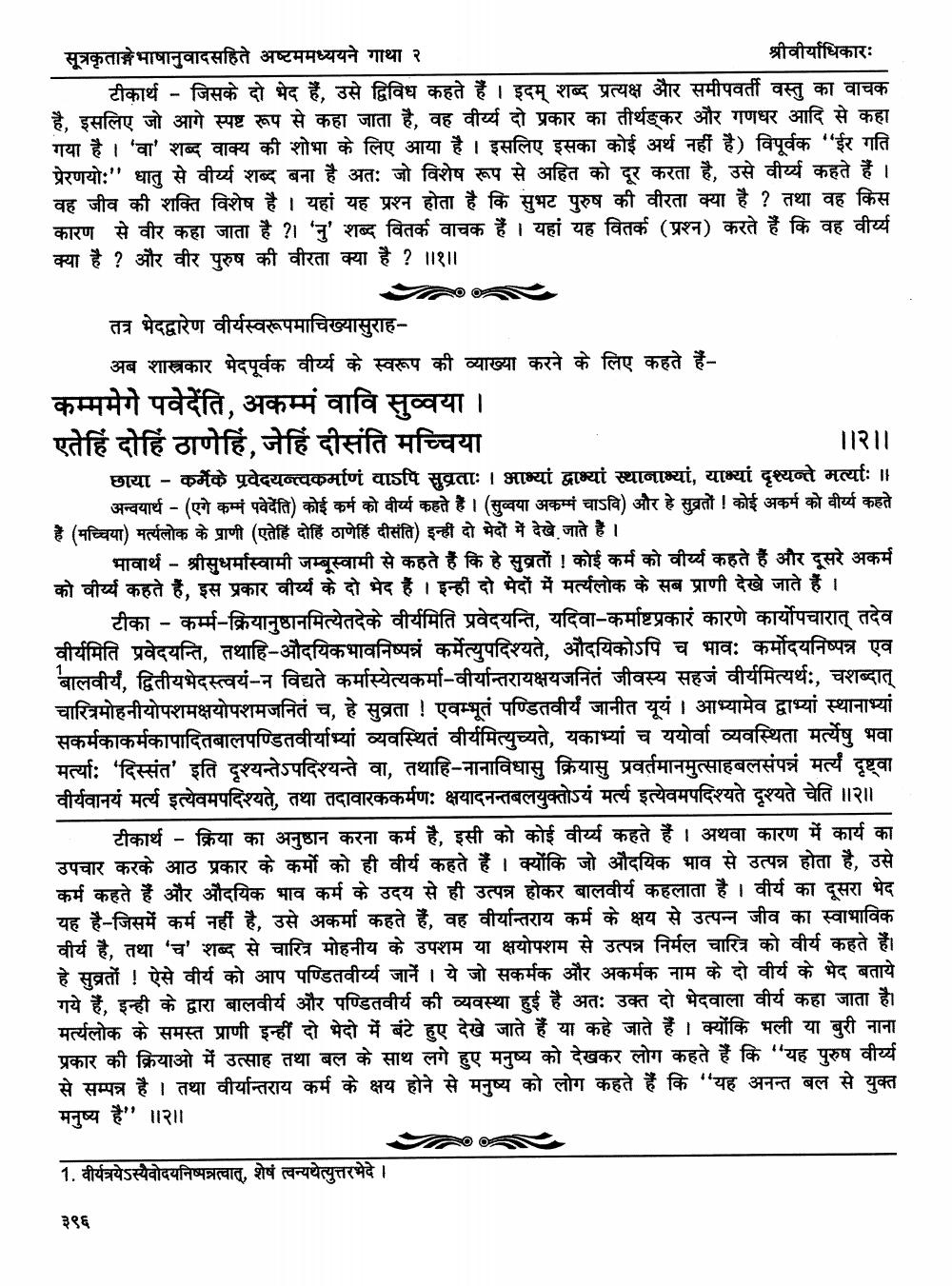________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते अष्टममध्ययने गाथा २
श्रीवीर्याधिकारः
टीकार्थ जिसके दो भेद हैं, उसे द्विविध कहते हैं । इदम् शब्द प्रत्यक्ष और समीपवर्ती वस्तु का वाचक है, इसलिए जो आगे स्पष्ट रूप कहा जाता है, वह वीर्य्य दो प्रकार का तीर्थङ्कर और गणधर आदि से कहा गया है । 'वा' शब्द वाक्य की शोभा के लिए आया है। इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है) विपूर्वक "ईर गति प्रेरणयोः " धातु से वीर्य्य शब्द बना है अतः जो विशेष रूप से अहित को दूर करता है, उसे वीर्य्य कहते हैं । वह जीव की शक्ति विशेष है । यहां यह प्रश्न होता है कि सुभट पुरुष की वीरता क्या है ? तथा वह किस कारण से वीर कहा जाता है ?। 'नु' शब्द वितर्क वाचक हैं। यहां यह वितर्क ( प्रश्न) करते हैं कि वह वीर्य्य क्या है ? और वीर पुरुष की वीरता क्या है ? ॥ १२ ॥
तत्र भेदद्वारेण वीर्यस्वरूपमाचिख्यासुराह
अब शास्त्रकार भेदपूर्वक वीर्य्य के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए कहते हैं
कम्ममेगे पवेदेंति, अकम्मं वावि सुव्वया ।
तेहिं दोहिं ठाणेहिं, जेहिं दीसंति मच्चिया
॥२॥
छाया -
कर्मेके प्रवेदयन्त्वकर्माणं वाऽपि सुव्रताः । आभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां याभ्यां दृश्यन्ते मर्त्याः ॥ अन्वयार्थ - ( एगे कम्मं पवेदेति) कोई कर्म को वीर्य्य कहते हैं। (सुव्वया अकम्मं चाऽवि ) और हे सुव्रतों ! कोई अकर्म को वीर्य्य कहते हैं ( मच्चिया ) मर्त्यलोक के प्राणी ( एतेहिं दोहिं ठाणेहिं दीसंति) इन्हीं दो भेदों में देखे जाते हैं ।
भावार्थ - श्रीसुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे सुव्रतों ! कोई कर्म को वीर्य्य कहते हैं और दूसरे अकर्म को वीर्य्यं कहते हैं, इस प्रकार वीर्य्य के दो भेद हैं। इन्हीं दो भेदों में मर्त्यलोक के सब प्राणी देखे जाते हैं ।
टीका - कर्म्म- क्रियानुष्ठानमित्येतदेके वीर्यमिति प्रवेदयन्ति यदिवा - कर्माष्टप्रकारं कारणे कार्योपचारात् तदेव वीर्यमिति प्रवेदयन्ति, तथाहि - औदयिक भावनिष्पन्नं कर्मेत्युपदिश्यते, औदयिकोऽपि च भावः कर्मोदयनिष्पन्न एव बालवीर्यं द्वितीयभेदस्त्वयं न विद्यते कर्मास्येत्यकर्मा-वीर्यान्तरायक्षयजनितं जीवस्य सहजं वीर्यमित्यर्थः, चशब्दात् चारित्रमोहनीयोपशमक्षयोपशमजनितं च, हे सुव्रता ! एवम्भूतं पण्डितवीर्यं जानीत यूयं । आभ्यामेव द्वाभ्यां स्थानाभ्यां सकर्मकाकर्मकापादितबालपण्डितवीर्याभ्यां व्यवस्थितं वीर्यमित्युच्यते, यकाभ्यां च ययोर्वा व्यवस्थिता मर्त्येषु भवा मर्त्याः 'दिस्संत' इति दृश्यन्तेऽपदिश्यन्ते वा, तथाहि - नानाविधासु क्रियासु प्रवर्तमानमुत्साहबलसंपन्नं मर्त्यं दृष्ट्वा वीर्यवानयं मर्त्य इत्येवमपदिश्यते, तथा तदावारककर्मणः क्षयादनन्तबलयुक्तोऽयं मर्त्य इत्येवमपदिश्यते दृश्यते चेति ॥२॥ टीकार्थ क्रिया का अनुष्ठान करना कर्म है, इसी को कोई वीर्य्य कहते हैं। अथवा कारण में कार्य का उपचार करके आठ प्रकार के कर्मों को ही वीर्य कहते हैं। क्योंकि जो औदयिक भाव से उत्पन्न होता है, उसे कर्म कहते हैं और औदयिक भाव कर्म के उदय से ही उत्पन्न होकर बालवीर्य कहलाता है। वीर्य का दूसरा भेद यह है - जिसमें कर्म नहीं है, उसे अकर्मा कहते हैं, वह वीर्यान्तराय कर्म के क्षय से उत्पन्न जीव का स्वाभाविक वीर्य है, तथा 'च' शब्द से चारित्र मोहनीय के उपशम या क्षयोपशम से उत्पन्न निर्मल चारित्र को वीर्य कहते हैं। हे सुव्रतों ! ऐसे वीर्य को आप पण्डितवीर्य्य जानें। ये जो सकर्मक और अकर्मक नाम के दो वीर्य के भेद बताये गये हैं, इन्ही के द्वारा बालवीर्य और पण्डितवीर्य की व्यवस्था हुई है अतः उक्त दो भेदवाला वीर्य कहा जाता है। मर्त्यलोक के समस्त प्राणी इन्हीं दो भेदो में बंटे हुए देखे जाते हैं या कहे जाते हैं। क्योंकि भली या बुरी नाना प्रकार की क्रियाओ में उत्साह तथा बल के साथ लगे हुए मनुष्य को देखकर लोग कहते हैं कि "यह पुरुष वीर्य्य से सम्पन्न है । तथा वीर्यान्तराय कर्म के क्षय होने से मनुष्य को लोग कहते हैं कि "यह अनन्त बल से युक्त मनुष्य है" ॥२॥
-
1. वीर्यत्रयेऽस्यैवोदयनिष्पन्नत्वात् शेषं त्वन्यथेत्युत्तरभेदे ।
३९६