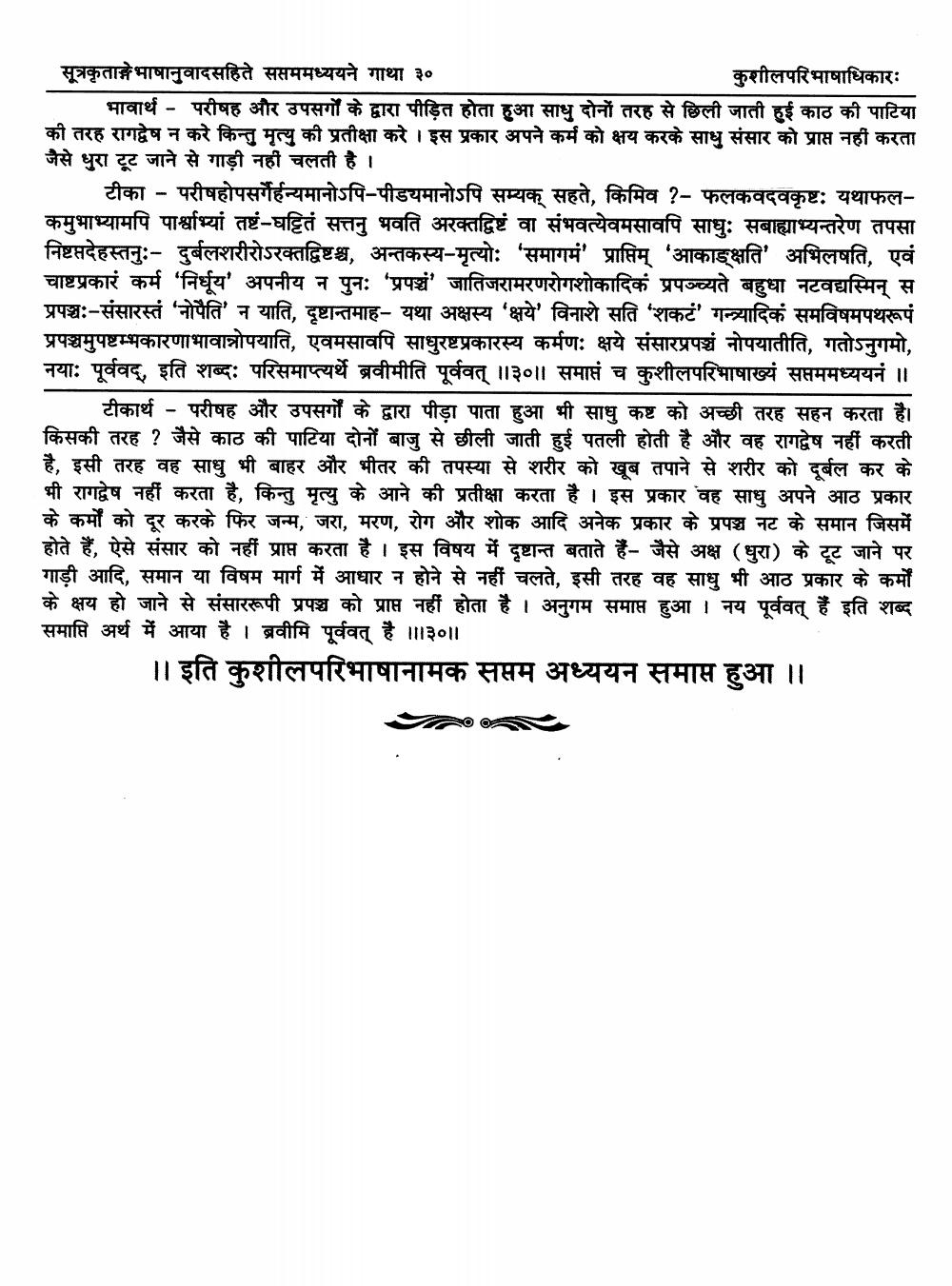________________
सूत्रकृतानेभाषानुवादसहिते ससममध्ययने गाथा ३०
कुशीलपरिभाषाधिकारः भावार्थ- परीषह और उपसर्गों के द्वारा पीड़ित होता हुआ साधु दोनों तरह से छिली जाती हुई काठ की पाटिया की तरह रागद्वेष न करे किन्तु मृत्यु की प्रतीक्षा करे । इस प्रकार अपने कर्म को क्षय करके साधु संसार को प्राप्त नहीं करता जैसे धुरा टूट जाने से गाड़ी नहीं चलती है।
टीका - परीषहोपसर्गेर्हन्यमानोऽपि-पीडयमानोऽपि सम्यक् सहते, किमिव ?- फलकवदवकृष्टः यथाफलकमुभाभ्यामपि पार्श्वभ्यां तष्टं-घट्टितं सत्तनु भवति अरक्तद्विष्टं वा संभवत्येवमसावपि साधुः सबाह्याभ्यन्तरेण तपसा निष्टप्तदेहस्तनुः- दुर्बलशरीरोऽरक्तद्विष्टश्च, अन्तकस्य-मृत्योः 'समागम' प्राप्तिम् 'आकाङ्क्षति' अभिलषति, एवं चाष्टप्रकारं कर्म 'निर्धूय' अपनीय न पुनः 'प्रपञ्चं' जातिजरामरणरोगशोकादिकं प्रपञ्च्यते बहुधा नटवद्यस्मिन् स प्रपञ्चः-संसारस्तं 'नोपैति' न याति. दष्टान्तमाह- यथा अक्षस्य 'क्षये विनाशे सति 'शकट' गन्त्र्यादिकं सम प्रपञ्चमुपष्टम्भकारणाभावान्नोपयाति, एवमसावपि साधुरष्टप्रकारस्य कर्मणः क्षये संसारप्रपञ्चं नोपयातीति, गतोऽनुगमो, नयाः पूर्ववद, इति शब्दः परिसमाप्त्यर्थे ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥३०॥ समाप्तं च कुशीलपरिभाषाख्यं सप्तममध्ययनं ॥
टीकार्थ - परीषह और उपसर्गों के द्वारा पीड़ा पाता हुआ भी साधु कष्ट को अच्छी तरह सहन करता है। किसकी तरह ? जैसे काठ की पाटिया दोनों बाजु से छीली जाती हुई पतली होती है और वह रागद्वेष नहीं करती है, इसी तरह वह साधु भी बाहर और भीतर की तपस्या से शरीर को खूब तपाने से शरीर को दूर्बल कर के भी रागद्वेष नहीं करता है, किन्तु मृत्यु के आने की प्रतीक्षा करता है । इस प्रकार वह साधु अपने आठ प्रकार के कर्मों को दूर करके फिर जन्म, जरा, मरण, रोग और शोक आदि अनेक प्रकार के प्रपञ्च नट के समान जिसमें होते हैं, ऐसे संसार को नहीं प्राप्त करता है । इस विषय में दृष्टान्त बताते हैं- जैसे अक्ष (धुरा) के टूट जाने पर गाड़ी आदि, समान या विषम मार्ग में आधार न होने से नहीं चलते, इसी तरह वह साधु भी आठ प्रकार के कर्मों के क्षय हो जाने से संसाररूपी प्रपञ्च को प्राप्त नहीं होता है । अनुगम समाप्त हुआ । नय पूर्ववत् हैं इति शब्द समाप्ति अर्थ में आया है । ब्रवीमि पूर्ववत् है ॥३०॥
॥ इति कुशीलपरिभाषानामक सप्तम अध्ययन समाप्त हुआ ।।